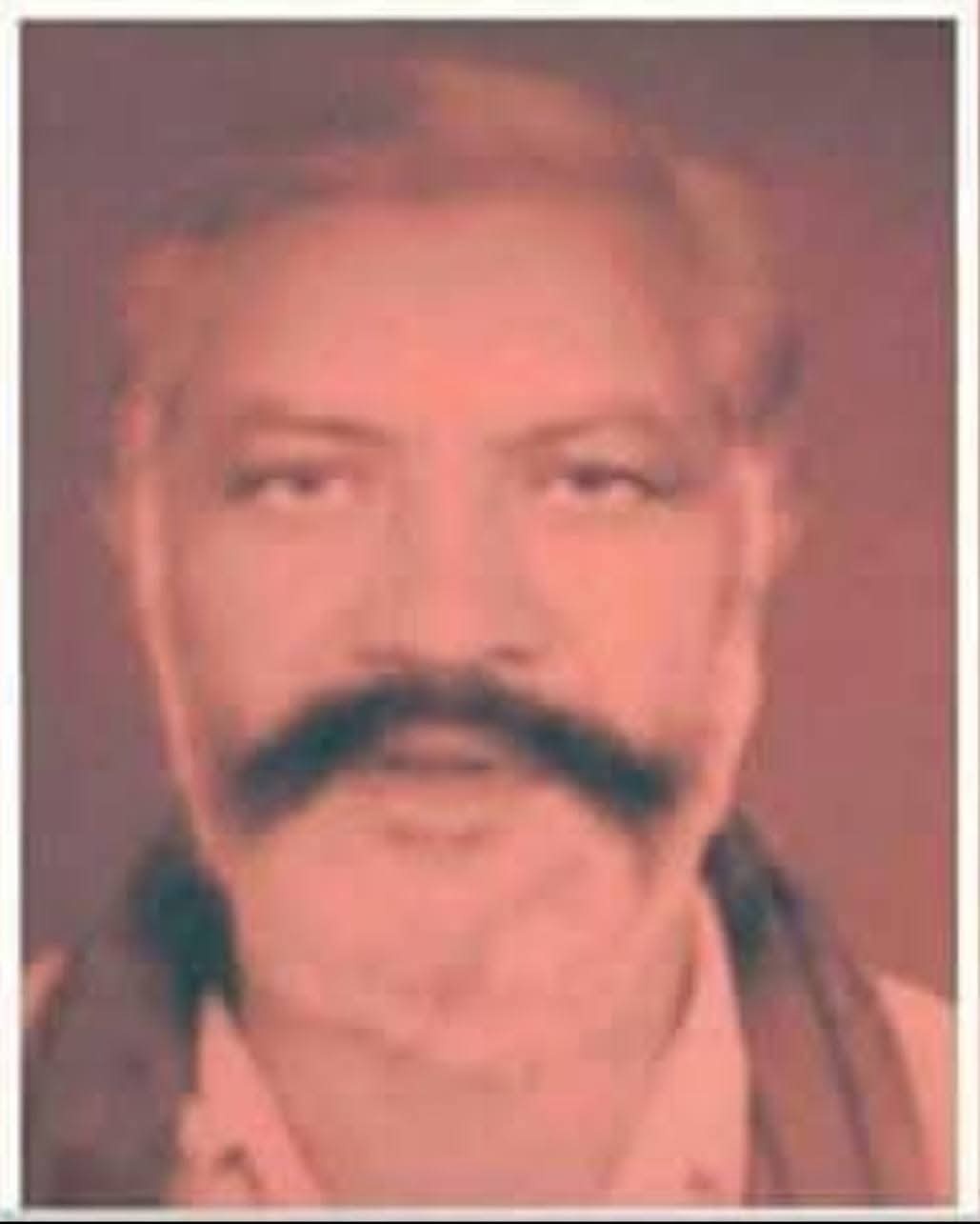एएसआई को विश्वसनीयता के संकट का सामना करना पड़ रहा है
स्वरति सभापंडित/ सी.पी. राजेंद्रन
पुरातत्वविद् के. अमरनाथ रामकृष्ण के विवादास्पद तबादले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) एक बार फिर जनता की नज़रों में आ गया है। तमिलनाडु में कीलाडी उत्खनन में अमरनाथ रामकृष्ण के नेतृत्व ने प्राचीन तमिल सभ्यता के इतिहास में जनता और अकादमिक जगत की काफ़ी रुचि जगाई है।
कीलाडी उत्खनन 2014 में शुरू हुआ, कीलाडी में उत्खनन से लगभग 7,500 कलाकृतियाँ मिलीं। इन खोजों ने एक परिष्कृत, शिक्षित और धर्मनिरपेक्ष नगरीय समाज के अस्तित्व का संकेत दिया और लौह युग (12वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व) और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल (6ठी-4थी शताब्दी ईसा पूर्व) के बीच ऐतिहासिक अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किए। विद्वानों ने तब से इस स्थल को वैगई घाटी सभ्यता का हिस्सा बताया है। कीलाडी बस्ती उस दूसरे शहरीकरण का हिस्सा हो सकती है जिसने छठी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था।
इस परियोजना में तब नाटकीय मोड़ आया जब 2017 में श्री रामकृष्ण का अचानक असम तबादला कर दिया गया। उनके तबादले को व्यापक रूप से निष्कर्षों को कमतर आंकने की कोशिश माना गया। तनाव तब और बढ़ गया जब एएसआई ने दावा किया कि कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं मिले और तीसरे चरण की खुदाई रोक दी। इससे तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद पैदा हो गए। मद्रास उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए इस स्थल को तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया, जिसने तब से 18,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ खोज निकाली हैं।
2021 में, श्री रामकृष्ण चेन्नई सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद् के रूप में तमिलनाडु लौट आए। 2023 में, उन्होंने पहले के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए पहले दो चरणों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालाँकि, एएसआई ने रिपोर्ट में संशोधन का अनुरोध किया। अपने निष्कर्षों का बचाव करते हुए, श्री रामकृष्ण ने उत्खनन स्थलों के भीतर विभिन्न घटना क्षितिजों से प्राप्त कार्बनयुक्त पदार्थों की पद्धतिगत कठोरता, स्ट्रेटीग्राफिक अनुक्रमण, भौतिक संवर्धन विश्लेषण और त्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग का हवाला दिया। ये घटनाएँ पुरातात्विक अभ्यास में राजनीति को रेखांकित करती हैं और एएसआई के सामने मौजूद विश्वसनीयता के संकट को दर्शाती हैं।
एक असंगत दृष्टिकोण केंद्र सरकार ने अपने रुख को यह कहते हुए उचित ठहराया कि व्यापक वैज्ञानिक सत्यापन के बिना केवल एक ही निष्कर्ष वैकल्पिक ऐतिहासिक आख्यानों को पुष्ट नहीं कर सकता। यह तर्क ज्ञान निर्माण में पद्धतिगत कठोरता और वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल का समर्थन करता है, लेकिन यह अन्य उत्खनन परियोजनाओं में एएसआई के आचरण में विसंगतियों को भी उजागर करता है।
तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में आदिचनल्लूर और शिवगलाई स्थलों पर उत्खनन से कीलाडी जैसा ही एक नमूना सामने आया। हालाँकि आदिचनल्लूर की खुदाई 20वीं सदी के आरंभ में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद्, अलेक्जेंडर री ने की थी, लेकिन यह स्थल लगभग एक सदी तक उपेक्षित रहा। जब 2004 में एएसआई के टी. सत्यमूर्ति के नेतृत्व में उत्खनन फिर से शुरू हुआ, तो लौह युग की उल्लेखनीय कलाकृतियाँ मिलीं, जो 3,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी बताई गई हैं। हालाँकि, एएसआई को इन निष्कर्षों को प्रकाशित करने में 15 वर्ष से अधिक समय और अदालती हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा।
हालाँकि, राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के उत्खनन ने एक अलग दिशा पकड़ ली। बहाज गाँव में 23 मीटर गहरी एक प्राचीन पुरावाहिनी (पैलियोचैनल) के उत्खनन ने कुछ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को इस स्थल को ऋग्वेद में वर्णित पौराणिक सरस्वती नदी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उत्खनन रिपोर्ट में ‘महाभारत काल’ से मानव बस्तियों के संबंध का भी दावा किया गया है, जो एक विवादास्पद समयावधि है जिस पर विद्वानों ने बहस की है। पौराणिक-ऐतिहासिक आख्यानों को इस तरह बिना आलोचना के अपनाना वैज्ञानिक ज्ञान निर्माण के सिद्धांतों के विपरीत है।
इन मामलों में एएसआई का आचरण पद्धतिगत राष्ट्रवाद के जाल को उजागर करता है—एक ऐसा ढांचा जो भारत के अतीत के एक विलक्षण, राज्य-स्वीकृत दृष्टिकोण को विशेषाधिकार देता है। इस दृष्टिकोण को अक्सर पद्धतिगत कठोरता, प्रयोजनमूलक व्याख्याओं और एकाधिकारवादी ज्ञानमीमांसा व्यवस्था के निर्माण के माध्यम से वैध ठहराया जाता है। भारत को एक सभ्यतागत अखंड के रूप में चित्रित करने की संस्था की कोशिश ने लंबे समय से विद्वानों के हलकों से आलोचना की है। आशीष अविकुंठक (2021) ने मनमाने तबादलों, विलंबित पदोन्नति, परेशान करने वाली कार्य स्थितियों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला, जो एएसआई में गुणवत्तापूर्ण कार्य में बाधा डालते हैं। सुप्रिया वर्मा और जया मेनन (2003) ने वैज्ञानिक अखंडता की कमी के लिए अयोध्या उत्खनन परियोजना की आलोचना की। जुर्गन न्यूस (2012) और दिलीप कुमार चक्रवर्ती (1988, 2003) ने एएसआई की पुरानी व्हीलर पद्धति पर निरंतर निर्भरता और व्यापक शोध डिजाइनों की कमी को समग्र व्याख्या में बाधा बताया।
एएसआई ने बड़े पैमाने पर एक बंद आंतरिक समीक्षा प्रणाली को बरकरार रखा है। अधिकांश शोध आंतरिक रिपोर्टों, संस्थागत मोनोग्राफ और बुलेटिनों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। इसके विपरीत, इसके वैश्विक समकक्ष जैसे जर्मनी में डॉयचेस आर्कियोलॉजिस इंस्टीट्यूट, फ्रांस में इंस्टीट्यूट नेशनल डे रिसर्चेस आर्कियोलॉजिक्स प्रिवेंटिव्स, और जापान की एजेंसी फॉर कल्चरल एयर्स नियमित रूप से अकादमिक मंचों पर निष्कर्ष प्रकाशित करते हैं। इससे पारदर्शिता, कार्यप्रणाली संबंधी जवाबदेही, विद्वानों की कठोरता को बढ़ावा मिलता है और पुरातात्विक अनुसंधान की सुगमता बढ़ती है। यह वैश्विक विद्वानों की भागीदारी को भी आमंत्रित करता है।
इन मुद्दों से परे, एएसआई का ज्ञानात्मक प्रयास राष्ट्रवादी उत्साह में तेज़ी से डूबता जा रहा है। पुरातात्विक उद्यम की ढहती वैधता व्यापक संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों, अधिक पद्धतिगत और वैज्ञानिक कठोरता, वित्तीय स्वायत्तता और एक मज़बूत ज्ञानात्मक ढाँचे की माँग करती है जो भारत के ऐतिहासिक अतीत की बहुलता को समाहित करे। द हिंदू से साभार
स्वरति सभापंडित शोधार्थी, सी.पी. राजेंद्रन सहायक प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेज, बेंगलुरु