असीम अली
आज़ादी के सात दशक से ज़्यादा समय बाद भी, उत्तर-औपनिवेशिक भारत और पाकिस्तान की राष्ट्र-निर्माण परियोजना पूरी होने से बहुत दूर नज़र आती है। कश्मीर में, भारतीय अभिजात वर्ग उस राज्य में (मनमाने ढंग से लोकतांत्रिक निलंबन के बाद) चुनावों के प्रबंधन को लेकर चिंताओं से घिरा हुआ है। इस बीच, पाकिस्तान अपने पश्तून-बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने नवीनतम आतंकवाद विरोधी अभियान (उर्दू में अज़्म-ए-इस्तेहकम, जिसका अर्थ है ‘स्थिरता के लिए संकल्प’) के बीच में है। यह लोकतांत्रिक जन आंदोलन – पश्तून तहफ़ुज़ आंदोलन – पर किए गए गंभीर दमन के बाद हुआ है, जो सैन्य शासन की क्रूरता के खिलाफ़ विरोध कर रहा था।
भारत और पाकिस्तान की कश्मीरियों और पश्तूनों के ‘भावनात्मक एकीकरण’ को सफलतापूर्वक अंजाम देने में असमर्थता की क्या वजह है? अगर कोई दोनों देशों के शासक अभिजात वर्ग (या दोनों देशों के महानगरीय नागरिक समाज के दिग्गजों) से पूछे, तो उनके स्पष्टीकरण में विद्रोही, पूर्व-आधुनिक ‘अन्य’ के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं शामिल हो सकती हैं। कश्मीरियों और पश्तूनों की छवियाँ उनके घरेलू जन-मीडिया में धार्मिक उग्रवाद, मर्दाना हिंसा, सामाजिक पिछड़ेपन और भावनात्मक अपरिपक्वता जैसी रूढ़ियों के साथ गढ़ी गई हैं।
फिर भी, हमें स्वतंत्रता से पहले शेख अब्दुल्ला (‘नया कश्मीर’ आंदोलन) और खान अब्दुल गफ्फार खान (खुदाई खिदमतगार आंदोलन) के नेतृत्व में चलाए गए जन आंदोलनों को याद करना चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और धार्मिक सहिष्णुता के प्रगतिशील आदर्शों की प्रतिज्ञा की थी। पठानों और कश्मीरियों (सौहार्दपूर्ण कश्मीर और पश्तून संस्कृति की विशिष्ट व्याख्याओं से जुड़े) के बड़े हिस्से ने उस समय सांप्रदायिक हिंसा का परित्याग कर दिया था जब यह पूरे उपमहाद्वीप में फैल रही थी।
कश्मीर में मीडिया की चुनावी कवरेज रोमांस और खतरे के उन परस्पर विरोधी प्रतीकों को प्रतिध्वनित करती है, जिनके माध्यम से कश्मीर को हिंदी सिनेमा में अक्सर दिखाया जाता रहा है। साथ ही कश्मीरी समाज की दिशा के बारे में भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। हमेशा की तरह, कश्मीरी या तो ‘आगे बढ़ रहे हैं’ (प्रगति और शांति की ओर) या ‘पीछे लौट रहे हैं’ (हिंसा और अलगाववाद की ओर)।
इसी तरह, कश्मीरियों के बारे में कहा जा रहा है कि वे या तो ‘मुख्यधारा’ में शामिल हो रहे हैं या उससे अलग-थलग रह रहे हैं। लेकिन मुख्यधारा क्या है और इसके मापदंड कौन तय करता है? बेशक, इन सवालों पर शायद ही कभी चर्चा होती है। फिर भी, ये आधार-स्व और पराए की अंतर्निहित रचना-ही हैं, जो कश्मीर की ‘वास्तविकता’ के बारे में हमारी समझ को छानते हैं। ये एक खास नज़रिया बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम (आधुनिक राष्ट्रवादी अभिजात वर्ग) कश्मीर को देखते हैं, जिसे इतिहासकार हफ्सा कंजवाल ने अपनी हालिया किताब, कोलोनाइजिंग कश्मीर: स्टेट-बिल्डिंग अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन में “औपनिवेशिक नज़र” के रूप में वर्णित किया है।
कंजवाल इस औपनिवेशिक नज़रिए के निर्माण का पता आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों से लगाते हैं। दरअसल, उनकी किताब के परिचयात्मक अंश में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को लिखे गए पत्र का एक खुलासा करने वाला अंश है।
इस आदान-प्रदान का उद्देश्य बाद वाले को कश्मीर के भारत में विवादित विलय की पुष्टि करने के लिए मनाना था। नेहरू लिखते हैं, “यह याद रखना चाहिए कि कश्मीर घाटी के लोग… वे नहीं हैं जिन्हें वीर लोग कहा जाता है।” वे आगे कहते हैं: “वे नरम हैं और आरामदेह जीवन जीने के आदी हैं… आम लोगों को मुख्य रूप से कुछ चीजों में दिलचस्पी है – एक ईमानदार प्रशासन और सस्ता और पर्याप्त भोजन। अगर उन्हें यह मिल जाए, तो वे कमोबेश संतुष्ट हो जाते हैं।”
इस प्रकार नेहरू अब्दुल्ला से राजनीतिक संप्रभुता के जटिल सवाल को छोड़ देने का अनुरोध करते हैं क्योंकि कश्मीर के सरल दिमाग वाले लोगों को उन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर भी, सात दशक बाद, संप्रभुता का मुद्दा – वैध अधिकार के स्रोत पर नियंत्रण – राज्य में एक केंद्रीय राजनीतिक चिंता बनी हुई है। ऐसा क्यों है?
अपने अध्ययन, “भारत की स्थापना और लोकप्रिय संप्रभुता” में, राजनीतिक वैज्ञानिक, ओर्नित शानी ने पता लगाया कि भारत स्वतंत्रता के बाद की अवधि में एक एकीकृत “लोकप्रिय संप्रभुता” को कैसे मजबूत करने में कामयाब रहा। चुनौतियाँ बहुत बड़ी थीं: “कई प्रतिस्पर्धी संप्रभुताएं” (स्व-शासन की अलग-अलग धारणाएं), “गहरी बहुलताएं” (जाति, वर्ग, भाषा) और इसी तरह की अन्य चुनौतियाँ।
ये चुनौतियाँ रियासतों के मामले में सबसे तीव्र थीं, जिन्होंने अपनी खुद की अनोखी संस्थाएँ विकसित की थीं। भारत कैसे सफल हुआ? शानी ने यह तर्क दिया कि “भारत में एकीकृत लोकप्रिय संप्रभुता मुख्य रूप से उस समय प्रचलित लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों पर बलपूर्वक हावी होने के बजाय काम करने के प्रयासों से प्रेरित थी”। दूसरे शब्दों में, भारतीय संघ ने स्व-शासन के विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ काम किया और उन्हें एक बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से एकीकृत लोकप्रिय परियोजना में एकीकृत करने की कोशिश की, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ वैध ‘लोगों की इच्छा’ के विषय पर जोर दिया गया।
इस प्रक्रिया के दो अपवादों में से, शानी ने कश्मीर और हैदराबाद का उल्लेख किया है, जहां हथियारों के बल पर विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, न कि बातचीत के ज़रिए लोगों की सहमति से। कश्मीर घाटी में कांग्रेस की राज्य इकाई भी बेहद कमज़ोर थी, क्योंकि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकप्रिय आंदोलन का बोलबाला था।
इस प्रकार, पीछे मुड़कर देखें तो, संप्रभुता के मुद्दे को सुलझाने के लिए स्वतंत्रता के बाद समायोजन की एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया की आवश्यकता थी। ऐसा राज्य सरकार को ‘नया कश्मीर’ (1930 के दशक में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रतिपादित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष रोडमैप) और ‘कश्मीरियत’ के सांस्कृतिक मुहावरे को राष्ट्रीय ढांचे के भीतर एकीकृत करने के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता देकर किया जा सकता था।
इसके बजाय, दिल्ली में नए सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग द्वारा बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया: ऊपर से नीचे तक शासन की दृष्टि से जबरन आधुनिकीकरण, लोकतांत्रिक समावेशन पर राजनीतिक प्रबंधन को प्राथमिकता देना। इतिहासकार फैसल देवजी ने स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस द्वारा गांधीवादी अहिंसा की “क्रांतिकारी” नैतिकता को त्यागने के साथ-साथ “जिम्मेदारी की पुरानी ब्रिटिश नैतिकता को अपनाने के बारे में लिखा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने खुद लड़ाई लड़ी थी।”
कश्मीरी नेताओं के राजनीतिक दावों की अनदेखी करते हुए, इस तरह के अहंकारी, बलपूर्वक नियंत्रण की भावना ने केंद्र सरकार को ‘1953 का तख्तापलट’ करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें शेख अब्दुल्ला को सत्ता से हटा दिया गया और बख्शी गुलाम मोहम्मद को सत्ता में बिठाया गया। ‘विशेष दर्जा’ और ‘अनुच्छेद 370’ पर गरमागरम बहसें कश्मीर में मौजूद लोकप्रिय, लोकतांत्रिक शासन की गंभीर रूप से सीमित प्रकृति को अस्पष्ट करती हैं।
उदाहरण के लिए, कश्मीर को विधानसभा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इंदिरा गांधी-शेख अब्दुल्ला समझौते के बाद 1977 तक इंतजार करना पड़ा। एक दशक तक लोकतंत्र के कामकाज के अंतराल के बाद, 1987 के धांधली वाले विधानसभा चुनाव ने घाटी को सशस्त्र उग्रवाद की ओर धकेल दिया।
सत्ता की सीमाओं की गहरी समझ रखने वाले भारतीय नेता एम.के. गांधी इस बदलाव को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। 1947 के अंत में, जब गांधी को कश्मीर में सैन्य हस्तक्षेप और इसके लिए उनके अस्पष्ट समर्थन पर चुनौती दी गई, तो उन्होंने जवाब दिया: “मैंने पहले ही कहा है कि मैं कोई नहीं हूँ और कोई भी मेरी बात नहीं सुनता।” अपने शिष्यों, नेहरू और वल्लभभाई पटेल का हवाला देते हुए, गांधी ने कहा कि जबकि स्वतंत्रता तक अहिंसा उनके लिए स्वीकार्य थी, “… अब वे आश्चर्यचकित हैं कि वे अहिंसा के साथ कैसे शासन कर सकते हैं। और फिर सेना है और उन्होंने सेना की मदद ली है। अब मेरा कोई मूल्य नहीं है।”
तीन-चौथाई सदी से ज़्यादा समय तक असफलताओं के अनुभव के बाद, उपमहाद्वीप के राष्ट्रवादी अभिजात वर्ग के लिए गांधी के नैतिक मूल्यों की ओर रुख करना बेहतर होगा। इतिहासकार अजय स्कारिया ने अपनी किताब अनकंडीशनल इक्वालिटी: गांधीज रिलिजन ऑफ रेजिस्टेंस में लिखा है: “उनके [गांधी] लिए, संप्रभु शक्ति केवल राज्य में ही नहीं है। बल्कि, हर आत्मा में बहुत ज़्यादा दरारें हैं, और संप्रभुता सर्वव्यापी है, जिसका इस्तेमाल हर रोज़ आत्मा द्वारा ही किया जाता है।”
गांधी यह भी समझते थे कि अहिंसा की अवधारणा को उनके गहरे-विभाजित आत्मा को पहचानने के आग्रह से अलग नहीं किया जा सकता। आत्म (चाहे ‘हिंदू आत्मा’ हो या ‘मुस्लिम आत्मा’ या ‘सिंहल-बौद्ध आत्मा’) को दी गई राजनीतिक रूप से गढ़ी गई पूर्णता या सीमा, राष्ट्रीय संप्रभुता के उपनिवेशवादी यूरोप के सिद्धांतों की तरह ही है, जिसकी वजह से पिछली सदी में उपमहाद्वीप में बहुत ज़्यादा खून-खराबा हुआ है।
क्या इस गहरे रूप से विखंडित, अपूर्ण स्व की पहचान हमें ‘अन्य’ के बारे में पूछताछ को खुद पर वापस लाने की अनुमति दे सकती है? क्या हम उतने ही आधुनिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील हैं जितना हम सोचते हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या कश्मीरियों के साथ अपने व्यवहार में पीछे हट रहे हैं?
क्या हम कश्मीर के साथ अपने व्यवहार में हिंसा से दूर जाने और शांति को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक ऐसी मुख्यधारा का निर्माण कर रहे हैं जो कश्मीर के लोगों के लिए मेहमाननवाज़ हो सकती है? द टेलीग्राफ से साभार
आसिम अली एक राजनीतिक शोधकर्ता और स्तंभकार हैं

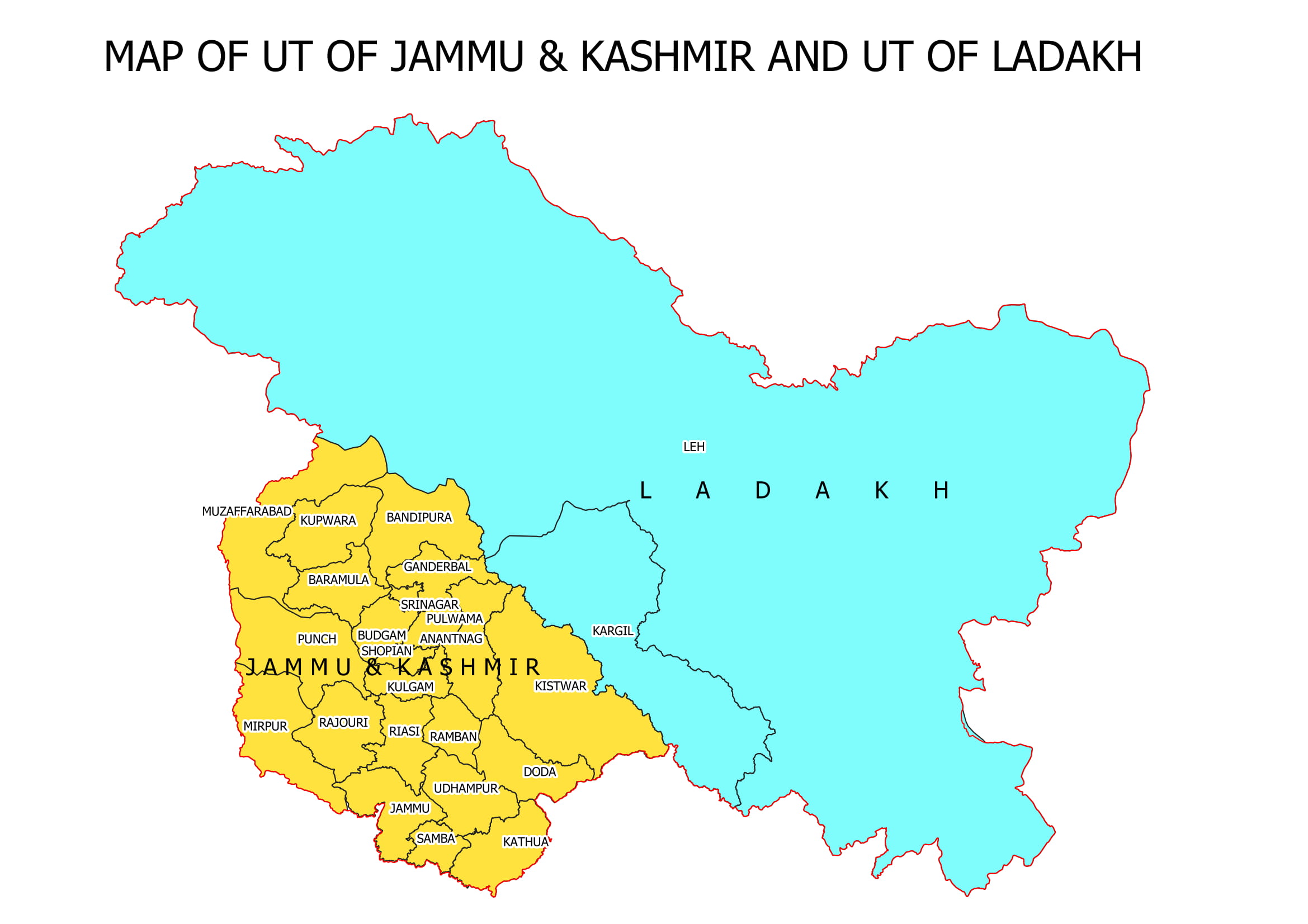



असीम अली का यह आलेख काश्मीर के इतिहास और राजनीति के यथार्थ को उद्घाटित करता है और
कुछ अनसुलझे सवालों को पूर्वाग्राह से मुक्त होकर मानवीय दृष्टि से देखने का आग्रह करता है।करता है