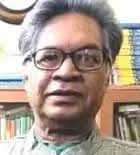“Can caste be annihilated?
Not unless we show the courage to rearrange the stars in our firmament .Not unless those who call themselves revolutionary develop a radical critique of Brahminism . Not unless those who understand Brahmanism sharpen their critique of capitalism. And not unless we read Babasaheb Ambedkar .If not inside our classroom ,then outside them .Until then we will remain what he called the ‘sick men’ and women of Hindustan ,who seem to have no desire to get well.”—Arundhati Roy .

हिंदी बौद्धिकों का ‘हिंदू’ होना
वीरेन्द्र यादव
आज़ादी के बाद वर्तमान दौर में भारतीय समाज जिन नई चुनौतियों के मुकाबिल है ,वह पहली बार है. स्वाधीनता आंदोलन की जनतंत्र व सर्वसमावेशी आधुनिक राष्ट्र की संकल्पना जिन संवैधानिक मूल्यों द्वारा सुनिश्चित की गई थी, वे संकट में हैं. नये संसद भवन में पुरोहितों के मंत्रोच्चारण की अनुगूंज के साथ चोल राजवंश के प्रतीक धार्मिक दंड सेंगोल की स्थापना, भारत के धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के पटाक्षेप की तैय्यारी है. इतिहास, संस्कृति, पाठ्यक्रम ,जीवनचर्या ,खान-पान सबकुछ पर बहुसंख्यक राजनीति की कड़ी निगहबानी है.
तर्क, ज्ञान. वैज्ञानिक सोच व बहुलवाद के बरक्स आस्था , अंधविश्वास, कर्मकांड , कुतर्क और अज्ञान की फसल लहलहा रही है. यह पहली बार है कि भारत में बौद्धिकों व चिन्तकों की घेराबंदी तर्क, विवेक ,वैज्ञानिक सोच के प्रसार व धर्म की एकल संरचना को न मानने के कारण की जा रही है. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम.एम. कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्याएं इसी हिंसात्मक प्रवृत्ति का दुष्परिणाम हैं. तमिल उपन्यासकार पेरुमल मेरुगन, तेलगू बौद्धिक कांचा इल्लैय्या , मलयाली लेखक एस. हरीश, संथाली मूल के लेखक हंसदा सोवेंद्र शेखर, गुजराती कवयित्री पारुल खक्कर, कोंकणी कवि विष्णु सूर्य वाघ व अन्य लेखकों की कृतियों के विरुद्ध कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों व दबंग जातिवादी तत्वों की गोलबंदी इस बदलते परिदृश्य की परिचायक हैं.
अब अरुंधति रॉय कथित राष्ट्रवादी हिन्दी बौद्धिकों के निशाने पर हैं. उच्च शिक्षा संस्थानों ,विश्वविद्यालयों व अन्य स्वायत्त संस्थानों में सत्तातंत्र का बढ़ता हस्तक्षेप बौद्धिक व अकादमिक स्वतंत्रता का दम घोंटने वाला है. रामायण, महाभारत ,गीता सरीखे धर्मग्रंथों व हिंदू कर्मकांडों की शिक्षा के विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं.
विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व सनातन के प्रति आस्था की शपथ दिलवाने की शुरुआत हो चुकी है. संवैधानिक पदों पर उच्चपदस्थ लोगों द्वारा परम्परा और संस्कृति की रक्षा के लिये जनप्रतिरोध का आह्वान किया जा रहा है. जिन पेरुमल मुरुगन ने कुछ वर्ष पूर्व इस रचनाविरोधी समय से त्रस्त होकर अपने लेखकीय व्यक्तित्व की ‘मृत्यु’ की घोषणा की थी, अब उन्होने धर्म और जाति के प्रश्नों पर न लिखने और सिर्फ मध्यवर्गीय विषयों तक सीमित रहने की विवशता प्रकट की है.
अपनी वेदना को उन्होंने ‘सांग्स ऑफ ए कावर्ड’ कविता संग्रह में अभिव्यक्त करते हुए लिखा है, “ अब मेरे भीतर एक सेंसर बैठ गया है, वह मेरे हर शब्द की परख कर रहा है. वह लगातार आगाह करता रहता है कि कोई एक शब्द गलत समझा जा सकता है या उसकी ऐसी व्याख्या की जा सकती है, यह एक वास्तविक बाधा है. लेकिन मैं इससे मुक्त होने में असमर्थ हूँ”.
अरुंधति रॉय व पेरुमल मुरुगन और उन सरीखे अन्य लेखकों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कोई अलग थलग परिघटना न होकर उस प्रवृत्ति का परिचायक है जो समूचे देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आवरण में साहित्य, फिल्म, नाटक से लेकर हर तरह की तार्किक वैचारिक अभिव्यक्ति के विरुद्ध हमलावर है.
दरअसल यह सब मात्र सांस्कृतिक दृष्यांतर न होकर भारतीय राष्ट्रराज्य को एकल हिंदू धार्मिक-राजनीतिक रंग में रंगने के घोषित इरादों का परिणाम है. इसके निशाने पर अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी ,स्त्री सहित व्यापक हाशिये का समाज है. भीमा कोरेगांव ,हाथरस ,ऊना , मणिपुर सरीखे घटनाक्रम इसकी निशानदेही करते हैं.
नागरिकता सबंधी संशोधन, कश्मीर सबंधी अनुच्छेद 370 , राममंदिर , मथुरा व काशी सरीखे अभियान इसी का परिणाम हैं. सनातन की रक्षा के नाम पर उत्तर भारत की ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थान’ की धार्मिक-राजनीति को दक्षिण भारत सहित समूचे देश पर थोपने की तैय्यारी सामने है.
कहने की आवश्यकता नहीं कि वर्णाश्रमी ब्राह्मणवाद का यह नया उभार हिंदुत्ववादी राजनीति के सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने का परिणाम है. स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक दौर में गांधी के धार्मिक सहमेल व सहिष्णुता के विचार और प्रभावी नेतृत्व के चलते जो हिंदुत्ववादी राजनीति व विचार हशिये पर था ,वह अब केंद्र में है. ठीक सौ वर्ष पूर्व
प्रेमचंद ने हिंदुत्ववादी विचार की निशानदेही करते हुए लिखा था, “हिंदुओं में इस वक्त सहिष्णु नेताओं का अकाल है. हमारा नेता वह होना चाहिए जो गम्भीरता से समस्याओं पर विचार करे. मगर होता यह है कि उसकी जगह शोर मचाने वालों के हिस्से में आ जाती है जो अपनी जोरदार आवाज़ में जनता की गंदी भावनाओं को उभारकर उनपर अपना अधिकार जमा लिया करते हैं. वह कौम को दरगुजर करना नहीं सिखाता , लड़ना सिखाता है ,उसका फायदा इसी में है.” ( जमाना,फरवरी,1924). स्वाधीनता आंदोलन का यह वह दौर था, जब हिंदू-मुस्लिम के बीच साम्प्रदायिक विभाजन एक बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित था और हिंदू लेखकों द्वारा इस्लाम विरोधी ‘रंगीला रसूल’, ‘विषलता’, ’विचित्र जीवन’ व ‘ इस्लाम का विषवृक्ष’ सरीखी पुस्तकें लिखी जा रही थीं.
‘कल्याण’ और ‘हिंदू पंच” सरीखी पत्रिकायें इस साम्प्रदायिक मनोदशा को तीव्र कर रही थीं . मैथिलीशरण गुप्त भी ‘भारत-भारती’ के पृष्ठों पर स्वर्णिम हिंदू अतीत का गौरवगान करते हुए यवनों के अन्याय और ब्रिटिश राज की उदारता की धर्मध्वजा फहरा रहे थे.
भारतेंदु तो पहले ही लिख चुके थे “…. मुसलमानों की भांति इन्होंने(अंग्रेजों) हमारी आँखों के सामने हमारी देव मूर्तियाँ नहीं तोड़ी और स्त्रियों को बलात्कार से नहीं छीन लिया, न घास की भांति सिर काटे गये और न जबर्दस्ती मुँह में थूक कर मुसलमान किये गए. भारत कृतघ्न नहीं है.यह सदा मुक्तकंठ से स्वीकार करेगा कि अंग्रेजों ने मुसलमानों के कठिन दंड से हमको छुड़ाया और यद्यपि अनेक प्रकार से हमारा धन ले गये किंतु पेट भरने को भीख माँगने की विद्या भी सिखा गये.” ( भारतेंदु समग्र, पृ. 732)
इसी सोच के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उर्दू के बारे में यह मत व्यक्त किया था कि “ अँगरेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है ,न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हों.” ( हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ.300) और यह भी कि “जिन अँगरेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है वे अब भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चर्य नहीं.” (उपरोक्त,पृ.307)
प्रेमचंद और फिराक गोरखपुरी की भाषा को देश की स्वाभाविक भाषा न मानने की यही वह समझ थी जिस पर ‘हिंदी,हिंदू, हिंदुस्थान’ की सोच पुष्पित-पल्लवित हुई थी और विनायक दामोदर सावरकर का ‘दो राष्ट्रों का सिद्धांत’ परवान चढ़ा था. इन्हीं दिनों हिंदू महासभा की सहोदर संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना (1925) भी हुई थी और ‘सनातन’ को हिंदू सुधारवादी आंदोलनों के बरक्स संकीर्ण हिदुत्व का चोला पहनाया गया था.
ऐसे समय में हिंदी समाज के ‘हिंदी, हिंदू ,हिंदुस्थान’ के उस सहजबोध का प्रत्याख्यान एक बड़ी चुनौती थी,जिसकी आधारशिला मुस्लिम की अन्य छवि और हिंदू धर्म की वर्चस्ववादी विभेदकारी-जातिसंरचना पर टिकी थी. प्रेमचंद ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ‘कर्बला’ नाटक, ‘हज़रत मुह्हमद की पुण्यस्मृति’ , ‘मनुष्यता का अकाल’, ‘हिंदू मुस्लिम एकता” , ‘सांप्रदायिकता और संस्कृति’ सरीखे कई लेख व टिप्पणियां लिखीं जिनमें इस्लाम व मुस्लिम समाज के प्रति निराधार विद्वेष का प्रतिकार किया गया था. प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखन में आए थे इसलिए वे उर्दू-हिंदी के कृत्रिम मज़हबी विभाजन को नकारते हुए धार्मिक व भाषाई एकता का भी पुरजोर तार्किक समर्थन कर सके थे. जहां वे हिंदू-मुस्लिम सौहार्द्र के पक्षधर थे ,वहीं उन्होने ‘सामाजिक न्याय’ को ‘स्वराज्य’ की अनिवार्य जरूरत मानते हुए लिखा था कि “हमारा स्वराज्य केवल विदेशी जुए से अपने को मुक्त करना नहीं है, बल्कि इस सामाजिक जुए से भी, जो विदेशी शासन से कहीं अधिक घातक है.” उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि “राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्ण-व्यवस्था, ऊँच-नीच के भेद और और धार्मिक पाखंड की जड़ खोदना है.” यही कारण था कि उन्हें ‘ब्राह्मण द्रोही’, ‘हिंदू द्रोही’ और ‘घृणा का प्रचारक’ तक कहकर लांछित किया गया. लेकिन इस सब के बावजूद वर्ग और वर्ण से मुक्त उनका सहित्यचिंतन व जीवनदर्शन आधुनिक साहित्य की पूर्वपीठिका के रूप में व्यापक स्वीकृति पाने में सफल रहा था.
प्रेमचंद के समकालीन और परवर्ती लेखन में इसकी जो सुदृढ़ परम्परा निर्मित और विकसित हुई उसने हिंदी समाज के सहजबोध को हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक सोच से मुक्त कर तार्किक व आधुनिक चेतना से युक्त मानस बनाने में एक सीमा तक सहयोगी भूमिका का निर्वहन किया. राहुल सांकृत्यायन, यशपाल , नागार्जुन ,भगवतशरण उपाध्याय, रांगेय राघव, अमृत राय आदि सरीखे लेखकों ने रचनात्मक लेखन के साथ साथ वैचारिक हस्तक्षेप भी किया. राहुल सांकृत्यायन की ‘भागो नहीं दुनिया को बदलो’, ‘वोल्गा से गंगा तक’ , ‘तुम्हारी क्षय’, ‘दिमागी गुलामी’ आदि , यशपाल की ‘रामराज्य की कथा’ ,भगवतशरण उपाध्याय की ‘खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर’ ,नागार्जुन का रामचरितमानस पर लेख इसके चंद उदाहरण है. ‘रामचरितमानस’ पर प्रगतिशील लेखकों के बीच तीव्र वैचारिक बहसों का भी यही दौर था. भारत विभाजन की त्रासदी पर ‘झूठा सच’( यशपाल), ‘आधा गांव’ ( राही मासूम रज़ा) , छाको की वापसी ( बदीउज्जुमां) व ‘तमस’ ( भीष्म साहनी) सरीखे उपन्यासों ने हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक मानस की पड़ताल करते हुए इसका प्रतिविमर्श रचा. बाद के दौर में बाबरी मस्जिद ध्वंस की परिघटना की छाया में लिखे गए ‘आखिरी कलाम’( दूधनाथ सिंह) , ‘हमारा शहर उस बरस’( गीतांजलि श्री),’काला पहाड़’ ( भगवान दास मोरवाल) सहित अन्य कई उपन्यासों ने इस विमर्श को अद्यतन संदर्भ प्रदान किया. लेकिन यह ध्यान देने की बात है अस्सी के दशक के बाद के इस समूचे दौर में कथा- विमर्श के केंद्र में जो उपन्यास चर्चा के केंद्र में रहे वे प्राय: मध्यवर्गीय आस्वादपरक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाले या उपभोक्तावादी संस्कृति के इर्द गिर्द तक सीमित रहे. विनोद कुमार शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी ,सुरेंद्र वर्मा आदि के उपन्यास इसका उदाहरण हैं. जबकि यही वह दौर था जब समूचा हिंदी क्षेत्र मंदिर-मंडल की परिघटना की जकड़बंदी में था. जब हिंदी पट्टी में नया ‘मैला आँचल’ लिखे जाने की जरूरत दरपेश थी तब रेणु की इस क्लासिक कृति के पुनर्पाठ से भी किनाराकशी की गई. रेणु ने ‘हिंदू राज की पताका’ और ‘संघ की काली टोपी’ के विमर्श को वर्णाश्रमी जाति-व्यवस्था के जिस द्वैत के माध्यम से उजागर किया था ,वह हिंदी क्षेत्र की सामाजिक संरचना पर उनकी गहरी पकड़ का परिणाम था. यही हश्र दूधनाथ सिंह के उपन्यास ‘आखिरी कलाम’ का हुआ ,जिसमें कहा गया था कि “…ब्राह्मणवाद ही इस देश की प्रगति में बाधक है. यह एक अलग तरह का उपनिवेशवाद है जिससे जनता को लड़ना पड़ेगा .कोई भी आज़ादी तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक ब्राह्मण उपनिवेश का खात्मा नहीं होगा.” इतना ही नहीं इसमें रामचरितमानस को हिंसक ग्रंथ और तुलसीदास के ‘उत्कृष्ट कविकर्म’ को ‘विचारों की तानाशाही’ के रूप में विश्लेषित किया गया है.
यह स्वीकार किया जाना चहिए कि इन सारे प्रयत्नों व हस्तक्षेप के बावजूद राजनीतिक स्वाधीनता और सामाजिक स्वाधीनता का जो सहमेल हिंदी सहित समूचे भारतीय समाज में सुदृढ़ होना चाहिए था ,वह न हो सका. इसके चलते भारतीय राष्ट्र-राज्य को समतावादी आधुनिक जनतंत्र बनाने की परियोजना आधी-अधूरी रही. वर्णाश्रमी जाति-तंत्र की सोपानीकृत व्यवस्था के उच्च सोपान पर अवस्थित द्विज समुदाय द्वारा अपने पारंपरिक विशेषाधिकारों से मुक्ति की चाहत तो वांछ्नीय थी, लेकिन व्यावहारिक नहीं. उत्तर भारत के स्वामी अछूतानंद , संतराम बी.ए., पेरियार ललई सिंह ,चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु सरीखे गैर-द्विज सबाल्टर्न बौद्धिकों द्वारा किए गये जनजागरण अभियान भी व्यापक रूप से प्रभावी न हो सके. कारण यह कि प्रभुत्वशाली वैचारिकी का प्रति-विमर्श होने के चलते सवर्ण बौद्धिकों को तो यह अस्वीकार्य था ही , मुख्यधारा के परिवर्तनकामी बौद्धिक भी धर्म और मिथक की इनके द्वारा की गई जनोन्मुख व्याख्या को लेकर सहज नहीं थे. ये सबाल्टर्न बौद्धिक ‘ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत’ की ही नियति को प्राप्त हुए थे. इनका उल्लेख न तो साहित्य की मुख्यधारा में शामिल हुआ , न ही वे प्रगतिशील साहित्य की जनवादी धारा में पांक्तेय हुए. कारण यह कि सोवियत क्रांति के प्रभाव व प्रेरणा के चलते वामपंथी आंदोलन समता ,समानता के समाजवादी मूल्यों का पक्षधर होकर वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए तो प्रतिश्रुत था ,लेकिन वर्ण व जाति आधारित शोषण के विरुद्ध अभियान उसके वर्गीय एजेंडे में शामिल नहीं था.
यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समूचे दौर मे कथित मुख्यधारा के हिंदी साहित्यिकों के बीच वर्णाश्रमी हिंदू सत्ता संरचना की आलोचना की परंपरा क्षीण हुई है. तुलसीदास ,रामचरितमानस और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ब्राह्मणवादी अवधारणाओं को पवित्र गाय के मानिन्द संरक्षित करने का भाव इस दौर में अधिक प्रबल हुआ है. तुलसी के बरक्स कबीर के प्रति आकर्षण पर हिंदी बौद्धिकों के बीच यह चिंता व्यक्त की जाने लगी है कि “दुर्भाग्यवश हिंदी लेखकों ही नहीं, पाठकों की नयी पीढ़ी भी तुलसीदास के प्रति घोर उपेक्षा का भाव रखती है और दोनों कबीर पर फिदा हैं,….नयी पीढ़ी के लोग कबीर के वर्णव्यवस्था तथा वाह्याचार विरोध को ही ल्क्ष्य मानकर उन्हें सर्वाधिक अंक देते हैं” . यहां तक कहा गया है कि “कबीर को आधुनिक घोषित करने का मुक्तिबोध का प्रयास स्वस्थ आलोचना का लक्षण नहीं है.” और यह भी कि “निर्गुण भक्ति को प्रगतिशील और आधुनिक मानने के इस अभियान को दलितों और पिछ्डों ने जोर-शोर से आगे बढ़ाया. आज दलित विमर्श के भीतर कबीर समर्थन और तुलसी विरोध की जो अतिरेकी गर्जना है उसका उत्स मुक्तिबोध का लेख ‘मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू है “ . यानी मुक्तिबोध दोषी हैं दलित टोलों में कबीरपंथ के लिए. यह एक बानगी है उस सवर्ण बौद्धिक मानस की जो तुलसी की उत्कृष्ट कविताई की ओट में ‘रामचरितमानस’ में सन्निहित ब्राह्मणवाद के वर्चस्व की आलोचना से बचता है और कबीर की स्त्रीदृष्टि की सीमा के बहाने उन पर ग्रहण लगाता है. तुलसी के ‘रामचरितमानस’ की यह रक्षा उस तार्किक प्रगतिशील दृष्टि के विरुद्ध है ,जिसके अंतर्गत बाबा नागार्जुन ने लिखा था कि “ रामचरितमानस हमारी जनता के लिए क्या नहीं है? सभी कुछ है! दकियानूसी का दस्तावेज़ है…नियतिवाद की नैय्या है …जातिवाद की जुगाली है . सामंतशाही की शहनाई है ! ब्राह्मणवाद के लिए वातानुकूलित विश्रामागार ..पौराणिकता का पूजा-मंडप ..वह क्या नहीं है ! सब कुछ है ,बहुत कुछ है ! रामचरितमानस की बदौलत ही उत्तर भारत की लोकचेतना सही तौर पर स्पंदित नहीं होती. ‘रामचरितमानस’ की महिमा ही जनसंघ के लिए सबसे बड़ा भरोसा होती है हिंदीभाषी प्रदेशों में .” ( नागार्जुन रचनावली, खंड 6 ,पृ. 269).
ध्यान देने की बात यह है कि नागार्जुन और दूधनाथ सिंह सरीखे लेखक सवर्ण हिंदू मानस, हिंदुत्व की राजनीति और ‘रामचरितमानस’ की जिस नाभिनालबद्धता को लक्षित कर सके थे ,उस पर इस दौर में सवर्ण हिंदी बौद्धिकों की चुप्पी है. इस पर हैरत इसलिए नहीं होना चाहिये क्योंकि इसके पूर्व डा. रामविलास शर्मा तो यह तक लिख चुके थे कि “तुलसीदास का स्वप्न श्रमिक जनता के लिए धरोहर है जिससे प्रेरित होकर वह समाजवाद के लिए मंजिल दर मंजिल बढ़ती जायेगी”. वे ‘सामाजिक न्याय’ की अवधारणा को अलगाववादी मानते थे .उनका स्पष्ट मत था कि “ शोषण का माध्यम वर्ग शोषण है. किसी का शोषण इसलिए नहीं होता कि वह पंडित है या चमार है या किसी जाति का है.” वे ब्राह्मणवाद पद से भी इंकार करते थे. यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मंडल-मंदिर के राजनीतिक उभार और दलित विमर्श की आमद के बाद हिंदी का बहुलांश सवर्ण बुद्धिजीवी अपनी जातिगत अवस्थिति में वापस लौट गया है. डा.नामवर सिंह ने भी आरक्षण का विरोध किया और वे ‘अपनी जाति पर गर्व करना’ बुरा नहीं मानते थे. ऐसे में याद आते हैं राजेंद्र यादव जिन्होंने बाबरी मस्जिद ध्वंस के पूर्व ही राजनीतिक हिंदुत्व की आहटों को सुना था और लगातार इसके विरुद्ध हिंदी बौद्धिकों को आगाह करते रहे थे. दरअसल राजेंद्र यादव के लिए दलित, स्त्री व अल्पसंख्यक की उपस्थिति मात्र प्रतिनिधित्व तक सीमित न होकर हिंदुत्व के प्रत्याख्यान की आधारभूमि की जरूरी शिनाख्त थी . उन्हीं के शब्दों में “मुर्दा सड़ांध और भविष्यहीन हिंदू समाज की जड़ताओं को पहली बार सिद्धों ने तोड़ा था ,उनमें दलित,स्त्री और बौद्ध थे. दूसरी बार संतों के भक्ति आंदोलन ने – वहां भी दलित, स्त्रियां और मुसलमान थे. ये आंदोलन क्षेत्रीय नहीं अखिल भारतीय थे. निश्चय ही इक्कीसवीं सदी ने वही मजबूरियां फिर पैदा कर दी हैं कि ये कुचली ,दबी और हाशिए पर फेंकी गयी शक्तियाँ फिर हमें ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ से मुक्त करें और अपना इतिहास नये सिरे से खुद लिखें. मगर इसके लिए जरूरी शर्त यही है कि हम अपने-अपने समाजों के अंदर एक रूथलेस यानी बेबाक, बेलौस और निडर बहस के छूटे हुए सूत्रों को अपनी भाषा और अपने मुहावरों में देखने-समझने-कहने की फिर शुरुआत करें.” (मैं हँस नहीं पढ़ता,पृ.137) यह अनायास नहीं है कि राजेंद्र यादव कथित ‘हिंदी नवजागरण’ को ‘हिंदू नवजागरण’ के नाम से चिन्हित करते थे क्योंकि इसमें वर्णाश्रमी जातिभेद को विमर्शकारी नहीं बनाया गया था.
दरअसल जिस तरह प्रेमचंद स्वराज की राह में हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य को रोड़ा मानते थे उसी तरह राजेंद्र यादव भी आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण में बहुसंख्यकवादी सोच के खतरे के प्रति सजग थे. इसीलिए वे लगातार इसके विरुद्ध वैचारिक अभियान चलाते रहे. यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजेंद्र यादव की अनुपस्थिति के बाद यह अभियान लगभग थम सा गया है. सच तो यह है कि हिंदी साहित्यिकों और बौद्धिकों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वे ‘पोलिटिकल’ हिंदुत्व को तो हराना चाहते हैं ,लेकिन वर्णाश्रमी जातिवाद को समस्याग्रस्त किए बिना. वे निचले जातिगत सोपान पर अवस्थित दलित व पिछडों की प्रतिरोधी एकता को अस्मितावाद के नाम पर तो खारिज करते हैं ,लेकिन सवर्ण अस्मिता के दमनकारी उभार को राष्ट्रवादी चेतना में समाहित कर लेते हैं. हिंदी बौद्धिकों का यह सामाजिक अनुकूलन हिन्दुत्व की चुनौती और संवैधानिक संकट को अस्तित्व का प्रश्न न मानकर महज राजनीतिक मुद्दे तक सीमित कर देता है. इसलिये न तो वह सत्तातंत्र के विरुद्ध मुखर हो पाता है, न सत्ता द्वारा प्रदत्त लाभ-लोभ के अवसरों को छोड़ पाता है और न ही उसे गोदी मीडिया के मंचों से विकर्षण होता है . यहाँ तक कि न तो उसे गांधी के समकक्ष गोडसे को विमर्शकारी बनाने में कोई हिचकिचाहट महसूस होती है और न ही अकबर के मुकाबले तुलसी को ‘महाबली’ बनाने में. ऐसे में हिंदी की आदिवासी कवयित्री जसिंता केरकट्टा द्वारा गोदी मीडिया के पुरस्कार को ठुकराना एक प्रेरक कदम है. यह सचमुच विडम्बनात्मक है कि हिंदी के जिस वामपंथी कवि ने साहित्य अकादमी पुरस्कार इसलिये वापस किया था कि अकादमी ने एमएम कलबुर्गी की हत्या के बाद शोकसभा नहीं की थी , वही अब साहित्य अकादमी के स्वायत्त संस्था होने की दलील देकर उसका बचाव कर रहा है. यह सब कहने का आशय उन प्रयत्नों को कमतर करना नही है जो प्रतिरोध के सशक्त स्वर हैं. यह दर्ज़ किया जाना चाहिए कि ‘गूंगी रुलाई का कोरस’, ‘वैधानिक गल्प’ और ‘कीर्ति गान’ सरीखी आज के समय को दर्ज़ करने वाली औपन्यसिक कृतियां इसी दौर में लिखी गई हैं.
जरूरत है हिंदी लेखकों व बौद्धिकों द्वारा आत्मालोचना और अपनी भूमिका पर ठहरकर विचार करने की . हिंदी समाज और साहित्य का वर्तमान परिदृश्य गंभीर चिंता का विषय है. आज जनतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती महज राजनीतिक न होकर सामाजिक और सांस्कृतिक भी है. ऐसे ही समयों के लिए प्रेमचंद ने कहा था कि “साहित्य राजनीति के पीछे चलनेवाली चीज नहीं,उसके आगे-आगे चलनेवाला ‘एडवांस गार्ड’ है.” क्या हिंदी लेखक अपनी इस भूमिका के निर्वहन के प्रति सजग है? ( मेरी पुस्तक ‘विमर्श और व्यक्तित्व ‘ में शामिल लेख )
वीरेंद्र यादव के फेसबुक वॉल से साभार