वरिष्ठ साहित्यकार ओमसिंह अशफ़ाक ने एक विचारोत्तेजक टिप्पणी लिखी है। वह लोक संस्कृति से वामपंथियों के जुड़ाव की कमी को लेकर चिंतित और गुस्सा हैं। शायद वह कहना चाहते हैं कि वामपंथी दलों के नेताओं/ कार्यकर्ताओं ने त्योहारों के जरिये लोगों से जुड़ने की जगह दूरी बनाकर रखी, जिस कारण जनता उनसे छिटक गई जबकि आम आदमी के हितों के लिए सबसे मजबूती से लड़ाई अगर किसी विचारधारा के वर्करों ने लड़ी है तो वे कम्युनिस्ट ही हैं। प्रतिबिम्ब मीडिया उनके विचार से सहमत नहीं है क्योंकि रीति रिवाजों और संस्कृतियों से छोटा-बड़ा हर व्यक्ति जुड़ा होता है। बस वह इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करता और वामपंथी दलों के कार्यकर्ता और समर्थकों की भी संभवतः यही सोच रही है, वे खासतौर पर आडंबर में विश्वास नहीं करते हैं जिसे वर्तमान में लोक-संस्कृति और धर्म का प्रमुख स्वरूप मान लिया गया है। हमारे देश में पिछले एक दशक से हर चीज के प्रदर्शन खासतौर पर धार्मिक आयोजनों के दौरान भव्यता के स्तर पर भौंडे प्रदर्शन की चकाचौंध से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के जरिये इसके प्रचार-प्रसार ने दूरगामी असर डाला है। लेकिन लोक संस्कृति से दूरी को लेकर एक बुद्धिजीवी जब चिंता और गुस्सा व्यक्त करता है तो उस पर खुलकर बहस होनी ही चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रतिबिम्ब मीडिया के प्रबुद्ध पाठक इस पर अपनी राय रखें और स्वस्थ और सार्थक बहस में भागीदारी करें। संपादक
लोक संस्कृति से गायब कम्युनिस्ट!
ओम सिंह अशफ़ाक
इस रक्षाबंधन पर देखने में आया कि 75 साल की आयु के कामरेड अपनी 80-85 साल उम्र की बहनों से राखी बंधवा रहे हैं! इससे पहले प्राय: ऐसी तस्वीरें देखने में नहीं आती थीं।
आखिर बहुत लंबे अरसे के बाद कामरेड़ों को भी अपनी लोक संस्कृति से जुड़ने का ख्याल आया। लोक संस्कृति से कटने का नुकसान यह हुआ है कि कामरेड अपने भाईचारे से,रिश्तेदारों से,गोत्र-समुदाय से और अंततः समाज से ही कटकर अलग-थलग हो गए हैं? जब आप सब जगह से कट जाते हैं तो आपकी राजनीतिक ताकत भी खत्म हो जाती है,नगण्य रह जाती है? फिर तो आपकी पार्टी या संगठन सिर्फ़ कागज पर सिमट जाता है। वही हुआ भी है। 40-50 साल से नौजवान काडर कम्युनिस्ट पार्टियों में नहीं आ रहा है। सिर्फ ट्रेड यूनियनों के सहारे ये पार्टियां चल रही हैं, वहां भी मुख्यत: कर्मचारी और अध्यापक लेवी व चंदा देकर पार्टी का कोष भरते हैं जोकि राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन-सम्मेलनों के मौके पर और ज्यादा राशि जमा हो जाती है। उससे कम्युनिस्ट पार्टियों के “दफ्तर और रसोई” (कम्युनिटी-किचन) साल भर चलते रहते हैं और ‘सरप्लस’ चंदे से नयी जगहों पर नए भवन बना लिए जाते हैं।.. लेकिन जब भाजपा और मोदी जैसा शासक सत्ता में आ जाता है तो “सो सुनार की और एक लोहार की” कहावत चरितार्थ हो जाती है! कम्युनिस्टों ने 100 साल में चंदा व लेवी से जितने भवन बनाए थे; मोदी के 5 साल के राज में ही भाजपा ने 100 गुना ज्यादा भवन बनाकर खड़े कर दिए हैं? मतलब यह है कि संपत्ति के ‘मामले और काडर’ के मामले में भी भाजपा कम्युनिस्ट पार्टियों से 100 गुना या हजार गुना आगे निकल गई है।
वामपंथी सिर्फ विचारधारा के बल पर भाजपा से आगे होने का दावा कर सकते थे लेकिन यहां तक आते-आते उस मामले में भी बहुत पिछड़ गए हैं। क्योंकि उन्होंने अपने “देश-काल” की जरूरतों को पहचाना ही नहीं और ना ही उसके मुताबिक अपनी कार्य योजना बनाई है? इसलिए वामपंथ का ‘हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर’ आज दोनों अप्रासंगिक बना दिए गए हैं। यह देश और समाज के लिए बहुत दुखद स्थिति है और कम्युनिस्टों को छोड़कर सारा देश इसको समझता भी है और चिंतित भी है। बस कम्युनिस्ट समझने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज के बारे में कभी दूसरी तरह से सोचना, देखना, सुनना-गुनना सीखा ही नहीं है? बेशक अपने दफ्तरों में बैठकर वे ‘डाइलेक्टिकल थिंकिंग’ पर बहस जरूर करते रहे हैं।

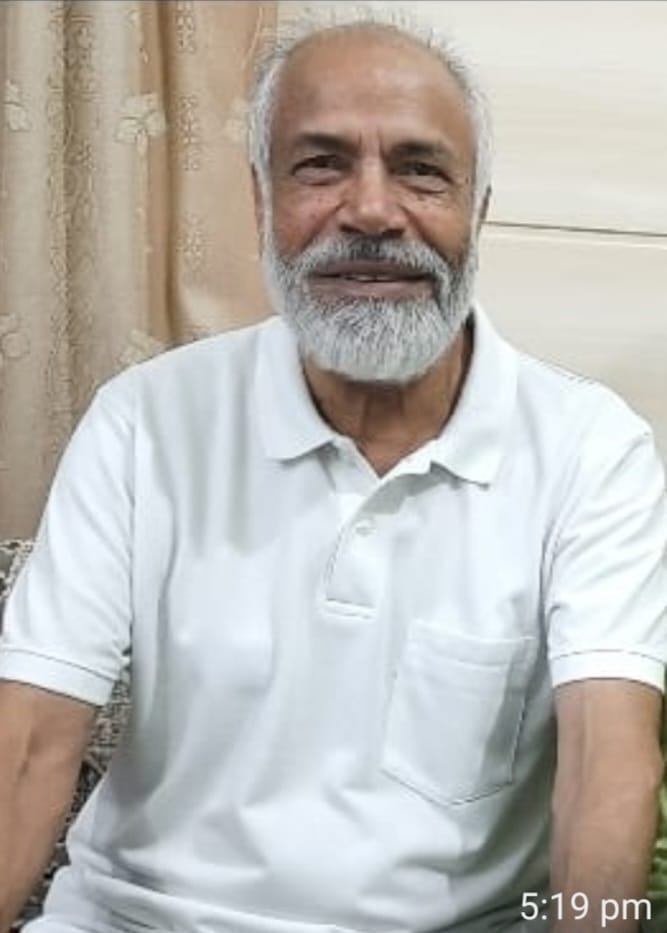



लोक संस्कृति से गायब कम्युनिस्ट पर ओम सिंह अशफ़ाक से कुछ लोगों की बात हुई और लोगों ने उनकी टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चूंकि राय मौखिक तौर पर थी तो अशफ़ाक जी से निवेदन किया गया कि वह उसे लिखित रूप में दे देें। अशफ़ाक जी ने प्रतिक्रिया का सार जिस रूप में दिया है उसे वैसे ही प्रकाशित कर रहे हैं साथ में उनकी राय भी है।
टॉपिक पर कुछ लिखित टिप्पणियों के अलावा कुछ लोगों से अनौपचारिक मौखिक वार्तालाप भी हुआ है जिसमें उनकी मुख्य चिंता इस बात को लेकर थी कि यदि हम कम्युनिस्ट भी तीज- त्योहारों एवं परंपरागत मेलो-ठेलों की प्रचलित रूढ़ियों पर अमल करेंगे तो उससे तो “अंधविश्वास और पाखंडवाद” का ही प्रचार-प्रसार होगा,उसको बढ़ावा मिलेगा? उनकी यह शंका निराधार तो नहीं है लेकिन हमें इसके अन्य पहलुओं पर भी गौर करनी होगी।
मिसाल के तौर पर हम यहां “रक्षाबंधन और करवा-चौथ” जैसे दो त्योहारों पर चर्चा कर सकते हैं:
‘रक्षा-बंधन’ को लेकर उनका तर्क है कि इस त्योहार की परंपरा का संदेश है कि स्त्री (यहां पर बहन) कुदरती तौर पर कमजोर है और उसको अपनी रक्षा के लिए भाई के ऊपर निर्भर रहना चाहिए? इसलिए बहन से भाई के हाथ में राखी का धागा बांधने का प्रचलन चलाया गया जिसके जरिए भाई बहन को उसकी रक्षा का “आश्वासन और वचन” देता है!.. यह ‘सन्देश’ स्त्री के मन में हीन- भावना पैदा करता है और उसको पुरुष की आधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करता है जोकि आधुनिक समाज में ‘लैंगिक-समानता’ के विचार को आहत करता है? और इस तरह से समानता पर आधारित एक न्याय पूर्ण समाज के रास्ते में बाधा बनता है। जाहिर है कि उपरोक्त स्थापना से सही सोच के सभी इंसान जरूर सहमत होंगे और हमें भी इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अत: यह स्पष्ट है कि इस पर हम सबकी राय समान है।
हमारे विमर्श का मुद्दा यह है कि आखिर क्यों कम्युनिस्ट लोग लोक-संस्कृति से गायब हुए हैं या कट गए हैं और अब वे किस तरह से “लोक संस्कृति की लोक-धारा” में लौट सकते हैं। जाहिर है यह काम अपने तीज-त्योहारों मेले-ठेलों से अलग होकर तो नहीं होगा? जिस तरह किसी बरसाती-नाले के पानी की समुद्र से मिलने की आकांक्षा गंगा-जमुना जैसी सदाबहार नदियों में समाहित हो जाने से ही पूरी हो सकती है अन्यथा दस- बीस,पचास-सौ किलोमीटर बहकर वह अंततः सूख जाएगा और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस संकट का समाधान कैसे हो? शायद एक उपाय कारगर हो सकता है:
हमें इन त्योहारों की परंपरागत व्याख्या में निहित “नकारात्मक” संदेश को विस्थापित करके उस जगह को वैकल्पिक “सकारात्मक” संदेश से भरना होगा। और यह काम इसमें कुछ नई परंपराएं जोड़कर किया जा सकता है। जैसे रक्षाबंधन पर एक बहन भाई की कलाई पर राखी का धागा बांधती है इसी तरह से भाई भी अपनी बहन की कलाई पर राखी का धागा बांधे और परस्पर “सहयोग,समानता और एक-दूसरे की रक्षा” के विचार की स्थापना करें!..
ऐसे ही “करवा-चौथ” पर भी किया जा सकता है। जब कोई पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत-उपवास करती है तो उसका पति भी इसी भावना को लेकर अपनी पत्नी के लिए व्रत करे, छलनी के माध्यम से उसके चेहरे का दीदार करे,उसी के साथ उपवास खोले,समान आसन पर,साथ बैठकर भोजन करे और जो ‘रिचुअल्स’ इस अवसर पर पत्नी करती है,वह भी वैसा आचरण करे! इससे यह त्योहार भी “दो-तरफा और समान-आचरण” का उपक्रम बन जाएगा! ‘सकारात्मक संदेश’ इसकी नकारात्मकता को दूर कर देगा।.. शेष पारिवारिक,सामुदायिक और सामाजिक आयोजनों में भी इसी तरह से परिवर्तन,संशोधन एवं संवर्धन किया जा सकता है। ऐसा आचरण करके आस्तिक-नास्तिक आध्यात्मिक गैर-आध्यात्मिक सब लोग लोक-संस्कृति की मुख्य धारा में लौट सकते हैं,समायोजित हो सकते हैं और अपने परिवार,समुदाय एवं समाज से नई पहचान एवं नई ताकत हासिल कर सकते हैं। कृपया इस टिप्पणी पर भी आप अपने विचार हमसे साझा करेंगें तो विमर्श आगे बढ़ेगा और कोई सर्वमान्य हल जरूर निकल कर आएगा।
-ओम सिंह अशफा़क, कुरुक्षेत्र।
“लोक संस्कृति में निहित मेले,नृत्य यहां तक कि भजन-कीर्तन के आनन्द की स्वाभाविक प्रवृत्ति से वंचित क्यों रखा जाए जनमानस को किसी भी विचारधारा के नाम पर।
“मुझे तो खूब आनंद आता है। हां, राजनीतिक दृष्टि से मैं लेफ़्ट की आर्थिक नीतियों का भी पक्षधर हूं, किंतु सामान्य जनजीवन में आर्थिक पक्ष ही तो सब कुछ नहीं। मैंने दिन भर कड़ा श्रम करने वाले श्रमिकों को भी सायंकाल या रात्रि में झुग्गियों में सामूहिक रूप से डफली पर रामायण की चौपाइयों का कीर्तन करते और आनंद मग्न होते देखा है।
इसी तरह रक्षाबंधन पर बहन-भाई के और करवा चौथ पर पति-पत्नी के प्रेम-पक्ष की अनदेखी नहीं की जा सकती,मानसिक-आत्मिक आनंद हेतु, अन्यथा जीवन महानीरस होगा।
-डा.अमृतलाल मदान,प्रोफेसर (सेवानिवृत)आरकेएसडी पीजी कॉलेज,कैथल (हरियाणा)
अशफ़ाक जी ने बिल्कुल सही नब्ज पर हाथ रखा है। कम्युनिस्ट सिर्फ हर बात की आलोचना तो करते हैं लेकिन किसी घटना, रीति-रिवाज या परम्परा में निहित भावना या लगाव अथवा आस्था को नहीं समझते जो सदियों से चली आ रही हैं। समाज अनंत काल से अपनी परम्पराओं, आस्थाओं और भावनाओं को अपने-अपने ढंग जी रहा है। कम्युनिस्ट एक निश्चित समय में प्रचारित हुई विचारधारा है जो समाज से बड़ी नहीं हो सकती। आपने बिलकुल सही मुद्दे पर सटीक टिप्पणी की है।
-करमचंद केसर,हरियाणवी गजल के मशहूर शायर और अध्यापक,कैथल (हरियाणा)
आपका ऊपरोक्त लेख (लोक संस्कृति से गायब कम्युनिस्ट) और जयपाल जी के जो विचार हैं उक्त पोस्ट में, उनके बारे में भी मेरी वही टिप्पणी है कि कम्युनिज्म में भाववाद बिल्कुल गायब है इसलिए उनके विचारधारा को ‘कम्युनिस्ट- रूढ़िवाद’ नाम दिया जा सकता है।
अभी उस दिन (राखी वाले दिन) मेरी 5 साल की पोती ने मुझसे सवाल किया था कि लड़के लड़कियों को राखी क्यों नहीं बांधते? मैंने अपने शब्दों में उसे उत्तर देने की कोशिश की पर मैं नहीं दे सका क्योंकि वास्तव में मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। क्योंकि उसका अबोध मन पिछले इतिहास को नहीं जानता इसलिए बच्चों के मन में ये सवाल उठते हैं।
अभी भी मेरे मन में यह सवाल अटका हुआ है। यह मुझे असहज करता रहता है।
-सरदार बलदेव सिंह महरोक, वरिष्ठ लेखक एवं बाल साहित्यकार, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
‘राखी की बधाई!
हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं’
कहकर बहनों का
आए दिन अपमान बंद हो!”
-विकास नारायण राय, पूर्व आईपीएस,फरीदाबाद (हरियाणा)
अशफाक जी की बात से सहमत हूं, लेकिन मेरी कुछ जिज्ञासा है-
1. पहली जिज्ञासा ‘कम्यूनिस्ट’ शब्द से है। इस विचारधारा से इतर व्यक्ति भी तो आपके साथ जुड़ सकता है।
2. हमें परम्परागत और रुढीवादिता को छोड़ इस त्योहार को केवल भाई – बहन के मिलन का अवसर मानना चाहिए,चाहे वो चचेरे ही क्यों ना हों। वेसे भी आजकल तथाकथित जागरुक समाज में Single Child की परम्परा है और सरकारें भी इस परम्परा को संरक्षण दे,बढा रही हैं।
3. आज के उपभोक्तावादी युग में तुलना निर्रथक हो गई है। हमारी मां भी घर की बहु थी और पत्नी भी है। अंतर आप समझ सकते हैं।
4. मेरे जैसे अंतिम समय तक पिता से बोलने में हिचकिचाते थे/हैं लेकिन आज के बच्चे पिता को ‘यार पापा’ बोलते हैं।
5. इसलिए Transition के दौर में चलते चले जाओ।
6. आपके विचारों पर टिप्पणी के लिए माफी।
-डा.अतुल यादव, प्रोफेसर (इतिहास) अंबाला (हरियाणा)
ओम सिंह अशफ़ाक ने प्रतिक्रिया का स्वागत करते हुए ‘पॉइंट वाइज’ स्पष्टीकरण दिया है:
1. यहां हमारा ‘फोकस’ केवल एक ‘व्यक्ति’ पर नहीं बल्कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के “विचार एवं समूह” पर है।
2. वैसे तो कोई भी त्यौहार खुद “परंपरागत एवं रूढ़िवादिता” है। लेकिन कोई सरकार/संगठन/व्यक्ति उस पर पाबंदी (Ban) नहीं लगा सकता है।
3. उपभोक्तावाद का जोर तो जरूर है। लेकिन ‘सास और बहू’ दो अलग पीढ़ियां होती हैं और हर दौर में सामाजिक मूल्यों में कुछ ‘बदलाव’ तो होता ही है। मूल्यांकन इस बात का होना चाहिए कि इस बदलाव में ‘पॉजिटिव और नेगेटिव’ कितना है।
4. बीते दौर में बच्चों को इतनी आजादी नहीं थी। उनको डराया,धमकाया और दंडित किया जाता था। लेकिन आजकल बच्चे माता-पिता से भी ‘समानता का व्यवहार’ चाहते हैं।
5. संक्रमण काल (transition period) तो दो-दौर के बीच में होता ही है। क्योंकि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है,जो ‘कंटिन्यूटी’ में चलती है, एक दौर से दूसरे दौर में सीधे ‘छलांग’ नहीं लगाई जा सकती है।
6. मैंने तो विमर्श को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए खुद ही सबकी प्रतिक्रिया/राय/टिप्पणी मांगी थी।।आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है।
आग्रह है कि फिर से मेरे वक्तव्य को ध्यान से पढ़ें और समग्रता में एक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दें कि हमारे त्यौहारों में से ‘नकारात्मकता’ विस्थापित करके उनमें ‘सकारात्मक’ मूल्य कैसे जोड़े जा सकते हैं।