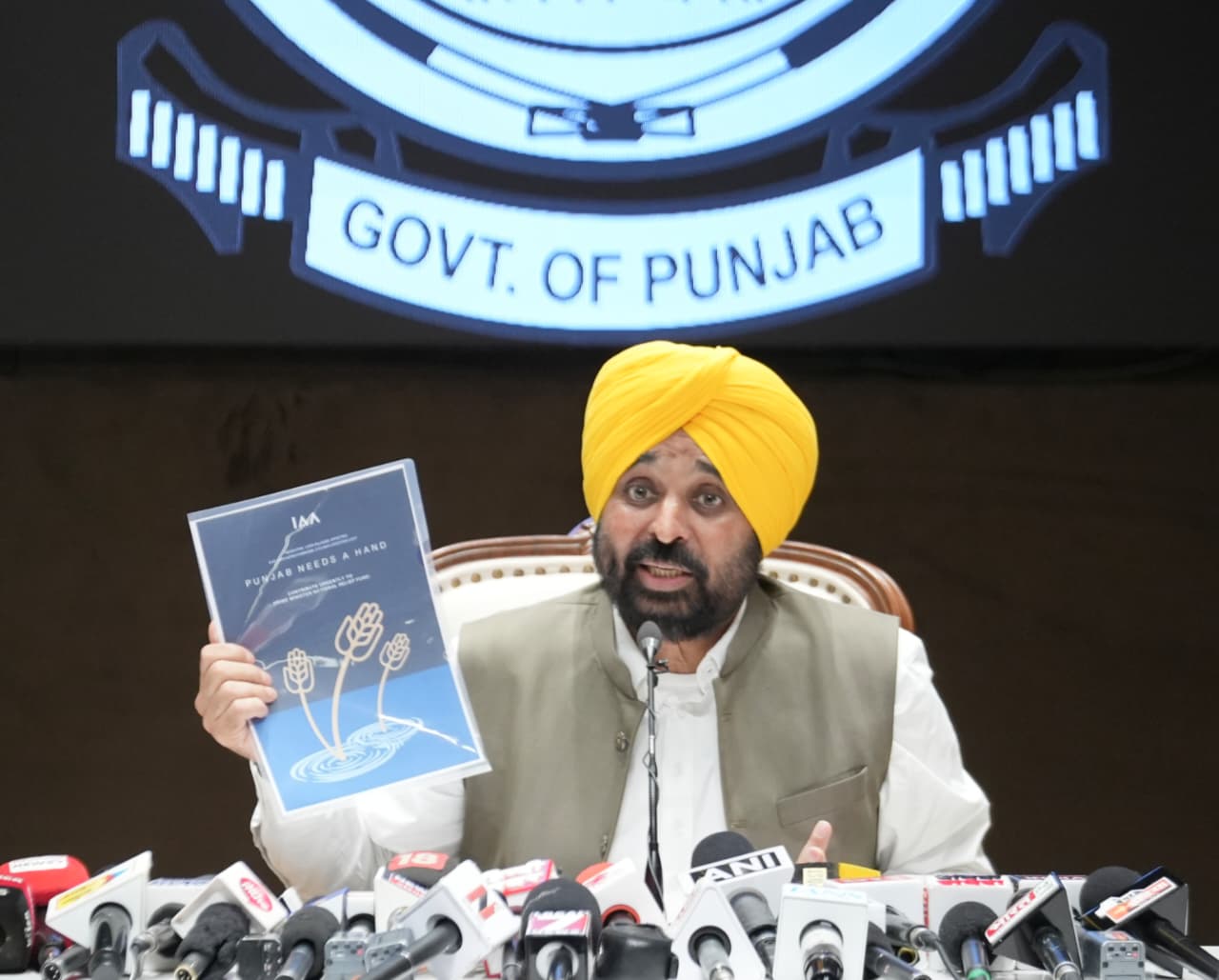अमेरिकी पक्ष
भारत के लिए आत्मविश्वासपूर्ण व्यावहारिकता को अपनाने का एक अवसर
रसेल स्टैमेट्स
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग निश्चित रूप से, शायद जल्द ही, एक व्यापार समझौते पर पहुँच जाएँगे। तर्क और विवेकशीलता वस्तुतः यही तय करते हैं। और हालाँकि भारत और उसके सबसे बड़े निर्यात बाज़ार तथा सबसे स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार के बीच व्यापार तनाव कुछ ऐसा नहीं है जिसकी भारत को चाहत थी, फिर भी हो सकता है कि यही वह चीज़ हो जिसकी उसे ज़रूरत है। यह समझौता कैसा दिख सकता है? यह देखने के लिए कि इन वार्ताओं में भारत की ‘जीत’ होती है या ‘हार’, आपको विशिष्ट मुद्दों को नज़रअंदाज़ करना चाहिए—जैसे अमेरिका से और ज़्यादा अल्फाल्फा? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आसान प्रमाणन प्रक्रियाएँ?—और व्यापक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
भारत को अपने हित में एक बड़े, सकारात्मक व्यापार समझौते की आवश्यकता है, और वह वर्तमान स्थिति को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकता है। भारत के दृष्टिकोण से, एक सफल व्यापार समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि वार्ताकार वर्तमान संभावनाओं को समझते हैं या सीमित क्षेत्रों के हित वाले छोटे-मोटे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमेरिकी भाषा में, भारत को या तो बड़ा कदम उठाना चाहिए या घर लौट जाना चाहिए।
टैरिफ विवाद और असामान्य रूप से सीधी कूटनीतिक भाषा स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित लगती है, लेकिन भारत के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है कि वह एक चुनौती को रणनीतिक लाभ में बदल सके। भारत का सम्मानजनक संयम उसे इस अवसर का उपयोग लंबे समय से लंबित आर्थिक सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में करने की अनुमति देता है, जिससे भारतीय व्यवसायों को लाभ होगा, क्षेत्रीय साझेदारियों को मज़बूती मिलेगी, और देश को चीनी प्रभाव के एक अधिक प्रभावी प्रतिकारक के रूप में स्थापित किया जा सकेगा—और साथ ही रूस और चीन के साथ उचित संबंध भी बनाए रखे जा सकेंगे। विकल्प है गतिरोध और अनाकर्षक साझेदारों के साथ एक निरंतर निम्न भूमिका।
डेयरी आयात पर जनता का रुख भारत की बुनियादी चुनौती को दर्शाता है; अगर स्वदेशी भारत के लिए अच्छा है, तो स्वदेशी अमेरिका के लिए अच्छा क्यों नहीं है? ज़रा सोचिए: इसी समय, अमेरिका के मध्य-पश्चिम में कहीं, अमूल दूध उत्पादों से लदे ट्रक, जिनमें अमूल ताज़ा, अमूल गोल्ड और अमूल स्लिम एंड ट्रिम शामिल हैं—जो अमूल के अमेरिकी परिचालन में अमेरिकी गायों से उत्पादित हैं—पटेल ब्रदर्स जैसी भारतीय-अमेरिकी किराना श्रृंखलाओं या कॉस्टको जैसी वेयरहाउस दिग्गज कंपनियों की ओर जा रहे हैं।
फिर भी, अगर अमूल ने उसी अमेरिकी-निर्मित अमूल दूध को भारत में निर्यात करने की कोशिश की, तो मौजूदा भारतीय नियम सुरक्षा चिंताओं से लेकर धार्मिक प्रथाओं और छोटे किसानों की सुरक्षा की ज़रूरत तक, कई तरह की आपत्तियों का हवाला देकर उसे रोक देंगे। विडंबना साफ़ है: भारत अपने छोटे डेयरी किसानों को अमूल अमेरिका द्वारा उत्पादित दूध के आयात से बचाता है, जिसका स्वामित्व अमूल इंडिया के पास है, जो खुद छोटे भारतीय डेयरी किसानों का एक समूह है।
यह बस एक उदाहरण है जहाँ भारत तर्क देता है कि उसके लोग सुरक्षा के हक़दार हैं, लेकिन अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए टैरिफ़ लगाना किसी न किसी तरह से अनुचित है। यह बिल्कुल भी विश्वसनीय स्थिति नहीं है, और इस पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम का गुस्सा साफ़ और तर्कसंगत है। ऐसे रुख़ छोड़ने से भारत को बहुत कम नुकसान होता है और ज़्यादा विश्वसनीयता मिलती है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की 2024 की राष्ट्रीय व्यापार अनुमान रिपोर्ट भारतीय व्यापार बाधाओं की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करती है, जिनका समाधान वास्तविक संप्रभुता से समझौता किए बिना किया जा सकता है। क्या भारत की राष्ट्रीय गरिमा सचमुच डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स पर अनावश्यक प्रतिबंधों पर निर्भर करती है? क्या दुनिया के सबसे विनियमित बाजारों में पहले से ही स्वीकृत उपकरणों पर घरेलू पुनःपरीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताएँ लागू होनी चाहिए? क्या भारतीय निरीक्षकों को सचमुच हर विदेशी रासायनिक संयंत्र का दौरा करने की आवश्यकता है?
ये संप्रभुता के मामले नहीं हैं, बल्कि एक पुराने नियामक दर्शन के अवशेष हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों व्यवसायों का गला घोंट रहे हैं। व्यापार वार्ताओं में ऐसे प्रतिबंधों को हटाने को ‘रियायतें’ मानकर, भारत वह कर सकता है जो उसे दशकों पहले कर लेना चाहिए था: आर्थिक उदारीकरण का वादा पूरा करना। इस दृष्टिकोण की खूबसूरती इसकी राजनीतिक स्वीकार्यता में निहित है – जिन सुधारों को ‘विदेश-समर्थक’ नीतियों के रूप में घरेलू प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, वे वार्ता में जीत के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार्य हो जाते हैं।
मौजूदा व्यापारिक तनाव भारत के क्षेत्रीय संबंधों की संभावनाओं को उजागर करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और श्रीलंका, सभी ने शुरुआती टैरिफ आकलन में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है, जहाँ उन्हें क्रमशः 10%, 20% और 20% की दरें मिली हैं। इसे एक झटके के रूप में देखने के बजाय, भारत को इसे इन पड़ोसियों के साथ आर्थिक एकीकरण को गहरा करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए।
संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध विशेष ध्यान देने योग्य हैं। भारतीय कंपनियाँ संयुक्त अरब अमीरात को अपने संचालन के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में देख रही हैं, जहाँ उन्हें बेहतर बुनियादी ढाँचा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं तक बेहतर पहुँच और व्यापार-अनुकूल वातावरण मिलता है। रणनीतिक रूप से, संयुक्त अरब अमीरात अफ्रीकी बाज़ारों के लिए एक प्राकृतिक सेतु प्रदान करता है जहाँ भारतीय कंपनियाँ अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के अमेरिकी प्रयासों में सहयोग कर सकती हैं।
यह दृष्टिकोण शानदार रणनीतिक लाभ प्रदान करता है: भारत अपने आर्थिक प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता है, क्षेत्रीय साझेदारों को समर्थन देता है, तथा बीजिंग से सीधे टकराव लिए बिना या रूस और चीन के साथ पारंपरिक साझेदारियों को त्यागे बिना चीनी विस्तार को रोकने में मदद करता है।
भारत के लिए यह श्रेय की बात है कि सरकार ने अमेरिकी वार्ताकारों की असामान्य रूप से सीधी भाषा का जवाब देने में उल्लेखनीय संयम दिखाया है। भारत की संयमित प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि देश एक आत्मविश्वासी मध्यम शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है जो बिना अपना संयम खोए कठिन साझेदारों से भी बातचीत करने में सक्षम है।
भारत की ताकत अपने हितों को आगे बढ़ाते हुए भू-राजनीतिक परिदृश्य में संबंध बनाए रखने की उसकी क्षमता में निहित है। चीन और रूस, अपने बयानबाज़ी समर्थन के बावजूद, अमेरिकी बाज़ारों के लिए सीमित आर्थिक विकल्प प्रदान करते हैं। भारत के साथ चीन का भारी व्यापार घाटा और सार्थक बाज़ार पहुँच प्रदान करने में उसकी अनिच्छा, साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था कैलिफ़ोर्निया या टेक्सास से भी छोटी होने के कारण, यह स्पष्ट करते हैं कि ये संबंध, महत्वपूर्ण होते हुए भी, अमेरिकी आर्थिक साझेदारी का विकल्प नहीं बन सकते।
इन परिस्थितियों में कुछ सुधार की आवश्यकता अवश्य है। अमेरिका के साथ अपने कथित विशेष संबंधों पर भरोसा करने की भारत की कोशिश ने मूल रूप से वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की प्रकृति को गलत समझा है। रूसी तेल खरीद के कारण लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ, हालाँकि राजनीति से प्रेरित था, यह दर्शाता है कि भारत ने बाज़ार पहुँच पर प्रतिबंधों के प्रति शत्रुता को कितनी बुरी तरह से गलत समझा।
वर्तमान व्यापार टकराव अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक असाधारण स्पष्टता का क्षण प्रस्तुत करता है—भारत के लिए रक्षात्मक रुख त्यागकर उस आत्मविश्वासपूर्ण व्यावहारिकता को अपनाने का अवसर जिसने पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की इतनी अच्छी तरह से सेवा की है। जिस प्रकार जापान और चीन ने अमेरिकी बाज़ारों और घरेलू निवेश के लिए ‘हाँ’ कहते हुए अमेरिकी माँगों को ‘ना’ कहने के तरीके खोज निकाले, उसी प्रकार भारत अपने विकास को गति देते हुए अपनी गरिमा बनाए रख सकता है।
प्रश्न यह नहीं है कि क्या भारत इस अवसर के लिए ‘हां’ कहने के लिए पर्याप्त आश्वस्त है, बल्कि यह है कि क्या वह इतना बुद्धिमान है कि यह समझ सके कि संकट का यह स्पष्ट क्षण वास्तव में वह अवसर प्रस्तुत करता है, जिसे दशकों की आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता ने प्राप्त नहीं होने दिया है: भारत का आर्थिक रूपांतरण एक वास्तविक उदारीकृत, वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में पूर्ण होना, जो पूर्व और पश्चिम, विकसित और विकासशील विश्वों के बीच सेतु का काम करे।
इस दृष्टि से, अमेरिका से प्रतिबंधित अमूल ताजा भी जीत जैसा स्वाद लेगा। द टेलीग्राफ से साभार

रसेल स्टैमेट्स नई दिल्ली स्थित लॉ फर्म, सर्कल ऑफ काउंसल्स के भागीदार हैं और भारतीय और विदेशी कंपनियों और निवेशकों को व्यावसायिक मामलों, नियामक मुद्दों और जटिल विवादों पर सलाह देते हैं।