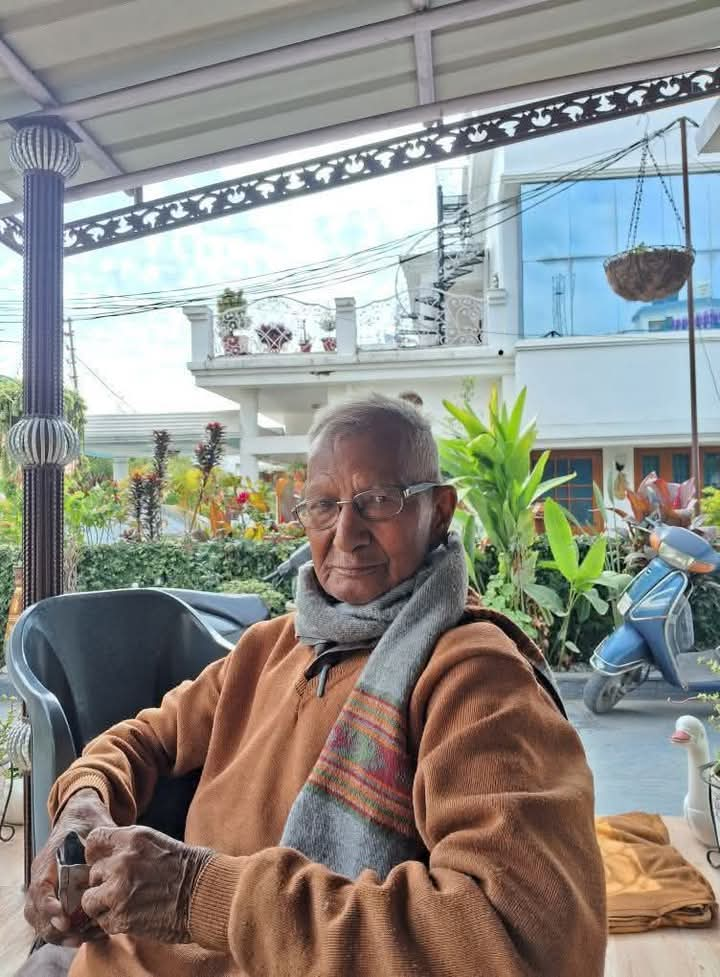हिमाचल में प्रकृति बीमार
कुलभूषण उपमन्यु
हिमाचल को लेकर माननीय न्यायाधीश पार्दिवाला की टिपण्णी सामयिक और सटीक दिखाई पड़ रही है. इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर समय रहते हिमाचल में प्राकृतिक विध्वंस के कारणों को गंभीरता से लिए बिना यहाँ जारी विकास गतिविधियों को यूं ही जारी रखा गया तो प्रदेश के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा.
हिमाचल प्रदेश भूगर्भीय दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है. यह भूकंपीय दृष्टि से जोन 4 और 5 में पड़ता है. भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के फल स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है. अभी तक भी भारतीय प्लेट उत्तर की ओर लगभग एक सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है. जिससे अभी तक भी हिमालय निर्माण की स्थिति में ही है. इसकी ढलाने और चट्टानें अभी तक कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजर कर पक्का होने की स्थितियों का इंतजार कर रही हैं. इन भूगर्भीय प्रक्रियाओं को पूर्णता प्राप्त करने में हजारों से लाखों साल लग जाते हैं.
प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र तेज़ ढलानों वाले हैं जिससे भूस्खलन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाति हैं. ज्यादातर पर्वतीय संधियों में बनी घाटियाँ जहां ज्यादातर लोग बसे हैं, वे हजारों सालों में आये भूस्खलनों के मलबे के तलछट से बने हुए हैं. जिसमें रेत पत्थर और मिट्टी का मिश्रण जमा हुआ है. जिसकी आपस में पकड़ ढीली होती है. कुछ चट्टानी क्षेत्र हैं जिनमें स्लेट वाली चट्टाने हैं जिनमें से बहुत सी अर्धनिर्मित अवस्था में हैं, इसलिए भुरभुरी हैं. शेष जो थोड़ी पक्की दिखाई देती हैं वे भी गर्मी सर्दी के तापमान में भारी बदलाव के कारण अपरदन का शिकार हो जाति हैं और फ्रैक्चर की स्थिति में आ जाति हैं. थोड़ी सी भी छेड़ छाड़ होने पर भूस्खलन का शिकार हो जाति हैं. भरमौर या किन्नौर में यह स्थिति विशेषकर देखने को मिलती है.
अत: हमारे पास एक ही मार्ग शेष है कि हम हिमालय की नाज़ुक प्रकृति को समझ कर उसके अनुरूप अपनी विकासात्मक गतिविधियों को दिशा दें और अनावश्यक छेड़ छाड़ से बचें. चिपको आन्दोलन के दौर से ही हिमालय के लिए विकास की अलग नीति की बात सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से उठाई जा रही है.
योजना आयोग के समय 1990 में डा. एस.जेड.कासिम की अध्यक्षता में इस आशय का एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था. जिसकी रिपोर्ट 1992 में आ गई थी जिसमें विशेषज्ञों की राय के साथ चिपको आन्दोलन के नेताओं के अनुभवों को भी शामिल किया गया था. हिमाचल के सन्दर्भ में तत्कालीन मुख्य मंत्री शांता कुमार का भी वक्तव्य उसमें शामिल है. वह एक आधार दस्तावेज़ हो सकता है. उसमें समय अनुसार आये नए अनुभवों और वैज्ञानिक समझ के चलते जरूरी बदलाव किये जा सकते हैं.
हालांकि नीति आयोग में भी हिमालयन रीजनल काउंसिल का गठन किया गया था किन्तु उसकी कोई गतिविधि नजर नहीं आई. इस वर्ष माननीय अध्यक्ष विधान सभा हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा में आपदा पर विशेष चर्चा करवा कर एक अच्छी पहल की है. इस तरह की चर्चाओं को और ज्यादा गंभीरता से किया जाना चाहिए ताकि हम आपदा राहत से आगे निकल कर आपदा आने के कारणों के समाधान तक पंहुच सकें.
इस वर्ष लगातार तीसरा साल है जबकि एक के बाद एक बड़ी आपदा आई है. अगर हर साल यही हाल रहा तो सर्वोच्च न्यायालय की आशंका सच होते देर नहीं लगेगी. जिला मंडी के थुनाग, जंजैहली क्षेत्र के बाद अब मणिमहेश यात्रा जिला चंबा में भयानक तबाही हुई है. हजारों लोग यहाँ वहां फंसे हैं. यातायात के साथ संचार के साधन भी अवरुद्ध हो गए हैं. प्रशासन भरपूर प्रयास कर रहा है. किन्तु अप्रत्याशित स्तर पर आपदा आने पर हर कोई हतप्रभ हो जाता है. सामान्य तैयारी तो प्रशासन ने की होती है किन्तु ऐसी अप्रत्याशित आपदा में वह ना काफी साबित होती है.
ऐसे बड़े आयोजनों में अच्छा हो यदि ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सीमित संख्या को ही यात्रा पर एक समय जाने दिया जाए. भले ही यात्रा की अवधि बढ़ा दी जाए. मौके पर व्यवस्था में लगे अधिकारीयों को सेटेलाइट फ़ोन उपलब्ध होने चाहिए ताकि संचार व्यवस्था के असफल हो जाने के समय भी उससे व्यवस्था संबंधी कार्यों में बाधा न आये.
चंबा-भरमौर मार्ग के साथ कितनी ही छोटी बड़ी जलविद्युत उत्पादन परियोजनाएं बनी हैं. उनके क्रियान्वयन के लिए चौड़ी सड़कें बनाई गईं. लोगों के दिमाग में भी यह आशा थी कि अच्छी सडकें इस बहाने बन जाएंगीं. किन्तु हुआ उल्टा ही है. छोटी सड़क तंग भले थी किन्तु इतने भूस्खलन उसमें नहीं आते थे. परियोजनाओं से इतना पैसा सरकार या कंपनियों के खाते में जा रहा है तो इन सड़कों को टिकाऊ बनाने का कार्य क्यों नहीं किया जाता?
यह बात अब व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी है कि जलविद्युत परियोजनाएं, चौड़ी सड़कें, और अवैज्ञानिक सड़क निर्माण तकनीक, बहुमंजिला इमारतें, बाढ़ के दायरे के अंदर निवास निर्माण ही मुख्यत: आपदाओं का कारण हैं. अत: हमें हिमालय में विकास के टिकाऊ वैकल्पिक तरीकों को खोजना और अपनाना होगा.
किन्तु इसके लिए यह जरूरी है कि हम नम्रता पूर्वक यह स्वीकार करें कि गलत विकास मॉडल के चलते ही यह तबाहियां हो रही हैं. हिमालय के लिए अलग वैकल्पिक विकास नीति बना कर उसका प्रयोग हिमाचल से ही शुरू होना चाहिए. हमारी सरकारों और सामाजिक संगठनों की सक्रियता इस दिशा में जारी रहनी चाहिए जब तक कि टिकाऊ विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता.
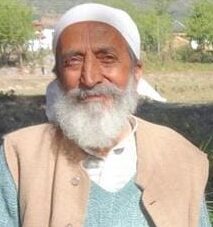
लेखकः कुलभूषण उपमन्यु