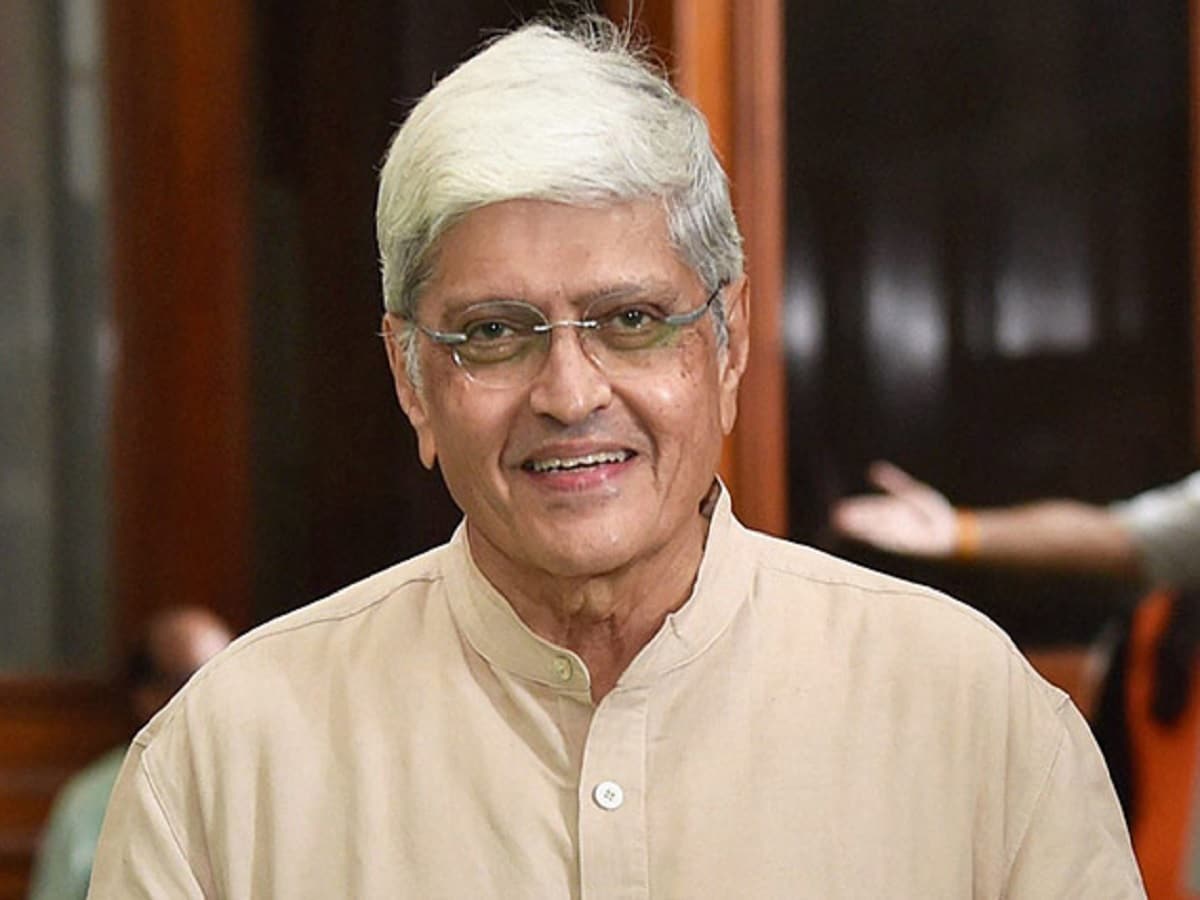भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक टाइम बम जैसा
नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, “किसी बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित न रखें, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।” भारत की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में, यह उद्धरण आज विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत की शिक्षा प्रणाली पुरानी हो चुकी है। हम छात्रों को ऐसी नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं जो या तो तेज़ी से लुप्त हो रही हैं या विकसित हो रही हैं।
इस बीच, काम का भविष्य उभरती हुई तकनीकों द्वारा आकार ले रहा है, जिसका नेतृत्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कर रहा है, जो इन सभी में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी है। एआई हमारे काम करने और सोचने के तरीके को नया रूप दे रहा है, और हमारे शोध से पता चलता है कि दुनिया भर में 70% तक मौजूदा नौकरियाँ प्रभावित होंगी, और कई मौजूदा नौकरियों में 30% तक कार्य पूरी तरह से स्वचालित हो जाएँगे।
इस समय एआई के विकास और कार्यान्वयन से जुड़ी ढेरों नई नौकरियाँ पैदा हो रही हैं। एआई के ज़रिए यह तकनीकी बदलाव दुनिया और रोज़गार बाज़ार को पहले ही बदल रहा है, जबकि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम अद्यतन चक्र तीन साल का होता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धिशील है, और अगर हम छात्रों को अप-स्किल, क्रॉस-स्किल और री-स्किल नहीं कराते हैं, तो कई छात्र पीछे छूट जाएँगे।
पी-स्किल, क्रॉस-स्किल और री-स्किल। भारत के ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ को लंबे समय से देश के भविष्य के विकास का एक प्रमुख चालक माना जाता रहा है। 35 वर्ष से कम आयु के 80 करोड़ से अधिक लोगों के साथ, यह देश दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक होने का दावा करता है।
हालाँकि, यह जनसांख्यिकीय ‘संपत्ति’ शिक्षा और वास्तविक दुनिया के कौशल, डिग्रियों और रोज़गार योग्यता के बीच बढ़ते अंतर के कारण ‘दायित्व’ में बदलने का ख़तरा लगातार मंडरा रहा है। अगर इस अंतर को दूर नहीं किया गया, तो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक जनसांख्यिकीय टाइम बम में बदल सकता है – जो एक बड़े पैमाने पर विरोधाभास है।
कड़वी सच्चाई यह है कि भारत हर साल लाखों स्नातक तैयार करता है, लेकिन इनमें से कई स्नातक अभी भी अल्प-रोज़गार में हैं और तेज़ी से बेरोज़गार होते जा रहे हैं। आम धारणा के बावजूद, यह समस्या सिर्फ़ सामाजिक विज्ञान या गैर-STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के छात्रों की ही नहीं है।
पिछले एक दशक के आँकड़े बताते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों से निकले 40%-50% इंजीनियरिंग स्नातकों को नौकरी नहीं मिली है, जो शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की ज़रूरतों के बीच चिंताजनक अंतर को उजागर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा कॉलेज या विश्वविद्यालय जा रहे हैं, फिर भी नियोक्ता सही कौशल वाली प्रतिभाएँ ढूँढ़ने में बढ़ती कठिनाई की रिपोर्ट कर रहे हैं। देर से ही सही, शिक्षक इस समस्या को स्वीकार कर रहे हैं, और आज 61% उच्च शिक्षा क्षेत्र के नेता इस बात से सहमत हैं कि पाठ्यक्रम तेज़ी से बदलती रोज़गार बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप नहीं हैं।
बेमेल संबंध हाई स्कूल में शुरू होता है
जैसे-जैसे एआई क्रांति तेज़ हो रही है, भारत कौशल संकट का सामना कर रहा है। मैकिन्से के अनुसार, 2030 तक हर 10 में से लगभग सात भारतीय नौकरियाँ स्वचालन के कारण खतरे में हैं। इसका मतलब है कि अगले पाँच वर्षों में ही देश में एक बड़ा और अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल सकता है। बेशक, यह पूरी तरह से बुरी खबर नहीं है।
विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि एआई और अन्य नई तकनीकें 2030 तक 17 करोड़ नए रोज़गार पैदा करेंगी। समस्या यह है कि इसी अवधि में, नए सृजित रोज़गारों की इस संख्या में से आधे से ज़्यादा (9.2 करोड़) ख़त्म हो जाएँगे। इसलिए, कौशल विकास को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा।
चुनौती यह है कि भारतीय युवा कार्यबल में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या पुराने या अप्रासंगिक कौशल के साथ ऐसा कर रही है। यह विसंगति हाई स्कूल से ही शुरू हो जाती है, जहाँ छात्र मौजूदा करियर के विविध विकल्पों से लगभग अनजान होते हैं।
2022 के माइंडलर करियर जागरूकता सर्वेक्षण से पता चला है कि कक्षा 8 से 12 तक के 93% भारतीय छात्र केवल सात करियर विकल्पों के बारे में जानते हैं, जिनमें से अधिकांश पारंपरिक भूमिकाएँ हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या शिक्षक। इसके विपरीत, आधुनिक अर्थव्यवस्था 20,000 से ज़्यादा करियर विकल्प प्रदान करती है।
हैरानी की बात है कि केवल 7% छात्र ही अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान औपचारिक करियर मार्गदर्शन प्राप्त करने की बात कहते हैं। जागरूकता की इस कमी के कारण हमारे लाखों सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली छात्र ऐसी डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं जो उनकी योग्यता या बाज़ार की ज़रूरतों से मेल नहीं खातीं। हमारी बातों पर यकीन न करें।
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 65% से ज़्यादा हाई स्कूल स्नातक ऐसी डिग्रियाँ हासिल करते हैं जो उनकी रुचियों या क्षमताओं के अनुरूप नहीं होतीं। इस चिंताजनक वास्तविकता का अर्थ है कि छात्र अपनी डिग्रियों के बाद तेज़ी से बदलते रोज़गार बाज़ार के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते, जिससे भारत का बेरोज़गारी संकट और भी गहरा हो जाता है।
डिजिटल उपकरण, लेकिन एनालॉग मानसिकता
हालाँकि भारत में अब ज़्यादातर छात्रों के पास कुछ न कुछ तकनीक उपलब्ध है क्योंकि स्मार्टफ़ोन काफ़ी सस्ते हो गए हैं, और सरकार ने कंप्यूटर और एआई लैब भी शुरू करने की कोशिश की है, फिर भी ज़्यादातर स्कूल अभी भी पारंपरिक, परीक्षा-केंद्रित पाठ्यक्रम ही अपनाते हैं। करियर की खोज या नौकरी के लिए तैयार कौशल के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
परिणामस्वरूप, छात्र डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित व्यावहारिक अनुभव का अभाव रखते हैं। दरअसल, मर्सर-मेटल द्वारा तैयार ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स 2025 में पाया गया कि केवल 43% भारतीय स्नातक ही नौकरी के लिए तैयार माने जाते हैं। इंटर्न और नए स्नातकों के साथ हमारे अनुभव में, यह आंकड़ा, अगर कुछ भी हो, तो समस्या के पैमाने को कम करके आँकता है।
एडटेक प्लेटफ़ॉर्म मुख्य रूप से करियर की खोज या कौशल विकास के बजाय परीक्षा की तैयारी और रटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोर्सेरा, उडेमी और इसी तरह के अन्य प्लेटफ़ॉर्म ने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है, लेकिन इनसे प्राप्त प्रमाणपत्र तेज़ी से वस्तुगत होते जा रहे हैं। स्कूली पाठ्यक्रम बदलते रोज़गार बाज़ार से कटे हुए हैं, जिससे छात्र आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पाते। केवल कुछ ही राज्य बोर्डों और केंद्रीय निकायों ने करियर की तैयारी के लिए रूपरेखाएँ शुरू की हैं, और उससे भी कम ने उभरते करियर मार्गों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है।
भारत सरकार ने, अपने श्रेय के लिए, कई पहलों की शुरुआत की है जिनका उद्देश्य कौशल अंतर को पाटना है, सबसे प्रमुख है कौशल भारत मिशन, जिसका लक्ष्य 2022 तक 400 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। बड़े पैमाने पर वित्त पोषण के बावजूद, मिशन इस लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया। कई प्रणालीगत मुद्दों ने इस विफलता मंक योगदान दिया है: कौशल भारत मिशन के अलावा, अन्य नीतियों का एक संक्षिप्त सूप भी लॉन्च किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), प्रधानमंत्री युवा योजना (पीएमवाईवाई), आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प), प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना, और कई अन्य शामिल हैं। भारत को एक सुसंगत रणनीति की आवश्यकता है जो शिक्षा और कौशल विकास को उद्योग की मांगों के साथ संरेखित करे।
हमने गहन शोध किया है और इसके लिए एक मंच तैयार किया है। हम इस समाधान को साकार करने के लिए नीति आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) और कौशल मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं। कौशल विकास के लिए एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग आवश्यक होगा।
निर्णायक दशक में, भारत की एक वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और रोज़गार को एक सुसंगत राष्ट्रीय ढाँचे में एकीकृत करने की उसकी क्षमता पर निर्भर है। भारत के युवा या तो एआई-संचालित दुनिया में फलने-फूलने के लिए आवश्यक कौशल से लैस होंगे या पीछे छूट जाएँगे। यह केवल शिक्षा या रोज़गार का संकट नहीं है; यह एक ऐसा संकट है जहाँ हमारा पूरा सामाजिक अनुबंध बिखर सकता है।
1990 में मंडल आयोग के दिनों में छात्रों का सविनय अवज्ञा आंदोलन इस बात का गवाह है कि युवाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कितनी तबाही मचा सकते हैं, जो हिंसा, पुलिस के साथ झड़प, संपत्ति के विनाश और कुछ मामलों में पुलिस की गोलियों से होने वाली मौतों में बदल सकती है। अगर भारत अभी कार्रवाई नहीं करता है, तो इससे अत्यधिक साक्षर, यहाँ तक कि शिक्षित लेकिन बेरोज़गार युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार होने का खतरा है जो एक टाइम बम बन सकती है। विश्व बैंक आर्थिक समीक्षा ने लैंट प्रिचेट के एक लेख में इस विरोधाभास को बड़े पैमाने पर उजागर किया है।
“सारी शिक्षा कहाँ चली गई?” ऐसे संकट के परिणाम भयावह हैं। अच्छी खबर यह है कि यह एक पूरी तरह से हल करने योग्य समस्या है। भारत को अपने युवाओं को कल की नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के करियर के लिए तैयार करना होगा। समय बीत रहा है और यह हम पर निर्भर है कि हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को संपत्ति या दायित्व में बदलें। द हिंदू से साभार
मार्टिन व्हाइटहेड एक व्यवहारिक अर्थशास्त्री और PwC के पूर्व पार्टनर हैं
अमर आनंद सिंह वर्तमान में ऑरोविले इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य निवेश अधिकारी और ऑरो ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के संस्थापक हैं। वे टायबोर्न कैपिटल के प्रबंध निदेशक और संस्थापक टीम के सदस्य थे।
रितु कुलश्रेष्ठ ने लेख के प्रारंभिक चरणों में, विशेष रूप से डेटा सामग्री और प्रारूपण में सहायता की।