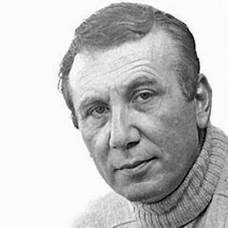भारत के त्रिपिटक में क्या खास बात है?
जयंत सेनगुप्ता
राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रगानों के अलावा, सभी राष्ट्र-राज्यों के लिए कुछ विशेष मुहावरे, प्रतीक चिन्ह, दृश्य संकेत, नारे, रैली के नारे वगैरह बेहद प्रिय होते हैं। भारतीय इतिहास में, तीन ऐसे नारे और दृश्य प्रतीक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं—वंदे मातरम, भारत माता और जय श्री राम। ये दोनों नारे एक जैसे प्राचीन नहीं हैं, और देशभक्तों, सैनिकों, भक्तों, दंगाइयों वगैरह पर आरोप लगाने की इनकी क्षमता और इस्तेमाल समय के साथ घटते-बढ़ते रहे हैं। लेकिन इनमें से एक या एक से ज़्यादा नारे हमारे रोज़मर्रा के संवेदी जगत में हमेशा मौजूद रहते हैं—वे आवाज़ें जो हम सुनते हैं, वे ख़बरें जो हम पढ़ते हैं, वे चिंताएँ जिनसे हम परेशान होते हैं, वे झगड़े जो हम शुरू करते हैं। इस त्रिपिटक में क्या खास बात है?
तीनों में से सबसे पुराना, वंदे मातरम (माँ के लिए एक भजन), शायद ही कभी विवादों से मुक्त रहा हो। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 के दशक में रचित, यह पहली बार 1882 में संन्यासी विद्रोह पर उनके उपन्यास, आनंदमठ, में सार्वजनिक रूप से प्रकट हुआ। रवींद्रनाथ टैगोर (जिन्होंने इसे पहली बार 1896 में गाया था) और अरबिंदो घोष द्वारा उच्च स्थान प्राप्त, और 1890 के दशक से लेकर स्वतंत्रता तक एक प्रेरणादायक वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों द्वारा वंदे मातरम का नारा एक एकजुटता के आह्वान और राष्ट्रवादी उद्देश्य के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा, दोनों का काम करता था।
हालांकि, जैसा कि सब्यसाची भट्टाचार्य की पुस्तक, वंदे मातरम: द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग, दस्तावेज करती है, 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भी, गीत की कथित ‘मूर्तिपूजक’ प्रकृति ने कुछ हलकों में गलतफहमी पैदा की थी। 1930 के दशक के अंत में, भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मानने का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह दुर्गा का आह्वान है और एक ऐसे उपन्यास का हिस्सा है जो मुसलमानों के विरोधी है। इससे हिंदू राष्ट्रवादी नाराज हो गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर, टैगोर ने एक समाधान सुझाया, जिसमें वंदे मातरम के पहले दो छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने की सिफारिश की गई। ये शेष छंदों और मूल उपन्यास में उनके स्थान के संदर्भ से स्वतंत्र थे, लेकिन फिर भी भक्ति और बलिदान के विषयों का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके संशोधित संस्करण को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया, जो ‘धर्मनिरपेक्ष सफ़ाई’ की एक प्रक्रिया थी, जिसने अवसरवादी राजनीतिक विनियोग और तब से इस गीत को राष्ट्रीय या सांप्रदायिक अर्थ देने का रास्ता खोल दिया।
अर्थों का ऐसा हेरफेर भारत माता पर भी लागू होता है, जो भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे स्थायी छवियों में से एक है। हालाँकि इसे एक एकीकृत रूपक माना जाता है, लेकिन इसके दृश्य चित्रण की व्याख्याएँ ध्रुवीकरणकारी हो सकती हैं। हाल के महीनों में, यह केरल में एक अप्रिय विवाद का केंद्र रहा है, जहाँ राज्यपाल ने एक आधिकारिक कार्यक्रम में भगवा ध्वज से सुसज्जित भारत माता का चित्र स्थापित किया, जिसके बाद राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कई नेताओं ने इसका विरोध किया कि एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह का उपयोग एक धर्मनिरपेक्ष ढाँचे में पक्षपातपूर्ण ढंग से शामिल करने के समान है।
1904 में सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित, भारत माता, एक मातृदेवी के रूप में भारत का एक भावपूर्ण और आध्यात्मिक चित्रण थी। हालाँकि, समय के साथ, उनके दृश्य चित्रणों को कई अन्य व्यक्तियों और संगठनों द्वारा पुनः रूपांतरित किया गया, जिसमें भगवा ध्वज, ‘अखंड भारत’ के मानचित्र, हिंदू पौराणिक आडंबरों के साथ-साथ भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ भी शामिल किए गए। सुमति रामास्वामी की पुस्तक, द गॉडेस एंड द नेशन: मैपिंग मदर इंडिया, भारत माता की ऐसी दृश्य व्याख्याओं के कई उदाहरण प्रस्तुत करती है—एक पालन-पोषण करने वाली माता के रूप में, जो अनाज का एक ढेर, एक माला, या एक चरखा जैसी प्रतीकात्मक वस्तुएँ धारण किए हुए हैं; एक देवी-आकृति के रूप में, जिसका शरीर भारत के भौगोलिक आकार के अनुरूप स्पष्ट रूप से “मानचित्र-चित्रित” है; या एक योद्धा देवी के रूप में, जो अक्सर शेरों से घिरी होती हैं और तलवार या त्रिशूल से लैस होती हैं, जो मोटे तौर पर दुर्गा के समान होती हैं। सच कहूँ तो, भारत जैसे देश में, कलात्मक रचनात्मकता और कल्पना की इतनी विविधता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। टैगोर और द्विजेन्द्रलाल राय सहित अन्य ने राष्ट्र को माता के रूप में देखने की प्रबल कल्पना की, जो शक्ति के प्रतीक से परिपूर्ण थी और अवनीन्द्रनाथ की तपस्वी प्रतिमा से बिल्कुल भिन्न थी।
संक्षेप में, कलाकारों, नागरिकों, राजनेताओं और अन्य लोगों द्वारा भारत माता की शैलीगत, शक्ति-प्रधान छवियों को पसंद करने में कुछ भी गलत नहीं है, जब तक कि उनका उपयोग प्रतीकात्मक इशारों के रूप में नहीं किया जाता है जो वैचारिक संकेत के सूक्ष्म रूपों के रूप में कार्य करते प्रतीत होते हैं। यहीं पर केरल में समस्या है – एक संवैधानिक कार्यालय में धार्मिक राष्ट्रवाद के एक ‘गैर-आधिकारिक’ प्रतीक को कथित रूप से सम्मिलित करना, जो पारंपरिक रूप से गैर-राजनीतिक और औपचारिक है। चूँकि भारत माता अशोकन सिंह स्तंभ जैसा कोई मान्यता प्राप्त प्रतीक नहीं है, इसलिए उनका अति विशिष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व सरकारी कार्यों में एक समस्याजनक तत्व बन जाता है। इस प्रकार, भारत माता को लेकर केरल की लड़ाई में दांव विरोध प्रदर्शन की रसद से कहीं अधिक गहरे हैं। वास्तव में, इस प्रतीक को इस बात की कसौटी में बदलकर कि भारत सार्वजनिक संस्कृति में देशभक्ति और धर्मनिरपेक्षता को कैसे परिभाषित करता है, वे भारत के संघीय, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के मर्म को छूते हैं।
अब इस त्रिपदी के अंतिम भाग, जय श्री राम की बात करते हैं, जिसकी जड़ें भक्ति परंपराओं में हैं, खासकर उन परंपराओं में जो राम को विष्णु के अवतार और धर्म के अवतार के रूप में पूजती हैं। भक्ति समुदायों में, खासकर तुलसीदास से प्रभावित समुदायों में, राम का नाम जपना एक आध्यात्मिक अभ्यास था जो नैतिक जीवन पर ज़ोर देता था। सीता-राम, राम राम, जय रामजी की, और जय सिया राम जैसे सामान्य अभिवादन पारंपरिक रूप से विनम्रता और भक्ति का प्रतीक रहे हैं।
लेकिन अधिक मुखर जय श्री राम का प्रयोग 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक दैनिक बोलचाल में कम ही किया जाता था। एक भक्ति मंत्र से लेकर आस्था, राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति के मध्य में अपनी वर्तमान स्थिति तक के विकास में, रामानंद सागर द्वारा रामायण का टेलीविजन रूपांतरण (1987-88) एक प्रमुख उत्प्रेरक था, जिसने धार्मिक पौराणिक कथाओं को लोकप्रिय संस्कृति में बदल दिया। उसके बाद के दशकों में, जय श्री राम राजनीतिक लामबंदी का एक शक्तिशाली उपकरण और एक पौराणिक-राष्ट्रवादी आख्यान का केंद्र बिंदु बन गया है, जो विशेष रूप से हिंदुत्व विचारधारा के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान यह एक राजनीतिक युद्धघोष बन गया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान भीड़ द्वारा लगाए गए नारों में यह एक था, हाल के वर्षों में इसका सार्वजनिक और प्रदर्शनात्मक उपयोग प्रार्थना के बजाय दावे से जुड़ा हुआ है, उदाहरण के लिए, भीड़ हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के दौरान जबरदस्ती जप करना, विशेष रूप से 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान। स्वयंभू गौरक्षकों के लिए मुस्लिम मवेशी परिवहन करने वालों को हिंसक, यहां तक कि जानलेवा हमला करते हुए यह जप करने के लिए मजबूर करना भी काफी सामान्य हो गया है।
इस नारे का इस्तेमाल समुदायों को भड़काने या ध्रुवीकरण करने के लिए, खासकर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में, हाल के वर्षों में बंगाल में भाजपा द्वारा सावधानीपूर्वक आयोजित रामनवमी जुलूसों में भी देखा गया है। अपनी ध्रुवीकरण शक्ति की कहानी में एक रणनीतिक मोड़ देते हुए, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी 2025 में राज्य में रामनवमी समारोहों के दौरान इस नारे का एक पुराना रूप — हल्का जय सिया राम — लगाया, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव के एक सावधानीपूर्वक गढ़े गए राजनीतिक संदेश के साथ भक्ति का मिश्रण करके भाजपा से धार्मिक स्थान वापस लेने की कोशिश की गई। स्पष्ट रूप से, लोकतांत्रिक भारत में राजनीतिक गणनाएँ, विशेष रूप से राष्ट्र की ‘आत्मा’ पर दावा करने वाले प्रतिस्पर्धी प्रतीकों को लेकर, बहिष्कार, ध्रुवीकरण, पुनर्ग्रहण, विनियोग और पुनर्विनियोग की पेचीदा और अक्सर विरोधाभासी गतिशीलता पैदा करती हैं।
जैसे-जैसे हमारा 79वाँ स्वतंत्रता दिवस नज़दीक आ रहा है, यह याद रखना ज़रूरी है कि भारतीय राष्ट्र, अपने विचारों और कल्पनाओं की विशालता में, बहुसंख्यकवादी ताकतों द्वारा राष्ट्र की बहुलवादी कल्पनाओं पर थोपी गई कट्टरपंथी और संकीर्णतावादी विकृतियों से कहीं अधिक महान है। संविधान का अनुच्छेद 1 देश को ‘इंडिया’ और ‘भारत’ के रूप में परिभाषित करता है – एक द्वैत और एक समझौता जो 1946-50 के दौरान संविधान सभा में भारत के परस्पर विरोधी विचारों पर हुई बहसों से उत्पन्न हुआ था। लेकिन भारत, भारत माता के समान और समरूप नहीं है, जिसका दृश्य प्रतीकात्मकता का एक भयावह इतिहास रहा है। इसलिए संविधान ने हमें जो दिया है, उससे आगे न बढ़ें। और राम और सीता को, जिन्हें हम एक जोड़े के रूप में प्यार करते हैं, अलग-थलग न करें, भले ही सीता को कितने ही कष्ट सहने पड़े हों। हमारे इतिहास के इस मोड़ पर, हमें विवेकशील देशभक्तों की ज़रूरत है, न कि उकसाने वालों और उत्पीड़कों की। फोटो और लेख टेलीग्राफ आनलाइन से साभार
जयंत सेनगुप्ता अलीपुर संग्रहालय के निदेशक हैं।