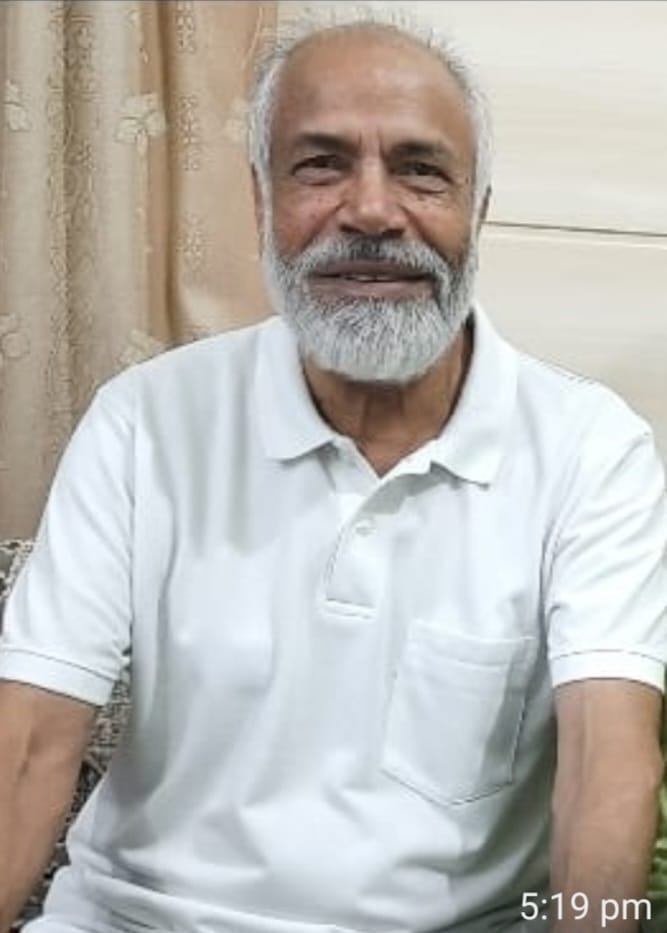जेपी की राजनैतिक भूल का खामियाजा भुगतता देश!
1952 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत के बाद, पंडित नेहरू ने जयप्रकाश नारायण को अपनी सरकार में उपप्रधानमंत्री के पद पर शामिल होने का निमंत्रण दिया । नेहरू चाहते थे कि जेपी उनके “विवेक के रक्षक” के रूप में काम करें और जब भी उन्हें लगे कि नेहरू गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उन्हें सलाह दें । नेहरू ने कांग्रेस पार्टी और जेपी की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विलय का प्रस्ताव भी रखा।
नेहरू को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेपी की असाधारण संगठनात्मक क्षमताओं का एहसास था, और वे उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे । नेहरू ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और महसूस किया कि उनके कैबिनेट सदस्य “डरपोक लोग” थे जो अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं रखते थे । ब्रज कुमार नेहरू के संस्मरण के अनुसार, नेहरू ने जेपी से कहा था कि उन्हें “किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बता सके कि वे कहां गलत जा रहे हैं और सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकल्प सुझा सके।”
जेपी ने नेहरू के सभी प्रस्तावों को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे खुद को गांधी के उत्तराधिकारी और एक संत जैसी हस्ती मानते थे, जो राजनीतिक पद के प्रलोभन से बहुत ऊपर थे । 1952 और 1953 के दौरान नेहरू ने जेपी को कई बार प्रस्ताव दिया, लेकिन जेपी ने लगातार मना कर दिया । नेहरू ने जेपी के इनकार को शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी लेने की अनिच्छा के रूप में देखा, और निराश रहे कि उनका चुना हुआ उत्तराधिकारी राष्ट्र के नेतृत्व की जटिलताओं में शामिल नहीं होगा ।
1970 के दशक में, जब जेपी ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने आरएसएस और जनसंघ को अपने आंदोलन में शामिल कर लिया । उन्होंने सोचा था कि इस गठजोड़ से वे आरएसएस को “असांप्रदायिक” बना सकेंगे और इसे अपने क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बना सकेंगे । जब उनकी आलोचना हुई तो जेपी ने कहा था, “अगर आरएसएस फासीवादी है तो मैं भी फासीवादी हूं।”
जेपी की पहल पर ही 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ । 3 नवंबर 1977 को जेपी ने पटना में आरएसएस के एक विशाल प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए इसे एक क्रांतिकारी संगठन बताया जो समाज को बदल सकता है और जातिवाद को समाप्त कर सकता है । उन्हें विश्वास था कि आरएसएस एक नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है।
लेकिन आरएसएस के अन्य इरादे थे । जनसंघ के नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस ने जेपी से वादा किया था कि वे आरएसएस की सदस्यता छोड़ देंगे, लेकिन यह एक राजनीतिक चाल थी और उन्होंने कभी अपनी सदस्यता नहीं छोड़ी । आरएसएस ने जेपी के आंदोलन का उपयोग केवल राजनीतिक वैधता और सम्मान पाने के लिए किया ।
जेपी अपने जीवन के अंतिम दिनों में गहरे दुख और पीड़ा में थे जब उन्होंने देखा कि आरएसएस समर्थक उन्हें अपना पितामह बताने लगे थे । वे आरएसएस की मोरारजी देसाई सरकार को अस्थिर करने की साजिश से पूरी तरह अवगत थे, जिसके कारण अंततः सरकार का पतन हो गया । जेपी के कई सहयोगी अब स्वीकार करते हैं कि जेपी का आंदोलन एक भूल थी और इसने आरएसएस के उदय का मार्ग प्रशस्त किया ।
आज के भारत में आरएसएस और बीजेपी का जो प्रभुत्व है, उसकी नींव काफी हद तक जेपी के उस निर्णय में छिपी है जब उन्होंने आरएसएस को राजनीतिक मान्यता प्रदान की । यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था अगर जेपी ने नेहरू का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता और शासन की जिम्मेदारी उठाई होती, तो शायद देश की राजनीतिक दिशा कुछ और होती। नेहरू रिवाइव्स फेसबुक वॉल से साभार