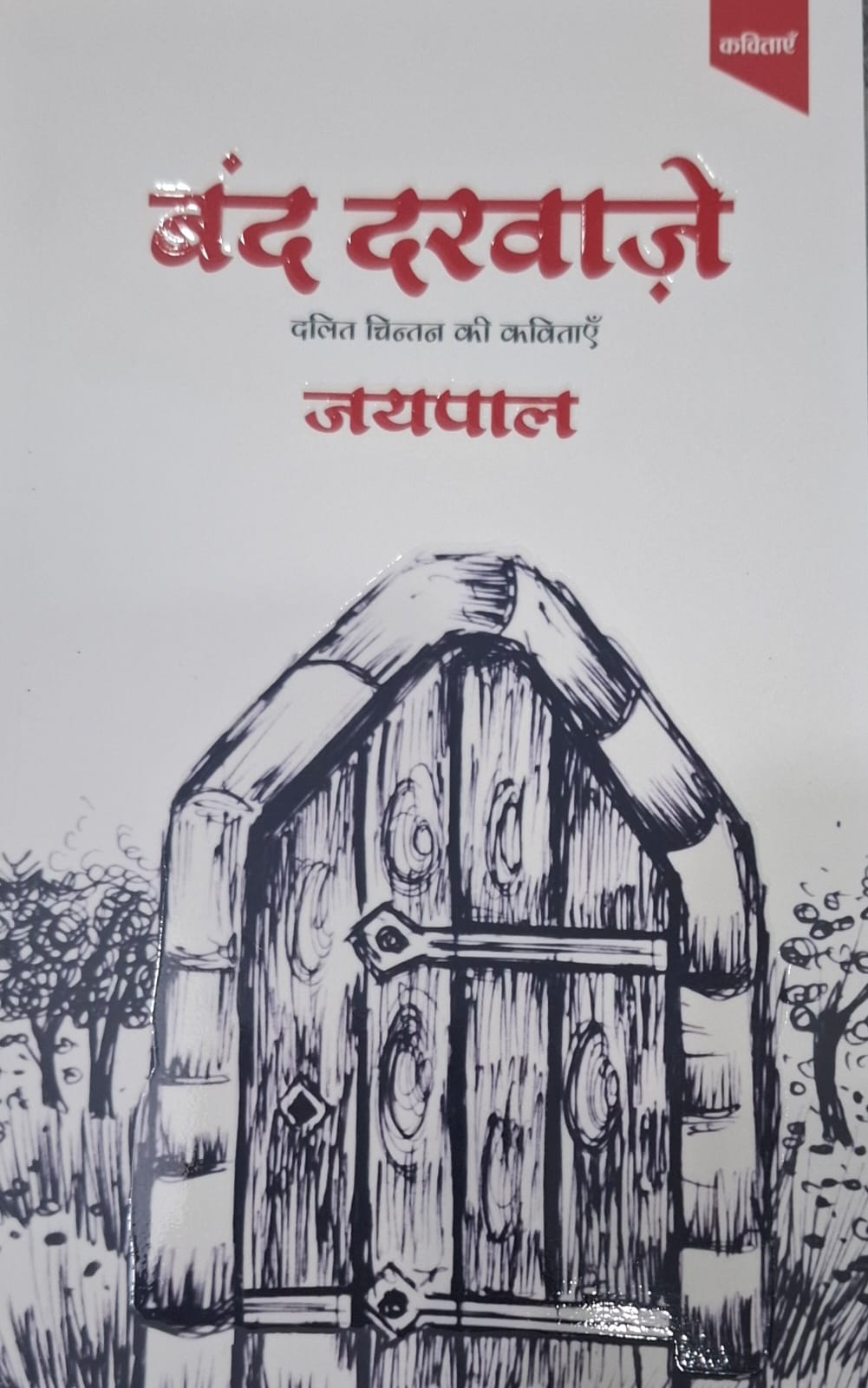केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का सांस्कृतिक कांग्रेस का उद्घाटन भाषण
सांस्कृतिक संस्थाओं की स्वायत्तता को योजनाबद्ध ढंग से कमजोर किया जा रहा
केरल के मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन ने दिनांक 20 से 22 दिसंबर 2025 को केरल में आयोजित सांस्कृतिक कांग्रेस का उद्घाटन किया उनके उद्घाटन भाषण का अविकल हिंदी अनुवाद (पूर्ण पाठ) प्रस्तुत है:-
सम्मानित आयोजकगण, आदरणीय लेखक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और प्रिय साथियो,
जैसा कि आप जानते हैं, एक सांस्कृतिक कांग्रेस हमारे लिए कुछ नया है। हम विज्ञान कांग्रेस, इतिहास कांग्रेस और इसी तरह के अन्य मंचों से परिचित रहे हैं, लेकिन संस्कृति के क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है। किंतु आज की भारतीय परिस्थितियाँ हमें ऐसी कांग्रेस आयोजित करने के लिए विवश कर रही हैं। साम्प्रदायिक ताकतें हमारी संस्कृति के उस धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को तोड़ने का सक्रिय प्रयास कर रही हैं, जिसने विभिन्न जीवन-पद्धतियों को मानने वाले लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह- अस्तित्व सुनिश्चित किया है।
दाँव पर हमारी सामाजिक जीवन की समावेशिता लगी हुई है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह स्थिति राष्ट्र और समाज की एकता के लिए अत्यंत घातक है। इसी पृष्ठभूमि में इस कांग्रेस का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह अत्यंत संतोषजनक है कि आयोजकों ने इस ऐतिहासिक आवश्यकता को पहचाना और केरल सरकार के पूर्ण समर्थन के साथ विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं और अकादमियों के संयुक्त तत्वावधान में इतने बड़े सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया।
मुझे आशा है कि यह कांग्रेस देशभर में स्पष्ट संदेश देगी कि भारत के लोग साम्प्रदायिक आधार पर राष्ट्र को बाँटने के हर प्रयास का दृढ़ता से प्रतिरोध करेंगे। केरल में इस आयोजन का विशेष महत्व है— एक ऐसा राज्य जिसकी धर्मनिरपेक्ष परंपराएँ समृद्ध हैं और जहाँ साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लंबे समय से निरंतर संघर्ष होते रहे हैं।
हम आज देश के जीवन के एक निर्णायक मोड़ पर एकत्र हुए हैं। भारत आज एक खतरनाक चौराहे पर खड़ा है। संविधान के मूल्यों को नकारने वाली शक्तियाँ लगातार मजबूत होती जा रही हैं। वर्ष 2025, जो आरएसएस की शताब्दी का वर्ष है, आत्ममंथन का अवसर बनने के बजाय एक विभाजनकारी को राजनीतिक परियोजना को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने का माध्यम बनाया जा रहा है। यह परियोजना भारत को एक संकीर्ण, बहिष्करणवादी राष्ट्र के रूप में ढालना चाहती है, जिससे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बुनियाद कमजोर हो रही है।
यह हमला अमूर्त नहीं है; यह ठोस, योजनाबद्ध और सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे कानून नागरिकता को ही धर्म के आधार पर पुनर्परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ जैसे प्रस्ताव संघीय ढांचे को कमजोर कर सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहते हैं। प्रशासनिक कार्रवाइयाँ—जैसे मतदाता सूचियों का मनमाना और बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण—लाखों लोगों के मतदान अधिकारों को खतरे में डाल रही हैं। ज्ञान, संस्कृति और इतिहास की रक्षा करने वाली संस्थाओं को एक खास संदेश वैचारिक एजेंडे के अनुरूप ढाला जा रहा है। जब राज्य स्वयं बहुलतावाद को कमजोर करने, असहमति को दबाने और घृणा को सामान्य बनाने का औजार बन जाए, तब प्रतिरोध विकल्प नहीं, बल्कि कर्तव्य बन जाता है।
ऐसे समय में संस्कृति की भूमिका केंद्रीय हो जाती है। इतिहास हमें स्पष्ट सबक देता है—फासीवादी और तानाशाही शक्तियाँ सबसे पहले सांस्कृतिक क्षेत्र पर हमला करती हैं। मुसोलिनी ने लोकज्ञान पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि उसे उसमें प्रतिरोध की चिंगारी दिखती थी। हिटलर चित्रकला से डरता था और नाज़ियों ने किताबें और कलाकृतियाँ जलाईं, क्योंकि वे जानते थे कि महान कला संकीर्ण विश्वदृष्टि को चुनौती देती है। लेखक, कलाकार, इतिहासकार और तर्कशील चिंतक इसलिए निशाने पर होते हैं क्योंकि संस्कृति आलोचनात्मक सोच, सामूहिक स्मृति और नैतिक साहस को पोषित करती है।
हमने इस भय को हिंसा में बदलते देखा है। नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम.एम. कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे तर्कवादी और बुद्धिजीवियों की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे अंधविश्वास, जाति-व्यवस्था और साम्प्रदायिक राजनीति पर सवाल उठाते थे। दाभोलकर को तर्कशील सोच के प्रचार के लिए मारा गया। पानसरे को संघ परिवार की कथा को चुनौती देने वाली उनकी रचनाओं के कारण निशाना बनाया गया। कलबुर्गी को धार्मिक रूढ़िवाद पर सवाल उठाने के लिए मार दिया गया। गौरी लंकेश को जातिवाद और बहुसंख्यकवाद के खिलाफ निर्भीक आवाज़ बनने के कारण हत्या का शिकार होना पड़ा।
पेरूमल मुरुगन जैसे लेखकों को डर और धमकियों के ज़रिये चुप करा दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें यह घोषणा करनी पड़ी कि वे अब लिखना बंद कर देंगे। स्टैन स्वामी जैसे कार्यकर्ताओं को उनके अंतिम दिनों में भी गरिमा और न्याय से वंचित रखा गया—यह इस बात का कठोर प्रमाण है कि किस तरह राज्य की मशीनरी और गढ़े हुए मामलों का उपयोग असहमति को कुचलने के लिए किया जाता है। ये अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं; ये चेतावनियाँ हैं। ये संकेत देती हैं कि ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ स्वतंत्र सोच को ही अपराध माना जा रहा है।
ऐसा समय आ रहा है जब सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के लिए अस्तित्व की जगह सिकुड़ती जा रही है। कलाकारों को निजी विकल्पों के लिए धमकाया जा रहा है, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाले फिल्मकारों पर हमले हो रहे हैं, और लेखकों को उनके विचारों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। हम क्या देखें, क्या खाएँ, क्या पढ़ें और क्या मानें—इन सब पर हमारा अधिकार लगातार सीमित किया जा रहा है।
साथ ही हम इतिहास और ज्ञान के व्यवस्थित भगवाकरण को भी देख रहे हैं। प्रतिष्ठित धर्मनिरपेक्ष और भौतिकवादी इतिहासकारों को अकादमिक संस्थाओं से हटाया जा रहा है। डी.डी. कोसांबी, इरफान हबीब और के.एन. पनिक्कर जैसे विद्वानों की बौद्धिक परंपरा पर हमला हो रहा है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जैसी संस्थाओं को सलाहकार निकाय भंग कर और एक खास विचारधारा के समर्थकों को नियुक्त कर पुनर्गठित किया जा रहा है। शोध संस्थानों पर वस्तुनिष्ठ, प्रमाण-आधारित अध्ययन छोड़ने का दबाव है। जटिल सामाजिक इतिहास को सरलीकृत साम्प्रदायिक कथाओं में बदला जा रहा है। यह केवल अतीत की बात नहीं है; यह भविष्य की पीढ़ियों की समझ को नियंत्रित करने का प्रयास है।
देश की सांस्कृतिक संस्थाओं की स्वायत्तता को योजनाबद्ध ढंग से कमजोर किया जा रहा है, और हाल की घटनाएँ इस प्रवृत्ति को स्पष्ट कर देती हैं। यह अत्यंत निंदनीय है कि साहित्य अकादमी—जो साहित्यिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाई गई एक स्वायत्त संस्था है—ने कथित रूप से अपने पुरस्कारों की संस्तुतियाँ केंद्र सरकार की मंज़ूरी के लिए भेजी हैं। यह उसके इतिहास में अभूतपूर्व है। बिना नियमित सचिव के काम कर रही संस्था का सत्ताधारी प्रतिष्ठान से अनुमति माँगना स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर सीधा हमला है। यह कोई अलग-थलग चूक नहीं, बल्कि वर्तमान शासन के तहत सांस्कृतिक, शैक्षणिक और बौद्धिक संस्थाओं को राजनीतिक नियंत्रण में लाने के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है।
इसी संदर्भ में लेखकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका निर्णायक हो जाती है। संस्कृति समाज का आभूषण नहीं, उसकी अंतरात्मा है। जब लोकतांत्रिक स्थान सिमटता है, तब संस्कृति को प्रतिरोध का विस्तार करना होता है। ऐसे समय में तटस्थता केवल अन्याय को मजबूत करती है।
केरल का अपना इतिहास बहिष्करण की राजनीति के विरुद्ध एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। केरल की सामाजिक प्रगति उसकी जीवंत सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं से अलग नहीं है। हमारी पठन संस्कृति, पुस्तकालय, साहित्य और रंगमंच गहरे जन आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने जातीय उत्पीड़न, सामंती शोषण और सामाजिक असमानता को चुनौती दी।
केरल श्री नारायण गुरु, अय्यंकाली, अय्यावैकुंड स्वामीकल और चट्टंबी स्वामीकल द्वारा संचालित पुनर्जागरण आंदोलनों की भूमि है। पलियं संघर्ष, कल्लुमाला आंदोलन और मरुमारक्कल संघर्ष जैसी लड़ाइयों ने सामाजिक पदानुक्रम को सीधे चुनौती दी। अरुविपुरम में श्री नारायण गुरु का प्रतिष्ठापन और सहोदरन अय्यप्पन का मिश्रभोजन का आह्वान जाति और साम्प्रदायिक दीवारों पर प्रहार के प्रतीक थे।
केरल में संस्कृति कभी अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं रही। वह गाँवों, कार्यस्थलों और सड़कों तक पहुँची। पंडित करुप्पन की ‘जातिकुम्मी’ (1905) जैसी रचनाओं ने लोकप्रिय लोकभाषा में सामाजिक-धार्मिक प्रभुत्व को चुनौती दी।
प्रगतिशील साहित्य आंदोलन ने निर्णायक मोड़ दिया। 1937 में त्रिशूर और 1944 में शोरानूर सम्मेलनों से “कला मनुष्य के लिए है” का उद्घोष हुआ। ई.एम.एस. नंबूदरीपाद, के. दामोदरन और पी. केसव देव जैसे विचारकों ने इसे वैचारिक स्पष्टता दी। श्रमिकों, किसानों और वंचितों के संघर्ष साहित्य के केंद्र में आए। साहित्य यथार्थ का दर्पण ही नहीं, परिवर्तन का औजार भी बना। थकज़ी शिवशंकर पिल्लै की ‘थोट्टियुडे माकन’ मानवीय गरिमा को केंद्र में रखकर आज भी प्रासंगिक है।
नाट्य और लोक कलाओं ने इस प्रभाव को और व्यापक किया। कथा-प्रसंगम जैसी परंपराएँ जनता तक पहुँचीं। केरल पीपुल्स आर्ट्स क्लब जैसी संस्थाओं ने संस्कृति को जन आंदोलन बनाया। दमन और सेंसरशिप के बावजूद कलाकारों ने सत्ता से सच बोलना नहीं छोड़ा।
कम्युनिस्ट आंदोलन ने इन सांस्कृतिक धाराओं को निरंतरता और दिशा दी। भूमि सुधार, शिक्षा सुधार और श्रम अधिकार केवल नीतियाँ नहीं थे, बल्कि सामाजिक चेतना के सांस्कृतिक पड़ाव थे। ये सुधार गरिमा और सुरक्षा के आधार बने।
लेकिन इस विरासत को स्वाभाविक नहीं मान लिया जा सकता। आज संस्कृति को राजनीति से अलग करने की कोशिश की जा रही है। यह खतरनाक भ्रम है। हर सांस्कृतिक कर्म का राजनीतिक संदर्भ होता है। अन्याय के समय मौन रहना यथास्थिति का समर्थन करना है।
आज हमारा दायित्व स्पष्ट है। हमें धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा बौद्धिक ईमानदारी और नैतिक साहस से करनी होगी। यह केवल संस्कृति की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत की अवधारणा—बहुलता, समानता और संवैधानिक नैतिकता—की लड़ाई है।
इतिहास हर पीढ़ी की परीक्षा लेता है। यह हमारी परीक्षा है।
आइए, स्पष्टता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इसका सामना करें।
धन्यवाद।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के उद्घाटन भाषण का अनुवाद नवाब शिकोह ने किया है।