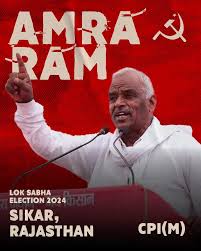भूटान यात्रा वृत्तांत-3
बारिश में बोलते मौन पर क्षण भर
-अरुण माहेश्वरी
भूटान में अंतिम तीन दिन हमने पारो में बिताए। तीनों दिन लगातार बारिश होती रही । पर यह किसी धूसर आसमान की बारिश नहीं थी। बरसता हुआ एक स्वच्छ नीला आसमान था, सफेद झक तैरते हुए बादल और उनके निर्मल और पारदर्शी तल से झांकते पहाड़ । धूसर आसमान तो शहरों की धूल से बनता है । यहाँ की बारिश में धूल नहीं, एक उजली ताजगी थी, जैसे प्रकृति अपनी आत्मा को धोकर चमका रही हो।


हम इसी में छाता ताने इस दुकान, उस दुकान, इस कैफ़े, उस कैफे में भटकते रहे। अभिभूत होकर वहाँ के ऐतिहासिक अजायबघर को देखा, पर पर्यटकों के आकर्षण के कई स्थल छूट भी गए। सबसे अधिक खेद टाइगर नेस्ट, अर्थात् उस ऊंचाई तक न जा पाने का रहा जहां से बर्फीली पहाड़ियों की गहन शृंखलाएं मानो शून्य में प्रवेश करती दिखाई देती है। पर वहाँ पहुँचने के लिए घंटे भर की कठिन चढ़ाई थी, और हम उस चढ़ाई के लिए मन से तैयार भी नहीं थे।
यही वह क्षण था जब हमने महसूस किया कि हर कोई हर चीज़ नहीं देख सकता, पर जो कुछ अनदेखा रह जाता है, वह अस्तित्व से मिट नहीं जाता। ऐलेन बाद्यू की भाषा का इस्तेमाल करें तो इस संसार के सत्य सर्वकालिक ठोस अपवादों (universal concrete exceptions) के रूप में होते हैं । इसीलिए अनदेखा रह जाना भी होने का एक रूप है।
बारिश में नहाती प्रकृति पारो की गलियों को एक नई ताजगी दे रही थी। दुकानें रंगीन, पर सजग थीं । छोटे-छोटे बुद्ध, प्रार्थना चक्र, रेशमी थंका चित्र, और बौद्ध नीति-नैतिकताओं के मिथकीय कला-रूप जिनमें करुणा, जन्म-पुनर्जन्म और शांति के विचार दृश्य के साथ ही वस्तु बन जाते हैं। ये दुकानें सिर्फ व्यापारिक स्थल नहीं लगती, कला और विश्वास के संग्रहालय भी लगती है । हर वस्तु किसी कथानक का प्रतीक, और हर रंग किसी नैतिक उपदेश का रूपक था। और पारंपरिक मिथकीय आकृतियाँ बौद्ध मोनेस्ट्रीज से उपजी अजीबोगरीब रूप-कथाओँ से घिरी विशेष जीवन शैली का प्रदर्शन लगती है । इसे ही कहते हैं जीवन में दर्शन और संस्कृति की सत्तर्क उपस्थिति (Logos) का आख्यानों के जरिए मिथकों (Mythos) में रूपांतरण । तर्क और भाषा का संसार विश्वास, कल्पना और स्वप्निल प्रतीकों में बदल जाता है ।
पता नहीं क्यों, हमें भूटान या शायद बौद्ध संस्कृति के बाजार की ये कलाकृतियाँ जीवन में उस संक्रमण की सजीव मिसाल लगते हैं, जो अभिनवगुप्त की भाषा में भाषा की सद्विकल्पता के परे प्रमाता को दुर्विकल्पता के अँधेरे में डालते हैं, जहां अर्थ गतिशील नहीं, स्थिर और निर्विकल्प हो जाते हैं । सब कुछ कहीं अटक सा गया जान पड़ता है ।
दरअसल, इस चाक्षुष मिथकीयता की अपनी विडंबना है । यह जितनी सुंदर लगती है उतनी ही दुर्बोध भी होती है। यह अनुभव नहीं, उसकी प्रतिकृति रह जाता है। और जब हम इस सारे विषय को आलोचकीय नजर से देखते हैं तो लगता है कि शायद यही ‘सत्तर्कता का अभाव’ भूटान के जीवन में बहुत गहराई तक पसरे मौन को भी एक हद तक परिभाषित करता है । एक ऐसा मौन जो आलोचना से कोसों दूर समर्पण से पैदा होता है ! यहाँ सिर्फ प्रार्थना-ध्वज लहराते हैं, पर कहीं से कोई प्रश्न हवा में नहीं उठता । क्या यही है राजशाही के सामने नत-मस्तक जनतंत्र का मूल मंत्र !
जो भी हो, बरसात से धुली गलियाँ, लकड़ी के घरों की खिड़कियों से झाँकते लाल और पीले प्रार्थना झंडे, खास भुटानी, बल्कि सरकारी पोशाकों (घो और किरा) में चलते फिरते लोग, सब कुछ किसी ध्यानस्थ, पोस्टकार्ड-चित्र की तरह सौम्य, सुंदर और स्थिर लग रहा था।
बहरहाल, हम भूटान के जीवन में गहराई तक पसरे मौन की चर्चा कर रहे थे । कोई भी मौन तो पूरी तरह से रिक्त नहीं होता। उसमें निश्चित तौर पर भीतर, बहुत गहरे में ही सही, कुछ गूंजता जरूर है, अन्यथा भूटान का मौन हमें इस कदर बेहद लुभाता नहीं ! यह सुख और संतोष में निहित स्वातंत्र्य है; आधुनिक जीवन की अतृप्त लालसा से जुड़े उल्लासोद्वेलन (जुएसॉंस) के स्वातंत्र्य के भैरव भाव के बजाय पूर्व-आधुनिक संपन्न जीवन का भरिततनु स्वातंत्रय्-भाव ! जैसे बारिश की हर बूँद स्वच्छ, नीले आसमान से सीधे धरती की गोद में गिरते हुए अपने होने के अर्थ को पा ले रही हो !
भूटान के बाज़ारों में भटकते हुए हमें स्थानीय जीवन को थोड़ा जानने का अवसर मिला। एक बात स्पष्ट थी कि भूटान का समाज शिक्षा और स्वास्थ्य की सार्वजनिक सुविधाओं से संपन्न, शरीर और मस्तिष्क दोनों से एक स्वस्थ समाज है। पढ़-लिख कर यहां के लोग बाहर जाते हैं, काम करते और पैसे कमाते हैं, और फिर लौट आते हैं, अपने देश के मौन की ओर । यह लौटना किसी कर्तव्य के चलते नहीं, स्वच्छंदता और स्वातंत्र्य की स्वात्म-चेतना के चलते होता है।
हमने थिम्पू की सड़कों पर अनेक कराओके (karaoke) बार के साइनबोर्ड देखें । पर उनके अंदर के शोर और उद्दाम भाव को वहां की सड़कों पर कहीं नहीं देखा । वहां खूब शराब पी जाती है, संभवतः ठंडे प्रदेश के कारण भी, पर कहीं सामाजिक जीवन में उसका असंयम नहीं दिखाई दिया। उल्टे थिम्पू की ‘सिम्पली भूटान’ प्रदर्शनी में आगंतुकों का स्वागत ही स्थानीय व्हाइट वाईन से करते पाया ।
इसीलिए बार-बार यही कहने की इच्छा करती है कि भूटान का मौन सिर्फ अनुशासन का नहीं, आत्म-विश्वास का मौन है, जिसमें एक विकसित भाषा खामोशी को अपना लिया करती है ।
दरअसल, मौन और मौन में भी काफी फर्क होता है । कमज़ोर की चुप्पी उसके सुरक्षा का कवच होती है, जबकि मज़बूत की चुप्पी अन्य से स्वतंत्रता का प्रकाश। भूटान का मौन शायद इस दूसरी श्रेणी में आता है । यह अपनी स्वायत्तता से उत्पन्न चुप्पी है, जो अन्य की स्वीकृति की मोहताज नहीं।
इसमें कुछ अंश अगर हमारे कवि विनोद कुमार शुक्ल के आत्म- साक्षात्कार की चुप्पी का है तो एक बड़ा अंश हमारे प्रिय कवि शमशेर बहादुर सिंह के सधे हुए मुखर मौन का भी है । विनोद कुमार शुक्ल जैसे कहने की आवश्यकता से ही मुक्त होकर कहते हैं, विचार के भीतर के मौन को सुनते दिखाई देते हैं, वहीं शमशेर कहने को ज़रूरी मानते अनोखे सौन्दर्य का रचाव करते हुए ज़ुबान खोलते थे । शमशेर का मौन कभी स्थायी नहीं था, वह भीतर के सघन चिंतन की तपिश का परिणाम था । वह प्रतीक्षा का मौन मौक़े पर संगीत की तरह फूटता था ।
उसी तरह भूटान के लोग अपने मौन के भीतर जीते हैं, गाते और नाचते है, अपनी प्रकृति की रक्षा करते हुए खुद की प्रकृति को रचते हैं। सचमुच, मौन केवल न बोलना नहीं, स्वयं को इस तरह साधते रहना है कि जीवन के सत्य के सामने बोलने की कलाबाज़ियों का कोई मूल्य न बचे; बोलने की आवश्यकता ही न रह जाए।
भूटान के प्राकृतिक सौंदर्य, आम जीवन की सरलता और सौम्यता को हमने अपनी इस यात्रा में स्वातंत्र्यपूर्ण मौन के भूगोल में ढलते देखा । ख़ुशियों का देश कहे जा रहे इस क्षेत्र से हम तन और मन, दोनों को तरोताज़ा कर वापस लौटे हैं।
1 नवंबर 2025 अरुण माहेश्वरी के फेसबुक वॉल से साभार

लेखक- अरुण माहेश्वरी