शिक्षा का अधिकार: व्यावहारिक पहलू
डॉ. रामजीलाल
लड़कों और लड़कियों के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत स्कॉटलैंड में 1560 के दशक में हुई, उसके बाद जर्मनी में पफाल्ज़-ज़्वेइब्रुकन में 1592 में और डेनमार्क में 1739 में इसकी शुरुआत हुई। हालाँकि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, लेकिन यह राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं थी, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो गई। प्रशिया 18वीं शताब्दी में अनिवार्य कर-वित्त पोषित शिक्षा शुरू करने वाला पहला जर्मन राज्य बना, जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की।
भारत में, गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च, 1910 को विधान परिषद में “निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा” का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने बाद में संविधान में अनुच्छेद 21(A) जोड़ा, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ और 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। हालाँकि, भारत को सार्वभौमिक शिक्षा लागू करने में 100 वर्ष लग गए।
वैश्विक शैक्षिक रैंकिंग 2024
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अनुसार, 2024 तक, भारत 66% की दर के साथ विश्व साक्षरता में 149वें स्थान पर है। 17 वर्षों में 48 अंकों के सुधार के बावजूद, भारत कई उन्नत देशों से पीछे है। 2025 में प्रकाशित 2024 की वैश्विक शैक्षिक रैंकिंग में, भारत दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्लोवेनिया, जापान, जर्मनी, फ़िनलैंड, नॉर्वे और आयरलैंड से पीछे, विश्व स्तर पर 101वें स्थान पर है। 2022 तक, भारत की समग्र साक्षरता दर 76% हो जाएगी, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.4% और महिला साक्षरता 68.4% होगी। यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में साक्षरता दर 99% या उससे अधिक है।
सरकारी स्कूलों में गिरावट
शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 और 2023-2024 के बीच, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित 10 राज्यों में सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है। इसके विपरीत, बिहार में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि सरकारी स्कूलों की संख्या 89,441 घटकर 2014-2015 के 1,107,101 से 2023-2024 में 1,017,660 रह गई। इसी अवधि के दौरान, निजी स्कूलों की संख्या में 42,944 की वृद्धि हुई, जिससे कुल संख्या 331,108 हो गई।
मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जहाँ सरकारी स्कूलों की संख्या 1,21,849 से घटकर 92,439 रह गई, जो 24.1% की कमी दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या में राष्ट्रीय गिरावट का 60.9% हिस्सा था और निजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि में 44.9% का योगदान था। जिन अन्य राज्यों में सरकारी स्कूलों की संख्या में गिरावट देखी गई, उनमें जम्मू और कश्मीर (21.4%), ओडिशा (17.1%), झारखंड (13.4%), नागालैंड (14.4%), गोवा (12.9%) और उत्तराखंड (8.7%) शामिल हैं। इसके विपरीत, बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या 74,291 से बढ़कर 78,120 हो गई, जो 5% की वृद्धि दर्शाती है।
निजी स्कूलों की अभूतपूर्व वृद्धि: दस राज्य
इसी अवधि के दौरान, सरकारी स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई, जो निजी स्कूलों की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ मेल खाती है। निजी स्कूलों की संख्या में 42,944 की वृद्धि हुई, जिससे कुल संख्या 3,31,108 हो गई। दस राज्यों में निजी स्कूलों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 14.9% से अधिक रही। उदाहरण के लिए, बिहार में निजी स्कूलों की संख्या 3,284 से बढ़कर 9,167 हो गई, जो 179.14% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। ओडिशा में यह संख्या 3,350 से बढ़कर 6,042 हो गई, जो 80.36% की वृद्धि दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या 77,330 से बढ़कर 96,635 हो गई, जो 24.96% की वृद्धि दर्शाती है।
निजी स्कूलों में गिरावट: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मेघालय
इसके विपरीत, मेघालय, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या में गिरावट देखी गई। मेघालय में, निजी स्कूलों की संख्या 2,274 से घटकर 2,152 हो गई, यानी 5.36% की कमी। दिल्ली में, यह संख्या 2,641 से घटकर 2,565 हो गई, यानी 2.88% की गिरावट। इसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश में भी 2,614 से घटकर 2,607 हो गई, यानी 0.27% की कमी।
स्कूल नामांकन में गिरावट
आंकड़े भारत में स्कूल नामांकन में सात वर्षों की चिंताजनक गिरावट दर्शाते हैं। यूडीआईएसई+ 2024-25 रिपोर्ट, जिसमें 14.71 लाख स्कूल शामिल हैं, बताती है कि 2021-2022 शैक्षणिक वर्ष में नामांकन 255.74 मिलियन के शिखर पर पहुँच गया था, लेकिन तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1-5) में नामांकन घटकर 104.38 मिलियन रह गया, जो 2023-24 की संख्या से 3.46 मिलियन और 2021-22 के शिखर से 17.46 मिलियन (14.33%) कम है। उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) और माध्यमिक (कक्षा 9-12) स्तरों में जहाँ न्यूनतम वृद्धि देखी गई, वहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के केंद्रबिंदु, आधारभूत स्तर पर उपस्थिति में गिरावट जारी है।
छात्र नामांकन में क्षेत्रीय अंतर
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नामांकन के पैटर्न अलग-अलग हैं। उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में नामांकन में वृद्धि हुई है, वहीं दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के कई राज्यों में इसमें गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, बिहार में नामांकन 2.13 करोड़ से घटकर 2.11 करोड़ हो गया; पश्चिम बंगाल में यह 2.48 करोड़ से घटकर 1.71 करोड़ हो गया; और महाराष्ट्र में यह 2.14 करोड़ से घटकर 2.13 करोड़ हो गया। सबसे ज़्यादा गिरावट दक्षिणी राज्यों में हुई: आंध्र प्रदेश में नामांकन 87.42 लाख से घटकर 84.55 लाख हो गया (2.89 लाख की गिरावट); केरल में यह 62.82 लाख से घटकर 61.64 लाख हो गया (1.18 लाख की कमी); तमिलनाडु में यह 1.30 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ हो गया (0.48 लाख की गिरावट); और कर्नाटक में यह 1.19 करोड़ से घटकर 1.18 करोड़ हो गया (0.14 लाख की कमी)।
केंद्र और दक्षिणी राज्य सरकारें इस गिरावट का कारण प्रजनन दर में कमी को मानती हैं, जो 1.1 से 1.9 के बीच गिर गई है, जो नामांकन में आनुपातिक कमी को दर्शाता है।
शिक्षकों की कमी
भारत के राज्य शिक्षा मंत्री के अनुसार, 2019 से भर्ती की कमी के कारण, वर्तमान में देश भर में लगभग 10.6 लाख शिक्षक पद रिक्त हैं। एक सुव्यवस्थित स्कूल प्रणाली के लिए, आदर्श शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए। हालाँकि, बिहार में यह अनुपात 1:50 तक हो सकता है। 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 1,04,125 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ प्रत्येक विद्यालय में केवल एक शिक्षक है।
एक ओर, शिक्षकों की भारी कमी है; दूसरी ओर, मौजूदा शिक्षकों पर अक्सर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ रहता है। यह असंतुलन बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जिन विद्यालयों में केवल एक शिक्षक है, यदि उस शिक्षक को अत्यधिक गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपा जाता है या वह अवकाश ले लेता है, तो पूरा विद्यालय बंद होने के लिए मजबूर हो सकता है। भारत में शिक्षकों की भारी कमी है, खासकर प्राथमिक और ग्रामीण स्कूलों में, जहाँ योग्य शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है।
देश भर में साक्षरता दर में सुधार के बावजूद, यह कमी कई कारणों से बनी हुई है, जिनमें धीमी और जटिल भर्ती प्रक्रिया, अपर्याप्त वेतन, असंतोषजनक कार्य परिस्थितियाँ और योग्य शिक्षकों की कमी शामिल है। परिणामस्वरूप, कई स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात चिंताजनक रूप से उच्च है, जो अक्सर अनुशंसित सीमा से अधिक होता है, जिससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
इस गंभीर संकट से निपटने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षकों के वेतन और नौकरी की सुरक्षा बढ़ाना आवश्यक है, जिससे यह पेशा अधिक आकर्षक और टिकाऊ बन सके। इसके अतिरिक्त, भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि योग्य शिक्षक कक्षाओं में अधिक तेज़ी से प्रवेश कर सकें। सभी बच्चों को समान और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्कूलों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार भी महत्वपूर्ण है।
शिक्षकों की इस कमी के परिणाम गंभीर और दूरगामी हैं। भीड़-भाड़ वाली कक्षाएँ शिक्षकों की छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की क्षमता में बाधा डालती हैं, जिससे कार्यात्मक निरक्षरता का खतरा बढ़ जाता है, जहाँ छात्रों के पास बुनियादी पठन कौशल तो हो सकता है, लेकिन विषयवस्तु की गहरी समझ का अभाव होता है। यह निरंतर संकट शिक्षा की गुणवत्ता और भारत की अगली पीढ़ी की संभावनाओं के लिए एक गंभीर खतरा है। इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए अभी से कदम उठाने होंगे।
शिक्षकों पर गैर-शिक्षण कार्यों का बोझ
शिक्षक मुख्य रूप से छात्रों को शिक्षित करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं; हालाँकि, सरकार द्वारा 36 ऐप और पोर्टल लागू किए जाने के कारण, उन पर गैर-शिक्षण कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इन प्लेटफ़ॉर्म पर शिक्षकों को 100 से ज़्यादा शैक्षणिक और प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, जिससे अक्सर वे शिक्षक की बजाय कार्यालय क्लर्क बन जाते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के दैनिक निर्देश और मुख्यमंत्री कार्यालय की शिकायतें तत्काल ध्यान देने की माँग करती हैं, जिससे शिक्षण समय और भी कम हो जाता है।
जब शिक्षक स्कूल के समय में ये काम पूरा नहीं कर पाते, तो उन्हें स्कूल के बाद या छुट्टियों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनके छात्रों के लिए बहुत कम समय बचता है। इस बोझ के कारण शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और इसके कारण छात्रों का प्रदर्शन गिरता है, अनुशासनहीनता बढ़ती है और स्कूल छोड़ने की दर बढ़ती है। अत्यधिक कार्यभार शिक्षकों के स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और समग्र कल्याण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। संक्षेप में, गैर-शिक्षण कार्यों का बोझ शैक्षिक प्रक्रिया को बाधित करता है, शिक्षकों को थकावट में योगदान देता है और शिक्षा की गुणवत्ता को कम करता है। इस दबाव को कम करने और शिक्षकों को अपने प्राथमिक मिशन, यानी छात्रों को शिक्षित करने पर पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
भारत में एकल-शिक्षक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात
2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 104,125 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ प्रत्येक विद्यालय में केवल एक शिक्षक है। यह संख्या 2016-17 शैक्षणिक वर्ष में 92,275 से बढ़कर अब 100,000 हो गई है। 2024-2025 के लिए यूडीआईएसएफ की रिपोर्ट बताती है कि इन विद्यालयों में लगभग 3.386 मिलियन छात्रों का प्रबंधन एक ही शिक्षक द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 9,508 एकल-शिक्षक विद्यालय हैं; दिल्ली में 771; और हरियाणा में 43,400।
यह स्थिति उत्तर प्रदेश में लगभग 620,000, दिल्ली में 771 और हरियाणा में 43,400 छात्रों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है। इन एकल-शिक्षक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात में काफ़ी भिन्नता हो सकती है, एक छात्र पर एक शिक्षक से लेकर एक शिक्षक पर 96 छात्रों तक। उदाहरण के लिए, बिहार में शिक्षक-छात्र अनुपात सबसे ज़्यादा 96:1 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है जहाँ यह अनुपात 70:1 है। इसके विपरीत, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह अनुपात काफ़ी कम है, जो आमतौर पर प्रति शिक्षक 10 से 15 छात्रों के बीच होता है।
बिहार के सरकारी हलकों में, इन एकल-शिक्षक विद्यालयों को “मिनी स्कूल” कहा जाता है। तेलंगाना में एक-छात्र, एक-शिक्षक विद्यालय का एक उल्लेखनीय उदाहरण सामने आया है। 8 जनवरी, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, खम्मम ज़िले के वायरा मंडल में एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के साथ केवल एक चौथी कक्षा का छात्र ही शिक्षा ग्रहण करता है। यह विद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित होता रहता है कि छात्रों की शिक्षा बाधित न हो, जो कम नामांकन के मामलों में भी, शिक्षा के अधिकार के संरक्षण के लिए तेलंगाना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह निर्णय वैश्विक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। स्कूलों को बंद करने के बजाय, सभी बालिका विद्यालयों को उन्नत करने की अनुशंसा की जाती है। निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या सार्वजनिक शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर चिंताएँ पैदा करती है। निजीकरण की ओर यह रुझान दर्शाता है कि सरकार शिक्षा में पहुँच और समानता को प्राथमिकता नहीं दे रही है। निजीकरण और उदारीकरण को लगातार बढ़ावा देकर, भारत सरकार शिक्षा में जन कल्याण के प्रति अपने दृष्टिकोण का स्पष्ट संदेश देती है। ये नीतियाँ जनहित की कीमत पर निजीकरण को बढ़ावा देती प्रतीत होती हैं।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक उद्देश्य भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमें यह पूछना होगा: क्या भारत वास्तव में एक वैश्विक नेता (विश्व गुरु) बन सकता है? यह एक ज्वलंत प्रश्न है।
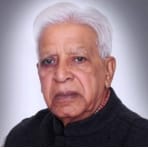
लेखक- डॉ रामजी लाल


