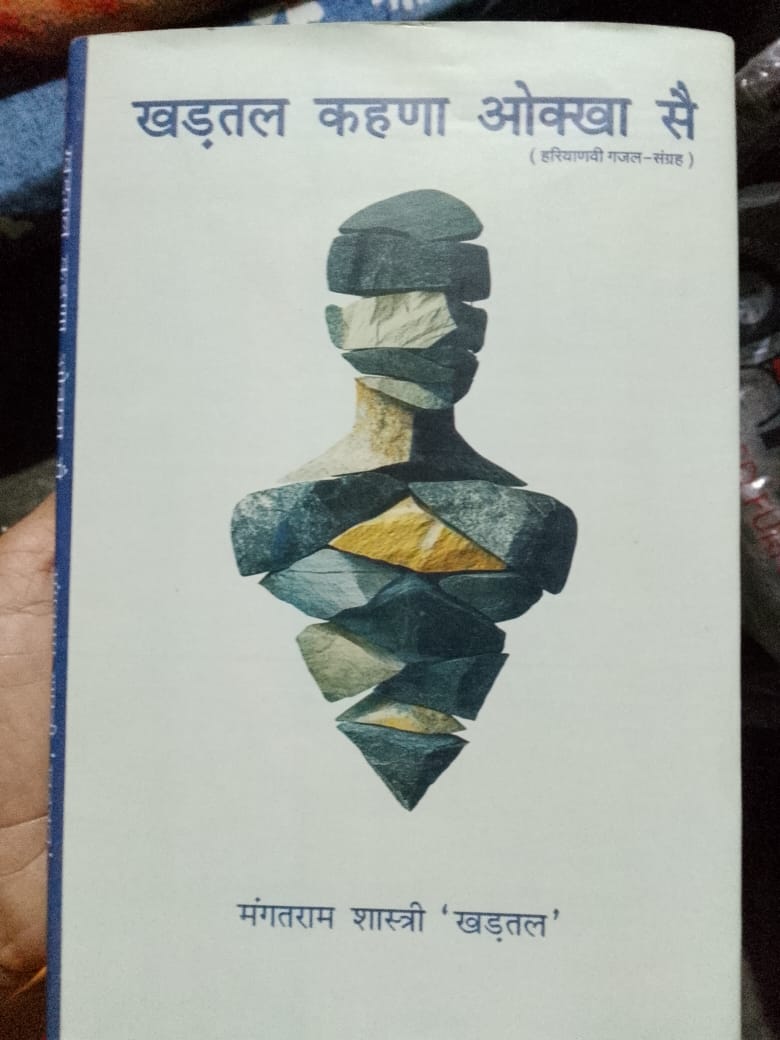कविता
झीनी चादर
गौहर रज़ा
एक चश्मा
एक पतली लाठी
एक चरख़ा
एक झीनी चादर
साये के जैसा
धुंधला, धुंधला
जिस्म, के जिस में
सारी धरती की हिंसा के
ज़हर को पी जाने की हिम्मत
हैराँ हूँ मैं
चश्मे के पीछे दो आँखें
वक़्त के बहते धारे की
सदियों के अंदर झांक रही हैं
लाठी जिसने
हिंसा के सागर की तह में
प्रेम की राहें खोज निकाली
चरखा, जिस की कोख से निकले
नाज़ुक धागे
ज़ुल्म की चक्की के पाटों से
उलझ गए थे
हैरान हूँ मैं
मेरे वतन की इन गलियों में
ऐसा शख्स भी गुज़रा था जो
आग-ओ-धुंए के जंगल में भी
मानवता का बोझ उठाये
आज़ादी से घूम रहा था
हैरान हूँ मैं
आग के जंगल में शोलों ने
उसका रस्ता छोड़ दिया था
हैरान हूँ कि
मेरे वतन की इन गलियों में
ऐसे शख्स के पाँव पड़े थे
जिस के नक़्श मिटाने वाले
आग और खून की बारिश ले कर
मैदां में उतरे हैं, पैहम
लेकिन अबके यूँ लगता है
थक कर हिम्मत हार चुके हैं
मुझ को यक़ीन है
जिस धरती पर
झीनी चादर बिछी हुई हो
उस धरती पर
हिंसा का विष बाटने वाले
जब भी उठेंगे , तब हारेंगे
फिर से अमन की धुन बिखरेगी
प्यार के नाज़ुक सुर जागेंगे
———–