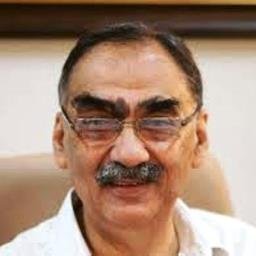भारत का रणनीतिक आत्मसमर्पण
सुशांत सिंह
चीन और भारत को एक साथ लेकर चलने वाले एक पर्यायवाची शब्द ‘चिंडिया’ की चर्चा पश्चिमी मीडिया में 2004 से ही हो रही थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। कुछ साल बाद यह एशिया में साझा महत्वाकांक्षा के एक मुहावरे के रूप में लोकप्रिय हो गया; कई लोगों ने दो प्राचीन सभ्यताओं के एक साथ उभरने के बारे में खूब गीत गाए। यह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने और उनकी ज़ोरदार कूटनीति के बहुप्रचारित वादे से पहले की बात है। आज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। नई दिल्ली खुद को इस्लामाबाद के साथ जोड़कर देखती है, चीन के लिए एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि उसके असहज, कमज़ोर पड़ोसी के रूप में। अब, भारत-चीन की बातचीत साझेदारी के बारे में कम और असंतुलन के बारे में ज़्यादा है। बीजिंग, वाशिंगटन के समकक्ष खड़ा है।
हाल के महीनों में, मोदी सरकार ने कई मंत्रियों और अधिकारियों को बीजिंग भेजा है, संभवतः अगस्त-सितंबर में मोदी की चीन यात्रा की नींव रखने के लिए। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह, एस. जयशंकर, अजीत डोभाल और विक्रम मिस्री की ये शटल यात्राएँ पिछले अक्टूबर में विवादित लद्दाख सीमा पर “संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण” करने के लिए बनी समझ को और मज़बूत कर रही हैं। लेकिन किसी भी तरह के समानता के दावे से कोसों दूर, यह कूटनीतिक नृत्य-रचना मोदी के 11 साल के शासन के बाद की घबराहट—शायद कमज़ोरी—को उजागर करती है। जहाँ सरकार सीमा पर चीन के खिलाफ़ अपनी मज़बूती के घरेलू आख्यान से चिपकी हुई है, वहीं ज़मीनी हक़ीक़त बेहद कड़वी है। चीन-भारत सीमा न तो सामान्य है और न ही विवाद-मुक्त, और नई दिल्ली अपने दावों के अनुसार घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है।
2020 में सीमा संकट शुरू होने के बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक समझदारी भरा आधार रखा था: अगर सीमा सामान्य नहीं है, तो चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। यह प्रस्ताव अब और भी खोखला लगता है। अक्टूबर में हुई सहमति के बाद, सीमा पर हालात गलवान से पहले वाली यथास्थिति तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई इलाकों में प्रमुख बफर ज़ोन भारतीय गश्ती दल की पहुँच से बाहर हैं। पूर्वी लद्दाख में अतिरिक्त भारतीय तैनाती जारी है, जिससे सैनिकों की कमी और बढ़ रही है, जिससे भारतीय सेना चुपचाप जूझ रही है। ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिनका आधिकारिक तौर पर खंडन नहीं किया गया है, कि चीनी गश्ती दल को अरुणाचल प्रदेश के कुछ विवादित इलाकों में जाने की अनुमति दी जा रही है। इस जनवरी में अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने पर, सेना प्रमुख ने यह दावा करके सवाल को टाल दिया कि गश्त का फैसला स्थानीय कमांडरों पर छोड़ दिया गया है। मानो भारत की सीमाओं की पवित्रता सैन्य अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर बातचीत का विषय हो, न कि भारत के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की चिंता का विषय।
ज़मीनी स्तर पर बीजिंग का लगातार दबदबा मोदी सरकार की टेलीविज़न और अख़बारों में ज़ोरदार बयानबाज़ी का एक शर्मनाक नतीजा बन गया है। यह कभी स्वीकार नहीं किया जाता कि द्विपक्षीय संबंधों में अब चीन की पहल है। भारतीय अधिकारियों द्वारा चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने के साथ, सरकार बीजिंग की सुविधानुसार किसी भी शर्त पर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए और भी ज़्यादा बेताब दिखती है।
सीमा, चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, चीनी दबाव की केवल एक धुरी मात्र है। व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में, नई दिल्ली को एक रणनीतिक निर्भरता का सामना करना पड़ रहा है जो मोदी सरकार के आत्मनिर्भरता के नारे का मखौल उड़ाती है। चीन ने भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति रोक दी है। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनें, डीएपी जैसे उर्वरक, और यहाँ तक कि एप्पल के भारत में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रतिभाएँ भी बीजिंग की बाधाओं को पार कर रही हैं। चीनी निवेश को रोकने या आयात को प्रतिबंधित करने के भारत के प्रयास कारगर नहीं हुए हैं। ये केवल भारत के सीमित प्रभाव और सापेक्ष कमज़ोरी को रेखांकित करते हैं। बीजिंग की पकड़ पहले से कहीं अधिक मज़बूत होती जा रही है क्योंकि उसका अनुपालन भारतीय उद्योग, बुनियादी ढाँचे और यहाँ तक कि कृषि के कामकाज के लिए भी महत्वपूर्ण है।
कूटनीतिक रूप से, चीन के हालिया त्रिपक्षीय प्रयोग—अफगानिस्तान-पाकिस्तान के साथ और अलग-अलग पाकिस्तान-बांग्लादेश के साथ—दक्षिण एशिया में भारतीय प्रभाव को कम करने की बीजिंग की लालसा को दर्शाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पहले से ही संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान को हाशिए पर धकेलने के लिए, मोदी सरकार ने सार्क का दम घोंट दिया, लेकिन विकल्प के तौर पर बिम्सटेक का निर्माण भी बांग्लादेश की हालिया घटनाओं के बाद दम तोड़ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, बीजिंग की यात्रा के 10 महीने बाद, सितंबर में भारत का दौरा करेंगे। यह पहली बार है जब किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद नई दिल्ली को अपने पहले पड़ाव के रूप में नहीं चुना। भूटान चीन के साथ सीमा समझौते के लिए बेताब है, लेकिन भारतीय दबाव के आगे उसे बमुश्किल रोका जा रहा है—कौन जाने कब तक। मोदी का ‘पड़ोसी पहले’ का नारा तब खोखला लगता है जब दक्षिण एशियाई राजधानियों का जोर बीजिंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पर है।
चीन का आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है कि वह एकतरफ़ा तौर पर भारतीयों को वीज़ा जारी करना शुरू कर देता है और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर देता है, बिना भारत द्वारा चीनी पर्यटकों के लिए वीज़ा जारी करने या द्विपक्षीय उड़ानें फिर से शुरू करने का इंतज़ार किए। वह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान की निंदा करने की माँग करने जैसे द्विपक्षीय मुद्दे को उठाने पर भारत को नसीहत भी दे सकता है। बस इतना ही नहीं। तिब्बत मुद्दे पर तीखा हमला करके, दलाई लामा के जन्मदिन पर मोदी को चेतावनी देकर, और हालिया सैन्य झड़प के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करके, बीजिंग द्विपक्षीय संबंधों की शर्तें तय करता है, जबकि नई दिल्ली की प्रतिक्रियाएँ ज़्यादातर औपचारिक ही रहती हैं या इससे भी बदतर, गायब ही रहती हैं।
चीन की इस बहुस्तरीय चुनौती के प्रति मोदी सरकार की वास्तविक प्रतिक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा, रियायती रही है। 2023 में जयशंकर का यह बहाना कि “देखो, वे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मैं क्या करूँगा?”, भू-राजनीतिक अंतर्दृष्टि से कम और मोदी की लाचारी की घोषणा ज़्यादा थी, जैसा कि आज स्पष्ट है। बीजिंग मोदी की हिम्मत की परीक्षा ले रहा था, और मोदी झुक गए। विश्वसनीय निवारक क्षमता या राष्ट्रीय क्षमता बनाने के बजाय, सरकार ने नुकसान को सीमित करने पर ही संतोष कर लिया है। जिसे जयशंकर ने “सामान्य बुद्धि का प्रश्न” कहा, वह मूलतः चीन के साथ संबंधों को बीजिंग की शर्तों पर फिर से स्थापित करने के समान है।
इस रुख़ के दो कारण हैं। पहला, नए युग की तमाम बातों के बावजूद, मोदी के नेतृत्व में भारत वास्तविक आंतरिक शक्ति का निर्माण करने में विफल रहा है। रक्षा आधुनिकीकरण अधूरा है, संसाधनों से रहित है, और राजनीतिक समर्थन के बिना है। अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है, और अति-राष्ट्रवादी बयानबाज़ी का अभियान संरचनात्मक सुधारों का एक ख़राब विकल्प है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सरकार के भव्य बाहरी संतुलन में कोई ठोस आधार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लेन-देन के प्रति समर्पित हैं; उन्हें मोदी द्वारा उनके साथ की गई दो चुनावी रैलियों की कोई परवाह नहीं है। उनका प्रशासन भारत से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कुछ ख़ास नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है, लेकिन बीजिंग के विरुद्ध भारत की सुरक्षा को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं रखता।
यह सब मोदी और उनके समर्थकों के लिए एक कड़वी सजा है। भारत आर्थिक प्रगति के लिए चीन की इच्छाशक्ति पर और रणनीतिक समर्थन के लिए अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, लेकिन दोनों ही उसे छोड़ दिए जाने का जोखिम उठा रहे हैं। न तो जयशंकर की तीखी ज़बान और न ही बॉलीवुड द्वारा डोभाल पर की गई प्रशंसा इस नाकामी की भरपाई कर सकती है, जो मोदी की खोखली व्यक्ति- और घटना-आधारित विदेश नीति से उपजी है। विभिन्न देशों से मिले कई पुरस्कार मोदी को चीन के सामने खड़े होने या ट्रंप का सामना करने का साहस नहीं दे पाएँगे।
एक तरह से, यह स्थिति 1962 की हार के बाद जवाहरलाल नेहरू के सामने आई किसी भी स्थिति से कहीं ज़्यादा ख़राब है। चीन ने युद्धविराम और एकतरफ़ा वापसी की घोषणा तो की ही, साथ ही उसने भारत से क्षेत्रीय माँगें भी रखीं। नेहरू ने इन सभी को अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, मोदी शासन के 12वें वर्ष में, भारत आंतरिक शक्ति का निर्माण करने में असमर्थ है, सार्थक बाहरी समर्थन हासिल नहीं कर पा रहा है, चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करने और बीजिंग द्वारा निर्धारित शर्तों पर द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दबाव बनाने पर मजबूर है।
यह बात साफ़ तौर पर कही जानी चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल ने क्षेत्रीय और वैश्विक, दोनों स्तरों पर भारत की साख को कम कर दिया है। भारत अब शर्तें तय नहीं करता। सीमाओं के समझौता होने और प्रभाव खत्म होने के साथ, नई दिल्ली अब चीन के वर्चस्व का विरोध करने में असमर्थ, पराश्रित और शब्दों या कर्मों में असमर्थ है। यह ताकत नहीं, बल्कि समर्पण है। द टेलीग्राफ से साभार
सुशांत सिंह येल यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं।