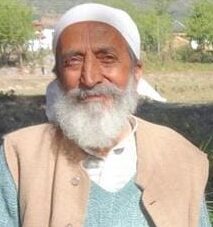किस तरह बिगड़ी पहाड़ी खेती और ग्रामीण व्यवस्था
कुलभूषण उपमन्यु
पहाड़ के लोग ज्यादातर खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर आधारित आत्मनिर्भर जीवन जीते रहे हैं. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आवागमन की सुविधाओं का अभाव स्वाभाविक था. जिसके चलते लोगों ने आत्मनिर्भर जीवन पद्धति को विकसित किया जो खेती के इर्दगिर्द घूमती थी. पहाड़ में खेती का अर्थ है खेती, पशुपालन,और दस्तकारी का मिश्रित रूप, जिसमें वन संसाधनों की मुख्य भूमिका थी. इस मिश्रित जीवन यापन पद्धति के लिए अधिकांश संसाधन वन भूमियों से ही प्राप्त किये जाते थे. खेती, पशुपालन और दस्तकारी आपस में एक दूसरे पर आश्रित भी थे और पूरक भी थे. पशुपालन में भेड़, बकरी पालन शामिल ही था. पौष्टिक भोजन के लिए अन्न खेती से और दूध घी पशुओं से, जंगली कंद-मूल,फल, सब्जियां पर्याप्त मात्रा में वनों से मिल जाता था. वन संसाधन घास चारे से भरपूर होते थे. अच्छे चरागाह उपलब्ध थे. इस कारण पशु संख्या को सीमित करने के कोई दबाव नहीं थे.
पशुपालन खूंटे पर नहीं होता था बल्कि मुख्यत: चरागाहों में खुले चरान से होता था इस लिए सामूहिक रूप से दोचार लोग पूरे गांव के पशुओं को चुगा कर ले आते थे या जहां ऐसा संभव नहीं होता था वहां कठिन श्रम न कर सकने वाले घर के सदस्य ही चराई का काम कर लेते थे जिससे मुख्य श्रम शक्ति खेती दस्तकारी के श्रमसाध्य कार्यों के लिए बची रहती थी. नकद जरूरतों के लिए भेड़ बकरी पाली जाती थीं जिसका नाम ही “धन” इसीलिए पड़ा है. गाय भैंस के दूध से घी बनाने का प्रचलन था क्योंकि सबके पास दूध होता था इसलिए दूध की बिक्री कम ही थी. दूध बेचना अच्छा भी नहीं समझा जाता था.
पहाड़ का देसी घी अमृतसर आदि पंजाब की मंडियों तक भेजा जाता था. खेती के लिए देसी खाद गोबर और भेड़ बकरियों की मेंगनों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी. घुमन्तू पशु और भेड़ बकरी चारक सर्दियों में निचले कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आ जाते और गर्मियों में ऊंचाई वाले बर्फानी चरागाहों में चले जाते. आने जाने के दौरान वे जब मध्यवर्ती कृषि प्रधान क्षेत्रों से गुजरते तब जुताई के बाद खाली खेतों में “धण” (भेड़ बकरियों का रेवड़) को रात में आराम करने के लिए बिठाया जाता जिससे उनके मल मूत्र से खेत में बढ़िया खाद मिल जाती. बदले में भेड़ बकरी वालों को अन्न के रूप में कुछ भुगतान किया जाता. जिसके दर इलाके के मुताबिक तय रहते थे. यहाँ तक कि राजा चंबा ने ये दर तय कर रखे थे जो पड़ोसी जिला काँगड़ा के क्षेत्रों पर भी लागू होते थे.
खेतों की मेड़ों पर चारे के वृक्ष उगाए जाते जिनसे मौसमी हरा चारा मिलजाता. कुछ चारा खेती के अवशेषों से मिल जाता बाकी कमी वनों में उपलब्ध चारे के पेड़ों और चराई से पूरी हो जाती. लोगों ने कुछ मल्कियत घासनियां भी प्रबंधित कर रखी थीं. यानि बाहर से चारा मंगवाने की सोचने की भी जरूरत नहीं थी. बिना कोई पैसा खर्च किये ये साधन उपलब्ध थे. खेती भी लाभदायक थी पशुपालन में भी नकद कमाई हो जाती थी. पशुओं को माल कहा जाता था. हर घर में दोचार पशु तो होते ही थे. धीरे धीरे यह संतुलन बिगड़ने लगा.
वनों को साफ काट कर बेचा जाने लगा, उनके स्थान पर नए पेड़ व्यापारिक प्रजातियों के लगाये गए. चारे का अकाल पड़ने लगा. आबादी बढ़ने से इंधन की मांग बढ़ती गई. भेड़ बकरी के चारे के लिए उपयोगी झाड़ियां और रहे सहे वृक्ष भी इंधन की भेंट चढ़ने लगे. चारे का संकट और गहरा होता गया. रही सही कसर हरित क्रांति के बीजों के साथ आये खरपतवारों ने पूरी कर दी. आज स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा चरागाह खरपतवारों की भेंट चढ़ कर अनुपजाऊ हो गए हैं. पशुओं के लिए चारा पंजाब हरयाणा से मंगवाना पड़ रहा है. जिसकी कीमत दस से पन्द्रह रु. किलो तक बैठती है. इतने मंहगे चारे से पशु पालन लाभकारी नहीं रहा. एक समय भूमिहीन भी पशु पाल कर अपना जीवनयापन कर लेते थे अब तो भूमालिकों के भी हाथ खड़े होने लग पड़े.
पशुधन जो ग्रामजीवन की रीढ़ थी सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया जाने लगा. जिससे एक ओर उपलब्ध आय खत्म हो गई दूसरी ओर वही बेसहारा पशु फसलों को उजाड़ने लगे. खेती को खेती ही खाने लगी. फसलों के लिए पूरा देसी खाद उपलब्ध नहीं रही. मिट्टी की उत्पादकता घट रही है. पहले अपना बीज, अपना बैल, अपनी खाद से जमीन में जो कमाया वह अपना ही था. अब तो बीज, रासायनिक खाद, पॉवर टिलर आदि सब बाहर से खरीदना है. ले देकर अपनी मजदूरी के बराबर आय भी छोटी जोत वाले प्राप्त नहीं कर पाते इस कारण खेती छोड़ कर लोग मजदूरी को बेहतर समझने लगे हैं.
दसवीं या जमा दो तक पढ़े बच्चे भी मजदूरी करने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई तक जा रहे हैं. खेती थोड़ा बहुत बागवानी वाले क्षत्रों में ही लाभदायक बची है या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बेमौसमी सब्जी का उत्पादन संभव है. बाहरी हिमालय और शिवालिक क्षेत्र तो बिलकुल घाटे की खेती करने को अभिशप्त हो चुके हैं. वनों से जब मिश्रित वृक्ष झाड़ी प्रजातियां लुप्त हुईं उसके साथ ही वन्य प्राणियों का भोजन भी खत्म हो गया अब वे भी खेती उजाड़ने में व्यस्त हैं. बंदरों का कोई इलाज आज तक सरकारें निकाल नहीं पाई हैं. उस पर सूअर और नीलगाय भी फसलों को तबाह कर रहे हैं.
दस्तकारी को तो औद्योगीकरण की एकांगी नीतियां निगल गईं. जैव विविधता के नष्ट होने के कारण बहुत से दस्तकारी के लिए जरूरी संसाधन भी समाप्त हो गए. ऊनी उत्पादों को सिंथेटिक वस्त्र उद्योग चट कर गया. पत्तलों को प्लास्टिक और कागज़ की प्लास्टिक परत चढ़ी प्लेटों ने निगल लिया. कुम्हार, लोहार, जुलाहा, तेली, मोची, सब तो गांव से गायब हैं. गांव में हर वस्तु शहरों की ही तरह बाजार से आ रही है. और बाजार तो अब विश्व भर तक फ़ैल गया है. स्थानीय ग्रामीण जो उत्पादक आत्मनिर्भर इकाई था अब केवल ग्राहक बन गया है. ग्राहक भी नहीं अब वह कष्टमर है यानि इन तमाम विज्ञापन जनित प्रलोभनों से उत्पन्न मांग को पूरा न कर पाने की चाहत के कष्ट से मर.
यदि इस तकनीकी विकास की प्रक्रिया में लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को भी जोड़ा जाता और औद्योगिक विकास का मॉडल भारतीय ग्रामीण जरूरतों और शक्ति की पहचान के आधार पर बनाया जाता तो ग्रामीण क्षेत्र रोजगार की तलाश में शहरी झुग्गियों में नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त न होते. गांधी जी इसी तरह की ग्रामीण औद्योगीकरण की समझ को विकसित करने की बात करते रहे.
आज भी हम स्वदेशी का नारा लगा रहे हैं किन्तु यह नकली स्वदेशी है. स्वदेशी तो वह होता जिसमें ग्रामीण दस्तकारी के विनाश के बिना उन उत्पादक कार्य की समझ और संस्कार रखने वाले ग्रामीण दस्तकारों को आधुनिक तकनीकों से लैस करके उत्पादन में प्रवृत्त किया जाता. किन्तु उसके लिए तकनीक विकास, नवाचार शोध का आधार ही खड़ा नहीं किया गया. सारी जिम्मेदारी नवाचार की जिस औद्योगिक बड़े तंत्र पर डाली गई या राम भरोसे छोड़ी गई उसने दस्तकारी की कीमत पर अपना विकास तो कर लिया किन्तु गांव उजड़ने की कीमत पर. इस पर “यूस एंड थ्रो”संस्कृति ने प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को और बढ़ा दिया है जिसके चलते ग्रामीण आजीविकाओं के लिए संसाधनों की और ज्यादा कमी पड़ती जा रही है और टकराव बढ़ रहे हैं.
“उलटे बांस बरेली को” वाली स्थिति बन गई है. जो खुद उत्पादन करते थे अब खरीददार बना दिए गए और इसे हमने विकास माना. कम से कम दैनिक जरूरत की उन चीजों का उत्पादन जो गांव में हो सकता है फिर से गांव में वापस लाने की शुरुआत होनी चाहिए. इस उलटी समझ से मुक्ति का मार्ग कहीं न कहीं गांधी के आदर्श को समझ कर ही मिल सकता है. किन्तु गांधी को अब या तो ट्रेड मार्क बना दिया गया है, जिसके पीछे छिप कर अपने सही गलत को ढंका जा सकता है, या फिर सारी कमियों के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा कर गाली गलौच करके अपनी कुंठित सोच में आत्ममुग्ध हुआ जा सकता है. इससे उपर उठें तो निष्पक्ष चिंतन से रास्ते निकलेंगे किन्तु बहुत सी मूल प्रस्थापनाओं को पुनर्परिभाषित करके ही नया अध्याय लिखना होगा. पहाड़ में यह कार्य और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ संवेदनशील प्रकृति के चलते अच्छे या बुरे कार्य का असर भी जल्दी दीखता है. यहीं से प्रयोग का आरंभ हो तो पूरे देश के लिए भी दिशा निकलेगी.