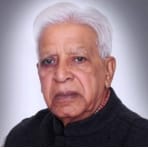हरियाणा दिवस पर विशेष लेख : 1 नवंबर 2025
हरियाणा में अलग राजधानी और अलग हाईकोर्ट नहीं: समाधान की कसक
डॉ .रामजीलाल
1 नवंबर 1966 को लगभग 59वर्ष पूर्व पंजाब के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप पंजाब,हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई. हरियाणा के लोगों के दिलों में हरियाणा की अलग राजधानी, हरियाणा का अलग हाईकोर्ट, के लम्बित मुख्य मुद्दों के समाधान की कसक आज भी है.
हरियाणा के अलग राजधानी
सन् 1950 में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ घोषित की गई .01 नवंबर 1966 को पंजाब का बंटवारा तीन राज्यों —हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हो गया.हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है.जबकि हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है. छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड ,मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड इत्यादि ऐसे छोटे राज्य हैं जिनकी अलग-अलग व राजधानियां हैं.
-
हरियाणा और पंजाब के नेताओं के मानसिकता
समय-समय पर हरियाणा और पंजाब के नेता चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार जताते हैं. संकीर्ण क्षेत्रीय मानसिकता और वोट बैंक के कारण, केंद्रीय, हरियाणा और पंजाब में एक ही पार्टी के नेताओं के अलग-अलग रुख उनके दोहरे मानदंडों को उजागर करते हैं. इसलिए, समस्या का कोई समाधान नज़र नहीं आता.
3.केंद्रीय स्थान पर एक अलग राजधानी
जीटी रोड पर किसी केंद्रीय स्थान पर हरियाणा के लिए एक अलग राजधानी स्थापित करने से प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उचित आवंटन, हरियाणा की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और जनता के समय और धन की बचत जैसे लाभ होंगे. उस व्यक्ति की हताशा और निराशा की कल्पना कीजिए जिसे रेवाड़ी से चंडीगढ़ 325 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा हो और वहाँ उसे कोई मंत्री या विधायक नहीं मिले और उसका काम पूरा न हो.नौकरशाह खुद को जनता का सेवक नहीं, मालिक समझते हैं और उन्हें चुनावों में वोट मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है. यही कारण है कि वे आम जनता के प्रति उदासीन और असंवेदनशील हैं. इसलिए केंद्रीय स्थान पर एक अलग राजधानी होनी चाहिए.
हरियाणा का अलग हाईकोर्ट:
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. भारत के संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होना चाहिए. छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड ,मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड इत्यादि छोटे राज्यों के भी अलग-अलग हाईकोर्ट हैं.इस समय भारतवर्ष में 25 उच्च न्यायालय हैं.
पंजाब और हरियाणा की राजधानी ही संयुक्त नहीं है अपितु दोनों राज्यों व चंडीगढ़ का हाई कोर्ट भी संयुक्त है जिसे पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट कहा जाता है.पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय सन् 1966 में एक अस्थाई व्यवस्था के रूप में था. परंतु लगभग 6 दशक के बाद भी इसका जारी रहना उचित नजर नहीं आता .परिणाम स्वरुप हरियाणा और पंजाब का अलग-अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए.
हरियाणा विधानसभा में पृथक उच्च न्यायालय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
हरियाणा विधानसभा ने मार्च 2002 और दिसम्बर 2005 में पृथक उच्च न्यायालय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था, परंतु केंद्र में चाहे एनडीए की सरकार थी अथवा यूपीए की सरकार थी हरियाणा विधानसभा के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया .
पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट :लंबित मामले व न्याय में विलंब
वर्ष 2014में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पृथक उच्च न्यायालय की वकालत करते हुए केंद्र सरकार से कहा ‘’पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित कुल 2,79,699 मामलों में से हरियाणा के मामले 1,40,359 हैं. यह पंजाब के 1,24,575 मामलों से अधिक है.” 12 वर्ष के पश्चात यह संख्या बढ़कर 30 सितंबर 2025 को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में मुख्य सिविल केस 2,56,6616तथा मुख्य क्रिमिनल केस 1,58 ,138(कुल मुख्य सिविल व क्रिमिनल केस 4,14,754) लंबित थे.
जनवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा की सभी अदालतों में 14,30,151 मामले लंबित थे. इनमें से 70% एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे. . इन लंबित मामलों में से 4,13,786 सिविल मामले और 9,92,135 आपराधिक मामले थे. इसके अतिरिक्त, 72,844 मामले परीक्षण और परीक्षण-पूर्व मामलों के कारण अनसुलझे रह गए. लेकिन अपुष्ट सूत्रों के अनुसार हरियाणा के जिला स्तरीय और अधीनस्थ न्यायालयों में क्रमश: 14,25,047 और 4,50,000 मामले लंबित हैं. बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे आयोगों और न्यायाधिकरणों, राजस्व विभाग के कानूनगो से लेकर ज़िला अधिकारियों तक, लालफीताशाही के कारण लाखों मामले लंबित हैं. संक्षेप में कहें तो हरियाणा की अनुमानित 30.9 मिलियन जनसंख्या में से 45 लाख हरियाणवी लोग मुकदमेबाजी में संलिप्त हैं.
मुकदमों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण :
मुकदमों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण हैं – प्रतिवादियों की अनुपलब्धता , नये मुकदमों का दायर होना, न्यायाधीशों की संख्या जनसंख्या के अनुपात से कम होना,स्थगन संस्कृति अपनाकर न्यायाधीशों द्वारा अगली तारीख देना व अवकाश पर होना(लंबित मामले 84,386), जनहित का अति महत्वपूर्ण मामला दायर होने पर तत्काल सुनवाई, वकीलों की अनुपस्थिति व वकीलों द्वारा अगली तारीख मांगना(लंबित मामले 2,72,558), वादी की अनुपस्थिति (लंबित मामले 40,655) ,वादी और प्रतिवादी के वकीलों के बीच मिलीभगत, तथा गवाहों का समय पर उपस्थित न होना.
समस्या का समाधान करने के लिए सुझाव
प्रथम,यदि दोनों राज्यों के अलग-अलग हाईकोर्ट स्थापित हो जाते हैं तो मुकदमों का भर काम होगा और जनता को शीघ्र व सस्ता न्याय प्राप्त होगा. हरियाणा की जनता का शीघ्र और संस्ता न्याय देने के हेतु हरियाणा का अलग उच्च न्यायालय बनने के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद ,रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ,सिरसा ,फतेहाबाद इत्यादि जिलों के लिए उच्च न्यायालय का एक अलग बेंच गुरुग्राम में स्थापित होना चाहिए.
द्वितीय, जनसंख्या के बढ़ऩे के कारण जिला स्तरीय और अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की संख्या का बढ़ाना शीघ्र व सस्ता निर्णय देने के लिए अत्यंत आवश्यक है.
तीसरा, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, आयोगों और राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए मामलों पर निर्णय लेने हेतु समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए.
चतुर्थ,यदि निर्धारित समय-सीमा में निर्णय नहीं दिया जाता है, तो उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए. यदि संतोषजनक उत्तर न मिले, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह जनता का स्वामी नहीं, बल्कि सेवक होता है और उसका मुख्य कार्य जनता को न्याय देना है, न कि उन्हें परेशान करना.
पाँचवाँ, व्यवस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर ज़ोर दिया जाना चाहिए और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जनता का विश्वास जगाना होगा. भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति ज़ब्त की जानी चाहिए. हालाँकि, इसके लिए सरकार की इच्छाशक्ति, नीयत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, जिसका स्पष्ट रूप से अभाव दृष्टिगोचर होता है.
सारांशतः हरियाणा के लिए अलग राजधानी एवं अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय संगठन का निर्माण करके प्रजातात्रिक ढ़ग से आन्दोलन चला जाए तथा प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जनता में जागरूक का पैदा करके राजनीतिक दलों और केंद्रीय, हरियाणा व पंजाब राज्य सरकारों पर दबाव डालना अत्यंत आवश्यक है.
लेखक दयाल सिंह कॉलेज, करनाल (हरियाणाः के पूर्व प्राचार्य एवं सामाजिक वैज्ञानिक हैं।