“ग्राम्शी ने क्रांति को केवल सत्ता–हस्तांतरण की घटना नहीं माना, बल्कि उसे एक लंबी सांस्कृतिक प्रक्रिया बताया। यदि पूँजीवाद अपनी स्थिरता विचारधाराओं और संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करता है, तो समाजवाद को भी उतना ही गहरा सांस्कृतिक वैधता-आधार चाहिए।”–ग्राम्शी पर महेश मिश्र का यह लेख कॉमन सेंस, वर्चस्व, प्रतिरोध, ऐतिहासीकरण सरीखी अवधारणाओं को जितनी स्पष्टता और सरलता के साथ प्रस्तुत करता है, वह सामान्यतः दुर्लभ है। वे बिन्दुवार इसकी भी चर्चा करते हैं कि इन अवधारणाओं का साहित्य के अध्ययन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
ग्राम्शी : वर्चस्व के ख़िलाफ़ दीर्घकालीन सांस्कृतिक युद्ध का प्रस्ताव
महेश मिश्र
एंटोनियो ग्राम्शी क्लासिकल मार्क्सवाद से अलग पहचान रखते हैं। वस्तुत: वाम-विचार में वे विकास का अगला चरण हैं। ग्राम्शी ने मार्क्सवाद में वह तत्व जोड़ा जो लंबे समय तक उपेक्षित था—मानव इच्छा, विचार और संस्कृति की निर्णायक भूमिका। यदि मार्क्स का नारा था, ‘दुनिया के मज़दूरो, एक हो’, तो ग्राम्शी ने यह जोड़ा कि यह एक होना तभी संभव है जब वे अपने जीवन को सांस्कृतिक रूप से बदलें और नयी वैचारिक सत्ता क़ायम करें।
ग्राम्शी का सबसे मौलिक हस्तक्षेप उस बिंदु पर था जहाँ क्लासिकल मार्क्सवाद ने अपने विश्लेषण को लगभग स्थिर कर दिया था—आधार और अधिरचना के रिश्ते पर। मार्क्स ने अपनी रचना Preface to the Critique of Political Economy (1859) में कहा था कि समाज का “आधार” (आर्थिक उत्पादन संबंध) उसकी “अधिरचना” (राजनीति, क़ानून, विचारधारा) को निर्धारित करता है। इस परंपरा में चेतना को केवल प्रतिबिम्ब माना गया।
ग्राम्शी ने प्रिज़न नोटबुक्स में इस रेखीय व्याख्या को तोड़ा। उनके लिए अधिरचना मात्र परजीवी संरचना नहीं थी, बल्कि सक्रिय, सृजनशील और कभी–कभी निर्णायक भी हो सकती थी। वे लिखते हैं कि
चेतना भौतिक वास्तविकता का प्रतिबिम्ब मात्र नहीं है, बल्कि वह सृजनात्मक शक्ति है जो स्वयं यथार्थ को रूपान्तरित करने में सक्षम है (Consciousness is not a passive mirror of material reality, but an active force that can transform it)।
इसके लिए जनता की सहमति और नैतिक नेतृत्व आवश्यक है। यही कारण है कि ग्राम्शी ने वर्चस्व को राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र बनाया।
उनके लिए दल का कार्य केवल आर्थिक माँगों को संगठित करना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक विश्व-दृष्टि भी निर्मित करना होता है। सत्ता प्राप्त करने से पहले ही समाज में वैचारिक वर्चस्व स्थापित करना अनिवार्य है। इस अर्थ में क्रांति एक दीर्घ–कालीन सांस्कृतिक युद्ध (war of position) है, जो प्रत्यक्ष विद्रोह से कहीं अधिक कठिन और निर्णायक है।
यहाँ उनका तात्पर्य यह था कि धर्म, शिक्षा, साहित्य, बुद्धिजीवी और मीडिया जैसी संस्थाएँ केवल पूँजीवादी व्यवस्था की छाया नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता के स्रोत हैं। यदि शासक वर्ग केवल उत्पादन के साधनों पर क़ब्ज़ा कर ले तो भी उसका प्रभुत्व टिकाऊ नहीं होगा; उसे लोगों की सहमति और नैतिक अनुकरण चाहिए।
यही वह बिंदु है जहाँ चेतना (consciousness) राजनीतिक बन जाती है। ग्राम्शी बार–बार इस बात पर ज़ोर देते हैं कि किसी भी क्रांतिकारी प्रक्रिया की सफलता इस पर निर्भर है कि मज़दूर और अधीन-वर्ग कितनी गहराई से अपने अनुभवों को समझते हैं और उन्हें किस प्रकार एक व्यापक वैचारिक दृष्टि में पिरोते हैं।
लेकिन चेतना का यह रूपांतरण अपने आप नहीं होता। इसके लिए ज़रूरत होती है क्रांतिकारी पार्टी की—एक ऐसी संस्था जो न केवल राजनीतिक माँगों को समन्वित करे, बल्कि पूरे समाज के लिए एक नये नैतिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण का निर्माण करे।
उसे “ट्रेड-यूनियन कांशसनेस” से “क्लास कांशसनेस” तक की यात्रा करनी होगी। और यह यात्रा पार्टी के नेतृत्व में संभव है। लेकिन यहाँ एक कठिन प्रश्न उठता है—क्या यह पार्टी, जो समाज का नैतिक और वैचारिक नेतृत्व करने वाली है, अंततः अधिनायकवादी (authoritarian) नहीं हो जाएगी? ग्राम्शी ने इस प्रश्न से बचने की कोशिश नहीं की। वे स्वीकार करते हैं कि क्रांतिकारी पार्टी में अनुशासन और केंद्रीयकरण आवश्यक है, पर साथ ही वे यह भी मानते हैं कि उसका उद्देश्य जनता की सक्रिय भागीदारी और आलोचनात्मक चेतना को बढ़ाना होना चाहिए। यानी पार्टी का नेतृत्व दबाव पर नहीं बल्कि सहमति पर आधारित होना चाहिए। यह वही हेजेमनी है जिसके बिना कोई भी प्रभुत्व टिक नहीं सकता। इसलिए पार्टी का चरित्र केवल राजनीतिक–संगठनात्मक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक है।
इस बिंदु पर ग्राम्शी का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने क्रांति को केवल सत्ता–हस्तांतरण की घटना नहीं माना, बल्कि उसे एक लंबी सांस्कृतिक प्रक्रिया बताया। यदि पूँजीवाद अपनी स्थिरता विचारधाराओं और संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करता है, तो समाजवाद को भी उतना ही गहरा सांस्कृतिक वैधता-आधार चाहिए।
»»»
इस तरह हम मान सकते हैं कि बीसवीं शताब्दी के यूरोपीय मार्क्सवाद में यदि किसी विचारक ने इस परंपरा को भीतर से हिलाकर रख दिया तो वह अंटोनियो ग्राम्शी थे। फेमिया अपनी पुस्तक ग्राम्शी का राजनीतिक चिंतन (Gramsci’s Political Thought) की भूमिका में लिखते हैं कि ‘ग्राम्शी मनुष्य की व्यक्तिपरकता को मार्क्सवाद के केन्द्रीय तत्त्व के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं’ (He attempts to establish human subjectivity as a core element of Marxism)।
क्लासिकल मार्क्सवाद में जहाँ ऐतिहासिक प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ आर्थिक संरचनाओं का परिणाम माना गया, वहीं ग्राम्शी ने चेतना और विचारों को स्वायत्त, सृजनात्मक भूमिका दी।
ग्राम्शी का यह आग्रह केवल दार्शनिक नहीं था। वे एक ऐसे इटली में जी रहे थे जो उत्तर और दक्षिण, औद्योगिक नगर और कृषि–प्रधान गाँव, आधुनिक और परंपरागत शक्तियों के बीच बँटा हुआ था। यहाँ कैथोलिक चर्च की आध्यात्मिक सत्ता और राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरे थे। इसलिए उनके लिए यह स्पष्ट था कि मात्र आर्थिक संरचना से राजनीति और समाज की गतिशीलता को समझा नहीं जा सकता।
इसी पृष्ठभूमि से ग्राम्शी की सर्वाधिक चर्चित अवधारणा उभरी—‘Hegemony’। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने उस वैचारिक वर्चस्व के लिए किया जिसके बिना किसी वर्ग का राजनीतिक प्रभुत्व टिक नहीं सकता। यहाँ सत्ता केवल पुलिस, सेना या आर्थिक ताक़त से नहीं चलती, बल्कि शासक वर्ग अपने विचारों और जीवन–शैली को सामान्य और नैतिक बना देता है।
»»»
ग्राम्शी ‘कला कला के लिए’ (art for art’s sake) के रूप में साहित्य में कम, और इस बात में अधिक रुचि रखते थे कि साहित्य अर्थ, शक्ति और वर्ग-संघर्ष के व्यापक प्रश्नों में कैसे सहभागी होता है, कैसे पार्टिसिपेट करता है, कैसे इन सबको बदलता है, और इन सबसे वह कैसे अपने आपको ढालता है…
हम उनकी अवधारणाओं और साहित्य के मिलन-बिंदु या प्रचलित शब्दावली में कहें तो प्रवेश-बिंदुओं पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ उदाहरणों के माध्यम से यह समझेंगे कि साहित्य का ग्राम्शी के ढंग से मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है।
सांस्कृतिक वर्चस्व और सहमति (Hegemony and Consent)
ग्राम्शी का तर्क था कि शासक वर्ग केवल बल-प्रयोग से नहीं, बल्कि सहमति (consent) जीतकर—सांस्कृतिक मानकों, नैतिक मूल्यों और कॉमन सेंस के ज़रिए—अपनी शक्ति बनाए रखते हैं।
किसी साहित्यिक या कलात्मक कृति का जब हम मूल्यांकन कर रहे हों तो हमें सवाल करना चाहिए कि-
1) क्या यह कृति प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों को पुन: ला रही है, उन्हीं को बलीकृत कर रही है या फिर उन्हें चुनौती दे रही है?
2) क्या यह शासक विचारधारा (ruling-class ideology) को “स्वाभाविक” बनाकर पेश कर रही है, या उसके अंतर्विरोधों को उजागर कर रही है?
जैविक बनाम परंपरागत बुद्धिजीवी (Organic vs. Traditional Intellectuals)
ग्राम्शी लेखकों को “intellectuals” के रूप में देखते हैं। कुछ परंपरागत बुद्धिजीवी (traditional intellectuals) होते हैं जो शासक विचारधारा के अनुरूप रहते हैं और तटस्थ प्रतीत होते हैं…. ध्यान रखें कि ये तटस्थ प्रतीत होते हैं….होते नहीं हैं….ग्राम्शी नुआन्सेज़ पर विचार करने वाले लेखक हैं और वे इस बात की गहरी छानबीन करते हैं कि जो सतह पर दिख रहा है, वह अधूरा भी हो सकता है, असत्य और भ्रमोत्पादक भी…
दूसरी ओर कुछ ऐसे भी बौद्धिक होते हैं जो अपने वर्ग-हितों के अनुरूप सोचते हैं, जो उनकी पोजीशनैलिटी होती है, उसी के अनुक्रम में वे, उसी के संगत विचार करते हैं और सामान्य अर्थों में काउंटर-हेजेमनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स (organic intellectuals) होते हैं। ये शोषित वर्गों की चेतना को रूपायित करते हैं, उसे स्वरूप भी देते हैं और विकसित भी करते हैं।
इस संदर्भ में सवाल यह होना चाहिए कि—
1) लेखक किस प्रकार का बौद्धिक काम कर रहा/रही है?
2) क्या पाठ वंचित वर्ग के संघर्षों के साथ स्वयं को जोड़ता है या अभिजन आख्यानों/elite narratives को ही सुदृढ़ कर रहा है? यह जानबूझकर या अनजाने में भी हो सकता है।
साहित्य और कॉमन सेंस (Literature and Common Sense)
ग्राम्शी हमें यह समझने का एक गहरा उपकरण देते हैं कि चेतना विरोधाभासी होती है।
साधारण व्यक्ति का कॉमन सेंस परंपरा, धर्म, सत्ता और लोक-कथाओं से बुना हुआ होता है। इसमें न्याय और अन्याय दोनों ही को स्वीकार करने की क्षमता एक साथ मौजूद रहती है। इसीलिए साहित्य को पढ़ते हुए हमें अक्सर पात्रों या कथानकों में भी ऐसी ही द्वैधता दिखाई देती है—एक ओर सामाजिक मान्यताओं का पालन, दूसरी ओर उनकी आलोचना या उनसे मुक्त होने की आकांक्षा।
लेकिन ग्राम्शी के अनुसार, कॉमन सेंस कोई स्थिर या जड़ चीज़ नहीं। वह बदलता है, और उसी में से जन्म लेता है गुड सेंस—वह विवेक जो वास्तविक अनुभवों और सामाजिक जीवन की सच्चाइयों से निकलता है।
अच्छे साहित्य की सबसे बड़ी ताक़त यही है कि वह कॉमन सेंस की परतों को उजागर करता है, उनके भीतर छिपे गुड सेंस को सामने लाता है।
जब हम किसी उपन्यास या कहानी का विश्लेषण करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि—
1) लेखक किस तरह बड़े स्तर पर व्याप्त कॉमन सेंस (लोकधारणाओं, मिथकों, सत्ता द्वारा गढ़ी मान्यताओं) को सामने लाता है।
और फिर,
2) किस तरह पात्रों के संघर्ष, अनुभव या पीड़ा से कोई नया गुड सेंस उभरता है, जो अधिक आलोचनात्मक और वास्तविक है।
उदाहरण के लिए, सामाजिक यथार्थवादी साहित्य में अक्सर यही दिखता है कि पात्र शुरुआत में कॉमन सेंस की गिरफ़्त में होते हैं—वे ग़रीबी या शोषण को नियति मान लेते हैं। परंतु कथानक के भीतर अनुभव और संघर्ष उन्हें धीरे-धीरे यह समझाते हैं कि यह “ईश्वरीय इच्छा” नहीं बल्कि मनुष्य-निर्मित व्यवस्था है। यहीं से गुड सेंस जन्म लेता है।
इस बिंदु पर हम चाहें तो प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को याद कर सकते हैं।
इसलिए साहित्य के विश्लेषण में ग्राम्शी की दृष्टि हमें यह सिखाती है कि हमें केवल कथानक या सौंदर्य पर नहीं, बल्कि यह भी देखना है कि कहाँ कॉमन सेंस रूढ़ धारणाओं को पुनरुत्पादित कर रहा है और कहाँ गुड सेंस यानी आलोचनात्मक जागरूकता में रूपांतरित कर पा रहा है।
मूल्यांकन की यह प्रक्रिया साहित्य को मनोरंजन से ऊपर उठा सकती है, और सामाजिक आलोचना और परिवर्तन की ताक़त में बदलने की आकांक्षा की ओर, थोड़-सा ही सही, धकेल सकती है।
राष्ट्रीय-जनप्रिय और सांस्कृतिक संरचना (National-Popular and Cultural Formation)
ग्राम्शी ने ऐसी राष्ट्रीय-जनप्रिय (national-popular) साहित्यिक परंपरा पर बल दिया जो केवल अभिजन (elite) रुचियों तक सीमित न होकर जन-जीवन से गहराई से जुड़ती हो। पसंदगी का एक बड़ा हिस्सा कॉमन होता है…इस हिस्से में पड़ने वाले साहित्य को वे बड़ी आशा-भरी नज़रों से देखते हैं। पर इस श्रेणी में आने वाले साहित्य का मूल्यांकन करते समय हमें कुछ सवाल उठाने चाहिए। जैसे कि-
1) क्या पाठ का लोक-संस्कृति, जन-जीवन या सामूहिक संघर्षों से सार्थक जुड़ाव है?
या,
2) वह अभिजात, अलिप्त संवेदनाओं तक ही सीमित रहता है?
सब-अल्टर्न और उसका मौन (The Subaltern and Silence)
ग्राम्शी ने सब-अल्टर्न शब्द उन सामाजिक समूहों के लिए प्रयुक्त किया जो सत्ता से वंचित, प्रभावहीन और अपनी चेतना में विखंडित हैं। वे मौन हैं। उनके अनुसार यह मौन केवल अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि ऐसी संरचनात्मक असमर्थता है जिससे सब-अल्टर्न समूह अपने हितों को प्रभुत्वशाली ढाँचे में वैध रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते; इसीलिए ग्राम्शी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के उदय पर ज़ोर देते हैं जो इन अनुभवों को संगठित राजनीतिक भाषा, मुहावरे और शैली दे सकें।
बाद के विद्वानों—रणजीत गुहा और सब-अल्टर्न स्टडीज़ समूह—ने इस विचार को भारत के इतिहास-लेखन में विस्तारित किया। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने स्पष्ट किया कि भले ही सब-अल्टर्न बोले, उनकी आवाज़ सत्ता और ज्ञान के परिसरों में तब तक प्रवेश नहीं कर पाती जब तक किसी मध्यस्थ द्वारा उसे पुनर्व्याख्यायित न किया जाए (Can the Subaltern Speak?)।
संक्षेप में, ग्राम्शीय दृष्टि में सब-अल्टर्न का मौन संरचनात्मक है; उसे तोड़ना सांस्कृतिक संघर्ष और वर्ग के भीतर से निकले बुद्धिजीवियों के बिना संभव नहीं हो पाएगा।
किसी कलाकृति का मूल्यांकन करते समय हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि-
1) कौन-सी आवाज़ें अनुपस्थित, हाशिये पर, या केवल प्रभुत्वशाली दृष्टिकोणों के माध्यम से आ रहीं हैं? इनमें क्या भारी पड़ रहा है?
2) इन चुप्पियों को मुखर करने के लिए, उनको उभारने/पुनर्प्राप्त करने के लिए कौन-सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं?
ऐतिहासीकरण (Historicization)
ग्राम्शी की सांस्कृतिक दृष्टि का केंद्रीय आधार उसका ऐतिहासीकरण है। वे संस्कृति को किसी शाश्वत या निरपेक्ष सत्ता के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक ऐतिहासिक और सतत गतिशील प्रक्रिया मानते हैं, जो वर्गीय संघर्षों और सामाजिक शक्तियों की टकराहट से निर्मित होती रहती है। संस्कृति उनके लिए केवल विचारों का क्षेत्र नहीं, बल्कि श्रम, जीवनानुभव और सत्ता-संबंधों में गहराई से धँसा हुआ सामाजिक सत्य है।
ग्राम्शी लिखते हैं कि “every relationship of hegemony is necessarily a pedagogical relationship” अर्थात् हर वर्चस्व शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। वर्चस्वशाली वर्ग केवल बल के सहारे नहीं, बल्कि संस्कृति, शिक्षा और सामान्य धारणाओं- कॉमन सेंस (common sense) के निर्माण के ज़रिए समाज पर अधिकार क़ायम रखता है। यह कॉमन सेंस स्थिर नहीं होता है; यह ऐतिहासिक रूप से बदलता रहता है और इसी के भीतर आलोचनात्मक चेतना के बीज भी छिपे रहते हैं।
इसी संदर्भ में ग्राम्शी जैविक बुद्धिजीवियों (organic intellectuals) की आवश्यकता पर बल देते हैं जो शासक वर्ग की सेवा करने वाले पारंपरिक बुद्धिजीवियों से भिन्न होते हैं और जनता की ज़मीन से निकलते हैं और उनके बिखरे अनुभवों को ऐतिहासिक और राजनीतिक भाषा, टर्मिनालॉजी और टोन देते हैं। इस तरह वे संस्कृति को केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि निर्माण का साधन भी बना देते हैं।
साहित्य और कला पर ग्राम्शी की टिप्पणियाँ भी इसी ऐतिहासीकरण को दर्शाती हैं। वे दांते जैसे कवि को केवल एक “महान कवि” के रूप में नहीं, बल्कि अपने युग के राजनीतिक और सामाजिक उद्वेलन की उपज के रूप में समझते हैं।
दांते का डिवाइन कॉमेडी ग्राम्शी के लिए मध्यकालीन इटली की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना का प्रतीक है। इसी तरह लोक-कथाओं और धार्मिक विश्वासों को वे जनता के कॉमन सेंस का हिस्सा मानते हैं, जिन्हें समझने के लिए उनके ऐतिहासिक संदर्भ को देखना ज़रूरी है।
ग्राम्शी के लिए संस्कृति का अध्ययन तभी सार्थक है जब उसे ऐतिहासिक धरातल पर रखा जाए। बिना ऐतिहासिक विश्लेषण के संस्कृति की कोई भी व्याख्या अधूरी है, क्योंकि हर सांस्कृतिक रूप अपने भीतर सत्ता का तर्क और प्रतिरोध की संभावनाएँ, दोनों समेटे रहता है। यही दृष्टि उन्हें संस्कृति को वर्ग-संघर्ष का जीवित क्षेत्र और इतिहास के परिवर्तन का साधन समझने की ओर ले जाती है।
अतएव, किसी कृति के मूल्यांकन में हमें यह भी देखना चाहिए कि—
1) अमुक पाठ संदर्भित ऐतिहासिक कालखंड का किस तरह चित्रण करता है, कृति में किस वर्ग के प्रति सहानुभूति झाँक रही है…
2) क्या यथा-तथ्यता है या यथार्थ में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति है?
3) इस प्रवृत्ति का झुकाव किधर है? संक्षेप में, वह किन वर्ग-संयोजनों या विश्व-दृष्टियों की कल्पना करता है और किन दृष्टियों की आलोचना?
प्रतिरोध और प्रति-वर्चस्व (Resistance and Counter-Hegemony)
ग्राम्शी की दृष्टि में साहित्य और संस्कृति वर्चस्व (hegemony) के साधन भी हैं और उसके विरुद्ध चलने वाले प्रतिरोध की ज़मीन भी। वर्चस्व वहाँ सबसे प्रभावी होता है जहाँ वह सामान्य जीवन की भाषा और प्रतीकों में उतर जाता है, किंतु साहित्य अक्सर इसी धरातल पर उसकी दरारें उजागर करता है।
ग्राम्शी लिखते हैं: “The history of subaltern classes is necessarily fragmented and episodic” (Prison Notebooks)। यानी अधीनस्थ वर्गों की उपस्थिति हमें साहित्य और संस्कृति में बिखरे अंशों के रूप में मिलती है। यही बिखराव मौन प्रतिरोध का रूप लेता है।
साहित्य में यह प्रतिरोध अलग-अलग रूप धारण करता है। लोक-कथाएँ और लोक-गीत सत्ता की आधिकारिक भाषा से भिन्न एक वैकल्पिक स्मृति रचते हैं। यथार्थवादी उपन्यास अक्सर हाशिये के पात्रों को केंद्र में लाकर वर्चस्वशाली वर्ग की नैतिकता और भाषा को चुनौती देते हैं। व्यंग्य और लोक-भाषा का प्रयोग वर्चस्वशाली संस्कृति की गरिमा को भंग करता है, छेड़ता है। यह सब प्रतिरोध के रूप हैं—साहित्य का वह क्षेत्र जहाँ जनता अपनी आवाज़ दर्ज करती है, भले ही विखंडित, ढीले-ढाले और असंगत ढंग से ही ऐसा कर पाए।
लेकिन ग्राम्शी के लिए प्रतिरोध तभी निर्णायक बनता है जब वह काउंटर-हेजेमनी (प्रति-वर्चस्व) में बदलता है। वे लिखते हैं:
“The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born.” (Prison Notebooks)
यह नया तभी जन्म लेता है जब साहित्य और संस्कृति केवल असहमति न प्रकट करें, बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टि गढ़ें। उदाहरण के लिए, उन्नीसवीं शताब्दी के यथार्थवादी उपन्यासों ने न केवल अन्याय को दिखाया, बल्कि समाज की एक नई नैतिक और राजनीतिक चेतना भी निर्मित की। इसी तरह उपनिवेश-विरोधी साहित्य ने साम्राज्यवादी प्रभुत्व की भाषा को नकारते हुए जनता को आत्म-पहचान और सामूहिक इच्छा का नया आधार दिया। ग्राम्शी इसे “war of position” कहते हैं—लम्बा सांस्कृतिक संघर्ष, जिसमें प्रतीक, कथा, भाषा और संवेदना सभी युद्धक्षेत्र बन जाते हैं। साहित्य यहाँ जनता की सामूहिक चेतना को गढ़ने का साधन बन जाता है, और यहीं से प्रति-वर्चस्व का निर्माण संभव होता है।
संक्षेप में, साहित्य में प्रतिरोध जनता की मौन और बिखरी हुई आवाज़ है, जबकि प्रति-वर्चस्व वह संगठित रचनात्मक शक्ति है जो प्रभुत्वशाली संस्कृति के सामने एक वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करती है। ग्राम्शी की दृष्टि से कला और साहित्य का विश्लेषण इसी द्वंद्व को पकड़ने का प्रयास होना चाहिए।
इस प्रकार, किसी कृति के मूल्यांकन में हमें यह भी देखना चाहिए कि—
1) क्या टेक्स्ट प्रतिरोध के लिए वैचारिक/भावनात्मक संसाधन उपलब्ध कराता है?
2) क्या कृति एकजुटता, सामूहिक मुक्ति (solidarity, emancipation) या शक्ति-संरचनाओं के पुनर्संयोजन की ओर संकेत करती है?
व्यवहार में,
डिकेंस को आप परंपरागत बुद्धिजीवी की कोटि में रख सकते हैं—वे सामाजिक अन्याय की आलोचना तो करते हैं, पर बुर्जुआ ढाँचों से बाहर नहीं जाते।
जबकि न्गुगी वा थियोंग’ ओ (Ngũgĩ wa Thiong’o) को हम जैविक बुद्धिजीवी (organic intellectual) के रूप में पढ़ सकते हैं—जो साहित्य के माध्यम से प्रति-औपनिवेशिक लोकप्रिय चेतना (decolonial popular consciousness) को स्वर देते हैं। वे अफ्रीका में उपनिवेशवादी भाषा और संस्कृति के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए स्वदेशी भाषाओं में लिखते हैं। उनकी रचनाएँ यह दिखाती हैं कि साहित्य केवल यथार्थ का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि जनता की मुक्ति का साधन भी हो सकता है। न्गुगी का जोर इस बात पर है कि साहित्य को प्रतिरोध का औज़ार बनना चाहिए (Literature should not merely expose oppression but also participate in the cultural labour of emancipation)।
नया पथ से साभार

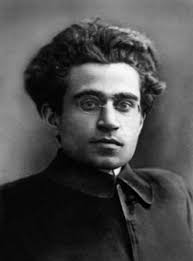



एंटोनियो ग्राम्शी पर महेश मिश्र का लेख बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हमारी राय में सभी रचनाकारों को इस लेख को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके जरिए ग्राम्शी दुनिया की मार्क्सवादी अवधारणा में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि मार्क्स ने अपनी स्थापना में पदार्थ/भौतिक पर ज्यादा जोर दिया जबकि ग्राम्शी ने चेतना/सांस्कृतिक पक्ष को सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तन में जरूरी बताया है। सामान्य अर्थों में कहा जा सकता है कि बिना “सांस्कृतिक-आधार” के आप “आर्थिक क्रांति के स्थायित्व” की गारंटी नहीं कर सकते हैं?