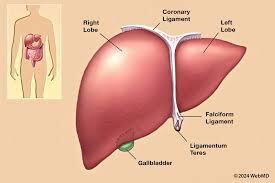भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग को समान बनाना
पुलाप्रे बालकृष्णन / अमन राज
फरवरी 2024 में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) कार्यालय द्वारा एक दशक से अधिक के अंतराल के बाद घरेलू उपभोग सर्वेक्षण के प्रकाशन से भारत में गरीबी दर का अनुमान लगाना संभव हो गया है। विश्व बैंक द्वारा अप्रैल 2025 में जारी किए गए ऐसे ही एक अनुमान ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है। यह अब तक गरीबी दर के बहुत कम होने की ओर इशारा करता है।
विश्व बैंक के अनुसार, “पिछले एक दशक में, भारत में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। अत्यधिक गरीबी (प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन) 2011-12 में 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.3 प्रतिशत हो गई…” (‘गरीबी और समानता संक्षिप्त: भारत’, 2025)। यदि यह वास्तव में एक सटीक विवरण है, तो यह संतोष की बात होगी, क्योंकि यह बताता है कि अत्यधिक गरीबी देश से लगभग गायब हो गई है।
उपभोग के एक पैमाने के रूप में ‘थाली भोजन’ गरीबी मापने का पारंपरिक तरीका, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने आधी सदी से भी पहले की थी, में सबसे पहले उस आय का निर्धारण करना शामिल है जिससे एक निश्चित कैलोरी मान का भोजन लिया जा सके, और फिर उससे कम आय वालों को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह एक शारीरिक दृष्टिकोण है और इसमें कुछ खूबियां हैं।
लेकिन, उदाहरण के लिए, वस्तुओं के उपभोग पर आधारित अन्य दृष्टिकोण भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक दृष्टिकोण यह मानता है कि मनुष्य भोजन को केवल उसकी कैलोरी सामग्री से कहीं अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें वह ऊर्जा, जिसे कैलोरी मापती है, पोषण और उससे मिलने वाली संतुष्टि को ध्यान में रखा जाता है। हमारा मानना है कि थाली भोजन इसी सोच को दर्शाता है, जिससे यह वास्तविक रूप में भोजन की खपत को मापने का एक स्वाभाविक विकल्प बन जाता है।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन के संयोजन के रूप में, थाली दक्षिण एशिया में भोजन की खपत की एक संतुलित और आत्मनिर्भर इकाई है, भले ही नामकरण इसके आसपास अलग-अलग हो। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने अनुमान लगाया है कि 2024 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में बताए गए मासिक व्यय में थालियों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी।
रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल ने चावल, दाल, सब्जी, रोटी, दही और सलाद से युक्त घर में पकाए गए थाली की लागत ₹30 आंकी है। इस मूल्य को अपनाने पर, हमने पाया कि 2023-24 में, दर्ज किए गए भोजन व्यय पर ग्रामीण आबादी का 50% और शहरी आबादी का 20% तक प्रति दिन दो थाली का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। यदि प्रतिदिन दो थाली को भोजन की खपत के न्यूनतम स्वीकार्य मानक के रूप में लिया जाता है।
हमारे निष्कर्षों में अंतर का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम यह नहीं मानते कि किसी परिवार की सारी आय भोजन पर खर्च करने के लिए उपलब्ध है। एक परिवार को केवल कार्यबल में बने रहने के लिए किराए, परिवहन, टेलीफोनी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर खर्च करना पड़ता है। अब, भोजन पर होने वाला खर्च शेष राशि के रूप में रह जाता है। इसलिए, हमने अपने अनुमान भोजन पर होने वाले वास्तविक खर्च पर आधारित किए हैं।
भोजन पर वास्तविक व्यय पर
यह माना जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भोजन की कमी से प्रभावी रूप से निपटती है। इसका आकलन करने के लिए, हमने पीडीएस के माध्यम से प्राप्त आपूर्ति के अनुमानित मूल्य सहित खाद्य उपभोग के मूल्य की गणना की है – चाहे वह खरीदी गई हो या मुफ्त। इस प्रकार उपभोग के मूल्य को समायोजित करने पर, दो थाली न खरीद पाने वाली आबादी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में घटकर 40% और शहरी क्षेत्रों में 10% रह जाता है। उल्लेखनीय है कि सब्सिडी वाले भोजन के बावजूद, शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी बहुत अधिक बनी हुई है।
पीडीएस की भूमिका
यह समझने के लिए कि भोजन की कमी को दूर करने के लिए पीडीएस का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, हमने व्यय वर्गों में प्रति व्यक्ति सब्सिडी का अनुमान लगाया। दिलचस्प बात यह है कि पीडीएस खरीद और आबादी के उन वर्गों द्वारा प्राप्त मुफ्त भोजन, जो एक दिन में दो से अधिक थाली खरीद सकते हैं, दोनों ही अधिक हैं।
उदाहरण के लिए, ग्रामीण भारत में, 90%-95% वर्ग में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त सब्सिडी, 0%-5% वर्ग में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त सब्सिडी का 88% है, जबकि पहले वर्ग का उपभोग व्यय तीन गुना से अधिक है, और हमारे अपने थाली सूचकांक के अनुसार इसे और समर्थन की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, शहरी भारत में, सब्सिडी व्यवस्था अत्यधिक प्रगतिशील है। लेकिन यहाँ भी लगभग 80% लोग पीडीएस से सब्सिडी वाली बिक्री और मुफ्त भोजन प्राप्त करते हैं, भले ही वे भी प्रति दिन दो से अधिक थाली खरीद सकते हों।
खाद्य वंचना और खाद्य सब्सिडी व्यवस्था की संरचना से संबंधित आँकड़ों के आधार पर, हम नीति निर्माण के तरीके पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले, खाद्य सब्सिडी के पुनर्गठन की गुंजाइश है, वितरण के निचले स्तर पर इसे बढ़ाया जा सकता है और ऊपरी स्तर पर इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि, हालिया उपभोग सर्वेक्षण से हमें पता चलता है कि एक बाधा का सामना करना होगा: 0%-5% फ्रैक्टाइल और 95%-100% फ्रैक्टाइल वाले व्यक्तियों के लिए अनाज की खपत लगभग समान है।
इससे पता चलता है कि चावल और गेहूँ, दोनों ही अनाजों की खपत का वांछित स्तर प्राप्त हो चुका है, क्योंकि सबसे अमीर लोग अपनी इच्छानुसार सभी अनाज खरीद सकते हैं। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सफलता की ओर इशारा करता है, क्योंकि इसने मुख्य भोजन की खपत को समान बना दिया है, साथ ही यह खाद्य अभाव को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की सीमाओं की ओर भी इशारा करता है। अनाज की खपत न केवल पूरी आबादी में अपने वांछित स्तर पर पहुँच गई है, बल्कि यह औसत घरेलू खर्च का केवल 10% ही है।
रसद और व्यय, दोनों ही दृष्टियों से, यह अपेक्षा करना अनुचित है कि सरकार किसी भी वर्ग को संपूर्ण खाद्यान्न वितरित कर सकती है। हालाँकि, एक मध्य मार्ग है, और वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से दालों के वितरण का विस्तार करना। वितरण के दोनों छोरों पर उपभोग के पैटर्न की आगे की तुलना में, हम पाते हैं कि अनाज के विपरीत, 0%-5% वर्ग में दालों की प्रति व्यक्ति खपत 95%-100% वर्ग की खपत का ठीक आधा है।
दालों की खपत:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उपयोग जनसंख्या की प्राथमिक खाद्य खपत को समान बनाने के लिए किया जा सकता है। दालों की खपत के वांछनीय स्तर को सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस का विस्तार वांछनीय और व्यवहार्य दोनों है – कई भारतीयों के लिए, प्रोटीन का एकमात्र स्रोत और एक बहुत महंगा खाद्य पदार्थ – वित्तीय पहलू को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के पुनर्गठन द्वारा संबोधित किया जा सकता है। 0%-5% के अनुपात में चावल और गेहूँ की प्रति व्यक्ति खपत का अर्थ है कि चावल और गेहूँ की पीडीएस पात्रता एक महत्वपूर्ण संख्या के लिए आवश्यक सीमा से कहीं अधिक है।
जनवरी 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को अनाज की आपूर्ति के लिए सब्सिडी व्यवस्था का विस्तार और कुछ राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को चावल का विशेष रूप से बड़ा हक, ज़रूरत को पूरा नहीं करते। इसके अलावा, सार्वजनिक धन के वैकल्पिक उपयोगों को देखते हुए, इनसे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। वितरण के निचले स्तर पर अनाज की वर्तमान पात्रता को हालिया उपभोग सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकतानुसार बताए गए स्तरों तक कम करने और ऊपरी स्तर पर इसे पूरी तरह से समाप्त करने से भारतीय खाद्य निगम के लिए भंडारण की आवश्यकता भी कम होगी, जिससे पर्याप्त लाभ होगा।
हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का विस्तार वंचित वर्ग की सबसे ज़रूरी खाद्यान्न, यानी दालों की ओर करने का प्रस्ताव रखा है, साथ ही उन लोगों के लिए सब्सिडी समाप्त करने का भी प्रस्ताव रखा है जिनका भोजन उपभोग एक उचित मानक, जैसे कि दिन में दो थाली, से अधिक है। अभी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोझिल और अप्रभावी दोनों है, क्योंकि यह संसाधनों को सीमित करती है। हमारा प्रस्ताव इसे संक्षिप्त बनाएगा, जिससे भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग को समान बनाने में मदद मिलेगी और सबसे गरीब परिवारों के उपभोग को अर्थव्यवस्था में देखे गए उच्चतम स्तर तक बढ़ाया जा सकेगा, जो एक वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण परिणाम है।