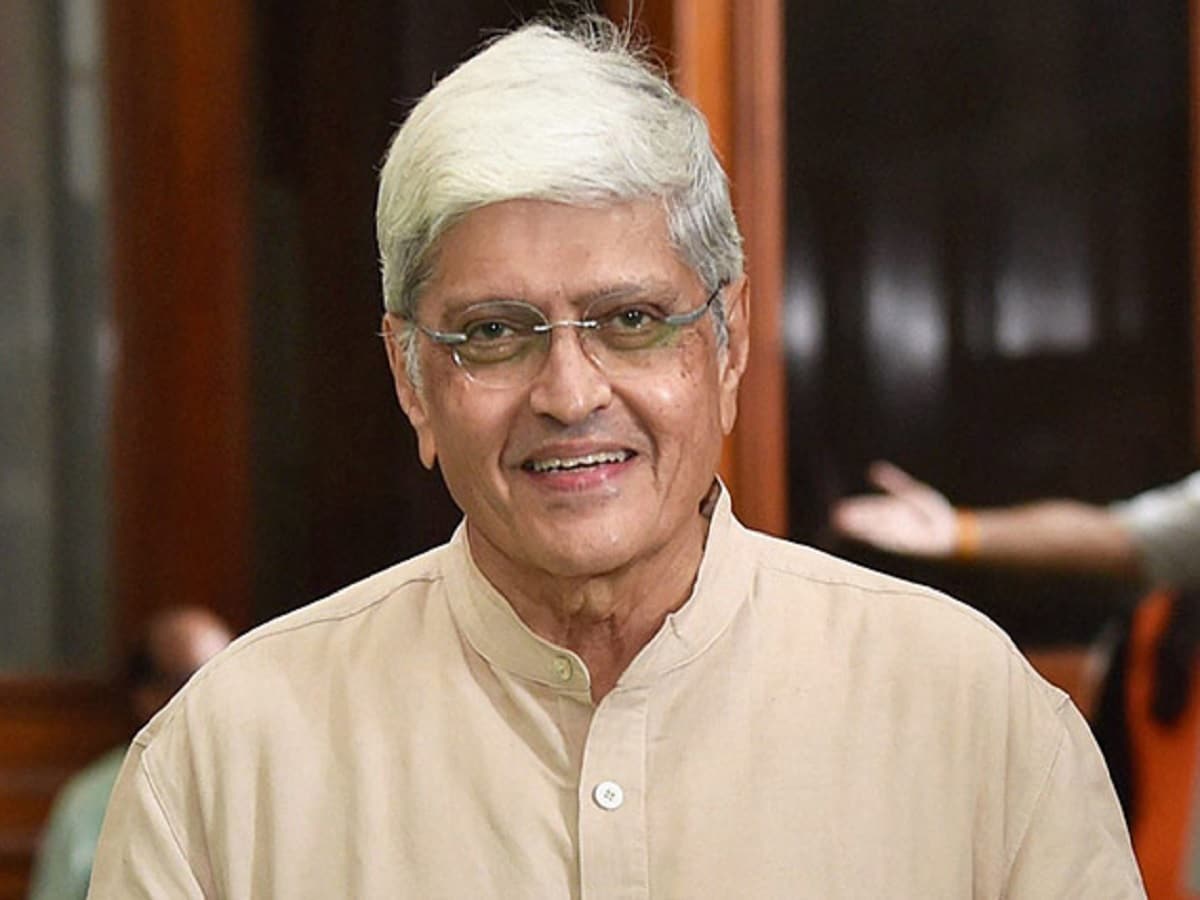हम भारतीयों का स्वभाव हो गया है कि विपत्ति आने पर हम हो हल्ला मचाते हैं। सरकारें भी जोर-शोर से राहत कार्य में जुट जाती हैं। यह स्थायी भाव हो गया है। हम पर्यावरण को की जिस तरह उपेक्षित नजरिये से देख रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक है। पिछले दिनों पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में प्रकृति का कहर बरपा था। पहले उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में सरकारों ने दौरा किया और पैकेज की घोषणा की लेकिन सबने माना की वह अपर्याप्त है। यहां तक कि देने वाले ने भी माना। लेकिन हम आपदा से कोई सीख नहीं ले रहे हैं। अपने लेख में गोपाल कृष्ण गांधी ने यही सवाल उठाया है और सलााह दी है कि हमें ठोस करने की जरूरत है। संपादक
आपदाः सरकारें समय और बजट के अनुसार राहत उपायों के साथ आगे आएँ
गोपाल कृष्ण गांधी
कलकत्ता में आई बाढ़ ‘कुछ खास’ थी।
“क्या आप ठीक हैं, महोदय?” मैंने कलकत्ता में अपने एक आदरणीय मित्र से टेलीफोन पर (जो काम कर रहा था) पूछा।
वह निश्चल था। न आत्म-दया, न ‘हे भगवान, हे भगवान, क्या कष्ट है!’ ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे यकीन था कि वह बारिश और उससे हुई तबाही से ज़्यादा विचलित नहीं हुआ था। और अगर था भी, तो वह मुझे ब्यौरों से परेशान नहीं करने वाला था।
एक और व्यक्ति भी उतना ही दृढ़ था, लेकिन ज़्यादा स्पष्ट। उसने बताया कि उनके घर में पानी भर गया था। और बिजली नहीं थी। “लेकिन,” उसने कहा, “हम बच गए हैं।” वह सभी पृथ्वीवासियों की ओर से बोल रहा हो सकता है। अभी तक।
एक तीसरे व्यक्ति ने अपने परिवार की किस्मत के बारे में खुलकर बताया। उसने बताया कि उसका घर एक तरह से ऊँचाई पर था, इसलिए बाढ़ का सबसे बुरा असर नहीं हुआ। यह वाकई खुशकिस्मती की बात थी क्योंकि उसकी माँ, जो नब्बे साल की हैं, अगर उन्हें पानी के स्तर से ऊपर रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता तो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती।
एक और दोस्त की बड़ी और बुज़ुर्ग बहन को एक ‘ऊँची’ जीप ढूँढ़नी पड़ी और अपने पूरी तरह से उजड़े हुए और ज़मीनी स्तर से कटे हुए घर से निकलकर अपने भाई के अपार्टमेंट तक किसी तरह गुज़ारा करना पड़ा।
कई परिवारों ने ट्रक किराए पर लिए ताकि अगर कोई आश्रय मिल जाए तो वहाँ पहुँच सकें।
लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास न तो पैसे थे और न ही ऊँचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने के साधन?
और उन बीमारों और कमज़ोरों का क्या, जो न तो अपनी मदद कर सकते थे और न ही किसी की मदद कर सकते थे? और वे लोग जो बाढ़ के दौरान बीमार पड़ गए, स्ट्रोक या दिल के दौरे का शिकार हो गए, और उन गर्भवती महिलाओं का क्या, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा?
कल्पनाशीलता इससे आगे जाने से हिचकिचाती है। फिर भी, यह कड़वी सच्चाई है कि कलकत्ता में अभी-अभी आई बाढ़, सिर्फ़ कलकत्ता में ही नहीं, बल्कि लगभग हर जगह आने वाले और भी बुरे संकटों का एक ट्रेलर मात्र है। आपके लिए यही जलवायु परिवर्तन है, मौसमों का ऋतुओं से बदलकर झटकों में बदल जाना।
ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र-स्तर में वृद्धि तटों और तटरेखाओं को बेरहमी से निगलने वाली है, और मैं यह कहकर कोई सनसनीखेज बात नहीं कह रहा हूँ कि जल्द ही भारत का भूभौतिकीय मानचित्र जैसा कुछ होगा जिसे हम दशकों से जानते हैं और भारत का भू-वास्तविक मानचित्र जैसा कुछ भी होगा – संकरा, सघन, जिसमें हिमालय जैसी परिचित विशेषताएँ होंगी जिनमें बिना बर्फ़ के चट्टानें दिखाई देंगी, नदियाँ अलग तरह से बहेंगी, आज के समुद्र तट समुद्र से घिरे होंगे।
अगर जलवायु परिवर्तन की मानव-निर्मित पीड़ा हमारे सामने है, तो भूकंपविज्ञानियों द्वारा भविष्यवाणी किए गए एक बड़े भूकंप की गूढ़ वास्तविकता भी हमारे कंधों पर दस्तक दे रही है।
हिमालय का आसन्न भविष्य, ग्लेशियरों के पिघलने और भूकंप के खतरे, दोनों के कारण, एक साथ होने वाली पीड़ा है।
लेकिन यह कॉलम इन ज्ञात जोखिमों के बारे में नहीं है। न ही इनके प्रति हमारी ज्ञात उदासीनता के बारे में।
यह अविश्वसनीय है कि हम हाल ही में कलकत्ता में हुए आघातों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। जीवन का ‘कार्य’ धीमा नहीं पड़ता।
त्योहारों और उत्सवों को फिर से शुरू करना होगा और हर आघात को भुला देना होगा। और सरकारें समय और बजट के अनुसार राहत उपायों के साथ आगे आएँ।
लेकिन मैं आगे आने वाली निश्चित विकट परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उससे जुड़े एक विषय पर बात कर रहा हूँ जिसके लिए 27 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने एक उल्लेखनीय भाषण दिया। जैसा कि अक्सर होता है, इस भाषण को वह ध्यान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। वैसे, राज्य और समाज द्वारा कड़ी कार्रवाई की माँग करने वाले कठोर संदेशों को वह ध्यान क्यों नहीं मिलता जो फलां व्यक्ति द्वारा फलां व्यक्ति की आलोचना करने और फलां व्यक्ति द्वारा फलां व्यक्ति से माफ़ी माँगने को मिलता है? तुकी देहरादून में 12वें सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे।
प्रतिक्रिया के बजाय एहतियात और रोकथाम के तरीके अपनाने की मांग करते हुए, तुकी ने कहा, “आपदा के बाद राहत देने में हम बेहतरीन हैं, लेकिन हमें पूर्व चेतावनी प्रणालियों, मज़बूत बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक प्रशिक्षण में और निवेश करना होगा और खंडित दृष्टिकोण से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा।” उन्होंने कहा कि परियोजनाएँ और शहरी नियोजन अक्सर अलग-अलग काम करते हैं, और फिर उन्होंने आपदाओं के एक और अहम पहलू—मानवीय पहलू—की ओर रुख किया। उन्होंने कहा, “हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर आँकड़े के पीछे एक मानवीय कहानी छिपी होती है। तवांग का एक किसान बेमौसम बारिश से अपनी फसलें खो देता है। किन्नौर का एक बच्चा भूस्खलन के कारण स्कूल से कट जाता है। केदारनाथ में एक परिवार बाढ़ के बाद घर फिर से बनाता है। उनके संघर्षों को हमारी नीतियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। विकास सिर्फ़ जीडीपी के बारे में नहीं है; यह सम्मान, सुरक्षा और आशा के बारे में है।”
मैं तुकी को नहीं जानता और मुझे उनके भाषण की रिपोर्ट से ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। पाठकों को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कॉलम उनका कोई प्रचार कर रहा है। भगवान न करे, बिलकुल नहीं। मैं तो बस इस बात से प्रभावित हूँ कि उन्होंने हमारी कमज़ोरियों और हमारी बेहद विकृत प्राथमिकताओं की हक़ीक़त पर कितनी गहरी नज़र डाली है।
लेकिन इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर मैं बात समाप्त करना चाहता हूँ।
आपदाओं के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करने के लिए सरकारों के पास धन की कमी क्यों होती है? मुख्यमंत्रियों को आपदा राहत के रूप में दी जाने वाली राशि से ज़्यादा की माँग क्यों करनी पड़ती है? सितंबर के अंत में कोलकाता में जो कुछ हुआ, उससे कुछ दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा भी गुज़र चुके हैं। गुड़गांव में बाढ़ के कारण दुनिया से कटे एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अनुभवी ने “राजनीतिक और नियुक्त कार्यपालिका की भारी विफलता” पर दुख जताया। बारिश से भीगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चिल्लाए, “मैं 1,600 करोड़ रुपये का क्या कर सकता हूँ?” उन्होंने कहा कि ज़रूरत 13,800 करोड़ रुपये की है।
केंद्र की अपनी निधि सीमाएँ हैं और राज्य सरकारों से यह पूछने के अपने कारण भी हैं कि क्या वे अपने आपदा राहत आवंटन और विधियों का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ चीज़ों के लिए पैसा कोई मुद्दा ही नहीं बनता? मैं समझ सकता हूँ कि देश की रक्षा और सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ केंद्र पर पूरा भरोसा किया जाना चाहिए कि कितना और कब खर्च करना है। इनके लिए धन की कमी नहीं की जा सकती। लेकिन प्राकृतिक आपदाएँ आतंक का एक रूप हैं जिनका नुकसान पहुँचाने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं होता, लेकिन फिर भी वे नुकसान पहुँचाती हैं। जिस तरह हम आक्रमणों या आतंकी हमलों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारियों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, उसी तरह हम प्राकृतिक उथल-पुथल के खिलाफ तैयारियों को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। हमारे जैसे देश में, आपदा प्रबंधन का एकमात्र (साझा नहीं) प्रभार संभालने वाला एक केंद्रीय मंत्री होना चाहिए जो रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जितना ही प्रमुख और विश्वासपात्र हो।
और उसे आपदा प्रबंधन जैसे सांसारिक अपरिहार्य कार्यों पर उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हम मंगल ग्रह पर पहुँचने, चाँद पर किसी भारतीय को उतारने और ग्रेट निकोबार को सिंगापुर, हांगकांग, सन सिटी और हॉलीवुड की उत्तर-आधुनिक प्रतिकृति बनाने जैसे दिव्य विकल्पों पर खर्च कर रहे हैं। उसे यह सुझाव देने में सक्षम होना चाहिए कि हम ओलंपिक की मेजबानी के विचार को टाल दें।
सच है, इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। मान, सम्मान नाम की भी कोई चीज़, किसी देश की काल्पनिक मजबूरियों जैसी। लेकिन क्या हमें शहर-दर-शहर, कस्बे-दर-कस्बे, खेत-दर-खेत बारिश और तूफ़ान, भूकंप और बाँध-फटने की भेंट चढ़ जाने देना चाहिए, सिर्फ़ इसलिए कि हम उस झटके का अंदाज़ा नहीं लगा पाए या उससे निपटने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए? अगर हम आसमान छू लें, भारतीय ओलंपियाड बन जाएँ, लेकिन जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वह गीली, फटी या झुलसी हुई हो, तो क्या इज्जत बचेगी, क्या मान और सम्मान?
हम लोग, जैसे कि मैंने जिन कलकत्तावासियों का उल्लेख किया है, दृढ़ और नवीन हो सकते हैं, हम अपनी पीड़ाओं पर विजय पा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में हमारी आंतरिक शक्तियों को सरकार की प्रतिक्रियाशील प्राथमिकताओं का समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका स्थान लेना चाहिए।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि पृथ्वी में भूकंप आए और दरारें पड़ जाएं, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, हिमालय में और उसके नीचे, इससे पहले कि ग्लेशियर पिघलने के कारण अचानक बाढ़ आ जाए और उसके बाद सूखी नदियों के तल में सूखा फैल जाए, इससे पहले कि चक्रवात हमारे तटों से भी बदतर स्थिति पैदा कर दें, हमें अपने वित्तीय और प्राथमिकता वाले सर्किटों को इस तरह से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है जो हमें आपदाओं और विपत्तियों से सुरक्षित कर सकें।
मंगल और चाँद कहीं नहीं जा रहे। ग्रेट निकोबार को अपनी शुद्ध हवा में साँस लेने की इजाज़त दी जा सकती है, हमारे महानगर की नहीं। ओलंपिक चार या आठ साल और इंतज़ार कर सकते हैं।
आगे आने वाली भयावहता की आशंका को केवल अथाह ख़तरे तक ही नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।द टेलीग्राफ ऑनलाइन से साभार