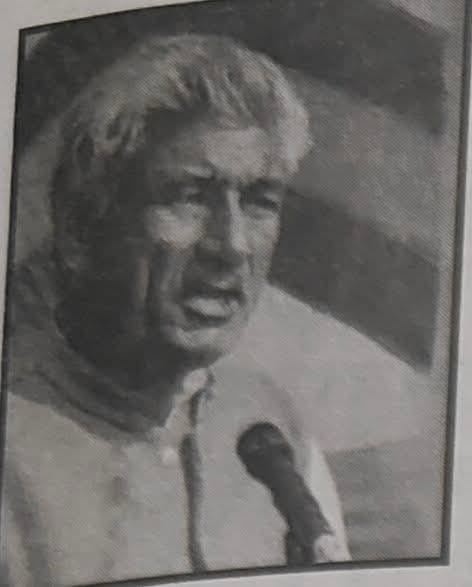न्यायाधीश की असहमति को छिपाना, न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करना
सुहृथ पार्थसारथी
संवैधानिक लोकतंत्र न केवल लिखित कानूनों से, बल्कि जैसा दक्षिण अफ़्रीकी क़ानून के प्रोफ़ेसर, एटियेन मुरेनिक द्वारा द्वारा कहे गए “न्याय की संस्कृति” से भी मज़बूत होते हैं। यानी, यह विचार कि सार्वजनिक शक्ति के हर प्रयोग की व्याख्या और बचाव किया जाना चाहिए। जैसा कि मुरेनिक ने कहा, “सरकार द्वारा दिया गया नेतृत्व उसके फ़ैसलों के बचाव में पेश किए गए मामले की तार्किकता पर आधारित होता है, न कि उसके अधीन बल से प्रेरित भय पर।”
भारत में न्यायाधीश राज्य से जवाबदेही की मांग करने के लिए नियमित रूप से इस सिद्धांत का सहारा लेते रहे हैं। लेकिन कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली को न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना द्वारा असहमति जताए जाने की मीडिया में आई खबरों से ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय की यह संस्कृति कॉलेजियम के द्वार पर ही समाप्त हो जाती है। जब न्यायालय द्वारा अपने सदस्यों के चयन की बात आती है, तो जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है।
व्यवस्था पर एक अभियोग इस तरह की असहमति आमतौर पर एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन कॉलेजियम और इसकी लगभग पूर्ण अस्पष्टता का मतलब है कि विरोध एक विफलता से ज्यादा एक निरर्थक कवायद साबित हुआ है। न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रस्ताव, जिसमें सिफारिश प्रदर्शित है, सर्वसम्मति का संकेत देता है। इसमें असहमति का कोई उल्लेख नहीं है। हमें न्यायमूर्ति नागरत्ना की आपत्ति के बारे में मीडिया में आई खबरों से ही पता चला। उन्होंने जो नोट लिखा था वह छिपा हुआ है, लेकिन हमें बताया गया है कि उनकी आपत्तियाँ “गंभीर” थीं। यह स्पष्ट नहीं है कि असहमति केंद्र सरकार के साथ साझा की गई थी या नहीं, जिसने सिफारिश के 48 घंटों के भीतर ही नियुक्ति की सूचना दे दी।
जो हम जानते हैं और जो हमें जानने की अनुमति है, उसके बीच का यह अंतर, उस व्यवस्था में निहित नियमों का प्रतीक है जो यह तय करती है कि हम अपने न्यायालयों में सदस्यों की नियुक्ति कैसे करते हैं। भारत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक ने शायद यह माना होगा कि ऐसे ठोस कारण थे जिनकी वजह से उम्मीदवार की पदोन्नति नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी उनके तर्क और बहुमत की प्रतिक्रिया, दोनों ही अज्ञात हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि असहमति केवल एक नियुक्ति को लेकर हो सकती है। यह संभव है कि कॉलेजियम के अन्य सदस्यों के पास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए भारी कारण रहे हों। लेकिन यह तथ्य कि जनता को कुछ भी नहीं बताया जाता, अपने आप में इस व्यवस्था पर एक दोषारोपण है – इसकी पारदर्शिता का अभाव, इसका लोकतांत्रिक पतन, और उन लोगों को अपनी बात समझाने से इनकार करना जिनके नाम पर यह काम करता है।
कॉलेजियम अपनी स्थापना के समय से ही पारदर्शिता के प्रति प्रतिरोधी रहा है। यह न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून का परिणाम है। “द्वितीय न्यायाधीश मामले” (1993) में स्थापित और “तृतीय न्यायाधीश मामले” (1998) में स्थापित, यह प्रणाली उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय के पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशों को प्रधानता प्रदान करती है। वे निजी तौर पर विचार-विमर्श करते हैं, न्यूनतम प्रकटीकरण के साथ निर्णयों को दर्ज करते हैं, और शायद ही कभी अपने तर्कों की व्याख्या करते हैं।
2017 की शुरुआत में, कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव प्रकाशित करना शुरू किया। लेकिन ये प्रस्ताव बहुत ही कम थे और औपचारिक घोषणाओं से ज़्यादा कुछ नहीं थे। 2018 में थोड़े समय के लिए, न्यायालय ने कॉलेजियम के निर्णयों और अस्वीकृतियों के विस्तृत कारण अपलोड किए। हालाँकि, यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि यह तर्क दिया गया कि खुलासे से प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच सकती है।
. न्यायमूर्ति नागरत्ना की असहमति गोपनीयता के इस दुराग्रह की कीमत को उजागर करती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश की आपत्ति भी जनता के लिए अति संवेदनशील मानी जाती है, तो हमें यह पूछना होगा कि क्या कॉलेजियम ने न केवल अस्पष्टता को अपनाया है, बल्कि जवाबदेही को पूरी तरह से नकार दिया है।
कमजोर बचाव
अपने कारणों को गोपनीय रखने का बचाव हमेशा दो दावों पर टिका रहा है: यह कि खुलापन उन उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकता है जिनका चयन नहीं होता, और यह कि इससे व्यवस्था राजनीतिक दबावों के सामने आ जाएगी। उचित जाँच-पड़ताल करने पर, दोनों ही दावे ध्वस्त हो जाते हैं।
निस्संदेह, पारदर्शिता और प्रतिष्ठागत निष्पक्षता का मेल सावधानी से करने की आवश्यकता है। लेकिन अन्य संवैधानिक लोकतंत्र इसे भारत से बेहतर तरीके से प्रबंधित करते प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन का न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने मानदंड खुले तौर पर निर्धारित करता है और रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि उम्मीदवारों का मूल्यांकन कैसे किया गया। दक्षिण अफ्रीका में, उच्च न्यायिक पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार न्यायिक सेवा आयोग द्वारा लिया जाता है, और उनकी उपयुक्तता पर सार्वजनिक रूप से बहस की जाती है। दोनों ही प्रणालियाँ “निर्बाध” नहीं हैं, बल्कि दोनों ही इस मान्यता से आगे बढ़ती हैं कि वैधता “खुलेपन” से आती है।
इसके विपरीत, भारत कॉलेजियम को एक गुप्त सभा मानता आ रहा है। यहाँ तक कि असहमति का अस्तित्व भी हम तक लीक के ज़रिए ही पहुँचता है। अगर प्रतिष्ठा को होने वाला नुकसान एक वास्तविक चिंता है, तो इसका समाधान इसे कम करने के लिए सावधानीपूर्वक खुलासे की संरचना में निहित होना चाहिए। औचित्य को पूरी तरह से नकारना इसका समाधान नहीं हो सकता। और अगर राजनीतिक दबाव का डर है, तो गोपनीयता शायद ही इसे रोक पाए।
आखिरकार, कार्यपालिका कॉलेजियम की असुविधाजनक सिफारिशों को टालती और टालती रहती है। वह पुनर्विचार के लिए नाम लौटा सकती है या पुनः सिफारिश होने पर, उसे लंबित रख सकती है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति का वारंट जारी करने से पहले ही रुक सकती है।.
यहाँ दांव भारत के लोकतंत्र के मूल में है। आज चुने गए न्यायाधीश भारत के सबसे ज़रूरी संवैधानिक प्रश्नों के परिणामों को आकार देंगे, जिनमें नागरिक स्वतंत्रता से लेकर कार्यपालिका की सीमाओं और केंद्र व राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन तक के मुद्दे शामिल हैं। जब नागरिकों को बिना किसी कारण के केवल यह बताया जाता है कि किसी न्यायाधीश को पदोन्नत किया गया है, या जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश की असहमति को गोपनीयता में छिपाया जाता है, तो संस्थागत वैधता समाप्त हो जाती है। हम अपनी अदालतों से राज्य के अन्य अंगों से जवाबदेही पर ज़ोर देने की अपेक्षा बिल्कुल उचित ही करते हैं। लेकिन ऐसा करके, क्या वे अपने लिए छूट का दावा कर सकते हैं?
न्यायमूर्ति नागरत्ना की असहमति ने न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति को नहीं रोका है। वास्तव में, यह संभव है कि कॉलेजियम के अन्य सदस्यों के पास उनकी नियुक्ति का समर्थन करने के अच्छे कारण रहे हों। वे क्या थे, यह हम कभी नहीं जान पाएँगे। लेकिन यहाँ बड़ा मुद्दा एक नाम से आगे तक फैला हुआ है। यह इस बात से संबंधित है कि क्या न्यायालय उसी सिद्धांत पर चलने के लिए तैयार है जिसे वह राज्य के हर अन्य अंग पर थोपना चाहता है: कि सार्वजनिक शक्ति के प्रत्येक प्रयोग को उचित ठहराया जाना चाहिए।
कई लोकतंत्रों में, गैर-निर्वाचित न्यायाधीशों द्वारा कानूनों को रद्द करने की चिंता को बहुसंख्यकवाद-विरोधी कठिनाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर जनता द्वारा चुने न गए लोग ही इतने अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है? पहली नज़र में, यह चिंता वास्तविक लगती है। लेकिन यह लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। लोकतंत्र केवल संख्याबल के आधार पर बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। सही ढंग से समझा जाए, तो यह इससे कहीं अधिक है: नागरिकों के बीच एक साझेदारी जो अधिकारों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि स्वतंत्रता और समानता सार्वजनिक जीवन का आधार बनें। गैर-निर्वाचित न्यायाधीश कानून की व्याख्या करके और बहुसंख्यकों की ज्यादतियों से अधिकारों की रक्षा करके यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यही कारण है कि संविधान एक अनिर्वाचित न्यायपालिका को असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। न्यायाधीशों का उद्देश्य स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, सरकार पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। ऐसा करके, वे लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करते, बल्कि उसकी सर्वोच्च आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।
कॉलेजियम को सुधार स्वीकार करना होगा
हालाँकि, न्यायपालिका को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्वयं जवाबदेही के सबसे कड़े मानकों पर खरा उतरना होगा। कॉलेजियम अक्सर न्याय के मामले में गोपनीयता की संस्कृति में सिमट गया है। जब तक यह सुधारों को स्वीकार नहीं करता, तब तक यह उस वैधता को कम करने का जोखिम उठाता है जिस पर इसका अधिकार टिका है। अतीत में बदलाव के कई अवसरों को ठुकरा दिया गया है; हर कदम आगे बढ़ने के बाद दो कदम पीछे हट गए हैं, और हर पीछे हटने से पारदर्शिता और ईमानदारी के वे मूल्य नष्ट होते गए हैं जिन पर लोकतंत्र निर्भर करता है।
एक न्यायपालिका जो स्वयं को खुलेपन के उन्हीं मानकों के अधीन रखेगी जिनकी वह दूसरों से अपेक्षा करती है, उसकी स्वायत्तता कमज़ोर नहीं होगी। इसके विपरीत, वह अपनी स्वतंत्रता को जनता के विश्वास और भरोसे पर और अधिक मज़बूती से स्थापित करेगी। द हिंदू से साभार
. सुहृथ पार्थसारथी मद्रास उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं