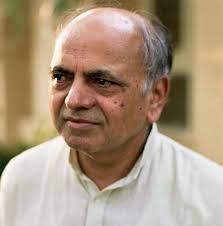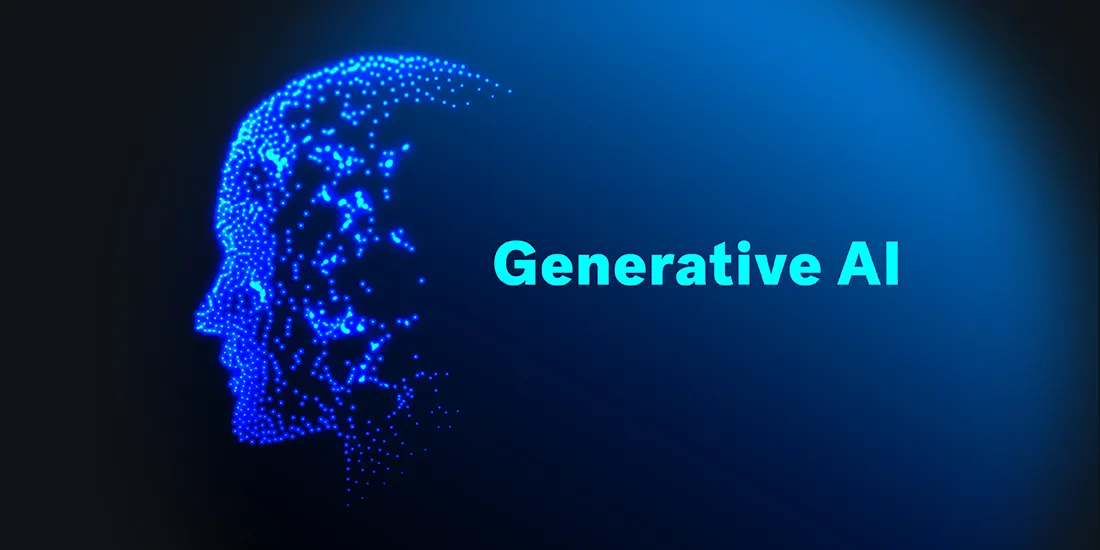जवाब का इंतजार है
जी. एन. डेवी
एक साल बाद, लंबे समय से प्रतीक्षित और विलंबित जनगणना प्रक्रिया शुरू होगी। यह सबसे पहले 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में शुरू होगी और बाद में 1 मार्च 2027 से भारत के बाकी हिस्सों में। हर जनगणना से पर्याप्त और सटीक डेटा मिलता है, जो विभिन्न कल्याणकारी नीतियों को तय करने के लिए आवश्यक होता है।

लेकिन जनगणना मूल रूप से 2021 में होनी थी। हालांकि सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद भी देरी का कारण नहीं बताया है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि कारण क्या हो सकता है।
चर्चा है कि हर दशक के पहले साल में जनगणना कराने की पुरानी परंपरा को बदलने का संबंध संसद में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में संभावित बढ़ोतरी से हो सकता है। संविधान संशोधन 84 (2002) और 87 (2003) के अनुसार, सांसदों की संख्या काफी बढ़ जाएगी।
अगर 2021 की जनगणना तय समय पर होती, तो संविधान संशोधन के अनुसार, अगला जनगणन 2031 में होने के बाद ही परिसीमन प्रक्रिया शुरू होती। लेकिन अब, 2029 के आम चुनाव से पहले ही परिसीमन प्रक्रिया होने की संभावना है। इसलिए, जनगणना में यह देरी, यह कह सकते हैं कि, परिसीमन प्रक्रिया को जल्द कराने का कारण बनी है। इसका एकमात्र आधार अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली जनगणना होगी।
संविधान के अनुच्छेद 246 के संदर्भ में बनाई गई सातवीं अनुसूची के नियम 69 के अनुसार जनगणना कराने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। यह अनुच्छेद “केंद्रीय सूची” के बारे में बताता है; और नियम 69 में सिर्फ़ एक शब्द है – “जनगणना”।
स्पष्ट है कि इस मामले में सरकार के पास पूरी शक्ति है; इसलिए, देश को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जनगणना कैसे डिज़ाइन की जाती है और कैसे की जाती है। इस संदर्भ में, तीन महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने चाहिए।
पहली बात जाति जनगणना के ढांचे से जुड़ी है। इस साल जून में सरकार ने घोषणा की कि राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना की जाएगी। पिछली जाति गणना 1931 में हुई थी; उस समय भारत का नक्शा बहुत अलग था।
उस गणना के आधार पर, उन समुदायों की जनसंख्या का पता लगाना संभव था जिन्हें हम अब डीनोटिफाइड और घुमंतू जनजाति के रूप में पहचानते हैं।
मैं यह भी बता दूँ कि डीएनटी को ‘जनजाति’ नहीं माना जाता, जैसा कि अनुसूचित जनजाति या जनजाति शब्द का मतलब होता है। डीएनटी वे समुदाय हैं जो बाकी भारतीय समाज से अलग हो गए – जाति और जनजाति दोनों से – 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के कारण, जो लॉर्ड मेयो के गवर्नर-जनरल रहते हुए औपनिवेशक प्रशासन द्वारा लाया गया था।
इन समुदायों को गलत तरीके से “अपराधी” कहा गया, उन्हें “सेटलमेंट” नामक नरम जेलों में रखा गया, उनसे सड़कों और रेलवे लाइन जैसी कड़ी और बिना वेतन वाली मजदूरी करवाई गई और उन्हें “जन्म से अपराधी” माना गया। इसका मतलब था कि समुदाय में पैदा होने वाला हर बच्चा अपराध का कलंक लेकर पैदा होता था। औपनिवक काल के दौरान कई कानूनों में और भी समुदायों को शामिल किया गया, जिससे – 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर – 1991 के आसपास उनकी जनसंख्या लगभग पांच करोड़ या उससे अधिक होने का अनुमान था।
1950 के दशक की शुरुआत में इन नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। 2014 में डीनोटिफाइड, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने के अलावा, उनकी स्थिति सुधारने के लिए बहुत कम किया गया है। जनगणना अधिकारियों के लिए सवाल यह है: क्या वे जनगणना ढांचे में ऐसे प्रावधान शामिल करेंगे जिससे देश को डीएनटी जनसंख्या की सही संख्या पता चल सके?
जाति के आधार पर गणना से मदद नहीं मिलेगी, जनगणना फॉर्म में डीएनटी पहचान से संबंधित एक विशिष्ट प्रश्न शामिल करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो देश कभी भी डीएनटी के मानवाधिकारों और कल्याण के मुद्दे को हल नहीं कर पाएगा।
दूसरा सवाल और भी मुश्किल है। यह धर्म से संबंधित डेटा इकट्ठा करने से जुड़ा है। घुमंतू समुदायों के साथ काम करते हुए, मैंने अक्सर ऐसे परिवार देखे हैं जो दो अलग-अलग धर्मों का पालन करते हैं।
कालबेलिया, मदारी, गारुड़ी, बहुरूपिया और गाड़ी लोहार अक्सर कहते हैं कि उनके परिवार में कुछ लोग मुस्लिम और कुछ हिंदू हैं। इस तरह के दो धर्म मानने वाले समुदाय गुजरात, राजस्थान और कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाए जाते हैं।
इसी तरह की स्थिति नॉर्थ-ईस्ट के सीमावर्ती इलाकों में भी है।
जनगणना में धर्म के बारे में पूछा जाने वाला सवाल लोगों को सिर्फ एक धर्म का नाम बताने या कोई धर्म न बताने के लिए मजबूर करता है, जिससे दो या कई धर्म मानने वाले लोग छूट जाते हैं। जनगणना में धर्म के बारे में ऐसे सवाल शामिल करने चाहिए जो धार्मिक पहचान को गलत न दिखा सकें। धर्म की गिनती का एक और जटिल पहलू आदिवासी समुदायों से जुड़ा है।
देश की कुल आबादी का लगभग 9% आदिवासी आबादी है, लेकिन अभी लगभग 13 करोड़ लोगों को अक्सर हिंदुओं और कुछ मामलों में ईसाइयों के साथ ही गिना जाता है।
2011 की जनगणना के अनुसार, 121 करोड़ लोगों में से 96.62 करोड़ हिंदू, 17.22 करोड़ मुस्लिम, 8.39 करोड़ ईसाई, 2.08 करोड़ सिख, 0.8 करोड़ बौद्ध, 0.4 करोड़ जैन और 0.8 करोड़ “अन्य” धर्म के थे। जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया, उनकी संख्या 28 लाख थी।
आखिरी दो श्रेणियों को जोड़ने पर कुल संख्या एक करोड़ से थोड़ी ज्यादा होती है। भारत में लगभग 13 करोड़ आदिवासी हैं। मानवशास्त्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि वे मंदिर आधारित धर्मों का पालन नहीं करते। क्या उन्हें जनगणना करने वालों की मर्ज़ी से ‘हिंदू’ या ‘ईसाई’ जैसी श्रेणियों में डाला जाएगा? जनगणना को संविधान में दिए गए किसी भी धर्म को मानने के मौलिक अधिकार का ध्यान रखना चाहिए।
तीसरा सवाल भाषा से जुड़ा है। पिछली जनगणना में, नागरिकों द्वारा बताई गई 1,369 “मातृभाषाओं” को 121 “भाषाओं” में ‘समूहीकृत’ कर दिया गया। यह काम बहुत अवैज्ञानिक तरीके से किया गया। जनगणना के अनुसार, कोई भाषा तभी ‘भाषा’ मानी जाएगी जब उसे कम से कम 10,000 लोग बोलते हों।
भाषा विज्ञान का कोई भी सिद्धांत इस अजीब तर्क को नहीं मानता। इसी तरह, कई भाषाओं को आस-पास की बड़ी भाषा का उप-सेट बताया गया। उदाहरण के लिए, भोजपुरी, जिसे पांच करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी भाषा मानते हैं, उसे हिंदी का उप-सेट बताया गया। सिर्फ हिंदी के मामले में ही ऐसे 55 और मामले थे।
जनगणना नागरिकों की भाषाई पहचान को क्यों नकारना चाहती है? उसे सांस्कृतिक तथ्यों और भाषाई वास्तविकताओं को बिना किसी बड़े बदलाव के, जैसा है वैसा ही दिखाना होगा।
1880 से चली आ रही यह प्रक्रिया, जिस पर आज भी लोगों का भरोसा है, का इस्तेमाल किसी एक धर्म या भाषा को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, तो जनगणना आयुक्त चुनाव आयुक्त जैसा ही दिखेगा। असल में, पहले से ही विवादित सीमांकन की प्रक्रिया और भी मुश्किल हो सकती है। द टेलीग्राफ ऑनलाइन से साभार
जी.एन. देवी एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं।