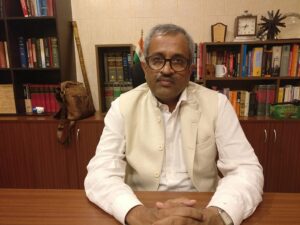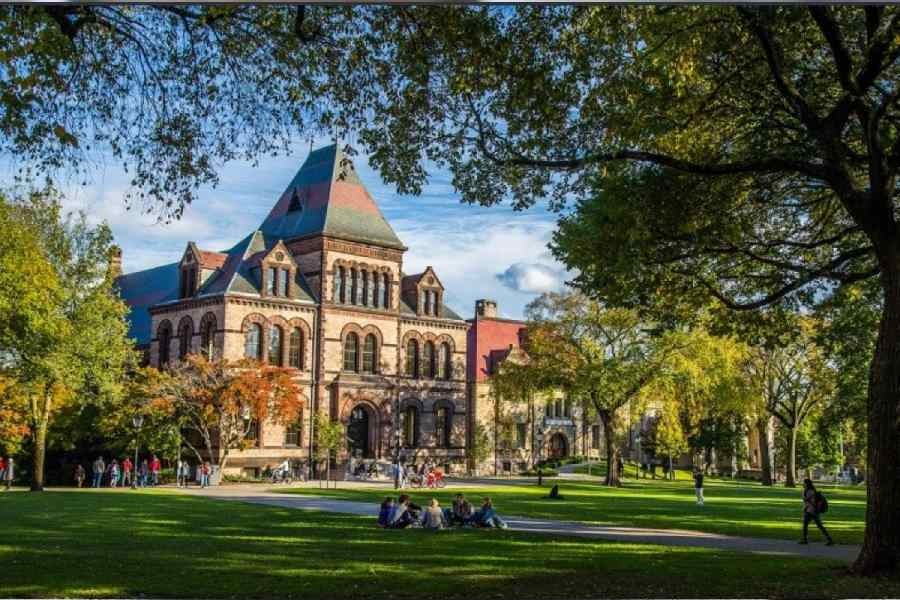संवैधानिक इतिहास में संशोधनवाद का एक पाठ
संजय हेगड़े
संवैधानिक इतिहास में एक शांत संशोधनवाद का बीजारोपण किया जा रहा है। कुछ टिप्पणीकार अब तर्क देते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव भारत के संविधान के वास्तविक निर्माता थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने पहले से तैयार संविधान को केवल और अधिक परिष्कृत किया। यह तर्क भले ही अध्यात्मवादी लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भारत की स्थापना की कहानी में दलितों की भूमिका को कम करने और उस नैतिक बल को मिटाने का प्रयास है जो बी.आर. आंबेडकर ने गणतंत्र के निर्माण में लगाया था।
पूरक, प्रतिस्पर्धी नहीं दोनों व्यक्ति संविधान के निर्माण के लिए अपरिहार्य थे, लेकिन उनकी भूमिका पूरी तरह से अलग थी। सर बी एन राव, एक प्रतिष्ठित सिविल सेवक और न्यायविद, जुलाई 1946 में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। उनका कार्य तकनीकी और प्रारंभिक था। राव ने ब्रिटिश भारत में, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रारूपण में मदद की थी। ग्यारह साल बाद, उन्हें संविधान सभा की समितियों की रिपोर्टों और अन्य संविधानों के अपने अध्ययन के आधार पर संविधान का एक कार्यकारी मसौदा तैयार करना था।
उन्होंने अमेरिकी, कनाडाई, आयरिश, ऑस्ट्रेलियाई और वीमर मॉडल की जांच की और फेलिक्स फ्रैंकफर्टर और हेरोल्ड लास्की जैसे न्यायविदों से परामर्श किया। अक्टूबर 1947 में, उन्होंने 243 लेखों और 13 अनुसूचियों के साथ अपना मसौदा प्रस्तुत किया। राव के दस्तावेज़ ने सभा को एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान किया।
आंबेडकर का कार्य एक अलग ही स्तर का था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, उन्हें एक कानूनी मसौदे को एक राजनीतिक अनुबंध में बदलना था। उन्होंने संविधान को विभाजन की उथल-पुथल, महात्मा गांधी की हत्या के दौर से गुज़ारा और संविधान सभा में इसके प्रावधानों का, हर खंड का, बचाव किया। उनकी ज़िम्मेदारी न केवल पाठ को नया रूप देना था, बल्कि तीव्र रूप से विभाजित हितों के बीच आम सहमति बनाना भी था। राव ने इसका ढाँचा तैयार किया। आंबेडकर ने इसे न्याय का एक जीवंत साधन बनाया।
आंबेडकर ने राव के योगदान को कभी नकारा नहीं। 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा को दिए अपने समापन भाषण में उन्होंने कहा: “जो श्रेय मुझे दिया जाता है, वह वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को जाता है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया था।”
उन्होंने यह भी कहा, “इसका कुछ श्रेय प्रारूप समिति के सदस्यों को भी जाता है, जिन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, 141 दिनों तक बैठक की… इसका कहीं ज़्यादा श्रेय संविधान के मुख्य प्रारूपकार श्री एस.एन. मुखर्जी को जाता है। जटिल से जटिल प्रस्तावों को सरलतम और स्पष्ट कानूनी रूप में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता, और न ही उनकी कड़ी मेहनत की क्षमता, की बराबरी शायद ही कोई कर सके।”
इस प्रकार, जिन शब्दों का प्रयोग अक्सर यह दावा करने के लिए किया जाता है कि संविधान के वास्तविक रचयिता आंबेडकर नहीं, बल्कि राव थे, वास्तव में इसके विपरीत हैं। आंबेडकर ने राव के कार्य को एक “रफ़ ड्राफ्ट” कहा था, न कि एक पूर्ण पाठ। प्रारूप समिति और संविधान सभा ने उस कच्चे माल को उस दस्तावेज़ में बदल दिया जो अंततः जनवरी 1950 में लागू हुआ। न ही ऐसा कोई प्रमाण मौजूद है जो यह दर्शाए कि राव ने कभी संविधान के रचयिता होने का दावा किया था। उस समय आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके पत्राचार से सम्मान और सहयोग का भाव प्रकट होता है। उन्हें “संविधान का जनक” घोषित करने का वर्तमान प्रयास, अभिलेखों और राव की अपनी विनम्रता, दोनों को विकृत करता है।
राजनीतिक मकसद
राव को ऊपर उठाने और आंबेडकर को हाशिए पर डालने का अभियान सिर्फ़ विद्वत्ता से प्रेरित नहीं है। यह इस विचार से असहजता को दर्शाता है कि एक दलित विचारक गणतंत्र की स्थापना के केंद्र में खड़ा हो सकता है। राव को संविधान के प्रमुख लेखक के रूप में पुनः स्थापित करना जातिगत विशेषाधिकार के लिए लेखकत्व को पुनः प्राप्त करने का एक प्रयास है। यह आंबेडकर की क्रांतिकारी विरासत को दबाता है और एक सामाजिक क्रांति को नौकरशाही की कवायद में बदल देता है। संविधान कोई निष्फल कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। यह, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक सामाजिक घोषणापत्र है जो व्यक्ति की गरिमा का वादा करता है। इसका जन्म संघर्ष, आशा और मुक्ति से हुआ है। यह सत्ता की मेज पर उत्पीड़ितों के आगमन का प्रतिनिधित्व करता है। आंबेडकर को इससे अलग करना इसकी आत्मा को छीनने के समान है।
संविधान सभा में आंबेडकर की उपस्थिति अपने आप में एक निर्णायक राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिणाम थी। वे मूल रूप से बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद वह सीट पाकिस्तान चली गई। कांग्रेस के भीतर कई लोग अतीत के मतभेदों के कारण उन्हें वापस लाने में हिचकिचा रहे थे। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से यह समस्या सुलझ गई।
हालाँकि गांधी और आंबेडकर के बीच पृथक निर्वाचिका मंडल को लेकर मतभेद थे, फिर भी गांधी ने ज़ोर देकर कहा कि आंबेडकर को संविधान सभा का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा कि अगर अनुसूचित जातियों को संविधान निर्माण से बाहर रखा गया तो कोई भी संविधान वैधता का दावा नहीं कर सकता।
परिणामस्वरूप, आंबेडकर बंबई प्रेसीडेंसी से पुनः निर्वाचित हुए। गांधी का आग्रह एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था। 1947 में, जब राष्ट्र धर्म के आधार पर विभाजित था, एक अलग-थलग दलित नेतृत्व इस विभाजन को और गहरा कर सकता था। आंबेडकर को शामिल करके, गांधी ने एक ऐसे संकट को रोका जो नए गणराज्य के जन्म के समय ही उसे कमज़ोर कर सकता था। आंबेडकर के बाद के नेतृत्व ने उस समावेश को सही साबित किया। उन्होंने संविधान निर्माण को एक नैतिक उद्यम में बदल दिया जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बाँध दिया।
राव के मसौदे ने संविधान को व्यवस्था और संरचना प्रदान की। आंबेडकर ने संविधान को नैतिक गहराई प्रदान की। मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों और कर्मकारिता संबंधी प्रावधानों पर उनकी छाप है। विधान सभा में उनके भाषणों ने संविधान को एक जीवंत नैतिक दर्शन बना दिया।
आंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता विफल हो जाएगी। उन्होंने कहा, “हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारते रहेंगे? अगर हम इसे लंबे समय तक नकारते रहेंगे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द दूर करना होगा, वरना असमानता से पीड़ित लोग उस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से खड़ा किया है।” यह चेतावनी आज भी भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे शक्तिशाली नैतिक कथन है।
भूलने का ख़तरा
प्रत्येक गणराज्य को अपनी स्मृति की रक्षा करनी चाहिए। राव को आंबेडकर से ऊपर उठाने का प्रयास, संविधान की क्रांतिकारी भावना को नष्ट करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। यह संविधान की स्थापना को सामाजिक परिवर्तन के बजाय तकनीकी दक्षता के रूप में प्रस्तुत करता है। आंबेडकर का सम्मान करने का अर्थ राव को कमतर आंकना नहीं है। दोनों ने गणतंत्र की निष्ठापूर्वक सेवा की। लेकिन संविधान एक कानूनी ढाँचे से कहीं अधिक है। यह राष्ट्रीय उद्देश्य का एक कथन है। इसके लिए एक विद्वान की सटीकता की आवश्यकता थी, लेकिन एक सुधारक के दृढ़ विश्वास की भी। आंबेडकर वह सुधारक थे।
जब संविधान को अपनाया गया, तो नेहरू, पटेल और प्रसाद समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से आंबेडकर की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया। किसी ने भी यह नहीं कहा कि राव संविधान के मुख्य लेखक थे। वे एक पाठ का मसौदा तैयार करने और राष्ट्र की अंतरात्मा को आकार देने के बीच के अंतर को समझते थे।
राव एक कुशल सलाहकार के रूप में प्रशंसा के पात्र हैं। आंबेडकर संविधान के नैतिक निर्माता के रूप में श्रद्धा के पात्र हैं। संविधान औपनिवेशिक शासन की शांति में नहीं, बल्कि विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या और जातिगत उत्पीड़न की छाया में लिखा गया था। आंबेडकर को इसके केंद्र में रखना प्रतीकात्मक उदारता नहीं, बल्कि यह संदेश था कि भारत की नई व्यवस्था उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगी जो कभी इससे वंचित थे।
आंबेडकर ने कभी भी अकेले लेखक होने का दावा नहीं किया। फिर भी, प्रारूप समिति का उनका नेतृत्व, हर खंड का उनका बचाव, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उनके दृष्टिकोण ने भारतीय गणराज्य को परिभाषित किया है। उनकी भूमिका को कम करना गणराज्य के मूल वादे के साथ विश्वासघात है। राव ने इस ढांचे का निर्माण किया; आंबेडकर ने इसे न्याय के साथ प्रस्तुत किया। सर बी.एन. राव संविधान निर्माता के रूप में कृतज्ञता के पात्र हैं। डॉ. बी.आर. आंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता और नैतिक संस्थापक बने हुए हैं।
उस सत्य को नकारना गणतंत्र को नकारना है। द हिंदू से साभार