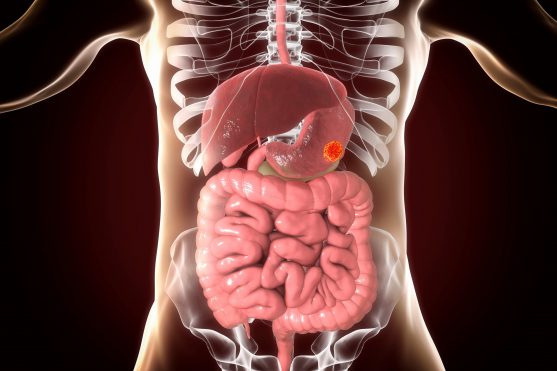तर्क, आस्था और सोचने की आज़ादी: एक बहस, जो स्टूडियो से निकलकर समाज तक जाएगी
धर्मेन्द्र आज़ाद
अभी हाल में लल्लनटॉप के मंच पर जावेद अख़्तर और मुफ्ती शमाइल के बीच ईश्वर, आस्था और तर्क को लेकर एक खुली बहस हुई। विषय कोई नया नहीं था, लेकिन सवाल वही थे जिन्हें अक्सर “संवेदनशील” कहकर दबा दिया जाता है—ईश्वर, धर्म, आस्था और तार्किक सोच।
बहस में जावेद अख़्तर सवाल पूछते दिखे— “किस आधार पर?”, “क्यों मानें?”, “सबूत कहाँ है?”
वहीं मुफ्ती आस्था की मजबूती, धर्म और परंपरा की बात करते रहे। यह टकराव किसी झगड़े जैसा नहीं था, बल्कि दो अलग-अलग सोचों का आमना-सामना था—और यही किसी जीवित, गतिशील समाज की पहचान होती है।
यह समझना ज़रूरी है कि इस एक बहस से न कोई आख़िरी फ़ैसला हुआ, न हो सकता था। न ईश्वर साबित हुआ, न खारिज। सच कहें तो ऐसी बहसों का मक़सद यह होना भी नहीं चाहिए। इनका असली काम होता है—दिमाग़ को हिलाना।
वो हल्का-सा झटका, जो कहता है:
“भाई, ज़रा सोच तो सही!”
मेरे हिसाब से असल दिलचस्प कहानी तो अब शुरू होगी। यह बहस स्टूडियो से बाहर निकलेगी। आने वाले दिनों में यही सवाल सोशल मीडिया पर तैरेंगे, चाय की दुकानों पर उठेंगे, पान की गुमटी पर बहस बनेंगे, ट्रेन के डिब्बों में तर्क-वितर्क होंगे और दफ़्तरों में कॉफ़ी के साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। लोग सहमत होंगे, असहमत होंगे, बहस करेंगे, कभी-कभी नाराज़ भी होंगे—लेकिन सोचेंगे ज़रूर, समाज में एक जरूरी विमर्श खड़ा होगा, और यही सबसे ज़रूरी बात है।
हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मोबाइल ऐप से भुगतान हो रहा है, रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस परत-दर-परत सच्चाइयाँ खोल रहा है, मंगल पर इंसान के भेजे यान घूम रहे हैं। ऐसे में तार्किक और वैज्ञानिक सोच के लिए ज़मीन पूरी तरह तैयार है। अंधविश्वासों और रहस्यों के लिए छिपने की जगहें सिमट रही हैं। अगर हर असहज सवाल का जवाब बस इतना ही होगा—“ऐसे ही होता आया है”
”ऊपर वाले की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता”
तो विचारों का टकराव तय है। इसी वजह से तार्किक सोच का विमर्श आगे बढ़ेगा, चाहे किसी को पसंद आए या न आए।
ऐसी चर्चाएँ किसी को रातों-रात आस्तिक या नास्तिक नहीं बनाएँगी, न किसी की आस्था छीनेंगी। लेकिन वे धीरे-धीरे यह एहसास ज़रूर कराएँगी कि सवाल पूछना अपराध नहीं है, तर्क करना दुश्मनी नहीं है, और असहमति कोई गुनाह नहीं है।
इस लिहाज़ से यह बहस कोई “नतीजा” नहीं, बल्कि एक सकारात्मक संकेत है—संकेत कि आने वाले समय में सवाल बढ़ेंगे, बहसें तेज़ होंगी, और सोच—और ज़्यादा खुली होगी।
क्योंकि आख़िरकार, चुप्पी से परंपराएँ चल सकती हैं, लेकिन समाज आगे बढ़ता है—सवालों से, नए विचारों से और नवाचार से।