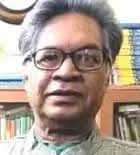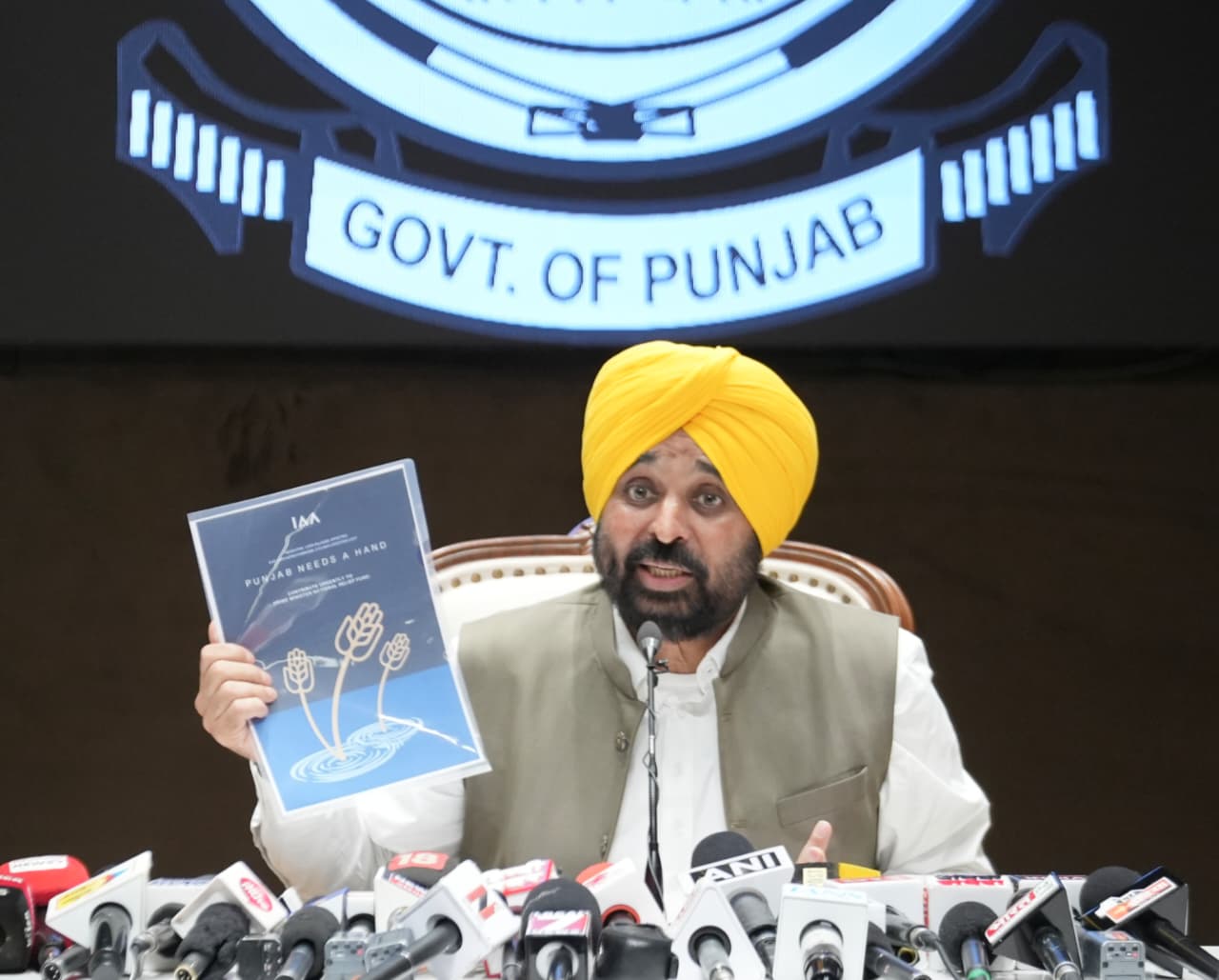बीच बहस में:
विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास- दृष्टि
वीरेंद्र यादव
हिंदी उपन्यास में दो दृष्टियों का टकराव आमने-सामने रहा है एक दृष्टि भारतीय समाज के संश्लिष्ट यथार्थ से मुठभेड़ करती हुई बदलते सामाजिक परिदृश्य की साक्षी रही है तो दूसरी विश्व नागरिकता की ललक में भाषाई खिलंदड़ेपन का नट संतुलन करते हुए ऐसी कलात्मक चकाचौंध को जन्म देती है जो यथार्थ को दृश्य ओझल कर देती है।
भाषाई खिलंदड़ापन अपनी अंतिम परिणतियों में त्रासद यथार्थ के साथ क्या सुलूक करता है विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास त्रयी ‘नौकर की कमीज’, ‘ खिलेगा तो देखेंगे’ एवं ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ इसका ज्वलंत उदाहरण है।
निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओंऔर विसंगतियों को अपनी कथावस्तु बनाने के बावजूद ये उपन्यास अपनी अंतिम परिणतियों में महज एक कलारूप बनकर रह जाते हैं ।
काल व परिवेश की कैद से मुक्त इन उपन्यासों का अपना एक स्वायत्त संसार है। इनके सभी पात्र सीमित क्रिया -प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लगभग सनकी से एक ही भाषा बोलते हुए सममानसिकता से ग्रस्त हैं।
‘नौकर की कमीज’ के मुख्य पात्र संतू बाबू के माध्यम से निम्न मध्यवर्गीय जीवन के प्रसंग विदुषकीय प्रक्षेपण की तरह प्रस्तुत होते हैं ,ना कि त्रासद यथार्थ के रूप में।
कहीं तो वह इतने निरीह व व्यक्तित्वविहीन दिखते हैं कि ‘ नौकर की कमीज’ पहनकर साहब के लाॅन की निराई करने लगते हैं तो कहीं सामाजिक स्थितियों के दार्शनिक व्याख्याकार । उनकी कुंठाएं भी छुद्र न होकर वैश्विक थीं ।
स्वयं संतू बाबू के शब्दों में “मैं कभी घोड़े पर नहीं बैठा था लेकिन हवाई जहाज में बैठना किताबें और सिनेमा में इतना सामान्य हो गया था कि हवाई जहाज में बैठना मुझे मालूम था। दिल्ली- मुंबई या भोपाल- दिल्ली या नागपुर- दिल्ली का हवाई किराया मुझे मालूम था। मुंबई के ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल की सुख सुविधा भी मुझे मालूम थी”।
इतना ही नहीं उन्हें यह संज्ञान भी था कि ” हम लोगों की सारी तकलीफ उन लोगों की होशियारी और चालाकी के कारण थी जो बहुत मजे में थे और जिससे हमारा परिचय नहीं था।”
वर्गीय समझ का यह पैनापन संतू बाबू को इन निष्पत्तियों तक ले जाता था कि “संघर्ष का दायरा बहुत छोटा था। प्रहार दूर-दूर तक और धीरे-धीरे होते थे इसलिए चोट बहुत जोर की नहीं लगती थी। शोषण इतने मामूली तरीके से असर डालता था कि विद्रोह करने की किसी को इच्छा नहीं होती थी।”‘
नौकर की कमीज’ के संतू बाबू की ये निष्पत्तियां व वर्गीय समझ का यह पैनापन उनके दैनंदिन जीवन के आचरण से सर्वथा बेमेल है ।सामान्य जीवन में जहां वे चेखव की कहानी ‘क्लर्क की मौत’ के मुख्य पात्र के नजदीक खड़े होते हैं वहीं बौद्धिक सोच में वह किसी क्रांतिद्रष्टा से कम नहीं ।
वास्तव में संतू बाबू के चरित्र की यह फांक भारतीय समाज के निम्न वर्गीय जीवन की फांक ना होकर स्वयं उपन्यासकार की दृष्टि की फांक है । यह उपन्यासकार द्वारा चरित्र को स्वयं (लेखक) से न अलग कर पाने की असफलता भी है।
उपन्यास के अंत में संतू बाबू द्वारा ‘नौकर की कमीज’ का चिंदी चिंदी करना और फिर प्रतीक दहन भी उपन्यास की सहज स्वाभाविक तार्किक परिणति न होकर लेखकीय आरोपण ही बनकर रह जाता है ।
जिस निष्कर्षवादी ‘ सुर्ख सबेरा’ को समाजवादी यथार्थवाद के खाते में दर्ज कर प्रतिबद्ध सृजनात्मकता के परखचे उड़ा दिए जाते थे, वही ‘नौकर की कमीज’ में कलात्मक अन्विति के रूप में प्रतिष्ठित होता है।
इसलिए नहीं कि नौकर की कमीज किसी वृहत्तर राष्ट्रीय रूपक या बड़े जीवन दर्शन को रेखांकित करता है बल्कि इसलिए कि भाषाई स्तर पर यह एक ऐसा शांत और निरुद्वेग मुहावरा प्रदान करता है जो जीवन में रचे पगे होने की प्रतीति कराते हुए भी उससे कहीं अलग और स्वायत्त रहता है।
दरअसल विनोद कुमार शुक्ल औपन्यासिक संरचना में एक ऐसा लिखने का खेल खेलते हैं, जो शाब्दिक तो है,लेकिन भाषिक नहीं है। विनोद कुमार शुक्ला की भाषा में बिंब और दृश्य शब्द दर शब्द पटे पड़े हैं ।
भाषा इन बिंबो व दृश्यों को चाक्षुष बनाने का एक माध्यम भर है। यह शाब्दिक खेल और भाषाई कौशल उनके बाद के दोनों उपन्यासों ‘खिलेगा तो देखेंगे’ और ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ में चरम पर है। इन दोनों ही उपन्यासों में न कोई सुसंगत कथा सूत्र है और न समय समाज की कोई हलचल । बस भाषा की डोर पर शब्दों का एक आलाप है जो किसी विलंबित खयाल की तरह कुछ रसज्ञ लोगों को भाव विभोर कर सकता है तो अधिकांश को भौचक।
भाषा का तिलिस्म गढ़ते गढ़ते विनोद कुमार शुक्ल अपने उपन्यासों की कथा भूमि को भी तिलिस्मी बना देते हैं, फिर चाहे वह आदिवासी अंचल का कोई गांव हो या पिछड़े इलाके का कोई कस्बा ।
लेकिन प्रकृति उनके यहां उस तरह नहीं आती जिस तरह रेणु के यहां। रेणु की तरह प्रकृति का ‘ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव’ विनोद कुमार शुक्ल के औपन्यासिक गद्य में नहीं है ।
वह प्रकृति का तिलिस्म गढ़ते हैं इस तिलिस्म को गढ़ने की प्रक्रिया में वह अपने औपन्यासिक पात्रों को भी तिलिस्मी बनाकर रख देते हैं। प्रकृति की इस सुरम्य व मनोरम उपत्यका को देखकर ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ के रघुवर प्रसाद के पिता को सहसा अहसास होता है कि “लगता है बहुत दिन जी गए और मृत्यु यहां से बहुत समीप हो ।
” क्लासिकी संगीत की ऊंचाइयों को छूती प्रकृति प्रेम की यह सार्वभौमिकता व सार्वकालिकता निम्न मध्यवर्गीय रघुवर प्रसाद के पिता को जिस काल्पनिक सुख संसार में ले जाती है, वह उनका अपना निजी अनुभव न होकर उस आभिजात्य सौंदर्य दृष्टि का परिणाम है जिसका वास्तविक जीवन जगत से सीधा कोई रिश्ता नही है।
शायद यही कारण है कि ‘ खिलेगा तो देखेंगे ‘ में आदिवासी जीवन की भरपूर छलकन के बावजूद आदिवासी जीवन का तनाव संघर्ष, वंचना एवं यातना यहां पूरी तरह अनुपस्थित है। ‘
नौकर की कमीज’ और ‘खिलेगा तो देखेंगे’ में जीवन यथार्थ के जो बचे खुचे चिन्ह थे वह ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ में पूरी तरह मिटते नजर आते हैं।
यूँ तो इस उपन्यास के केंद्र में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार है लेकिन इस परिवार के मुखिया रघुवर प्रसाद की चिंताएं कुछ विचित्र किस्म की हैं,कभी लावारिस साइकिल का मिलना उनकी समस्या बनती है तो कभी हाथी का लावारिस हो जाना। एक महाविद्यालय में गणित के प्राध्यापक होकर भी वे किसी मतिमंद बालक सरीखा व्यवहार करते हैं ।
उपन्यास के केंद्र में हाथी, खिड़की, पेड़ का कोटर , सांप नदी जल चट्टान और एक नवोढ़ा पत्नी है लेकिन ‘नौकर की कमीज ‘ और ‘ खिलेगा तो देखेंगे’ की तर्ज पर न तो इसमें कोई घटना, संघर्ष, जीवन- सत्य है न ही कोई कालखंड।
उत्तर- आधुनिकता के संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य के जिस तपोवन की चर्चा करते हैं विनोद कुमार शुक्ल ‘ दीवार में एक खिड़की रहती थी’ उपन्यास में इसी तपोवन की रचना करते हैं । लेकिन नामवर सिंह के ही शब्दों में न तपोवन जगत बन सकता है न साहित्य!
क्या विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में भारतीय समाज के जटिल यथार्थ की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है या की यह उपन्यास उत्तरआधुनिक शैली में नेटिव को एग्जॉटिक बनाकर विश्व बाजार में सेलेबल बनाने का उपक्रम है।
आखिर विश्व कथासाहित्य के वे कौन से मानदंड है जिनकी कसौटी पर विनोद कुमार शुक्ला विश्व कथा साहित्य में पांक्तेय बताए जाते हैं । यह कसौटी गेब्रियल गार्सिया मार्केज, चिनवा अचेबे, टोनी मारिसन, राल्फ एलिसन, जेम्स बाल्डविन, नदीन गार्डिमर व डारिस लेसिंग की साहित्यिक कृतियों से उपजा विश्व बोध है या की पश्चिमी पूंजीवाद से ऊबे- सुखी उन साहित्यिक कथाकारों का जो भाषाई खेल के जरिए साहित्य का विश्व मानकीकरण कर रहे हैं और उत्तर आधुनिकता जिनका नया शगल है।
यह अकारण नहीं है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति पूरी तरह निर्वासित है। राजनीति का यह निर्वासन और मूर्त स्थितियों का अमूर्तन ही उनके उपन्यासों की वह कलात्मक उपलब्धि है जिस पर हिंदी के कुलीनतंत्र की सर्वसहमति है ।
बकौल निर्मल वर्मा “हमने अपना देखने का तरीका राजनीतिक बना लिया। बाकी सब चीजें गौण कर दीं। जहां-जहां कुछ लेखकों ने इसे तोड़ने की कोशिश की है वहां-वहां वे सफल हुए हैं, ‘नौकर की कमीज’ एक उदाहरण है।” लेकिन क्या विनोद कुमार शुक्ल के औपन्यासिक मुहावरे में भारतीय समाज के वृहत्तर यथार्थ की रचना संभव है लेकिन जब औपन्यासिक सरोकार ‘अध्यात्म, ईश्वर और आत्मा’ तक सिमट कर रह गए हों तो यह प्रश्न गौण हो जाता है।
(‘उपन्यास और देस’ पुस्तक में शामिल)
वीरेंद्र यादव के फेसबुक वॉल से साभार