प्रतिबिम्ब मीडिया समाज के अपने अग्रजों के प्रति जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उनका या उन पर लिखी सामग्री प्रस्तुत करता है। यहां हम वरिष्ठ मार्क्सवादी आलोचक विमल वर्मा का आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं, जो संभवतः नब्बे के दशक में लिखा गया था। विमल जी का पिछले समय में 18 जून 2025 को निधन हो गया था। पाठकों के लिए हम वरिष्ठ लोगों की ऐसी सामग्री भविष्य में प्रकाशित करते रहेंगे। संपादक
खोए हुए काल की खोज
विमल वर्मा
यह कहना सही है कि भारतीय मनीषा के संस्कारों के अंतः संघर्ष का अध्ययन किया जाय तो उसमें नितांत आदिम और सद्यः आधुनिक स्तर एक साथ विवाद- संवाद में तरंगायित होते रहते हैं। लेकिन जिनकी सृजनशील यात्रा में ये छोर ( प्रमिटिव और अत्यंत आधुनिक सिविलाइज्ड) परस्पर संघात करते चलते हैं उनसे ही गहरे वागर्थ की सृष्टि भी संभव हो सकी है। प्रश्न उठता है कि आज के रचना संसार में मिथकीय काल चेतना के सहारे ऐतिहासिक काल चेतना को व्यक्त किया जा सकता है? कहना न होगा कि हमारे रोजमर्रा के संस्कार हमारी संस्कृति के बिम्बों, प्रतीकों में भी अपनी वास्तविक अर्थवत्ता पाते हैं। क्या मिथकीय अंतर्वस्तु में प्राचीन इतिहास के जटिल रूपाकारों, जटिल भावकल्पों के स्रोतों को खोजा जा सकता है? संस्कृतियों के इतिहास के उथल-पुथल को रूपायित करने में कृतिकार की नई चेतना उस विस्मृत अनुभूतियों से पाठकों को किस हद तक आंदोलित करती है? रचनाकार की कल्पना के ज्ञानात्मक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं? ये कुछ प्रश्न ‘अपने अपने राम’ की पाठ-प्रक्रिया में सहजता से उत्तर पा लेते हैं और दिलचस्प अनुभव यह होता है की पाठक यहां अपनी जातीय स्मृति के प्रीतिकर अनुभव का पुनरानुभव करने लगता है।
रचना की चेतना का विश्लेषण करते समय हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि इस उपन्यास के मिथक में परंपरा के जिन बिम्बों और प्रतीकों का विधान किया गया है वे इतिहास के किस पड़ाव को रूपायित करते हैं, उनमें यथार्थ का प्रतिबिम्बन कैसा है और उसमें भविष्य की कौन सी संभावना पकड़ में आती है?
उपन्यास के अंतर्वस्तु के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनमें वेदों, उपनिषदों, पुराणों से लेकर रामायण, महाभारत तक की यात्रा है। इसके प्रतीक 1500 ई.पू. से शुंगकाल तक बिखरे हैं। वैदिक ऋचाओं के मंत्र युग से लेकर पुराणयुग और पुराण युग से महाकाव्य युग का अंतर ऐतिहासिक विकासक्रम का ही प्रतिफल है। यहां पुराणों की महत्ता पर गौर कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा। पुराणों की रचना का महत् उद्देश्य ही यह था कि भारतीय मनीषा जो आत्मबोध विस्मृत कर रही थी, अभिशप्त थी, उसे उसके प्राचीन गौरव का स्मरण कराया जाय। यह उस कालखंड के पुनर्जागरण का सांस्कृतिक प्रयास था। और इस क्रम में अवतारवाद की अवधारणा ने जन्म लिया। इसी अंतराल में उपनिषद, जैन एवं बौद्ध साहित्य ने ऐतिहासिक एवं तात्विक उथल-पुथल उपस्थित किया। मैंने उक्त विवरण का संकेत इसलिए किया कि इस उपन्यास की संरचना में उक्त ग्रंथों में वर्णित तात्विकताओं की झलक मिलती है। इसकी कथावस्तु में महज जैन साहित्य या जातक की पीठिका खोजना अपर्याप्त है। इसमें जिन मिथक चरित्रों, बिम्बों एवं प्रतीकों से कथात्मकता की बुनावट की गयी है वे एक तरह से प्रज्ञात्मकता को भी वहन करते हैं। इसलिए ये संज्ञाएं एक कालखंड का इतिहास उसके परिवेश और उसकी सांस्कृतिक अनुगूंज समेटे हुए हैं।
गौर करने की बात है कि मंत्र और उपनिषद के युग में कबीलों के सामूहिक संपत्ति के अधिकारों का अवसान हो रहा था और वर्णाश्रम का उदय हो रहा था। कालांतर में संपत्ति का संचय समाज के एक समूह के अधिकार में आते-आते सत्ता के शिखर पर ब्राह्मण और पुरोहित आसीन होने लगे। उपनिषद युग तक आते-आते आदि भौतिकवाद आदर्शवादी विश्वदृष्टि में परिवर्तित होने लगा। समाज के विकास में विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भौतिकवाद स्वयं एक विचारधारा है। विचारधारा राजनीतिक, कानूनी, नैतिक सौंदर्य शास्त्रीय दार्शनिक पद्धति में प्रतिफलित होती है। इसलिए भौतिकवाद एवं आदर्शवाद के बीच संघर्ष एक विचारधारात्मक संघर्ष है।
वर्णाश्रम व्यवस्था तक आते-आते समाज के एक छोटे से हिस्से के हाथों में धन और संपत्ति का केंद्रीकारण प्रारंभ हुआ जिससे वर्गों का उदय हुआ और जातियां विभिन्न वर्गों में रूपांतरित हो गईं। इसीलिए सामाजिक (वर्गीय) टकराव मनु स्मृति, नारद स्मृति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परिलक्षित होते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ईसा पूर्व 10वीं और सातवीं शताब्दी के बीच आदिम कबीले समाज के भीतर से दास प्रथा पर आधारित राज्यों का उदय हो रहा था। “इस रूपांतरण की प्रक्रिया में ही बाद का वैदिक साहित्य जैसे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि रचे गए। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और वृहस्पति की विधि संहिताएं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा उसे कल का बौद्ध, जैन तथा अन्य साहित्य- ये हमें न केवल भारतीय दास प्रथा के विशिष्ट लक्षणों को समझाने में मदद करते हैं बल्कि उन परिवर्तनों को भी देखने और समझने में सहायता करते हैं जो कई सदियों के दौरान उसके विकास काल में हुए थे।” (के. दामोदरन)
‘अपने अपने राम’ की कई समीक्षाएं पढ़ने को मिलीं । इससे मुझे लगा कि अज्ञेय के ‘शेखर एक जीवनी’ के बाद यह सबसे विवादास्पद उपन्यास बताया जा रहा है। कई सवाल बड़ी गंभीरता से उठाए गए हैं। इनकी कथा में (विशेष कर भरत, रावण द्वारा सीता को बेटी कहना, आज के सांप्रदायिक माहौल में राम के चरित्र का महान आदर्शीकरण इत्यादि)। राम कथा के बारे में प्रख्यात भाषाविद् सुकुमार सेन ने ‘रामकथाप्राक इतिहास’ (1977) और ‘रामकथार तत्व’ (साहित्य परिषद पत्रिका, वैशाख चैत्र 1376 1378 बं.) लिखा है। इससे इस संदर्भ में नई-नई बातें मालूम हुईं। उन्होंने तथ्यों द्वारा यह विश्लेषित किया है कि राम की उपासना शुरू होने के पहले ही राम कथाएं प्रचलित थीं। जातक कथाओं में राम और सीता भाई बहन थे। एक चीनी कथा में सीता राम की पत्नी थी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। जैन साहित्य के अनुसार सीता रावण की पत्नी मंदोदरी की पुत्री थी। रावण का वध राम ने नहीं लक्ष्मण ने किया था। माइकल मधुसूदन ने भी ‘मेघनाथ बध’ नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की है। उसमें मेघनाद की तुलना में राम और लक्ष्मण का चरित्र बहुत निकृष्ट दिखाया गया है।
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब- जब समाज भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक अनुभव से गुजरता है तब तब मिथक नए रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। समाज के विकास के साथ साथ मिथक बी विकसित होते हैं। क्या मिथकीय रचनात्मकता समाज के सांस्कृतिक संघर्ष की निरंतर प्रक्रिया नहीं रही है ? इतिहास संबंधी घटनाओं में कल्पना के मनमानी विस्तार की कम गुंजाइश रहती है। लेकिन राम के मिथक व्यक्तित्व में गतिशीलता है, वह रचनाकार व्यक्तित्व को वह स्वतंत्रता देती है कि वह इस प्रतीक के माध्यम से अपने व्यक्तिगत सृजनशील दृष्टि को विकसित करे और नई-नई कल्पनाओं से नवीन उद्भावनाओं को जन्म दे। परंतु प्रतिबद्धता यह हो वह प्रतीक समस्त जातीयता का प्रतीक बन सके। जहां तक पात्रों, परिस्थितियों और घटनाओं का संबंध है, उनसे संबद्ध अस्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबद्ध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन में तर्कपरक संहति हो । आज मनुष्य और समाज के अध्ययन और रूपायन में भौतिक सिद्धांतों और प्रणालियों के वैज्ञानिक बोध से तटस्थ और निस्संग नहीं हुआ जा सकता। काल्पनिक पात्रों और घटनाओं को भी ऐतिहासिक य़थार्थता के संदर्भों में इस तरह संश्लिष्ट कर दिया जाए कि समस्त लोक व व्यक्तित्व उसमें सहज रूप से अभिव्यांजित हो जाए। सब मिल कर मिथक अपने सांस्कृतिक बोध से जुड़ा होता है। तभी पुरातन मिथक नए जीवन बोध के अनुरूप नयी व्याख्या के साथ रूपांतरित हो सकता है।
कथा संरचना में तत्कालीन राज सत्ता के कई अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। राजपुरोहित की भूमिका में वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष। इस ताने-बाने में उसे काल में एक साथ सामंती समाज के सांस्कृतिक इतिहास, दशरथ और उनका राज दरबार, कैकेई के नारीगत अस्तित्व की समस्या, राजा दशरथ का अन्य रानियों के साथ सामंती संबंध, राम द्वारा पुरोहितवाद के ह्रासशील शक्तियों के क्रमशः पराभव की अनिवार्यताओं के संदर्भ तथा तत्कालीन यथार्थ की विकास प्रक्रिया में जनपक्षधरता तथा भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से स्वयं उनकी चेतना के दो स्तरों में होने वाले विश्वदृष्टियों का संघर्ष इत्यादि। इनमें जो विविध प्रकार के संबंधों की अभिव्यक्ति हुई है उनके इस कलात्मक रूपांतरण की प्रक्रिया में ही इस रचना की संरचना के विकास का विश्लेषण किया जा सकता है। यही नहीं, वशिष्ठ और राम का तरल द्वंद्व, जो अंतर्वस्तु से लेकर रूप तक में व्यक्त हुआ है, उसके लिए ‘अपने-अपने राम’ के पाठकीय ग्रहण की परिस्थितियों पर विचार करने के लिए भी हमें विवश करता है । हम आज ब्राह्मणवाद के प्रजंड इंझावात में फंसे हैं। सचेत नागरिकों की अनुभूति में सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं के आतंककारी और दमनकारी दबावों में अनिश्चय की मनोदशा का जो संघारक संकेत मिल रहा है उन परिचित तथा अपरिचित शक्तियों से सुरक्षा के लिए या तो आत्मलीन हो जाएं या फिर परंपरा के विकास के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जीवन के संकेतों और संदेशों की खोज करें। चूंकि साहित्य ही संस्कृति का केंद्रीय रूप होता है इसलिए इतिहास और समाज के अमूर्तीकारण से उत्पन्न धारणाओं और सिद्धांतों का निषेध करते हुए अपने व्यक्तिगत तथा ऐतिहासिक, सामूहिक अनुभव के रूपों में संस्कृति को पहचानें। इस संदर्भ में लेखक ने वह चेतना तो दे ही दी है कि आदिकालीन युग में सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करने वाली भौतिक परिस्थिति कैसी थी जिसमें राम और वशिष्ठ का द्वंद्व होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में उपन्यास में हम राम के गहरे आत्मसंघर्ष का साक्षात्कार करते हैं। उसमें ब्राह्मणवाद एवं राजपुरोहितों व्यवस्था के दमनात्मक स्वभाव की जो अनुभूति होती है वह राम के साथ पाठकों में भी एक गहरी उद्विग्नता प्रगट करती है। “महाराज तो तर्क और विमर्श पर आ गए। शास्त्र और धर्म तो मानने न मानने के क्षेत्र हैं। यहां तर्क से काम नहीं चलता। इस तरह तर्क करने लगें तब तो कोई भी कह बैठेगा की परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण की और बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? शास्त्र में लिखा है तो मानना ही होता है। (वशिष्ठ पृष्ठ ४)
“शास्त्र और धर्म तो युग के अनुरूप बदलते रहते हैं आचार्य। कृतयुग का आचरण त्रेता में निंदनीय हो जाता है। त्रेता के आदर्श द्वापर में नहीं चल सकते। द्वापर के विधान कलियुग में युग-वाह्य हैं। फिर इनकी अंतिम कसौटी क्या है? तर्क और विवेक ही तो! वेद सृष्टि के आदि में रचे गए थे। कहते हैं सृष्टि से भी पहले जिस प्रजापति ने वेदों के ज्ञान से सृष्टि की, उसका आचार, जिस वैवश्वत मनु ने धर्म का प्रथम विधान किया, उसका आचार क्या आज हमें मान्य हो सकता है। क्या कोई है जो अपनी दुहिता के साथ पिता के विवाह का अनुमोदन करे… यदि शास्त्र तर्क और विवेक के प्रतिकूल पड़ता हो तो तर्क को झुठलाने के स्थान पर शास्त्रीय विधान को बदलिए आचार्य।” (अपन अपने राम पृ. 4)
“ आशय कुछ विशेष नहीं है। जब आप रावण और बृथ की बात कर रहे थे तब मैं सोच रहा था, सभी राक्षस ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? क्या इसका एक कारण यह नहीं है कि जिन अपराधों के लिए समाज के अन्य लोगों को दंड मिलता है उन्हीं के लिए ब्राह्मणों को दंड मुक्ति मिली हुई है? दूसरों से यदि अपराध हो भी जाता है तो दंड प्रयोग से वे सुधर जाते हैं। यदि ब्राह्मणों में से कोई अपकर्मी हुआ तो वह निर्बाध होने के कारण, राक्षस बन कर ही रहता है। यदि ब्राह्मणों के लिए भी दंड की व्यवस्था हो तो समाज अधिक मर्यादित रहे”। … विचार करने की स्वतंत्रता क्या अपराध करने की भी स्वतंत्रता है, आचार्य? (अपने-अपने राम पृ. 5 )
मर्यादा के प्रश्न पर वशिष्ठ की धारणा थी कि “जिस रस्से से हाथी को बांधा जाता है उसी से बकरी को तो नहीं बांधते राजन। मनुष्यों के लिए बने नियम देवताओं पर कैसे घटित हो सकते हैं। ब्राह्मण आकृति मात्र से मनुष्य होता है पर वह है तो साक्षात देवता। पृथ्वी पर आने पर तो भगवान को भी मनुष्य रूप धारण करना होता है। यही ब्राह्मण की बाध्यता है, अन्यथा वह तो अग्नि का रूप है। आहुत है वह। जैसे देवताओं का भाग अग्नि में डालकर देवताओं तक पहुंचाया जाता है वैसे ही ब्राह्मण के मुख में पहुंच कर भी वह देवों, पितरों और पुण्य कोषों में पहुंचता है। नियम बाह्य तो ब्राह्मण रहेगा ही।” यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को सामान्य मनुष्य के मिथ में बदलना क्या स्वयं मिथ को मथना नहीं है? इसलिए लेखक ने रचना को संस्कार देने के लिए परम्परागत रचना विवेक में अपने युग के अनुभव को मिलाना चाहा है। यहां पाठक केवल भावों आस्वाद को ही रसानुभूति नहीं करते, बल्कि उसके माध्यम से तथ्यों में अन्विति बोध करने और उन्हें और अधिक बहिर्मुख वर्चस्व में स्वायत्त करने की छूट पाते हैं। राम और वशिष्ठ के कर्म संशक्ति में जिन मूल्यों की सृष्टि कर परम्परा और परिवेश को द्वंद्वात्मकता रची गई है वह जागरूक लोकोचित गहरी प्राणवत्ता के साथ उभरा है। और यहां हमें निर्मम बौद्धिक कसौटी पर अपने आदिम और आधुनिक संस्कारओं पर घिसने और परखने के लिए आग्रहशील बनाता है। यहां शब्दों का मूल प्रत्ययों की तरह इस्तेमाल किया गया है। जिन लोगों के मस्तिष्क में संस्कृति और धर्म के सहज निष्कपट और सीधे विकास की अवधारणा घुसी है उनके लिए लेखक ने इस विकास के भीतर वर्ग और वर्ग की विभिन्न श्रेणियों के जटिल कारकों की भूमिका से अवगत कराया है।
कहना न होगा कि जब रूपबंध लेखक को प्रामाणिक रचनाओं से परे न जाने दे तो रचनाकार उस तथाकथित ढांचे में ही ठहर जाने को बाध्य हो जाता है। परंतु महान रचनाकरा अपनी मौलिक सृजनशीलता के कारण समय और समाज की उपस्थिति का अपना ढंग गढ़ता है। वह उपन्यास में अन्तर्निहित तार्किकता में देखी जा सकती है। इस उपन्यास में यहां रचनाकार बुद्धि से संवेदना धरातल पर उतरा है। क्योंकि यहां चेतना के गवाक्ष से दृश्यों को पकड़ा गया है। रचना केवल इतिहास के यथार्थ को ही नहीं पकड़ती बल्कि उसमें कुछ रचती भी है। और अपने-अपने राम में यह रचाव सकारात्मक तत्व है जिसमें दृश्य बंधों के माध्यम से रचना का आशय ही व्यंजित नहीं होता बल्कि इस माहौल में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उसकी अपनी हिस्सेदारी की भूमिका भी निभाती है। यहां दृश्यों के बिम्ब मिथक और इतिहास के संश्लेषण के रूप में रूपायित किए गए हैं। उपन्यास दर्शन के सूत्रों से प्रारम्भ होता है। बहुत से उपन्यासों में दर्शन के ऊहापोह में भावावेग में खो जाते हैं, अनुभूतियां शिथिल हो जाती हैं लेकिन भगवान सिंह की स्वाभाविक रचना सामर्थ्य के फलस्वरूप ही साहित्य और संस्कृति की चिन्ता ने दार्शनिक चिंतन की अधुनातन गतिविधियों के प्रति भी जिज्ञासु और संवेदनशील बनाया है। राम और शम्बूक के माध्यम से अपनी ही मुख्य परम्परा पर शंका उठायी गयी है और उन शंकाओं से उद्भूत तर्क –संरचनाओं को परम्परा के भीतर ही स्वतंत्र प्रस्थानों के रूप में निर्मित किया गया है। दर्शन में क्रिया कलारों के व्यावहारिक लक्ष्य जुड़े रहते हैं। वह विश्व को मानवीय लक्ष्यों के अनुसार ज्ञान का उपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। इस उपन्यास में वशिष्ठ और राम दोनों अपने समय के मानवीय क्रिया कलाप को नियंत्रित करने के अपने-अपने लक्ष्य के अनुसार यज्ञ और ब्राह्मणों के वर्चस्व तथा राम द्वारा, उत्पादन सम्बन्धों के विकास के अनुभवों द्वारा वास्तविकता का आत्मीकरण करते हुए उसे संस्कृति के जगत में व्यावहारिक गतिविधियों में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। वह अपने प्रयास को एक वांछित, आवश्यक और आदर्श रूप में परिकल्पित परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं। जाहिर है कि प्रगतिशीलता का पक्षधर अपनी सांस्कृतिक धारा की विरासत को वर्तमान के धुंध में उपेक्षित नहीं करता, बल्कि इतिहास की द्वंद्वात्मक चेतना ने लेखक को मुख्य दृष्टि दी है जिसके आधार पर वह इतिहास ग्रस्तता और सम्यक इतिहास बोध में अन्तर कर पाया है।
रचना के पाठ से लगता है कि दर्शन केवल संस्कृति की रचना भी करता है। हां, यह बात जरूर है कि दर्शन में संस्कृति एक तर्कसंगत अवधारणात्मक रूप धारण करती है। इस अवधारणा का रूपायन ही कृतिकार की प्रतिबद्धता है। कथा की समग्रता में जो संज्ञानात्मक गतिविधियां हैं उनका आधार एक विशेष लक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसी लक्ष्य के अधीन लेखक रचना के यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हुए उनका तानाबाना बुनता है। यहां यथार्थ इतिहास की द्वन्द्वात्मक भौतिक अवधारणा पर अवलंबित है। अर्थात वन्य युग से कृषि युग में संक्रमण या वन्य युग में अग्नि, वर्षा इत्यादि प्रकृति की शक्तियां एवं उनके अलौकिक देवरूपों को पूजा यज्ञ के द्वारा की जाती थी।
कालान्तर में कृषि युग में उत्पादन संबंध परिवर्तित हुए और यज्ञ की प्रासंगिकता समाप्त होने लगी। विज्ञान एवं तत्कालीन प्रविधि के उपयोग की वैचारिक वं व्यावहारिक धारणा को मूल्यों के रूप आमें स्वीकृति मिलने लगी जिससे सामाजिक संबंधों में अन्तरविरोध उग्रतर होने लगे। ब्राह्मणों, पुरोहितों, क्षत्रियों तथा अन्य जातियों में संघात शुरू हुए। यही ऐतिहासिकता और उसके सांस्कृतिक उत्पाद का सृजन भौतिक संपदा के साथ-साथ तत्कालीन समाज के विचारों, आदर्शों, उद्देश्यों, भावनाओं अन्तःदृष्टियों और संस्थानों के साथ एक नयी भावनात्मकता के साथ एक नया रूप लेकर उभरा है। गौर करने की बात है कि सामाजिक संबंधों का स्वरूप उसी समय तक अपनी गुणात्मक विशिष्टता बनाए रखता है जब तक वह ऐतिहासिक तौर पर बना रहता है। अर्थात जब वह उत्पादन शक्तियों के विकास के स्तर पर उनकी प्रकृति से मेल खाता है। उसकी अभिव्यक्ति घटनाओं, बिम्बों, प्रतीकों, चरित्रों के माध्यम से उपरिसंरचना में राजनीतिक, वैधानिक, नैतिक, सौन्दर्यात्मक, पौराणिक, धार्मिक अवधारणाओं तथा संस्थानों इत्यादि से व्यक्त होती है। परन्तु वे अभिव्यक्तियां अधिकांशतः ऐतिहासिक तौर पर निर्धारित उत्पादन पद्धति द्वारा किसी न किसी रूप में प्रतिबन्धित होती हैं।
यहां राम और वशिष्ठ का विरोध यूं ही नहीं उभरा है। उसके वस्तुगत कारण हैं। परस्पर विरोधी विचारों की प्रेरक शक्तियां तत्कालीन सामाजिक विकास की प्रक्रिया के भीतर अर्थात संस्कृति के आंतरिक अन्तरविरोधों के भीतर छिपी रहती हैं। रचनाकार ने उस समय की सभ्यताओं की शत्रुतापूर्ण अन्तर्वस्तु को, उनके विकास के अन्तर्विरोधी प्रकृति को पहचाना है। यह पहचान ही लेखक की गुणात्मक विशिष्टता है। क्या यह रचाव उस समय के देशकाल में सीमित समुदायों के विकास की विशेष अवस्था को, उसके सामाजिक, भौतिक, वैचारिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित नहीं करता है? लेखक ने वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों के मनोगत विचारों और भावनाओं को इतिहास के वस्तुगत तर्क के परिप्रेक्ष्य में सृजित किया है। उसमें पाठकों को यह दिशा – दृष्टि मिलती है कि इतिहास का मूल आधार सामाजिक चेतना से स्वाधीन होता है और यह भी कि यह प्रक्रिया मनुष्य की चेतना और इच्छाशक्ति के बीच (वशिष्ठ के) से गुजरे बगैर अपना स्वरूप ग्रहण करती चलती है। वशिष्ठ यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि मानव गतिविधियों के प्रत्येक स्तर पर भौतिक और भावनात्मक दोनों पक्ष परस्पर सम्बद्ध होते हैं। तत्कालीन जीवन के उत्पादन का अस्तित्व तथा विचारों आदि का रूप जो प्रतिबिम्बों, विचारों की ऋंखला में, चेतना में ढलता है , वह भौतिक उत्पादन के अस्तित्व से दूरगामी रिश्ता भले ही रखता हो परंतु पृथक नहीं हो सकता। लेखक ने उपन्यास में जो अंतिम तार्किक दुखांत, करुण परिणति उपस्थित की है उसमें पाठक को यह संज्ञानात्मक चेतना हो जाती है कि सभ्यता के विकास के दौरान विशेष ऐतिहासिक सभ्यता के ढांचे के भीतर समाज की सांस्कृतिक प्रगति के लगातार पारस्परिक (कान्डिशनिंग) अनुकूलन होता रहता है। इस इतिहास दृष्टि का संकेत है कि इतिहास के प्रति सजग आलोचनात्मक दृष्टि ग्रहण और त्याग के विवेक पर आधारित है।
उपन्यास ने केवल नये मूल्यों की सृष्टि ही नहीं की है, बल्कि उन्हें क नयी रचनात्मक व्यवस्था भी दी है। मूल्यों के उद्भव या उसकी स्वीकृति आकस्मिक नहीं होती, इतिहास के भीतर से जो अवधारणाएं उपजती हैं या विकसित होती हैं उन्हें ही मूल्य कहते हैं। कोई मूल्य स्थायी नहीं होता। वह निरन्तर गतिवान तत्व होता है। मूल्यों की पहचान के लिए, उनकी पड़ताल के लिए यथार्थ से जूझना होगा। यथार्थ से माने समय की वास्तविकता से है। यानी तत्कालीन इतिहास या समकालीन इतिहास में संघर्ष का जो स्वरूप है उसमें सामाजिक व्यवस्था को बदलने का जो बहुआयामी संघर्ष चल रहा है। उसमें पात्र, परिस्थितियां, लोक विश्वास जुडा हुआ है कि नहीं। उस मूल्य के साथ जीवन के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तनों की कामना ही नहीं, वह भी प्रक्रिया होती है कि पुरानी व्यवस्था के भीतर उसका द्वंद्वात्मक विकास हो रहा हो। ‘अपने-अपने राम’ में विचार भाव में संक्रमित हो रहे हैं और संस्कार आचरण में। इस संक्रमण का भाव –संस्कृति पारदर्शी बन गयी है। यानी वशिष्ठ के मूल्य असंगत हो उठे हैं। इस मूल्य का विघटन रचनात्मकता में व्यंजित होता है। राम और वशिष्ठ के संघर्ष में प्रवहमान,सृजनशील, अंकुरित मूल्यों के द्वारा ‘मुक्ति’ की प्रक्रिया आधुनिक नहीं तो और क्या है? यह मुक्ति प्रक्रिया परलोक से प्रेरित नहीं है, यह मुक्ति मानव, मुक्ति पर केंद्रित है। परम्परा के प्रति पुरातात्विक विवेक उतर आया है जो संशयों, प्रश्नों के माध्यम से गहन विचार मंथन की क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यही प्रगतिशील कला चिंतन ही नियामक आधार है।
मने दासप्रथा का जिक्र किया था। रावण का पूरा सन्दर्भ दास प्रथा के सन्दर्भों से ओतप्रोत है। राजनीतिक पद्धतियां सम्बन्धों, वस्तुओं को प्रभावित करती हैं। रचनाकार जहां सम्बन्धों और वस्तुओं के उन रूपों को संवेदना के माध्यम से ग्रहण करता है, वहीं संवेदना सौन्दर्यबोध में रूपायित हो जाती है। संवेदना और सौन्दर्यबोध यथार्थवाद से कैसा रिश्ता रखता है , वह द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध कैसा होता है, यह विचारणीय प्रशन है।
विश्वामित्र जाबालि के बारे में बातें कर रहे थे। “दिक रूप में विद्यमान ब्रह्म को उसने प्रकाशवान ब्रहम। दिक प्रसार में स्तिति जलमय समुद्र, स्थूलमय पृथ्वी, विराट अंतरिक्ष और उसके भी ऊपर द्युलोक को उसने अनन्तवान ब्रह्म …” (पृ. 92-93) “ इस तरह के ढेर सारे ऊल -जुलूल विचार भरे रहते उनके मन को।” (पृ, 20)
राम – “मुझे तो इन विचारों के पीछे एक व्यवस्थित और गहन चिन्तन दिखाई देता है”… “ इस विश्व ब्रह्मांड में जड़-चेतन, स्थूल-सूक्ष्म, सक्रिय-निष्क्रिय जो कुछ भी है सब एक ही सत्ता के विकास और अभिव्यक्ति के भिन्न-भिन्न रूप हैं। अर्थात परम सत्ता भूत जगत से अलग और वियोज्य नहीं है। इसे हम प्रकृति कहें या ब्रह्म , नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता।” (पृ.20) यह विचार राम के हैं जो सत्ता और बोध के बीच सम्बन्धों की अभिव्यक्ति हैं। राम की यह उक्ति दर्शन की भौतिकवादी द्न्द्वात्मक पद्धति की ओर इंगित करती है। और दार्शनिक संदर्भ का यथार्थवाद है जिसकी मूल भित्ति पर कथा संरचना ने भाव-प्रक्रिया के माध्यम से संवेदनात्मक रूप ग्रहण किया है।
इसी प्रकार देवता और मनुष्य के बारे में देवता मनुष्य से निकृष्ट होता है और वह कपटी लोगों का मानस पुत्र होता है। और अपने जीवन, कीर्ति और लाभ की चिंता या कामना करता है, उसे प्राप्त करने के लिए श्रम और प्रयत्न करता है… मनुष्य का यही उत्सर्ग पशु और मानव योनि की संधि रेखा पर झिझकते हुए खड़े मनुष्यों का सही अर्थ में मानवयोनि में प्रवेश करने की प्रेरणा और नैतिक बल देता है। ” यहां राम की श्रम सौन्दर्य के प्रति जो अभिरुचि है वह अस्तित्व और क्षय के बीच कर्ममय मानव जीवन की तार्किक निरन्तरता की ओर संकेत करती है।
“शक्ति रहने पर हर काम हर समय तो नहीं किया जा सकता, लक्ष्मण। इस प्रकृति को ही देखें जिससे हम सभी शक्ति ग्रहण करते हैं। कितनी अनंत शक्तियां और संभावनाएं इसमें अव्यक्त रूप से विद्यमान रहती हैं। इनमें से कुछ को ही यह व्यक्त करकता है और व्यक्त होती है। देश काल के अनुरूप ऋतु चक्र के रूप में, फूलों और फलों के रूप में, वर्षा और वात्या के रूप में, हमारे अपने विचारों, भावों और क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के रूप में। जो इनके उपयुक् देश और काल को जानता है वही अपनी शक्ति का प्रयोग कर के इच्छित फल प्राप्त कर सकता है। अर्थात व्यक्ति, जब अनुचित स्थान और समय पर अपनी पूरी शक्ति लगा देने के बाद भी विफल होता है तो देवज्ञों के जाल में फंस जाता है जो उसे धरती के काल से उठाकर आकाश के देश-काल में पहुंचा देते हैं। जो यहां की उपयुक्त परिस्थितियों की पहचान में असमर्थ हैं, वे ही वहां नक्षत्रों की स्थिति की गणना करने लगते हैं। ”
“ मैं षड्यंत्रकारियों के किसी गिरोह की बात नहीं कर रहा हूं। उसके लिए तो राज्य शासन हर तरह से समर्थ है। पर वशिष्ठ के विराट व्यवस्था के, एक विशाल प्रचार तंत्र के सूत्रधार भी हैं। वह एक ऋषि हैं। जिस शिलींभूत विचारधारा के वह शीर्ष पुरुष है, वह जितनी भी रोचक और जड़ क्यों न हो, अपनी कालदीर्घता के कारण वह शिला की तरह ही दृढ़ हो चुकी है। वह जिस प्रचार तंत्र के सूत्रधार हैं उसकी व्यापकता अवध के राज्य से कई सौगुनी है। उनकी आस्था अयोध्या के राज्य से अधिक पुरानी है और वशिष्ठ की बात मानें तो यह सृष्टि से भी पुरानी है। उनकी शक्ति की अनदेखी करना समझदारी नहीं है।” (पृ.103)
“सत्य और धर्म का आधार दृढ़ होता है लक्ष्मण, पर जैसे मूलगामी वृक्षों के ऊपर आकाश वेलि फैल जाती है वैसे ही सत्य के ऊपर मानवीय स्वार्थ जन्य झूठ का अम्बार छा जाता है। … सत्य के मूल पर छाने वाली आकाशवेलि सत्य का पोषण नहीं शोषण करती है। धर्म के नाम पर स्थापित संस्थाएं और केंद्र धर्म का पालन नहीं, हनन करती हैं।इन संस्थाओं और केंद्रों के पुरोधा और पुजारी धर्म के लिए नहीं होते। धर्म इनके लिए होता है। धर्म इनकी चरागाह है। धर्म चर का यह एक अपना ही अर्थ रखते हैं।”
“ प्रचार तंत्र अपने आप में सैन्य शक्ति से कम शक्तिशाली नहीं होता है। तुम क्रुध ङोकर वशिष्ठ का वध तो कर सकते हो , पर एक बार इसका प्रचार तो दूर,संदेह तक हो जाने पर पूरे साम्राज्य में हलचल मच जाएगी। इससे तुम्हारा ही शासन उलट सकता है। वंचना का एक ही उपाय है, भारी प्रतिदान। यज्ञ।”
“ हमें एक समानांतर प्रचारतंत्र का विकास करना होगा, लक्ष्मण। ऐसा प्रचार तंत्र जिसकी पहुंच सभी वर्णों और सभी जनों, यहां तक कि स्त्रियों और शूद्रों तक भी हो सके।” इस तरह वंचना और उपलब्धि के बीच जो इतिहास सम्मत सीमा रेखा खींची गई है, वह इतिहास के विशेष दौर में परस्पर विरोधी शक्तियों का मूल्यांकन और उसके अनुकूल रणनीति और कार्यनीति नहीं तो और क्या है? यह यथार्थवाद है जो सत्ता और बोध के बीच दार्शनिक सन्दर्भ और उपलब्धि के बीच इतिहास के संन्दर्भ की द्वंद्वात्मकता का चित्र उपस्थित करता है। क्या यह रूपायन मन को संस्कार देने वाली कथा के लिए परम्परागत रचना विवेक में अपने युग के अनुभव को मिलाना नहीं है? क्या इस रचनात्मक अस्मिता में अपने आस-पास को पहचान कर उससे सन्निहित दृष्टि को, वर्तमान परिवेश की जीवन्त गतियों से जोड़ने की प्रेरणा हमें नहीं मिलती? और साथ ही साथ पाठक उपन्यास के ढांचे में काल की संरचना के बोध को निर्वाह का कलात्मक रचाव और संहति की दृष्टि भी ग्रहण करते हैं। यही मिथक का समकालीन भाषा और मुहावरे में पुनर्विवेचन है। इसीलिए यह कहा जाता है कि मिथक संपूर्ण, मानव की अस्मिता को कालगत निरन्तरता में बांधता है। साहित्य का यही धर्म है कि रूपात्मक चिंतन द्वारा पाठक को वृहत्तर संदर्भ से जोड़ दे। यह उपन्यास उस समय के विश्व जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करने के साथ-साथ उस समय का जातीय आत्मदर्शन और उसके अस्मिता बोध को प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत कर पाया है।
इस कृति में स्मृति की एक नियामक भूमिका है। पात्रों, परिस्थितियों, घटनाओं, परिवेश द्वारा एक ओर काल –प्रवाह की चतना की अनुभूति होती है, दूसरी ओर उस प्रवाह का अनुभव करने वाले जन समुदाय को अपने आत्म की प्रतीति भी होती है।
“ छोटे –मोटे काम करते, चलते- बैठते उनका अतीत अपने समस्त दुःस्वप्नों के साथ आंखों के आगे आ जाता है और सामने की वस्तुएं इस तरह तिरोहित हो जाती हैं मानों उनका अस्तित्व ही न हो… (सीता) और (सीता, राम के प्रसंग में) उनके जीवन में स्वेच्छाचारी ढंग से काट कर अलग कर दिए गए कालखंड में जीवन की सम्पूर्ण अर्थवत्ता खोज निकालना क्या हमें प्रूस्त की याद नहीं दिलाता।”
“राम ने बिलखते हुए कहा था-“ तुम भाग्यशाली हो भरत ! तुमने पिताजी का श्राद्ध तो कर लिया।” चित्ररथ को राम का यह कथन कुछ भिन्न रूप में सुनाई पड़ता है, “ मुझे इस बात का कष्ट नहीं भरत कि मुझे राज्याधिकार से वंचित किया गया। पर मेरी अनुपस्थिति में पिताजी की मृत्यु और उस मृत्यु के उपरांत श्राद्ध कर्म तक में न बुलाए जाने की पीड़ा मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। महाराज का बड़ा पुत्र होने के बावजूद उनकी एक भूल के कारण राज्य पर भले मेरा अधिकार संदिग्ध हो, पर अंत्येष्टि का मेरा अधिकार तो था ही।” इस तरह रचना की भाषा में हमेशा संवेगात्मक तनाव की स्थिति बनी रहती है। और यहां एक साथ दो प्रकार की विरोधी वास्तविकताओं का साक्षात्कार होता है। यहां अनुभूति की संरचना सामान्य संदर्भ में देखी जा सकती है जो रचना के हर सृजनात्मक द्वंद्व –क्षणों में गतिशील होती हुई दीखती है। इसे कालबोध की विसंगति का प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं।यह संरचना अनेक आयामी, अनेक स्तरीय और क्रमशः जटिल होती गयी है। परन्तु अनुभूति की गुणात्मकता को बचाए रखा गया है।
इस कृति में घटनाओं के परिदृश्य को जहां बाहरी ऐतिहासिकता से गुम्फित किया गया है वहीं आंतरिक मनोवैज्ञानिक काल-परिदृश्य की भी बुनावट की गई है।जैसे सीता के निर्वासन के बाद राम का उसके बारे में बार-बार सोचना। लेखक यथार्थ की संरचना का वृत्त प्रस्तुत करते समय मनुष्य के बाहरी और चलचित्र जगत की कला- प्रविधिगत विशेषताओं के भी भाषागत पर्याय खोजे हैं। “ एक स्वप्न बार-बार सच कहें तो वह स्वप्न भी नहीं था। वह अपने अतीत के एक छोटे से अनुभव खंड की वापसी थी पर थी विकृत और विरूपित कि पहले से अधिक त्रासजनक बन जाती है। उन्हें स्वप्न में दिखाई देता कि विराध अपनी समाधि को तोड़कर निकल आया है। उसका आकार अपने असामान्य आकार की तुलना में कई गुना विशाल है और आँखें लाल नहीं हैं, दहकती हुई आग की शलाकाएं हैं, जो उसकी आँखों से सीधे निकलकर उनकी आँखों में प्रवेश करके उन्हें ज्योतिहीन करने चली आ रही है… सहसा उन्हें लगता अपने भागने के प्रयास में वह उस सिलोच्चय से एकाएक नीचे गिरे हुए हैं, एक गहरी कंदरा में। विराध ने सीता को पकड़ लिया है। सीता चीत्कार कर रही है। बचाओ। वह उठने का प्रयास करते हैं तभी अपना एक हाथ लम्बा बढ़ाकर विराध उनको उस खाई में ही दबाने का प्रयत्न करता है… कोई भी चट्टान उनके सिर पर नहीं गिरती।”
वास्तव में राम को सीता के बारे में दुश्चिन्ता है। और यह दुश्चिन्ता ही दमित होकर स्वप्न में भयानक रूप ले लेती है। वर्गसा के शब्दों “ काल की प्रतीति हमारे अनुभव का तात्कालिक तथ्य है।” प्रूस्त काल की वियुक्त, विखंडित, निरंतरता रहित, खंड खंड इकाइयों की लड़ी मानते थे। अज्ञेय के शब्दों में सतत वर्तमान अब के प्रत्येक क्षण में – हम एक साथ ही स्मरण और प्रतीक्षा दोनों करते रहते हैं। इसलिए वर्तमान का हमारा बोध, हमारी उपेक्षाओं –आकांक्षाओं सभी उतना ही नियंत्रित होता है जितना हमारी स्मृतियों से अनुशासित, हमारे वर्तमान को हमारा भविष्य भी उसी प्रकार निरूपित और नियंत्रित करता है जैसे हमारा अतीत।” (संवत्सर पृ. 84) यह गत्यात्मक परस्पर भेदकाल स्मृति की आकांक्षा, जटिल रूप में रूपायित की गयी है। इस प्रकार रचनाकार तत्कालीनता द्वारा उद्भूत जटिल रागात्मक स्थितियों और उससे उत्पन्न होने वाली विकृतियों तथा उतार-चढ़ाव पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। और कृति का अनुभव अपने निजी फार्म में उपस्थित किया गया है। क्योंकि हमारे संस्कार हमारी संस्कृति के बिम्बों और रूपकों में उजागर होते हैं।
विलियम फाकनर ने लिखा है-“ उपन्यास में समय बर्फ की तरह जमा रहता है, किन्तु ज्यों ही हम उसे सेल्फ से निकाल कर पढ़ना शुरू कर देते हैं, वह दुबारा से पाठक के जीवन में बहना शुरू कर देता है।” सचमुच में राम के युग का संघात स्वप्न और फैंटेसी में सबसे अधिक जीवन्तता के साथ चित्रित हुआ है। इसी तरह अनेक स्थानों पर आभ्यंतर एकालाप (इंटीरियर मोनोलॉग) राम, सीता, कैकेई के वृत्तांत में रचे गए हैं, जिसमें सम्प्रेषण के लिए मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान की विधियों और पद्धतियों की सारी संभावनाओं का रचनात्मक उपयोग किया गया है।
इस कृति के बारे में यह भी कहा गया है कि राम के चरित्र को ट्रैजिक बनाकर रूपायित किया गया है? क्या राम की वास्तविकता यही है? किसी पात्र के सचेत होने की सार्थकता तभी प्रमाणित होती है जब उसकी चेतना यथार्थ के साथ संघर्ष के क्षेत्र में उतरती है।
गौर करने की बात है कि सम्पूर्ण यूरोप में राजसत्ता लंबी अवधि तक चर्च के अपौरुषेय सर्वाधिकार से संघर्ष करते हुए सेकुलर बनी है। इसी रक्त पिपासु प्रक्रिया में क्रूसेड के इतिहास ने जो रक्त-स्नान किया है उसके वर्णन की जरूरत नहीं है। वह इतिहास की अनिवार्यता थी, विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण दौर था। क्या राम और वशिष्ठ का का द्वन्द्व लेखक के इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ओर इंगित नहीं करता? राम जब वशिष्ठ की शक्ति की समग्रता के बारे में लक्ष्मण को समझा रहे थे “ प्रचार तंत्र अपने आप में सैन्यशक्ति से कम शक्तिशाली नहीं होता और जब तब तो अधिक होता है। … बचने का एक ही उपाय है, भारी प्रतिदान…।” (पृ.105) और इसी प्रतिदान के आदर्श से उन्हें सीता को निर्वासित करने के लिए विवश होना पड़ा। यहां इस प्रसंग को लेकर पाठक को अनायास ईसा मसीह का स्मरण हो उठता है। सोलहवीं और सत्तरहवीं शताब्दी तक यूरोप में प्रत्येक जन विद्रोह में ईसा मसीह का नाम नारे के रूप में ध्वनित होता था। क्रिश्चियनिटी का उदय रोम साम्राज्य के निरंकुश क्रूर शोषण के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष के गर्भ से, दासों की मुक्ति की कामना लेकर हुआ था। और यीशु उसी प्रकार मुक्तिदाता के प्रतीक मान गए। पूंजीवाद के पूर्व ईसा पीड़ितों, दलितों के दैनंदिन संघर्ष के काल्पनिक नेता थे। उसी प्रकार यीशु के जन्म के साढ़े चार सौ साल पहले ही इस्काइलस के नाटक में यीशु की प्रमुख विशेषताएं नाटक के उपादान के रूप में वर्णित हुई हैं। प्रमथ्यु एक ऐसे देवता थे जो मनुष्यों के कल्याण के लिए स्वर्ग से आग चुरा लाए थे। देवताओं ने उसे अपराध समझकर उन्हें पहाड़ पर पत्थर लेकर चढ़ने उतरने का दण्ड दिया था। उन्हें जो यंत्रणा दी गई वह क्रूसविद्ध यीशु की यंत्रणा का दृश्य उपस्थित कर देता है। प्रमथ्यु कहता है- “ मैंने अग्नि की छिपी हुई ज्योति ला दी है जिसके कारण मनुष्य़ जाति के सामने कारीगरी विधा का द्वार खुल गया है।,… इसलिए आज हमें यह यंत्रणा मिली है। इस उद्धार दिन के प्राकश में क्रूसविद्ध (Crucified) एक असहाय देवता आज तुम्हारे सामने पत्थरों से बाद दिया गया है।”
ई. श्वाइत्जर ने यीशु के जीवन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि (1) यीशु मुक्तिदाता थे। (2) वह स्वयं कष्ट सह कर पाप मुक्त कर गए हैं। (3) यीशु तत्कालीन जनता को दासता से मुक्ति दिलाने के लिए आए थे। प्राचीन एवं वास्तविक परंपरा के अनुसार व्यक्तिगत यंत्रणा सहन कर वे संसार को पापमुक्त करना एवं सामाजिक संसार को पापमुक्त करना, सामाजिक संघर्ष करने में प्रमथ्यु तथा यीशु दोनों में एक समान हैं। मध्ययुग की अंग्रेज जनता यीशु को किस दृष्टि से देखती थी वह धर्म परक नाटकों का शोध करके देखा जा सकता है। आज भले वह यथार्थ न लगे परंतु जब तक गिरजा कैथोलिक पंथी थे तब तक वह नाटर की उनका नेतृत्व करते थे। (ऐश्चलस प्रम्थू ड्रामा जार्ज थाम्सन एश्चिलस एंड एथेन्स , हाडिनक्रेन इंग्लिस रिलीजन ड्रामा आफ द मिडिल एजेस आक्सफोर्ड- 1960. पेज -88)
मार्क्स ने धर्म की परिभाषा में दो परस्पर विरोधी पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। (1) “ धर्म एक साथ ही मस्तिष्क की शोकाकुल अवस्था की अभिव्यक्ति है (2) उसके विरुद्ध विक्षोभ भी है। पहली दशा में वह असमर्थता और उत्पीड़न के प्रति मन को बांधता है। दूसरी दशा के अनुसार उत्पीड़न तथा सामाजिक विषमता को दूर करने की अभिलाषा भी व्यक्त करता है। अतएव धर्म सामाजिक विकास की एक विशेष अवस्था में सामाजिक गुण बन जाता है और वह इतिहास की आर्थिक और सामाजिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लगता है।”
अतएव लेखक ने “ प्रतिदान” को क एकार्थी के रूप में प्रयोग किया है जो तत्कालीन ऐतिहासिक. धार्मिक, सामाजिक विकास की सीमा रेखा को प्रतिबिम्बित करता है। उस युग में पुरुष सत्ता प्रधान व्यवस्था में नारी की उपेक्षा, दमन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया ती। राम की दुर्बलता जो सीता के निर्वासन के संबंध में दिखाई गयी है, वह उस समाज व्यवस्था का एक वर्गगत चरित्र है जिसके प्रतीक राम हैं। नारी के प्रति यह वर्ग दृष्टि एक ऐतिहासिक यथार्थ है। इस तरह इस काल्पनिक मिथक ने राम को अवतार के कुहासे से निकालकरक मनुष्य की गरिमा दी है।
इस उपन्यास में सबसे जीवन्त चरित्र कैकेई का है। “ विश्वमित्र के विरुद्ध अभियान वशिष्ठ ने नहीं, कैकेई ने आरम्भ किया था।” कैकेई सफलता या असफलता को भूल नहीं मानती। उसकी दृष्टि में सबसे बड़ी भूल एक ही हो सकती है- अपने जीवन की अंतिम घड़ी से पहले अपना विश्वास खो बैठना। नारी होने की विवशता ने उसे शक्ति, सफलता, असफलता और भूलचूक को ठीक से वे ही परिभाषाएं नहीं पढ़ाई है जो पुरुषों को पढ़ने को मिलती है। वह रोती हुई सहायता की याचना करती हुई अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का प्रयोग कर सकती है, और जो स्त्री ऐसा कर सकती उससे पुरुष जीने का अधिकार भी छीन लेंगे। कैकेई जानती है कि कूटनीति ने राजभवनों में जन्म लिया है, अंतःपुरी में इसका विकास हुआ है और केवल स्त्रियां ही इसका भरपूर उपयोग कर सकती हैं। रजा सभाओं और मंत्रि परिषदों में जिस कूटनीति का मंथन होता है वह तो स्6 की कुटिलता की भूसी है जो अंतःपुर से उड़ कर वहां पहुंची है – फटक कर उठाए जाने के बाद और अपने दंभ के कारण पुरुष इसका भी प्रयोग करने में चूक कर जाता है।
राम ने कैकेई के बारे में लक्ष्मण को बताया कि- “ शक्ति के अलग-अलग रूप होते हैं, लक्ष्मण। युक्ति भी शक्ति का एक रूप है और छल भी एक प्रकार की युक्ति है। छोटी मां ने ही विश्वासघात नहीं किया, लक्ष्मण। विश्वासघात उनके साथ भी हुआ था। उन्होंने केवल यह किया कि जो हथियार उनके हाथ लग सकते थे उनको लेकर पूरी तैयारी से अपनी लड़ाई लड़ी और महाराज को पराजित कर दिया और उनसे राज्य छीन लिया। हम उनसे केवल द्वंद्व की स्थिति में ह । घृणा करना हमारे लिए न केवल अशोभन है अपितु पराजय भी।”
प्रथम चरण में कैकेई का अस्तित्व मूल्य बनकर प्रगट होता है। अपने अस्तित्व के संरक्षण-संवर्धन हेतु वह तत्पर और सक्रिय हुई। अस्तित्व प्रधान संघर्ष उसके अधिकार को अर्थात अस्तित्व रक्षा के प्रयत्नों से जुड़ा है। दूसरे चरण में वह संघर्ष अस्तित्व प्रधानता में रूपान्तरित होकर अस्मिता प्रधान हो जाता है। इस संघर्ष में वह अस्तित्व का संघर्ष अस्तित्व अस्मिता प्रधान बन जाता है। वह राजनीति और शक्ति के द्वारा नारी की अस्मिता को प्रतिष्ठित कर वशिष्ठ के माध्यम से संघर्ष को मन की अस्मिता के गंभीर और उच्च स्तर पर संयोजित करती है। “ मुझे केवल एक ही बात की पीड़ा होती है, आचार्य। मैं स्त्री क्यों हुई। यदि कुछ समय के लिए भी मैं आप (वशिष्ठ) हो जाती तो आप पाते, अयोध्या का इतिहास बदल चुका है।” … “ कैकेई की कसमसाहट उनके चेहरे पर उभर आई थी।” इतिहास को बदलने की मेधा वशिष्ठ में है, पर साधन? महायज्ञ की आग तो वशिष्ठ पैदा कर सकता है, पर महाहवि,” “ मैं यहां दुर्बल अनुभव करन लगता हूं? महाहवि का परिणाम कया है, वह मैं नहीं जानती। जो मुझसे संभव है वह अंत्याहुति के रूप में आप को अवश्य सौंप सकती हूं।” कैकेई उठी और कक्ष में चली गई। लौटी तो उनके हाथों में एक थैली थी। इसे वशिष्ठ के चरणों में रखते हुए बोली, “ अंत्याहुति’ और चुप हो गई।” उनकी चुप्पी शब्दों में मुखर थी।”
राम ने कैकेई के बारे में लक्ष्मण को बताया कि- “ शक्ति के अलग-अलग रूप होते हैं, लक्ष्मण। युक्ति भी शक्ति का एक रूप है और छल भी एक प्रकार की युक्ति है। छोटी मां ने ही विश्वासघात नहीं किया, लक्ष्मण। विश्वासघात उनके साथ भी हुआ था। उन्होंने केवल यह किया कि जो हथियार उनके हाथ लग सकते थे उनको लेकर पूरी तैयारी से अपनी लड़ाई लड़ी और महाराज को पराजित कर दिया और उनसे राज्य छीन लिया। हम उनसे केवल द्वंद्व की स्थिति में ह । घृणा करना हमारे लिए न केवल अशोभन है अपितु पराजय भी।”
प्रथम चरण में कैकेई का अस्तित्व मूल्य बनकर प्रगट होता है। अपने अस्तित्व के संरक्षण-संवर्धन हेतु वह तत्पर और सक्रिय हुई। अस्तित्व प्रधान संघर्ष उसके अधिकार को अर्थात अस्तित्व रक्षा के प्रयत्नों से जुड़ा है। दूसरे चरण में वह संघर्ष अस्तित्व प्रधानता में रूपान्तरित होकर अस्मिता प्रधान हो जाता है। इस संघर्ष में वह अस्तित्व का संघर्ष अस्तित्व अस्मिता प्रधान बन जाता है। वह राजनीति और शक्ति के द्वारा नारी की अस्मिता को प्रतिष्ठित कर वशिष्ठ के माध्यम से संघर्ष को मन की अस्मिता के गंभीर और उच्च स्तर पर संयोजित करती है। “ मुझे केवल एक ही बात की पीड़ा होती है, आचार्य। मैं स्त्री क्यों हुई। यदि कुछ समय के लिए भी मैं आप (वशिष्ठ) हो जाती तो आप पाते, अयोध्या का इतिहास बदल चुका है।” … “ कैकेई की कसमसाहट उनके चेहरे पर उभर आई थी।” इतिहास को बदलने की मेधा वशिष्ठ में है, पर साधन? महायज्ञ की आग तो वशिष्ठ पैदा कर सकता है, पर महाहवि,” “ मैं यहां दुर्बल अनुभव करन लगता हूं? महाहवि का परिणाम कया है, वह मैं नहीं जानती। जो मुझसे संभव है वह अंत्याहुति के रूप में आप को अवश्य सौंप सकती हूं।” कैकेई उठी और कक्ष में चली गई। लौटी तो उनके हाथों में एक थैली थी। इसे वशिष्ठ के चरणों में रखते हुए बोली, “ अंत्याहुति’ और चुप हो गई।” उनकी चुप्पी शब्दों में मुखर थी।”
“कैकेई की चुप्पी नहीं, एक विस्फोट की तैयारी थी, “ यह मेरी अंतिम लड़ाई है आचार्य और संभव है आप के लिए भी अंतिम अवसर। मैं आज कुछ छिपाऊंगी नहीं। मुझे केवल राम से नहीं, आप से भी लड़ना पड़ा है। आप के लोभ से। आप भूलकर भी न सोचें कि मैं राजसत्ता के लिए लड़ती रही हूं। मैं अपने सम्मान के लिए लड़ती रही हूं और मेरी पूंजी ये निष्क नहीं है, जिनको मैंने अंतिम सिक्के तक आपके पावों पर डाल दिया। मेरी पूंजी मेरा अभिमान है।” यही कैकेई के अस्मिता के संघर्ष की दृश्य-अदृश्य रूप प्रदर्शित होता है। अस्मिता प्रधान संघर्ष स्वाधीनता के गौरव से मण्डित होता है।
तीसरे चरण में कैकेई के निजी गौरव का निजी विकल्प निरर्थक साबित हुआ। कैकेई और वशिष्ठ के अनुसार उनके गौरव की रक्षा राम, सीता तथा पूरे समाज के गौरव के ह्रास द्वारा ही संभव हो सकती थी। इस निजी आंतरिक नैतिक असंगति में उलझकर उनके गौरव के सूत्र उनके हाथ से छूटते गए। इस तरह कैकेई की चेतना का संसार पूर्णतया विघटित हो गया। जैसे वशिष्ठ और कैकेई स्वयं चलते त्रासदी की दुनिया में पहुंच गए। स तरह कृति में पात्रों, परिस्थितियों, वातावरण द्वारा व्यक्त अनुभूति की संरचना में तत्कालीन जीवन में मौजूद अनुभूति की संरचनाओं की पकड़ पाठक को सहज हो जाती है। लेखक ने अपनी विशिष्ट रचनात्मक भाषा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं और हितों के बीच सह संबंध, तनाव और टकाव निर्मित किया है।
“लक्ष्मण का क्रोझ प्रचंड हो गया। प्रचंड क्रोध अर्थात चुप। भीतर ही भीतर छाती से ल कर मस्तक तक उबलता और उछलता हुआ लावा। महाज्वाला का अदृश्य अंतर्दाह जिसकी छाया उनके मुख की तमक में और जिसकी पीड़ा उनके चेहरे के तनाव से देखी जा सकती है।” (पृ.100)
“लक्ष्मण को पता ही नहीं चला कि श्रद्धाभिभूत होने के कारण कब और कैसे उनके दोनों हाथ संपुटित हो गए थे और उनका माथा उसी तरह झुक गया था जैसे सूर्य को नमस्कार करते हुए झुक जाता है।”
इस प्रकार कृति की भाषा-संरचना और उससे उद्भूत तनाव विभिन्न प्रकार के साहचर्यों से जीवन ग्रहण करती है। जाहिर ह कि भाषा की अर्थवत्ता शब्द के अर्थ व्यापार में प्रगट होती है। यहां अर्थों के टकराव और उस टकराव से उद्भूत होते हुए इस चरम अर्थ का आभास होता देती है। क्या लक्ष्मण के संबंध में भावनाओं और बिम्बों का अन्तःसंबंध एक नए प्रत्यय के स्तर पर स्थापित नहीं हुआ है? इस तरह गद्य में कविता की तरह भाषा, भाषा शक्ति के गहरे अन्वेषण और लेखक ने निरन्तर जीवन और भाषा के साथ विभिन्न प्रकार के परिचित सन्दर्भों के भीतर यात्रा करते हुए रूप ग्रहण करती है और यही नहीं इस कृति में एक साथ विभिन्न प्रकार के मनोभावों को छेड़ने में सफल हुई है। यथार्थ न तो सूचनाधर्मी होता है, न महज अनुभव कराने का तथ्य- वृत्तांत।
“अब क्या होगा आचार्य?… यही आशंका तो वशिष्ठ को ग्रसे जा रही थी। दैव्य और कातरता कुहासे की लहरों की तरह उनके मन को बार-बार घेर लेते हैं और आंखों के सामने एक चमकती हुई धुंध छा जाती है जिससे छोटी से छोटी वस्तु इतनी विकराल और विशाल लगने लगती है, समतल मैदान में भी गहरी खाइयों का भ्रम होने लगता है क् चारों ओर अपने मूर्तिमान भय के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता।”
“वसिष्ठ स्वयं भी जानते हैं कि अपराध चेतना उग्ररूप लेने पर इस मनोदशा में पहुंचा देती है और इसलिए वह अपनी भीति को बार-बार झटक कर अलग भी कर देते हैं। …वे उनके जीवन की ऐऐसी ठोस सच्चाइयां बन चुकी हैं कि इनके सामने वास्तविकता भी भ्रम प्रतीत होती है।”
“कैकेई के प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ ने कैकेई पर एक कातर दृष्टि डाली। उनके होठ खुले और फिर बंद हो गए। या तो उन्हें अपने विचारों के अनुरूप शब्द नहीं मिल रहे थे या कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। कुछ देर अनिश्चय की स्थिति से जूझने के बाद उनके मुंह से एक दबी हुई ध्वनि फूटी “डर”। कैकेई को इस समय वशिष्ठ एक शिकारी को देखकर दुबकने के प्रयास में अपने सिर को अपनी ही काया में धंसाते हुए आतंकित खरगोश लगे। …आचार्य की इस दशा को देखकर उन्हें लग रहा था कि ठंडी लहरें उनकी गर्दन से उठकर मेरुरज्जु से होती हुई नीचे की ओर दौड़ रही हैं और उनके हाथ – पांव ठंडे होते जा रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, न ही कुछ पूछा। वह केवल वशिष्ठ को देख रही थीं। वशिष्ठ के चेहरे पर होने वाले परिवर्तन उनके उच्चार को अर्थवत्ता प्रकट कर रहे थे। ”
इस तरह कृति में जटिल यथार्थ और उसे अनुभव की विविध छायाओं का साक्षात्कार होता है। लगता है जैसे रचना विधान में कविता की आंतरिक रचना – प्रक्रिया मूर्तमान हो उठी है। क्या इस भाषा –संरचना के माध्यम से भाषा और कल्पना की संवाद धर्मिता पर विचार नहीं किया जा सकता।
यथार्थ इकहरा नहीं होता। रूपाकात्मकता को ही विकसित करके एक साथ सब कुछ को व्यक्त किया जा सकता है। समाज में व्यक्ति की स्थिति की जगह उसकी चेतना की जटिलताएं महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इस प्रकार भाषा में ही दृश्य, घटना, विचार जन्म लेते हैं। गौर करने की बात है कि चलचित्र में पात्र को रखने वाली ऊर्जा भाषा ही होती है। वही संपूर्ण प्रक्रिया को सुसंगत स्वरूप प्रदान करती है। यह प्रक्रिया वर्णन से नहीं व्यंजना के सौंदर्य ग्रहण करती है।
यहां कृति में कथा प्रवाह दो स्तरों पर एक साथ संश्लिष्ट रूप ग्रहण करता है। एक स्तर पर कथा तो स्थूल प्रसंगों में प्रवाहित होती रही है। दूसरे स्तर पर इन प्रसंगों के संबंध चरित्रों (कैकेई, वशिष्ठ, राम, लक्ष्मण इत्यादि) की मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया एक साथ अलग विशेषता लिए हुए प्रगट होती रहती है। हमने ऊपर वशिष्ठ प्रसंग का उदाहरण दिया है। वहां पाठक को लगता है कि कृति के इस आधुनिक भावबोध में आस्था और संशय का अन्तर्द्वन्द्व अपनी समूची परंपरा के परिप्रेक्ष्य में मूर्तिमान हो उठा है। यहां जीवन मूल्यों के संघर्ष की दोहरी प्रक्रिया की प्रतीति होती है। वशिष्ठ की व्यक्तिगत रणभूमिक उनके भीतर का आभ्यांतरिक अन्तर्संघर्ष है। वस्तुतः अन्तर्जगत का संघर्ष की बहिर्जगत में व्यक्त किया हुआ है। और सामाजिक जीवन का बहिर्संघंर्ष अन्तर्जगत को प्रभावित कर अन्तर्संघर्ष का रूप धारण करता है। अतएव साहित्य सचमुच काल के सर्वसंहारक अंधड़ का प्रतिरोध करता है। इसी को काल चेतना या इतिहास चेतना कहते हैं।
भगवान सिंह ने राम के परंपरागत उनके दैवीय पहचान को अजनबी बना दिया है। यहां भा,क संरचना पात्रों के साथ पाठक की भी मनःस्थिति में संश्लिष्ट आलोड़न पैदा करती है। कथा- संरचना में तत्कालीन सामाजिक जीवन के विभिन्न तत्वों को समेट कर उन्हें व्यवस्थित ही नहीं किया गया है बल्कि उनमें एक नयी अर्थवत्ता दी गई है। लूकाच के शब्दों में कहा जा सकता है कि कला के “ शिखर तक पहुंचने का सीधा रास्ता रूप है।”

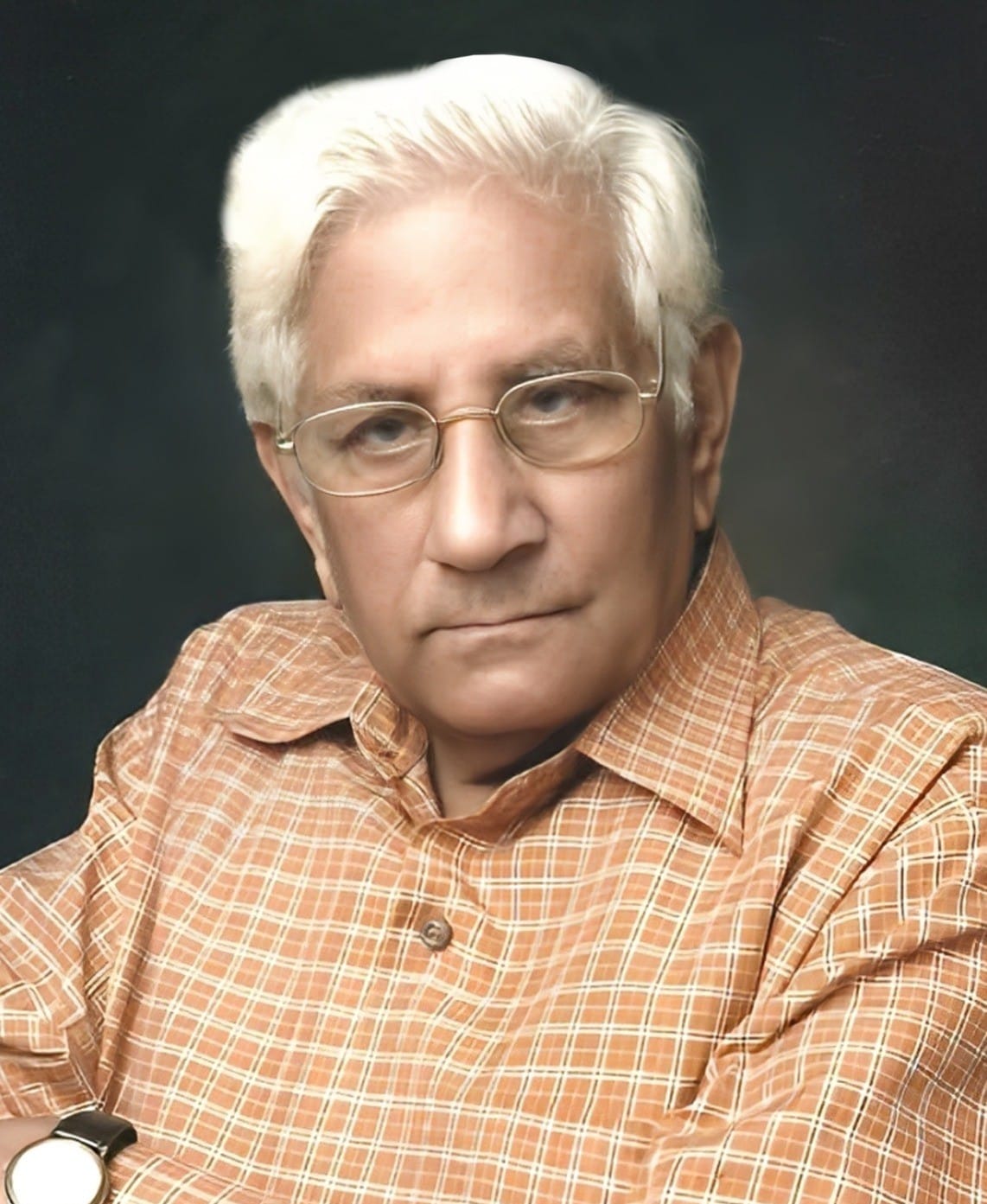

विमल वर्मा साहब द्वारा उपन्यास अपने-अपने राम की व्याख्या बहुत ही गहरी उतरकर देशकाल और परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुए उसे वक्त की सामाजिक संरचनाओं को समझने और विश्लेषित करने की दृष्टिकोण के साथ की गई है। इस व्याख्या की खास बात यह है कि यह पाठक के शाब्दिक और वार्षिक ज्ञान के साथ-साथ उसके पास उपलब्ध शब्दकोश की परीक्षा भी लेती है। इसलिए एक पाठक के लिए इस समीक्षा को पूरा पढ़ने का मतलब है कि एक विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण होना। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि ऐसे परीक्षार्थियों की सफलता का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा नहीं है।