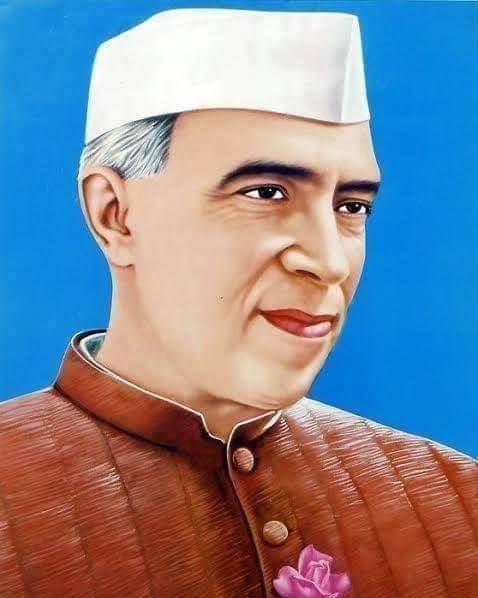जिन आपदाओं के बारे में हम बात करते हैं, वे हमारी प्राथमिकता तय करती है
(फ़ातिमा ओज़्डोगन, यूनिवर्सिटी डी मॉन्ट्रियल और अली असगरी, यॉर्क यूनिवर्सिटी )
मॉन्ट्रियल। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 1989 में, 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस घोषित किया। उस समय, इसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण को दुनिया भर में रोज़मर्रा की सोच का हिस्सा बनाना था।
वर्तमान में यह लक्ष्य पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है, क्योंकि आपदाएं पहले की तुलना में अधिक तीव्रता और आवृत्ति से आ रही हैं। हालांकि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी आपदा जोखिम और उनके प्रभावों को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आपदाओं को लेकर हमारी सोच और बातचीत का तरीका भी कई बार दीर्घकालिक संकटों को नजरअंदाज कर देता है। तात्कालिक घटनाओं जैसे भूकंप, तूफान और जंगल की आग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि जलवायु परिवर्तन जैसे धीमी गति से बढ़ने वाले संकटों पर कम।
ईश्वरीय दंड से मानवीय जिम्मेदारी तक
इतिहास में आपदाओं को अक्सर ईश्वर का दंड या आस्था की परीक्षा के रूप में देखा गया। प्राचीन ग्रंथों जैसे ‘गिलगमेश’ महाकाव्य, इस्लामिक परंपराएं, बौद्ध और हिंदू धर्मों में भी प्राकृतिक आपदाओं को आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से समझा गया।
हालांकि, 1755 में लिस्बन में आए भूकंप के बाद इस सोच में बदलाव आया। वोल्टेयर, रूसो और कांट जैसे प्रबुद्ध विचारकों ने आपदाओं को धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नजरिये से देखने की वकालत की।
मानवजनित जोखिम जैसे फैक्ट्री दुर्घटनाएं और रेल हादसे 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद बढ़े। इसके बाद विशेषज्ञों ने इन घटनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण कर आपदाओं के पूर्वानुमान और रोकथाम की दिशा में काम शुरू किया।
यह 20वीं सदी की शुरुआत में स्पष्ट हुआ कि समाज की संरचना, औद्योगिक नीतियां और तैयारियों का स्तर आपदाओं के प्रभाव को तय करते हैं। 1960 के दशक तक शोध का फोकस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कमजोरियों की ओर गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आपदाएं केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक असमानता, कमजोर शासन और बुनियादी ढांचे की विफलता का परिणाम हैं।
वैश्विक सहयोग और नीतिगत बदलाव
हाल के दशकों में आपदा प्रबंधन में ‘‘सुरक्षा’’ और ‘‘लचीलापन’’ जैसे सिद्धांत प्रमुख हो गए हैं। ह्योगो फ्रेमवर्क (2005–2015) और सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते इसी सोच को प्रतिबिंबित करते हैं।
आज विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि आपदाएं पूरी तरह प्राकृतिक नहीं होतीं, बल्कि इनमें मानवजनित कारण जैसे लापरवाही, गलत नियोजन और सुशासन की कमी भी अहम भूमिका निभाते हैं।
मीडिया का पक्षपातपूर्ण ध्यान
हालिया विश्लेषणों में पाया गया है कि मीडिया अचानक आने वाली आपदाओं को ज्यादा कवरेज देता है, जबकि धीमी गति से होने वाले संकटों को नजरअंदाज करता है। उदाहरण के तौर पर, 2010 में हैती में आए भूकंप की कवरेज में सीबीसी ने एक ही दिन में आठ घंटे तक का समय दिया, जबकि 2011 में अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में आए सूखे को प्रतिदिन औसतन दो मिनट से भी कम समय मिला।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 1970 से 2019 के बीच सूखे ने करीब 6.5 लाख लोगों की जान ली, जबकि इसकी हिस्सेदारी कुल प्राकृतिक आपदाओं में केवल 15 प्रतिशत रही। इसी अवधि में जलवायु और मौसम से जुड़ी घटनाएं आधे से अधिक आपदाएं रहीं और इनसे सबसे अधिक प्रभावित विकासशील देश हुए।
विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन जनित आपदाओं से 21.6 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं। इसी तरह, मृदा क्षरण और समुद्री जल स्तर में वृद्धि जैसे धीमे संकट दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं।
समग्र दृष्टिकोण की जरूरत
विशेषज्ञों का मानना है कि आपदाओं के प्रति हमारी प्राथमिकताओं को बदलना जरूरी है। इसके लिए मानवजनित कारणों को स्वीकार करना, कमजोर सामाजिक ढांचों की समीक्षा करना और समानता आधारित नीति निर्माण करना होगा।
समाज के रूप में हमें समग्र रणनीति अपनानी होगी जो हर प्रकार की आपदाओं को समान रूप से महत्व दे। इससे न केवल आपदा प्रबंधन बेहतर होगा बल्कि भविष्य के लिए हमारी सामूहिक तैयारी भी मजबूत होगी।द कन्वर्सेशन से साभार