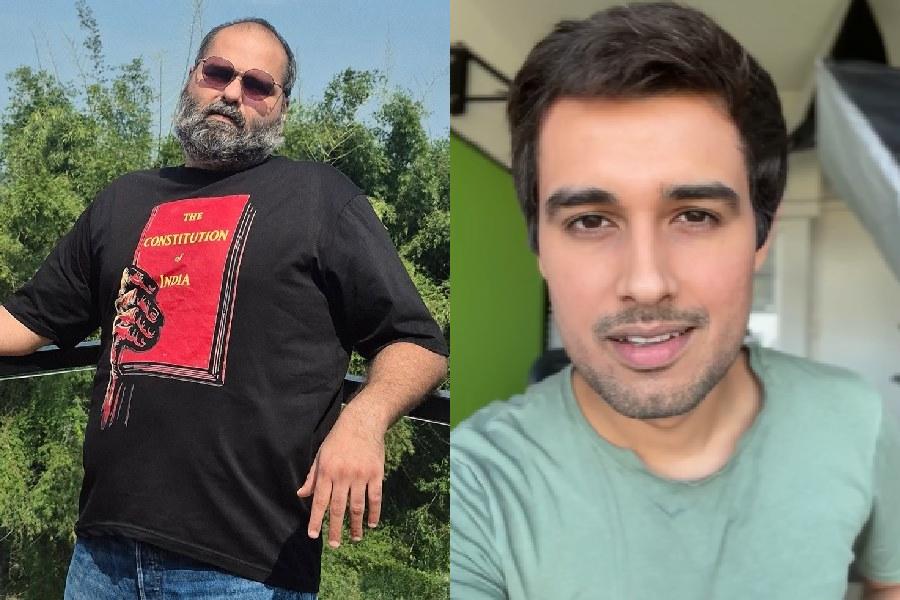चीन को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत
संजय बारू
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में घोषणा की कि चीन कई क्षेत्रों में अमेरिका को कड़ी टक्कर देगा, और आगे कहा, “यह भारत जैसे देश के लिए शिक्षाप्रद है।” चीन इतना सक्षम क्यों है? भारत चीन के रिकॉर्ड और अनुभव से वास्तव में क्या सीख सकता है? अगर चीन का अनुभव भारत के लिए “शिक्षाप्रद” है, तो क्या हमें उसका और गहराई से, लगन से और खुले मन से अध्ययन नहीं करना चाहिए? हमें वास्तव में क्या अध्ययन करना चाहिए? भारतीयों के लिए चीन से सीखने के कौन से माध्यम उपलब्ध हैं? दोनों सरकारें इस तरह के सीखने के अनुभव को सुगम बनाने के लिए कितनी तत्पर होंगी?
हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों के ‘सामान्यीकरण’, जिसका प्रतीक आंशिक रूप से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की बहाली है, से उम्मीद है कि लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। कलकत्ता से जल्द ही ग्वांगझोउ के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी, जो समकालीन चीन के कई गतिशील और तेज़ी से बढ़ते शहरी केंद्रों में से एक है।
उम्मीद है कि यात्रा संबंधों की बहाली और आसान वीज़ा नीति समकालीन चीन को समझने में भारत की रुचि को और व्यापक बनाएगी। उम्मीद है कि दोनों देश छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए पहुँच आसान बनाएँगे, और सिर्फ़ व्यापार और पर्यटन पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। व्यवसायियों के बीच बढ़ते संपर्क और पर्यटन में वृद्धि से दोनों देशों को एक-दूसरे के प्रति बेहतर समझ विकसित करने में भी मदद मिलेगी।
अब तक, चीन के बारे में ज़्यादातर भारतीयों के विचार पश्चिमी विद्वत्ता और मीडिया से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। बहुत कम भारतीयों ने समकालीन चीन का अध्ययन करने और उसे अपने साथी भारतीयों को समझाने में कोई कसर बाकी रखी है। अगर विदेश मंत्री को गंभीरता से लेना है, तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भारतीय चीन के अनुभव से सीख सकें और भारत भी अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सके?
चीन-भारत तनाव ने वर्षों से दोनों देशों में एक-दूसरे के प्रति अत्यधिक पूर्वाग्रही और नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। इससे भी बुरी बात यह है कि चीन के बारे में भारत की राय का एक बड़ा हिस्सा राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विदेश नीति के क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा गया है। सीमा समस्या, उस पर कभी-कभार होने वाली झड़पें, और भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक स्थिति, चीन पर भारतीय विमर्श पर काफी हद तक हावी रहती हैं।
चीन के शासन अनुभव, उसकी आर्थिक नीतियों, शहरी विकास और नगरपालिका प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा आदि पर भारत में शायद ही कोई विशेषज्ञता हो। अब समय आ गया है कि अर्थशास्त्रियों, शहरी योजनाकारों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और ऑटोमोबाइल निर्माण से लेकर पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास और पर्यावरण प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों के व्यवसायियों को चीन को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। हमने भू-राजनीतिक विश्लेषकों से काफी कुछ सुना और पढ़ा है। अब समय आ गया है कि सामाजिक विज्ञान और लोक नीति विश्लेषक, वैज्ञानिक और इंजीनियर आगे आएँ।
भाषा हमेशा से दोनों देशों के बीच सीधे संवाद में बाधा रही है। चीनी तकनीक ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। चीन ने ऐसे उपकरण बनाए हैं जो अनुवाद करते हैं। अगर कोई इस उपकरण में अंग्रेज़ी बोलता है, तो आवाज़ चीनी में और अंग्रेज़ी में अनुवाद हो जाती है। इससे सरल संचार आसान हो गया है। इसके अलावा, अब कई चीनी लोग इतनी अंग्रेज़ी जानते हैं कि वे किसी आगंतुक से बातचीत कर सकें। उम्मीद है कि इससे लोगों के बीच और व्यवसायों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
समकालीन चीन के साथ किसी भी सार्थक बातचीत का प्रारंभिक बिंदु यह है कि हम सबसे पहले उसके प्रभावशाली प्रदर्शन को पहचानें और स्वीकार करें। चीन एक ज्ञान-आधारित समाज और प्रौद्योगिकी-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इसने बुनियादी ढाँचे के विकास में उत्कृष्टता हासिल की है। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू, वुहान और अन्य प्रमुख शहर आधुनिक वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं जो एक साथ अद्भुत और सौंदर्यपूर्ण है। कई चीनी शहर चकाचौंध करते हैं।
अनुभव के लिए तैयार रहना चाहिए। उस अनुभव की सराहना करने और उससे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सदियों से चली आ रही भारतीय अभिजात वर्ग की पश्चिमी सोच ने उसे यह मानने के लिए तैयार नहीं किया है कि सिर्फ़ जापान ही नहीं, बल्कि पूर्व भी उससे आगे निकल गया है।
पिछली सदी के अंत में, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जैसे प्रतिष्ठित भारतीय जापान के आधुनिकीकरण और प्रगति से चकित थे। स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को जापान से सीखने और विज्ञान एवं उद्योग में निवेश करने की सलाह दी थी। टैगोर ने इस देश के बारे में काव्यात्मक रूप से लिखा। विश्वेश्वरैया स्वदेश लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन को नारा दिया, ‘औद्योगीकरण करो या नष्ट हो जाओ।’
कई मायनों में, आज का चीन कल का जापान है। लेकिन तब, जापान के उदय ने भारत में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं पैदा की थी। दरअसल, जवाहरलाल नेहरू इस बात से प्रेरित थे कि 1905 के रूस-जापान युद्ध में जापान एक ‘पश्चिमी’ देश – रूस – को हराने वाला पहला एशियाई देश था। दूसरी ओर, चीन अपने देश में नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ पैदा करता है।
हालाँकि दोनों देशों में ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ का नारा अक्सर लगाया जाता रहा है, लेकिन दोनों देशों ने कई चूकों के ज़रिए लंबे समय तक दोनों देशों के लोगों के बीच अविश्वास और विरोध को बढ़ावा दिया है। दोषारोपण से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों देशों के नेतृत्व, जिनमें वर्तमान नेतृत्व भी शामिल है, ने ऐसी गलतियाँ की हैं जिनसे विश्वास में स्थायी कमी आई है।
हालाँकि, इस बात की पूरी संभावना है कि हम एक बार फिर एक मोड़ पर हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूती से स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों को ऐसा अवसर मिला है और शायद यह आखिरी बार भी नहीं है जब उन्होंने किसी अवसर को गँवाया हो। जब देंग शियाओपिंग राजीव गांधी से मिले, जब वेन जियाबाओ मनमोहन सिंह से मिले, और जब शी जिनपिंग पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले, तो कूटनीतिक माहौल में आशावाद का माहौल व्याप्त था। फिर भी, ऐसे हर अवसर के बाद संबंध बिगड़ते गए।
आज भी, यह उम्मीद करना जल्दबाज़ी होगी कि रिश्तों को बिगाड़ने वाले गंभीर मतभेद सुलझ जाएँगे। भारत अपने पड़ोस में चीनी इरादों, महत्वाकांक्षाओं और निवेशों को लेकर सशंकित रहेगा, जबकि चीन भी पश्चिमी और एशियाई शक्तियों के साथ भारतीय इरादों और संबंधों को लेकर सशंकित रहेगा। चाहे जो भी हो, यह ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों और व्यवसायों के बीच बेहतर संपर्क हो।
भारतीयों को चीन के नागरिक समाज के साथ खुले मन से संपर्क करना चाहिए और न केवल एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र या आधुनिक शहरी बुनियादी ढाँचे के निर्माण में चीन के अनुभव से सीखने को तैयार रहना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि चीन ने अनुसंधान एवं विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और ज्ञान-आधारित राजनीति एवं समाज में किस प्रकार निवेश किया है। वास्तव में, मानव विकास में निवेश की हमारी आवश्यकता को देखते हुए, चीन का अनुभव और रिकॉर्ड भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भारत चीन से सीख सकता है कि अवसर की यह खिड़की बंद होने से पहले अपने ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ का कैसे लाभ उठाया जाए।
नागरिक समाज और व्यावसायिक संपर्क में वृद्धि अपनी चुनौतियाँ पैदा कर सकती है। उम्मीद है कि नौकरशाह, राजनयिक और सुरक्षा समर्थक इस नवजात लेकिन अत्यंत आवश्यक संपर्क को बाधित करने के लिए आगे नहीं आएंगे, जिसे बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रा में आसानी से सुगम बनाया जा सकता है। यह याद रखना उपयोगी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच गंभीर तनाव और मतभेदों के बावजूद, दोनों देशों के बीच लोगों के बीच और व्यावसायिक संपर्क उच्च स्तर पर बना हुआ है। वास्तव में, चीन के साथ अमेरिका का संपर्क भारत के साथ उसके संपर्क से कहीं अधिक व्यापक, गहरा और उच्च है। इसमें एक सबक है। द टेलीग्राफ ऑनलाइन से साभार
संजय बारू बिज़नेस स्टैंडर्ड के संपादक थे। उनकी नवीनतम पुस्तक “सेसेशन ऑफ़ द सक्सेसफुल: द फ़्लाइट आउट ऑफ़ न्यू इंडिया” है।