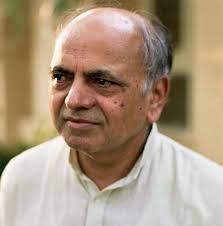मिली-जुली विरासत
सुकान्त चौधरी
सजनिकांत दास पिछली सदी में बंगाली साहित्य जगत में एक जानी-मानी हस्ती थे, उनकी विद्वत्ता के साथ-साथ उनकी हाज़िरजवाबी भी मशहूर थी। उनके जर्नल ‘शनिबारेर चिठी’ में एक कार्टून छपा था जिसमें “मिस्टर आई.सी. बनर्जी” और “वैष्णव श्री मधुसूदन” नाम के किरदार थे। बाद वाले, हालांकि नामाबली पहने हुए थे, लेकिन साफ तौर पर माइकल मधुसूदन दत्त थे, जो बंगाल पुनर्जागरण के पहले महान कवि थे, एक ईसाई धर्म अपनाने वाले और पश्चिमी रंग में रंगे शौकीन इंसान थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी शर्ट पेरिस में धुलवाते थे। सूट और टाई पहने “बीरसिंघा के” आई.सी. बनर्जी, ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय थे: ‘विद्यासागर’, जैसा कि दुनिया उन्हें जानती है, एक डिग्री या अकादमिक उपाधि थी। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बावजूद, उन्होंने जीवन भर धोती, चादर और चप्पल पहनी, जो उनकी सरकारी नौकरी के ड्रेस कोड के खिलाफ था।
टैगोर का तर्क है कि विद्यासागर के आक्रामक बंगाली पहनावे ने आत्म-सम्मान और मन की आज़ादी को दिखाया, जिसे टैगोर औपनिवेशिक भारतीय सोच के बजाय यूरोपीय सोच से जोड़ते हैं। उन्हें वही आज़ाद गरिमा उन अनपढ़ संथालों में भी दिखी, जिनके साथ विद्यासागर ने अपने आखिरी सालों में समय बिताया था।
टैगोर की टिप्पणी बहुत संतुलित है। वह आम औपनिवेशिक भद्रलोक की गुलामी वाली मानसिकता की निंदा करते हैं। लेकिन वह एक दुर्लभ भारतीय भावना की तारीफ़ करते हैं जो पश्चिमी भावना पर हावी हो सकती है। विद्यासागर के स्वाभिमानी स्वभाव में कुछ भी नकल करने जैसा नहीं है। यह उनके अस्तित्व के गहरे मानवीय सार का प्रमाण है।
यह इंसानियत सिर्फ़ भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसमें तर्कसंगत बुद्धि और ज्ञान की खोज शामिल है। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर, विद्यासागर ने इसके एकेडमिक प्रोग्राम में सुधार के लिए कुछ “नोट्स” तैयार किए। उन्होंने घोषणा की कि प्राथमिक लक्ष्य “एक प्रबुद्ध बंगाली साहित्य का निर्माण” होना चाहिए, जिसका मतलब न केवल कल्पनात्मक रचनाएँ बल्कि सभी ग्रंथ या ‘पत्र’ भी हैं। इसके लिए “यूरोपीय स्रोतों से सामग्री इकट्ठा करने” की ज़रूरत थी, जिसे बंगाली में शामिल करने के लिए संस्कृत विद्वानों के भाषाई कौशल की आवश्यकता थी। इसलिए “संस्कृत विद्वानों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य में पारंगत बनाने की आवश्यकता” थी। विद्यासागर ने अपने कॉलेज के पाठ्यक्रम में इस संश्लेषण पर काम किया, जिसका बनारस संस्कृत कॉलेज के ब्रिटिश प्रिंसिपल जेम्स बैलेन्टाइन ने विरोध किया।
तो यहाँ, इसके औपचारिक लॉन्च से एक सदी पहले, ‘तीन-भाषा फ़ॉर्मूला’ का ग्राउंडप्लान है, जो आज़ादी के बाद के असल मॉडल से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। वह हमारी अलग-अलग भूगोल और इतिहास के अलग-अलग तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। इसके उलट, विद्यासागर का मॉडल एक ऑर्गेनिक ढाँचा था। हर तत्व ज्ञान की तीन दुनियाओं को कवर करने वाले एक एकीकृत एजेंडा में एक-दूसरे से जुड़ा हुआ था: सम्मानित अखिल भारतीय परंपरा, इसका खास क्षेत्रीय विकास, और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। यह ज्ञान “वर्नाक्युलर स्कूलों” के नेटवर्क के ज़रिए “आम लोगों” तक पहुँचाया जाना था, जहाँ ऐसे टीचर “वर्नाक्युलर क्लास-बुक्स” पढ़ाते थे जो “अपनी भाषा के माहिर” थे, लेकिन उनके पास आधुनिक पश्चिमी शिक्षा से “उपयोगी जानकारी” भी थी। संस्कृत कॉलेज का मिला-जुला सिलेबस ऐसे टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। असिस्टेंट स्कूल इंस्पेक्टर के तौर पर अपने समय में, विद्यासागर ने ऐसे स्कूल स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिनमें लड़कियों के लिए कुछ स्कूल भी शामिल थे जो सफल नहीं हो पाए।
बैलेंटाइन के जवाब में, विद्यासागर ने “यूरोप के आगे बढ़ते विज्ञान” के महत्व पर ज़ोर दिया, जो अक्सर पारंपरिक भारतीय ज्ञान से अलग हो सकता है। इस मामले में, वे राममोहन राय के 1823 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखे गए पत्र का अनुसरण करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ़ पारंपरिक पूर्वी शिक्षा के लिए पैसे दिए, पहले कलकत्ता मदरसा में और फिर संस्कृत कॉलेज में। बाद वाले प्रस्ताव पर राममोहन ने विरोध में एक बेकार पत्र लिखा, जिसमें “गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञान” में शिक्षा की मांग की गई थी, जैसा कि “यूरोप के देशों” में सिखाया जाता था।
यह एजेंडा पहले से ही हिंदू कॉलेज में चल रहा था, जिसकी स्थापना भारतीयों ने कुछ यूरोपीय समर्थन से की थी। हिंदू संस्थापकों में से कई सैद्धांतिक रूप से रूढ़िवादी थे, इसलिए सुधारवादी राममोहन समझदारी से बैकग्राउंड में रहे; लेकिन वे सभी धर्मनिरपेक्ष “उदार शिक्षा” के पश्चिमी मॉडल के लिए प्रतिबद्ध थे। इसलिए हिंदू कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती थी। सदी के मध्य में इसके पड़ोसी संस्थान में भारतीय और पश्चिमी ज्ञान प्रणालियों को एक साथ लाने का काम विद्यासागर ने किया।
यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के एक लेक्चर से शुरू हुई बहस से जुड़ी है। उन्होंने मैकाले के 1835 के शिक्षा पर दिए गए मिनट के एंग्लिसिस्ट एजेंडा पर आरोप लगाया कि इसने आज तक भारतीयों में गुलामी की मानसिकता पैदा की है, और देसी ज्ञान सिस्टम और संस्कृति को नीचा दिखाया और खत्म किया है।
हो सकता है कि प्रधानमंत्री मैकाले के मिनट और भारतीय शिक्षा पर इसके बुरे असर के बारे में सही हों। लेकिन वह पारंपरिक भारतीय शिक्षा की शक्ति और लचीलेपन और विकसित भारतीय दिमाग की रचनात्मक सोच को कम आंक रहे हैं। राममोहन मैकाले से पहले के हैं। विद्यासागर बाद में आए लेकिन उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया। उस समय तक, भारतीय प्रतिभा पूरब और पश्चिम का अपना मेल बना रही थी, उनकी कई विरासतों को मिलाकर ऐसे नए आविष्कार कर रही थी जो भारतीय पुनर्जागरण और स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण धारा बने।
हमें औपनिवेशिक समय से मिली अपनी विरासत को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए – न कि जो अंग्रेज पीछे छोड़ गए, बल्कि वह जो, अगर हम देखें, तो हमारे अपने देशवासियों ने बनाया और हमें सौंपा। हम एक ज्ञान संबंधी बदलाव के कारण इसकी उपेक्षा करते हैं। राममोहन और विद्यासागर ने एक ऐसी विरासत की नींव रखी जो मौलिक रूप से समावेशी है।
टैगोर के शब्दों में, यह देता है और लेता है, मिलता है और मिल जाता है। इसके उलट, हम बाँटते हैं और झगड़ते हैं, छोटे-मोटे फ़ायदों के लिए टुकड़ों में उलझे रहते हैं। हम एक हिस्से को पकड़ लेते हैं और उसे अकेले में या तो अपना लेते हैं या ठुकरा देते हैं, पूरे ढाँचे को होने वाले नुकसान से बेखबर रहते हैं।
इसलिए हमारे लिए, इंग्लिश सीखना ज़रूरी तौर पर मातृभाषा को नज़रअंदाज़ करना है: कोई बात नहीं कि हमारा दो भाषाओं का ज्ञान सिर्फ़ एक सांस्कृतिक संसाधन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक संपत्ति भी है। चीन और जापान ने जानबूझकर इंग्लिश को बाहर नहीं किया: यह एक ऐतिहासिक कमी थी जिसे वे अब पूरा कर रहे हैं।
फिर से, हमारे लिए, किसी एक ब्रांडेड धर्म या उसके किसी खास कट्टर रूप को मानने का मतलब है दूसरों को बाहर करना और उन पर ज़ुल्म करना। इस तरह हम उन कीमती मिली-जुली परंपराओं को छोड़ देते हैं जो हमारे समाज को एक साथ जोड़े रखती हैं। इससे भी बुरा, हम हिंसा और झगड़े के बीज बोते हैं जहाँ हम शांति की फसल काट सकते थे।
इस तरह हम खुद को अपने औपनिवेशिक अतीत के मलबे तक ही सीमित रखते हैं। हम अपनी अनोखी मिली-जुली विरासत को या तो/या विकल्पों के रूप में देखते हैं, और एक को छोड़कर बाकी सभी फायदों को छोड़ देते हैं। इस तरह हम यह भी खो देते हैं, जबकि मैकाले, क्लाइव और कर्जन के भूत खंडहरों के बीच बैठकर हंसते हैं। द टेलीग्राफ से साभार
सुकांत चौधरी जादवपुर यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर हैं।