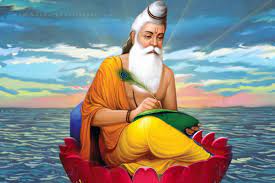जयंती विशेष
भारतीय काव्य के आदिकवि महर्षि वाल्मीकि
अरुण कुमार कैहरबा
महर्षि वाल्मीकि के जीवन के बारे में कोई खास प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन भारतीय साहित्य की अमर कृति रामायण उनकी रचना है। यही उनकी विद्वता, कवित्व, सोच, विचार व संवेदनशीलता का आधार है। इसी रचना में उनके जीवन के प्रसंग भी हैं। रामायण को देश के पहले महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। इस महाकाव्य ने भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य अनेक देशों के समाज, साहित्य व कलाओं को गहरे तक प्रभावित किया है।
महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे। चोरी-डकैती का काम करके गुजर-बसर करते थे। बुरे लोगों की भेंट जब अच्छे और विचारशील लोगों से होती है तो उनका जीवन किस तरह से बदल जाता है, इतिहास में ऐेसे बहुत से प्रसंग हैं। ऐसा ही तब होता है जब नारद ऋषि से रत्नाकर की भेंट होती है। रत्नाकर को सद् कार्यों की महत्ता का अहसास होता है और उनका जीवन बदल जाता है। वे चिंतन, मनन, अध्ययन के काम में समय लगाते हैं और इतिहास में महर्षि बनकर उभरते हैं। उस दिन उनका कवित्व उभर आता है, जब वे खेलने-कूदने में लगे क्रौंच पक्षी के जोड़े पर शिकारी द्वारा हमला करने को देखते हैं। जोड़े में से एक तड़प कर मर जाता है। तभी तपस्वी महर्षि वाल्मीकि सहज भाव से शाप के रूप में श्लोक का उच्चारण करते हैं-‘मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वती: समा:। यत्क्रौंचमिथुनादेकम् अवधी: काममोहितम॥’ यह श£ोक रामायण का पहला छंद था, जिससे भारतीय काव्य परंपरा की शुरूआत मानी जाती है। यही कारण है कि वाल्मीकि को आदिकवि या पहला कवि कहा जाता है।
इससे सिद्ध होता है कि वाल्मीकि की कविता की उत्पत्ति किसी रचनात्मक प्रयोग से नहीं हुई, बल्कि करुणा और संवेदना के विस्फोट से हुई। यह घटना यह दर्शाती है कि कविता केवल भाषा का खेल नहीं, बल्कि भाव का उद्गार है। भाषा का बड़े से बड़ा विद्वान तब तक कविता नहीं लिख सकता, जब तक उसके पास भाव नहीं होंगे। जब तक उसमें दूसरे का दुख देखकर करुणा का भाव नहीं जागेगा। सुमित्रानंदन पंत ने इसकी कल्पना करते हुए पहले कवि के बारे में कहा है- ‘वियोगी होगा पहला कवि, आह से उजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान।’ वाल्मीकि की पहली कविता का जन्म शोक से श्लोक में हुआ।
वाल्मीकि की काव्य-संवेदना की बात करें तो यह अत्यंत गहरी और मानवीय है। उनका काव्य भावों की विविधता से भरा हुआ है। उनके महाकाव्य में करुणा, प्रेम, त्याग और प्रकृति का सौंदर्य एक साथ प्रवाहित होता है। उसका केन्द्र बिंदु मानवता है।
वाल्मीकि की भाषा संस्कृत है। परंतु यह वैदिक संस्कृत नहीं, बल्कि लौकिक संस्कृत, जो सहज, प्रवाहमयी और मधुर है। उनकी शैली में कथात्मकता, संवादात्मकता और चित्रात्मकता का सुंदर समन्वय मिलता है। वाल्मीकि का कवित्व उनके पात्रों की गहराई में दिखाई देता है। वे प्रत्येक पात्र को भावनात्मक और मानवीय बनाते हैं —राम में आदर्श और करुणा दोनों, सीता में प्रेम और आत्मबल दोनों, हनुमान में वीरता और विनम्रता दोनों, रावण में अहंकार और विद्वता दोनों। उनकी यह संतुलित दृष्टि ही उन्हें एक महान कवि बनाती है। वाल्मीकि ने प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि नहीं माना, बल्कि भावनाओं का सहचर बनाया। वन, पर्वत, नदी, ऋतु — सब उनके काव्य में जीवित हैं। उदाहरण देखिए- नदीं तामनुयात्येष राम: सगरसूनुवत। (राम उस नदी के तट पर ऐसे चलते हैं जैसे सगर के पुत्र समुद्र की ओर बढ़े हों।) यह उपमा दृश्य रचने के साथ-साथ चरित्र की गरिमा को भी उभारती है।
वाल्मीकि के काव्य का उद्देश्य केवल सौंदर्य का प्रदर्शन करना ही नहीं है। बल्कि उनके काव्य में रस और नीति का संतुलन है। वे नीति व आदर्शों का संवर्धन करते हैं। उनका काव्य इस बात का प्रमाण है कि कविता केवल जीवन का अनुकरण ही नहीं करती, बल्कि जीवन का निर्देशन भी करती है। वैसे तो कवि वाल्मीकि की कविता में सभी रसों का समावेश है, लेकिन करुण रस प्रमुख है। सीता वियोग, दशरथ में करुण रस, सेतु निर्माण व रावण वध में वीर रस, राम सीता मिलन में शृंगार, वन के वातावरण में शांत रस, हनुमान लंगा गमन में अद्भुत रस बहुत ही सुंदर बन पड़ा है।
महर्षि वाल्मीकि का कवित्व उनके व्यक्तित्व की झांकी है। किसी कवि का आकलन करने के लिए उनकी कविता पर्याप्त मानी जानी चाहिए। वाल्मीकि की रामायण ने न केवल भारतीय काव्य का स्वरूप गढ़ा बल्कि आने वाले सभी काव्य रूपों— महाकाव्य, लघुकाव्य, नाटक, गद्य-काव्य — की बुनियाद रखी। उनकी देन केवल साहित्यिक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक, नैतिक और सौंदर्यबोध की दृष्टि से भी अनुपम है। वाल्मीकि की काव्य-दृष्टि ने केवल भारतीय साहित्य को नहीं, बल्कि विश्व साहित्य को भी प्रभावित किया।
रामायण की कथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों—इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार— की कला, नृत्य और नाट्य परंपरा में जीवित है। वाल्मीकि ने नायक के नैतिक संघर्ष की जो संरचना दी, वही आगे चलकर आधुनिक साहित्य तक पहुँची।
वाल्मीकि के अनुसार—काव्य मानवता का साधन है, न कि विलास का। उनका कविता में शब्द, लय और भाव मिलकर मनुष्य के भीतर करुणा और सत्य को जागृत करते हैं। इस दृष्टि से वे केवल कवि नहीं, बल्कि काव्य-दर्शन के प्रवर्तक हैं।
महर्षि वाल्मीकि की देन केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक परंपरा का सूत्रपात है—जिसमें भाव, विचार, नीति और कला का अद्भुत संगम है। भारतीय काव्य परंपरा का जो वृक्ष आज भी फल-फूल रहा है, उसकी जड़ें वाल्मीकि के उस एक श्लोक में हैं, जिसने शोक को श्लोक बना दिया और मानवता को काव्य का अमर उपहार दिया।
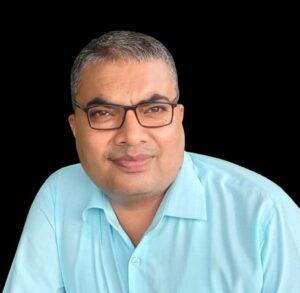
अरुण कैहरबा