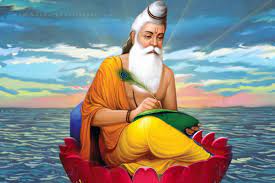जयंती पर विशेष
महर्षि वाल्मीकि, रामायण की रचना और वाल्मीकि समुदाय
मनजीत सिंह
राम कथा के इतिहास में महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के आश्रम चर्चित थे। लेकिन वाल्मीकि जी के आश्रम की ख्याति का एक और कारण भी था। वे पूर्व इतिहास को लिख भी रहे थे और नए इतिहास को गढ़ भी रहे थे। इस आश्रम की प्रसिद्धि के तीन मुख्य कारण हैं। यहां बैठ कर महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचन्द्र जी के इतिहास को लिपिबद्ध किया था। अयोध्या नरेश दशरथ और उनके सुपुत्र राम के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं यथा राम वनवास, राम-रावण विवाद, रावण द्वारा सीता का अपहरण, राम द्वारा सामान्य जन का संगठन खड़ा करना और उसी संगठन के बलबूते महाशक्तिशाली रावण को पराजित करना, अयोध्या का शासन सम्भालना, इस सब को पहली बार वाल्मीकि ने ही भविष्य की पीढिय़ों के लिए समग्र रूप में सुरक्षित किया। राम के इतिहास की अनेक घटनाओं का यह आश्रम साक्षी भी कहा जा सकता है। अयोध्या वापस आने पर राम के जीवन में एक लोकोपवाद का प्रसंग उपस्थित हो गया। वह किसी प्रजा जन द्वारा सीता पर लगाया गया आक्षेप था। राम के सामने संकट उपस्थित हो गया है। शायद सीता अपहरण से भी बड़ा संकट। उन्हें सीता पर सन्देह नहीं था, लेकिन प्रश्न सीता का तो था ही नहीं, यहां प्रश्न प्रजा का था। आक्षेप लगाने वाला राज्य की प्रजा में से था। आज की शब्दावली में कहें तो राज्य का नागरिक था।
इस स्थिति में राम के सामने अनेक विकल्प थे। पहला विकल्प तो अंग्रेजी भाषा में कहें तो इग्नोर करने का था। ऐसे अनेक लोग कहते रहते हैं। दूसरा विकल्प निराधार लांछन लगाने के आरोप में दोषी को दंड देने का है।
लेकिन राम ने राज्य व्यवस्था का एक नया सूत्र दिया। राज की व्यवस्था चाहे लोकतंत्र की हो, कुलीनतंत्र की या फिर राजतंत्र की ही क्यों न हो, राज तो लोकलाज से चलता है। यह किसी भी राज्य व्यवस्था का आदर्श या चरम बिन्दु कहा जा सकता है। उस चरम बिन्दु को व्यावहारिक रूप में धारण करना कितना मुश्किल है, वही क्षण राम के सामने उपस्थित हो गया था। यह परीक्षा की घड़ी थी। राम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने सीता का त्याग कर दिया। शायद सीता भी जानती थीं कि यह राजा या शासक होने का राम द्वारा स्वयं को दिया गया दंड है। राज सिंहासन यदि प्रजा द्वारा दिया गया पुरस्कार है तो प्रजा द्वारा दिया गया यह दंड भी राजा को लेना ही होगा। राज सिंहासन कांटों का ताज है। राजा यह ताज इसलिए धारण करता है ताकि प्रजा का मार्ग कंटक मुक्त हो जाए। राम को जब उनके पिता ने बनवास दे दिया था, तब राम ने उफ्फ तक नहीं किया था और अब जब सीता को वनवास मिल रहा था तो उसने भी उफ्फ नहीं किया। राम भविष्य के शासकों के लिए राजधर्म के मानदंड निर्धारित कर रहे थे। राज लोकलाज से चलता है।
राम के इतिहास का यह दूसरा हिस्सा है। राम स्वयं अयोध्या में थे, लेकिन उनकी अर्धांगिनी वाल्मीकि के आश्रम में आ गई थीं। इस प्रकार राम के वंश के इतिहास का यह दूसरा अध्याय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में घटित भी हो रहा है और साथ-साथ लिपिबद्ध भी किया जा रहा है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि, राम के इतिहास के केवल लेखक न रह कर, स्वयं उसका हिस्सा बन जाते हैं।
गर्भवती सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय पाती हैं। इसी आश्रम में राम के दोनों पुत्रों लव एवं कुश का लालन-पालन होता था। इस तरह ज्ञान साधना का वाल्मीकि आश्रम शस्त्र साधना का केन्द्र भी बन गया था। यहां लव-कुश के साथ ही हजारों युवा शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। यहां देश की सामाजिक व्यवस्था में भी एक नया प्रयोग हो रहा था। अभी तक की सामाजिक व्यवस्था में जो ज्ञान अर्जित करने में रुचि रखता था, उसे शस्त्रों के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं समझी जाती थी। जो शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, उनका ज्ञान साधना से कोई ताल्लुक नहीं होता था। लेकिन महर्षि वाल्मीकि भविष्य द्रष्टा थे। वे देश के भविष्य को देख रहे थे। हजारों वर्षों दूर के भविष्य को। अब वाल्मीकि से शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा केवल लव-कुश ही नहीं ले रहे थे बल्कि सप्त सिन्धु क्षेत्र के लाखों युवा इस आश्रम की ओर खिंचे चले आ रहे थे। महर्षि वाल्मीकि के लिए वे सभी लव और कुश का रूप ही हो गए थे। ये लोग सभी जातियों, सभी वर्णों के थे।
आज जिनको जनजाति समुदाय कहा जाता है, उन समुदायों के लोग भी यहां थे। वाल्मीकि आश्रम सही अर्थों में, यदि आज की शब्दावली में कहें तो समाजिक समरसता का राष्ट्रीय मंच बन गया था। लेकिन यकीनन इसमें सप्त सिन्धु क्षेत्र के लोग सर्वाधिक थे। ‘शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम्’ का पहला उदाहरण भी सप्त सिन्धु क्षेत्र का यह वाल्मीकि समाज ही कहा जा सकता है। राम के इतिहास का पूर्वार्ध आश्रमों से ही जुड़ा हुआ था। वशिष्ठ का आश्रम, विश्वामित्र का आश्रम। लेकिन वाल्मीकि के आश्रम की महत्ता इसलिए थी कि वे केवल राम की सन्तानों को ही नहीं बल्कि उनके साथ सामान्य युवाओं को भी प्रशिक्षित करके इस यात्रा के सनातन प्रवाह को आगे बढ़ा रहे थे। और यही उनके आश्रम की प्रसिद्धि का तीसरा कारण था। वे नए वाल्मीकि समाज की रचना कर रहे थे। उसे आकार दे रहे थे।
वाल्मीकि समुदाय का उदय
वाल्मीकि आश्रम में इन सभी जातियों के श्रद्धालुओं की अलग-अलग जातिगत पहचान समाप्त होकर एक नई पहचान उभर रही थी। महर्षि वाल्मीकि के शिष्य होने के नाते ये सभी अब वाल्मीकि हो गए। इसलिए ये वाल्मीकि कहे जाने लगे। सप्त सिन्धु क्षेत्र में एक नया समाज वाल्मीकि समाज आकार ग्रहण कर रहा था। वाल्मीकि कोई जाति नहीं थी बल्कि अनेक जातियों का एक समाज था। इस समाज में जातियों का अलग स्वरूप घुल गया था। यही कारण है कि वाल्मीकि समाज में अनेक जातियों के गोत्र पाए जाते हैं। आज के सन्दर्भ में इसका साम्य तलाशना हो तो ‘राधा स्वामी’ समाज में देखा जा सकता है। राधा स्वामी केन्द्र या आश्रम में आस्था रखने वाले श्रद्धालु की एक नई पहचान बनती है। यह नई पहचान राधा स्वामी कहलाती है। लेकिन राधा स्वामी कोई जाति नहीं है। राधा स्वामी समाज में अनेक जातियों के व्यक्ति हैं। दो सौ साल बाद यह जाति की पहचान राधा स्वामी पहचान में ही घुल जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि समाज की पहचान को समझा जा सकता है।
वाल्मीकि के आश्रम में तो एक साथ ही ज्ञान साधना, शस्त्र साधना और संगीत साधना हो रही थी। इसलिए सभी साधक संगीत में भी निपुण हो रहे थे। आश्रम में विद्वानों या ऋषि-मुनियों का आना-जाना लगा रहता था। लव और कुश दोनों भाई वाल्मीकि की आज्ञा से आश्रम में राम कथा का गायन करते। आश्रम का पूरा वाल्मीकि समाज राम कथा का गायन करता था। यह समाज राम कथा गा-गाकर राममय हो गया था। दूर-दूर से श्रोतागण इस संगीत की धारा का रसास्वादन करने के लिए पहुंचते थे। एक ऐसा वाल्मीकि समाज आकार ग्रहण कर रहा था जिसमें चारों वर्णों की योग्यता समाहित थी। वाल्मीकि समाज और राम कथा एकाकार हो गई थी। राम कथा के इतिहास की एक जड़ सप्त सिन्धु क्षेत्र में भी थी। उसके बाद यह जड़ कभी नहीं सूखी।
भारतीय साहित्य के इतिहास में राम कथा 2400 सालों से पढ़ी, सुनी और लिखी जा रही है। इन 2400 सालों में हर शताब्दी में कोई एक रामकथा लिखी गई है। भारत के अलावा नौ देश और हैं जहां रामायण को किसी न किसी रूप में पढ़ा और सुना जाता है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल शासकों ने भी वाल्मीकि रामायण को उर्दू में अनुवाद कराया था।
रामकथा पर कई विद्वानों ने रिसर्च की है, लेकिन सबसे डिटेल रिसर्च करने वालों में प्रो. फादर कामिल बुल्के का नाम है। 1935 में बेल्जियम से भारत आए मिशनरी कामिल बुल्के तुलसीदास की रामचरितमानस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रामकथा पर ही पीएचडी कर डाली। प्रो. बुल्के ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लिखी गई रामकथा पर रिसर्च की, उनकी इसी रिसर्च थीसिस पर ‘रामकथा’ नाम से किताब भी पब्लिश की गई। इसी किताब में दुनिया की उन तमाम रामकथाओं का जिक्र है। दुनिया में 400 रामकथाएं हैं। करीब 3,000 से ज्यादा ग्रंथों में राम का जिक्र है। रामनवमी पर प्रो. बुल्के की इसी रिसर्च से रामकथा की पूरी कहानी…
वाल्मीकि रामायण पहली, लेकिन राम का जिक्र उससे भी 100 साल पहले
साधारणतः ये माना जाता है कि राम के जीवन पर सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण है। कुछ हद तक यह सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम का पहली बार उल्लेख वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में किया था। वेदों में राम का नाम एक-दो स्थानों पर मिलता है।
ऋग्वेद में एक स्थान पर राम के नाम का उल्लेख मिलता है, ये तो स्पष्ट नहीं है कि ये रामायण वाले ही राम हैं, लेकिन ऋग्वेद में राम नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा का उल्लेख है। रामकथा का सबसे पहला उल्लेख ‘दशरथ जातक कथा’ में मिलता है। जो ईसा से 400 साल (अब से 2400 साल) पहले लिखी गई थी। इसके बाद ईसा से 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है।
वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है, क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन ही थे और सीता ने उनके आश्रम में ही लव-कुश को जन्म दिया था। लव-कुश ने ही राम को दरबार में वाल्मीकि की लिखी रामायण सुनाई थी।
ऋग्वेद में सीता को माना गया है कृषि की देवी, घास से मूर्ति बनाने का विधान
ऋग्वेद में अकेले राम का नहीं, सीता का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद ने सीता को कृषि की देवी माना है। बेहतर कृषि उत्पादन और भूमि के दोहन के लिए सीता की स्तुतियां भी मिलती हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सूक्त है जो कृषि के देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखा गया है। वायु, इंद्र आदि के साथ सीता की भी स्तुति की गई है। ‘काठक ग्राह्यसूत्र’ में भी उत्तम कृषि के लिए यज्ञ विधि दी गई है जिसमें सीता के नाम का उल्लेख मिलता है। साथ ही विधान भी बताया गया है कि खस आदि सुगंधित घास से सीता देवी की मूर्ति यज्ञ के लिए बनाई जाती है।
अध्यात्म रामायण में राम के साथ वनवास पर जाने के लिए सीता का अजीब तर्क
13वीं-14वीं सदी के ‘अध्यात्म रामायण’ और ‘उदार-राघव’ इन दो ग्रंथों में राम के वनवास वाले प्रसंग में राम और सीता का संवाद है, जिसमें सीता राम के साथ वनवास पर जाने के लिए अजीब तर्क दे रही हैं। प्रसंग है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। सीता साथ जाने की जिद पर अड़ी थीं। राम सीता को अयोध्या में ही रुकने के लिए अपने तर्क दे रहे थे। जब सीता को लगा कि राम नहीं मानेंगे और उन्हें अयोध्या में ही छोड़ कर अकेले जंगल चले जाएंगे तो सीता ने राम से कहा कि आज तक मैंने जितनी रामकथाएं सुनी हैं, उन सब में सीता राम के ही साथ वनवास पर जाती हैं तो आप मुझे यहां क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। सीता के इस तर्क के बाद राम मान गए और सीता उनके साथ वनवास पर चल दीं।
आनंद रामायण में सीता ने हनुमान को कंगन बेचकर फल खरीदने के लिए कहा
हनुमान का लंका में जाकर सीता से मिलना, अशोक वाटिका उजाड़ना और लंका को जलाने वाला प्रसंग तो लगभग सभी को पता है, लेकिन कुछ रामकथाओं में इसमें भी बहुत अंतर मिलता है। जैसे 14वी शताब्दी में लिखी गई ‘आनंद रामायण’ में उल्लेख मिलता है कि जब सीता से अशोक वाटिका में मिलने के बाद हनुमान को भूख लगी तो सीता ने अपने हाथ के कंगन उतारकर हनुमान को दिए और कहा कि लंका की दुकानों में ये कंगन बेचकर फल खरीद लो और अपनी भूख मिटा लो।
सीता के पास दो आम रखे थे सीता ने वो भी हनुमान को दे दिए। हनुमान के पूछने पर सीता ने बताया कि ये फल इसी अशोक वाटिका के हैं, तब हनुमान ने सीता से कहा कि वे इसी वाटिका से फल लेकर खाएंगे।
रंगनाथ रामायण में हनुमान ने विभीषण के लिए बनाई थी नई लंका
सेरीराम रामायण’ सहित कुछ रामायणों में एक प्रसंग मिलता है कि रावण ने विभीषण को समुद्र में फेंक दिया था। वह एक मगर की पीठ पर चढ़ गया, बाद में हनुमान ने उसे बचाया और राम से मिलवाया। विभीषण के साथ रावण का एक भाई इंद्रजीत भी था और एक बेटा चैत्र कुमार भी राम की शरण में आ गया था। राम ने विभीषण को युद्ध के पहले ही लंका का अगला राजा घोषित कर दिया था।
‘रंगनाथ रामायण’ में उल्लेख है कि विभीषण के राज्याभिषेक के लिए हनुमान ने एक बालूरेत की लंका बनाई थी। जिसे हनुमत्लंका (सिकतोद्भव लंका) के नाम से जाना गया। कुछ ग्रंथों में ये भी उल्लेख मिलता है कि अशोक वाटिका में सीता की पहरेदारी करने वाली राक्षसी त्रिजटा विभीषण की ही बेटी थी।
हनुमान ने राम को सलाह दी थी कि विभीषण से हमें मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी त्रिजटा सीता के प्रति मातृवत यानी माता के समान भाव रखती है।
उर्दू में भी रामकथा
अकबर-जहांगीर और शाहजहां के समय में रामकथा सिर्फ संस्कृत या हिंदी ही नहीं, उर्दू और फारसी में भी अनुवाद किया गया है। 1584 से 1589 के बीच अकबर ने अल बदायूनी से वाल्मीकि रामायण का उर्दू अनुवाद कराया था। जहांगीर के शासन काल में तुलसीदास के समकालीन गिरिधर दास ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। इसी काल में मुल्ला मसीही ने ‘रामायण मसीही’ भी लिखी थी। शाहजहां के समय ‘रामायण फैजी’ लिखी गई। 17वीं शताब्दी में ‘तर्जुमा-ए-रामायण’ भी लिखी गई। ये सभी वाल्मीकि रामायण के ही उर्दू ट्रांसलेशन थे।
16 वीं शताब्दी से अभी तक कई विदेशियों ने लिखी राम की कहानी
16वीं शताब्दी के बाद से भारत में कई ऐसे विदेशी भारत आए जिन्होंने रामकथा पर रिसर्च की और अपने हिसाब से उसे नए सिरे से लिखा।
1609 में जे. फेनिचियो नाम के मिशनरी ने लिब्रो डा सैटा नाम की किताब लिखी। इसमें विष्णु के दशावतार और रामकथा की पूरी डिटेल थी। ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी।
17वीं शताब्दी में ए. रोजेरियुस नाम के डच पादरी 11 साल भारत में रहे थे। 1651 में उनकी किताब द ओपन दोरे में रामकथा थी। ये भी वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित थी। इसमें राम के अवतार से उनके रावण वध के बाद अयोध्या लौटने तक की कहानी थी।
1658 में श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में छह साल तक रहे पी. बलडेयुस ने डच भाषा में लिखी किताब आफगोडेरैय डर ओस्ट इण्डिशे हाइडेनन में राम जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की कहानी है। इसमें सीता की अग्निपरीक्षा का भी जिक्र है।
18वीं शताब्दी में एम. सोनेरा नाम के एक फ्रेंच यात्री ने बोयाज ओस इण्ड ओरियंटल नाम की किताब लिखी थी, जिसमें एक छोटी राम कथा है। इस कथा के मुताबिक राम 15 साल की उम्र में अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास पर गए थे।
ऐसे ही 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच करीब 15 अलग-अलग यात्रियों ने भारत घूमने के बाद अपनी किताबों में राम कथा का जिक्र किया है। इनमें से ज्यादातर वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित हैं। फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली और डच भाषा की किताबों में राम का जिक्र मिलता है।
कौन थे फादर कामिल बुल्के
फादर कामिल बुल्के 1 सितंबर 1909 को बेल्जियम में पैदा हुए। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में बी.एससी करने के बाद 1935 में भारत आए। कुछ समय वे दार्जिलिंग में रहे। यहां उन्होंने तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बारे में सुना। रामचरितमानस से उन्हें काफी लगाव हुआ और इसी पर उन्होंने पढ़ाई शुरू की। 1941 में वे पादरी हो गए। उन्हें सबसे ज्यादा लगाव हिंदी साहित्य और तुलसीदास से था। 1945 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने हिंदी साहित्य की डिग्री ली। यहीं से रामकथा में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की।
प्रो. बुल्के की लिखी हिंदी-अंग्रेजी डिक्शनरी को सभी जगह मान्यता मिली। रामकथा पर उनकी रिसर्च को ही किताब के रूप में पब्लिश किया गया जिसका नाम था ‘रामकथा का विकास’। हिंदी भाषा के विकास और रामकथा पर रिसर्च के चलते 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को प्रो. बुल्के का निधन हो गया।
रामचरित मानस का फारसी और उर्दू में भी अनुवाद
रामचरित मानस को संस्कृत के अलावा फारसी और उर्दू में भी अनुवाद किया गया है. आज उन्हीं के बारे में जानते हैं।
भारत हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द का देश है। यह वह मुल्क है जहां लोग मजहब के नाम पर एकजुट होते हैं न कि उनमें मतभेद होता है। यह मुल्क़ अल्लामा इकबाल की उन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाला मुल्क है जिसमें उन्होंने कहा है कि ”मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना”। भारत राम और रहीम का मुल्क है। यहां एक सिख मोहम्मद साहब के बारे में जान सकता है तो वहीं एक मुस्लिम भगवान राम के बारे लिख सकता है। एक हिन्दू गुरू गोविंद सिंह की वंदना कर सकता है। भारत सभी मजहबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है।
गंगा जमुनी तहजीब ही है कि हिन्दुओं के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथों में एक ‘रामचरित मानस’ का कई मुसलमान शासकों ने उर्दू-फारसी में अनुवाद करवाया। राम वो नाम है जो हिन्दी, संस्कृत और उर्दू का भी भेद मिटा देता है। आइए जानते हैं रामचरित मानस मानस का कब-कब तर्जुमा फारसी और उर्दू में हुआ है।
अकबर ने सबसे पहले रामचरित मानस का फारसी में अनुवाद करवाया था।
अकबर ने वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी गई रामायण को पहली बार फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। 1584 में अकबर के आदेश के बाद मुल्ला अब्दुल बदायुनी ने पहली बार फारसी में रामायण का अनुवाद किया। इसका अनुवाद करने में बदायुनी को चार साल लगे। इसको लिखने के दौरान अब्दुल बदायुनी एक ब्राह्मण देबी मिश्र को नियुक्त किया था।
कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध (सिपाही विद्रोह) के बाद हुई लूट में फारसी रामायण की पांडुलिपि खो गई, हालांकि अकबर ने इसकी प्रतियां बनाने की अनुमति अपने दरबारियों को दी थी. इस फारसी रामायण की कुछ प्रतियां अभी भी दुनिया की कुछ लाइब्रेरी में मौजूद हैं। सबसे अच्छी स्थिति वाली प्रति महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय, जयपुर में मौजूद है। इसके अलावा एक अन्य प्रति जो अकबर की अनुमति से अब्दुल-रहीम खान-ऐ-खाना के लिए तैयार की गई थी, को फ्रीर आर्ट गैलरी, वाशिंगटन में संरक्षित किया गया है।
इसके अलावा 1623 ईस्वी में फारसी के प्रसिद्ध कवि शेख साद मसीहा ने भी ‘दास्ताने राम व सीता’ शीर्षक से रामकथा लिखी थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान फ़ारसी में रामायण के दो अन्य अनुवाद मुल्ला शेख सादुल्लाह और गिरदास द्वारा किए गए थे। शेख सादुल्ला ने बनारस में 12 साल संस्कृत की पढ़ाई और फिर रामायण की रचना की।
शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने रामायण का फारसी में खुद अनुवाद किया था। इसकी पांडुलिपि वर्तमान में जम्मू के एक व्यवसायी शाम लाल अंगारा के पास है। इस रामायण का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह “बिस्मिल्लाह-ए-रहमान अर-रहीम” से शुरू होती है। रामायण को 23 से ज्यादा बार फारसी में लिखा गया है। इनमें से कुछ का मूल संस्कृत से अनुवाद किया गया है जबकि अन्य तुलसीदास की रामायण पर आधारित हैं।
उर्दू में रामायण
उर्दू में लिखी गई रामायण पर दो दशक से भी ज्यादा शोध करने वाले अली जव्वाद ज़ैदी के मुताबिक उर्दू में पहली रामायण कई सौ साल पहले उर्दू में लिखी गई। उर्दू में पहली रामायण छंदबद्ध रूप में जगन्नाथ खुशरा ने लिखा था। इसको अदभुत रामायण का नाम दिया था। वहीं रामचरित मानस को उर्दू में नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में पहली बार छापी गई थी। रामायण का छंदबद्ध उर्दू अनुवाद पहली बार फिराकी साहब ने किया था।
मौलवी बादशाह हुसैन राणा लखनवी का रामायण
फारसी की तरह रामायण को उर्दू में भी कई बार तजुर्मा हुआ है। 1935 में मौलवी बादशाह हुसैन राणा लखनवी ने रामायण का उर्दू में अनुवाद किया। इन्होंने नौ पन्नों की रामायण लिखी. इनमें वनवास का खूबसूरत चित्र प्रस्तुत किया गया है। रामायण के उर्दू अनुवाद का एक उदाहरण देखिए…
रंजो हसरत की घटा सीता के दिल पर छा गई
गोया जूही की कली ओस से मुरझा गई।
इसके अलावा उर्दू में एक और राम कथा पर एक ग्रंथ रघुवंशी उर्दू रामायण वर्ष 1996 में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक बाबू सिंह बाल्यान हैं। यह एक प्रकार का शोध ग्रंथ है, जिसमें सभी प्रकार की उपलब्ध रामकथाओं तथा उनके लेखकों का विवरण दिया गया है।
अरबी में भी मौजूद है रामायण
उर्दू-फारसी की तरह ही अरबी में भी इसका अनुवाद हुआ है। क़तर-दोहा में इस्लामी संग्रहालय में रामायण के सबसे उत्तम अरबी अनुवादों में से एक रखा गया है। हालांकि इसके लेखन का विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसे श्रीलंका से प्राप्त किया गया था यह पुस्तक भारत में मुगल काल के दौरान 16 वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई थी यह सुंदर चित्रण के साथ स्पष्ट अरबी लिपि में लिखा गया है।
इंडोनेशिया में संग्रहालयों में अरबी में रामायण की कई किताबें हैं।
बिना बात यार किसी के हाथ न लगाता,
हम देसिया का खून होवे आग ते भी ताता,
यो जिसकी हवा में मुह फुल रया से तेरा,
तेरी जाड़ा में भारे एक मुक्का भतेरा,
पकड़ के न्याड़ धरती में गाड़दा,
लाईये न होड़ सारे चल्ले हाथ जोड़,
वाल्मीकि के सा बेटा कती तोड़ पाड़दा,
बड़ा खुद ने बतावे जो ये अकड़ दिखावे,
सुण मिन्ट भी लग्गे तेरी सारी झाड़ दा !!

लेखक मनजीत सिंह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उर्दू के सहायक प्राध्यापक हैं।