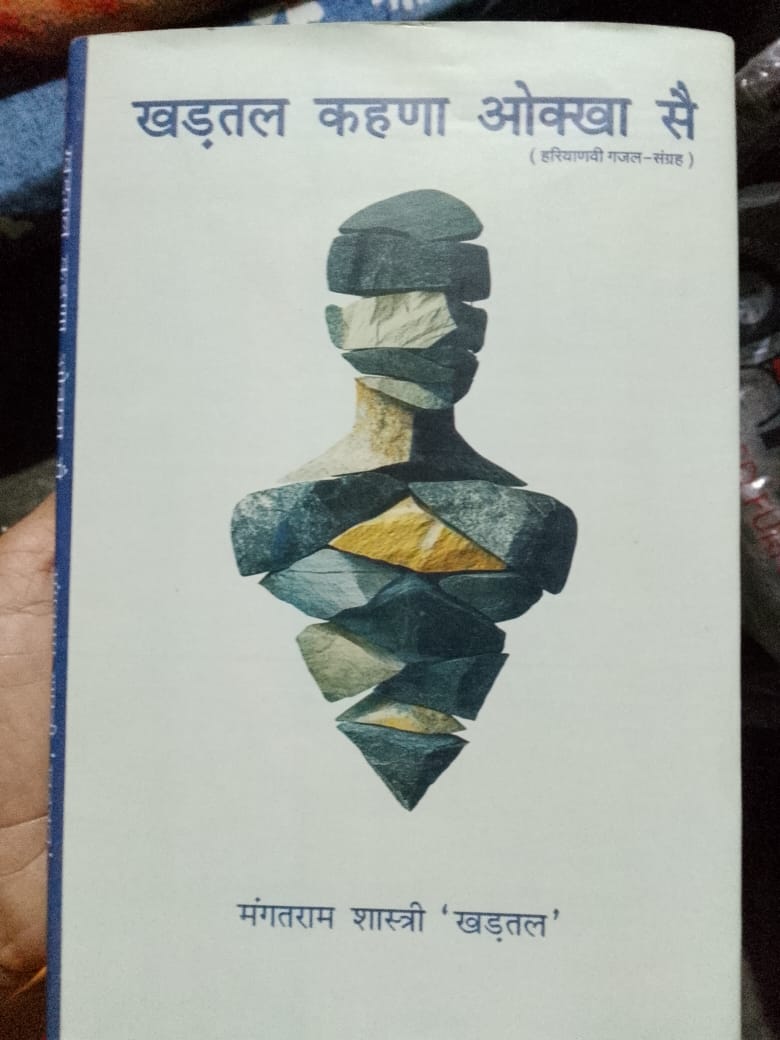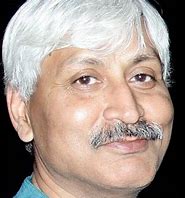
अपूर्वानंद
किसी की मृत्यु के बाद उसे कैसे याद किया जाना चाहिए? खास तौर पर उस व्यक्ति को जिसने ऐसी सरकार में सेवा की हो जो मुस्लिम विरोधी नीतियों और कार्यों के लिए जानी जाती हो? किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर कैसे शोक मनाया जाना चाहिए जिसने फासीवादी शासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो? किसी ऐसे व्यक्ति में गुण कैसे खोजे जाने चाहिए जिसने अपनी बुद्धि को फासीवादी नेता और पार्टी की सेवा में समर्पित कर दिया हो?
भारत में यह परंपरा रही है कि मृतक के बारे में बुरा नहीं कहा जाता। यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सबसे पहले खुद को स्वयंसेवक बताया था – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य – और भारत में मुस्लिम विरोधी राजनीति को लोकप्रिय बनाया, की मृत्यु के बाद भी सभी तरह के राजनेताओं ने उनकी प्रशंसा की।
लाल कृष्ण आडवाणी शारीरिक रूप से जीवित हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से मृत हैं। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो उस व्यक्ति में गुण तलाशते हैं जिसने भारत में मुस्लिम विरोधी राजनीति को ‘हिंदू धर्म’ का हिस्सा बनाने में सबसे कुख्यात भूमिका निभाई और जिसने बाबरी मस्जिद विध्वंस अभियान का नेतृत्व किया। जबकि उनके अभियान के परिणामस्वरूप हजारों मुसलमान मारे गए, हमें उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करने के लिए कहा जाता है जो सिनेमा का शौकीन था और अच्छा खाना पसंद करता था।
हम सभी को याद है कि सुषमा स्वराज की मृत्यु पर सभी राजनीतिक हलकों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर सिर मुंडवाने और नंगे फर्श पर सोने की उनकी धमकी को उनकी मृत्यु के समय भुला दिया गया। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनीं तो वह हमेशा के लिए हिंदू विधवा का जीवन जिएंगी। किसी तरह हम उन लोगों को प्रशंसनीय मानते हैं जिनकी राजनीति ‘विदेशियों’ के प्रति घृणा पर आधारित है।
क्या नफरत के प्रति यह सहिष्णुता हमारा राष्ट्रीय चरित्र है?
यह चिंतन नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय की मृत्यु पर जनता की प्रतिक्रिया से प्रेरित है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार को श्रद्धांजलि देना स्वाभाविक था, कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने उन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा और हास्य की भावना के लिए याद किया।
रमेश ने जटिल आर्थिक मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझाने की देबरॉय की क्षमता की प्रशंसा की, एक लेखक के रूप में उनकी कुशलता का उल्लेख किया। प्रताप भानु मेहता ने उनके व्यक्तित्व के आध्यात्मिक पक्ष को याद किया, महाभारत और पुराणों के उनके अनुवाद, उनकी संस्कृत विद्वता और गीता पर उनकी टिप्पणी पर प्रकाश डाला। मेहता ने लिखा कि देबरॉय की राजनीतिक संबद्धताएँ रहस्यमय थीं, लेकिन उनमें खुद को विवादों से दूर रखने की कला थी।
योगेंद्र यादव ने इन श्रद्धांजलियों को पढ़ने के बाद लिखा, “मैंने एक बार बिबेक देबरॉय की सार्वजनिक रूप से और बहुत कठोर आलोचना की थी। लेकिन इंसान सिर्फ़ एक बयान या फ़ैसले से कहीं ज़्यादा होता है। उनके आखिरी कॉलम और आज के शोक संदेश को पढ़कर मेरे मन में सम्मान और अफ़सोस की भावना भर गई – काश मैं उन्हें जानता होता।” उन्होंने जयराम की “एक प्रतिद्वंद्वी को आदर्श श्रद्धांजलि” की प्रशंसा की, और कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को याद करने की गरिमा जो राजनीतिक विभाजन को पार कर गया है।
लेकिन क्या बहुसंख्यकवादी, इस्लामोफोबिक राजनीति के साथ जुड़ना महज एक राजनीतिक अंतर के तौर पर खारिज किया जा सकता है? एक वैध राजनीतिक विकल्प? खुद को झगड़े से दूर रखने का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति नीति निर्माता के तौर पर जिस सरकार की सेवा करता है, उसकी सांप्रदायिकता से कैसे अछूता रह सकता है? चुप्पी के ज़रिए? क्या इसे बौद्धिक संयम कहा जा सकता है?
देबरॉय 2017 में आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने, हालांकि इससे पहले वे विभिन्न पदों पर सरकार में काम कर चुके थे। सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माता के रूप में, उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और अन्य उपायों को कैसे उचित ठहराया, जिन्होंने आम भारतीयों को तबाह कर दिया? क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार को इन नीतियों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए? या फिर उनके परामर्श का कोई महत्व नहीं था, भले ही वे अपने पद पर बने रहे?
महाभारत और पुराणों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए – धर्म और अधर्म के प्रश्नों से जूझने वाले ग्रंथ – वह विभाजन और घृणा को बढ़ावा देने वाली सरकार में अपनी भूमिका को कैसे समेट सकता है? किस तरह की आत्मा सही और गलत के बीच संघर्ष से ऊपर रहती है?
आज भारत में सबसे बड़ी नैतिक चुनौती क्या है? महाभारत से गहन जुड़ाव के बाद भी क्या इसे पहचानना इतना मुश्किल है?
जबकि देबरॉय की केवल सरकारी सेवा के लिए निंदा नहीं की जानी चाहिए, नीति निर्माता और सार्वजनिक बुद्धिजीवी के रूप में उनकी भूमिका निर्णय के अलग-अलग मानकों की मांग करती है। उनकी मृत्यु काफी बौद्धिक क्षमता के नुकसान का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन एक बुद्धिजीवी का असली मूल्य क्या परिभाषित करता है? क्या उन्होंने सत्ता के सामने सच बोलने का मौलिक कर्तव्य पूरा किया?
एक बुद्धिजीवी को अपने समय के महत्वपूर्ण सवालों की पहचान करनी चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। आज के भारत में, ये सवाल अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न, आम जनता के आर्थिक शोषण और नागरिक अधिकारों के हनन पर केंद्रित हैं।
लोकतांत्रिक मुखौटे के पीछे एक बहुसंख्यक निरंकुश शासन चलता है। इन मुद्दों पर किसी की प्रतिक्रिया उसकी बौद्धिक और नैतिक स्थिति निर्धारित करती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद में विद्वानों की उपलब्धियाँ प्रभावशाली होते हुए भी, समकालीन नैतिक जिम्मेदारियों से किसी को मुक्त नहीं करती हैं।
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने देबरॉय को नौकरी दी और महाभारत पर अपना काम करने के लिए जगह और संसाधनों का इस्तेमाल करने का मौका भी दिया। जब ऐसी खुली संस्था को खत्म किया जा रहा था, तो देबरॉय ने भविष्य के देबरॉय के काम करने के लिए इसे बचाने के लिए क्या किया?
क्या उन्होंने इसे बचाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया या नहीं? या फिर उन्होंने उस छोटी सी संस्था को बचाने के लिए कुछ करना उचित नहीं समझा क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के महान कार्य में लगी सरकार के लिए सीपीआर की मृत्यु आवश्यक हो गई थी? उस महान उद्देश्य के लिए सीपीआर की बलि दी जा सकती थी! कम से कम इस संबंध में उनके हस्तक्षेप का कोई सबूत हमारे पास नहीं है।
देबरॉय का अंतिम कदम गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के कुलपति पद से इस्तीफा देना था, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर अजीत रानाडे की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी। उनके अंतिम कदम – संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा खत्म करने की सिफारिश – को कई लोगों ने सिद्धांतवादी के बजाय प्रतिशोधात्मक माना।
जबकि मृत्यु अक्सर आलोचकों को चुप करा देती है और उदार स्मरण को प्रेरित करती है, समाज के सबसे हाशिए पर पड़े लोगों की प्रतिक्रिया एक सार्वजनिक व्यक्ति की विरासत का सही माप प्रकट करती है। आज के भारत में, क्या मुसलमान – सबसे अधिक उत्पीड़ित वर्ग – देबरॉय के निधन पर शोक मनाएगा? वे उस व्यक्ति को कैसे याद करेंगे जो आध्यात्मिक प्रश्नों में लीन रहा जबकि एक ऐसी सरकार की सेवा कर रहा था जिसने उनके उत्पीड़न को बढ़ावा दिया? और क्या गैर-मुस्लिम मुसलमानों से कहेंगे कि वे इतने छोटे न बनें कि उनके उज्जवल पक्ष को न देखें?
जब साथी नागरिक व्यवस्थित हिंसा और भेदभाव का सामना कर रहे हों, तो विद्वानों के हितों को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने के लिए असाधारण नैतिक अंधेपन की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब कोई ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार की सेवा करता हो। बौद्धिक उपलब्धियाँ, चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हों, संकट के समय नैतिक त्याग की भरपाई नहीं कर सकतीं। द वायर से साभार