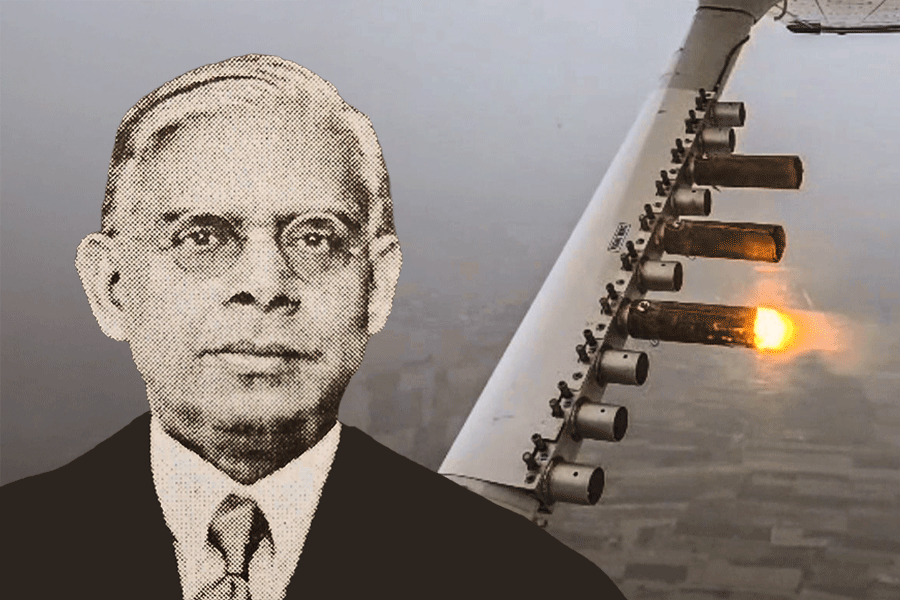एक प्रतीकात्मक छवि – द टेलीग्राफ से
भारतीय धर्मनिरपेक्षता की लगभग हर कसौटी पर खरी उतरती है दुर्गा पूजा
उद्दालक मुखर्जी
दुर्गा पूजा — एक सर्बोजोनिन त्योहार, यानी सभी का त्योहार — की मेरी सबसे पुरानी याद, विडंबना यह है कि बहिष्कार की है। 1980 के दशक की शुरुआत में, जब बंगाल में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हुए अभी एक दशक भी नहीं हुआ था, वाम मोर्चे के प्रति सहानुभूति रखने वाले कई परिवारों ने बच्चों के लिए कुछ सख्त, भले ही मामूली, लाल रेखाएँ बना रखी थीं जिन्हें पार करना मना था। इसलिए, जबकि मेरे जैसे परिवारों द्वारा पूजी जाने वाली लाल किताब में कपड़ों की खरीदारी या ठाकुर-दयालु के किसी अन्य, स्थायी जादुई अनुष्ठान जैसी उत्सव गतिविधियों में शामिल होने पर कोई रोक नहीं थी, स्पष्ट धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना अस्वीकार्य था।
इसलिए, मुझे याद है कि मैं अपने एकांत कोने से, मुँह में पानी भरते हुए, अपनी उम्र के बच्चों को एक वृद्ध महिला के चारों ओर इकट्ठा होते हुए, दोधीकोरमा (मिष्टी दोई, खोई, मुरकी और बताशे का एक स्वादिष्ट मिश्रण) का एक स्कूप लेने के लिए, लालसा से देखता था; या फिर एक कोने से, अपने दोस्तों को, पूजा के परिधानों में, अंजलि के दौरान पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार के दौरान श्रद्धा से सिर झुकाते हुए देखता था। ये रीति-रिवाज, बिना हमारे परिवारों द्वारा हम पर थोपे, हम सहज रूप से जानते थे, हमारे लिए वर्जित थे: ज़ाहिर है, ये एक वामपंथी कुनबे की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लंघन करते थे।
लेकिन देवी कोई पत्थर में गढ़ी गई आकृति नहीं हैं; वे मिट्टी और मिट्टी से बनी हैं जो आकार बदलती रहती हैं, न केवल उन्हें – मान लीजिए, एक मातृ अवतार से एक योद्धा अवतार में – बल्कि उनकी पूजा से जुड़े सांस्कृतिक अनुष्ठानों और उनके बारे में हमारी समझ को भी बदल देती हैं। इस प्रकार, जैसे-जैसे मेरा बचपन किशोरावस्था और बाद में युवावस्था में बदला, जैसे-जैसे मेरा मन पूजा के इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थव्यवस्था पर साहित्यिक और विद्वतापूर्ण कार्यों में रमता गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे एक पत्रकार के रूप में देश भर के विभिन्न सामुदायिक त्योहारों की यात्रा करने और उनका अध्ययन करने का अवसर मिला, जहाँ अक्सर धार्मिकता सामाजिक और सामुदायिकता पर हावी हो जाती थी, मैंने तर्क करना शुरू किया कि भारतीय राजनीति की विशिष्ट परिस्थितियों में वामपंथियों द्वारा दुर्गा पूजा को पवित्रता से जोड़ना, कम करने वाला, यहाँ तक कि दोषपूर्ण था।
यह फ्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता से काफ़ी हद तक उधार लेकर, चर्च और राज्य के बीच कठोर दूरी बनाए रखने की वकालत करने के लिए सामाजिक और धार्मिक के बीच के अंतर को कठोरता से नज़रअंदाज़ करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। दूसरी ओर, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संवैधानिक सिद्धांत, एक प्रेरणादायक प्रयोग, एक बहु-धार्मिक समाज में किसी भी धर्म के विरुद्ध भेदभाव का निषेध करते हुए, फ्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता के विपरीत, धार्मिक आयोजनों में सामूहिक भागीदारी को बहुत प्रोत्साहित करता है—राज्य की ओर से तटस्थ लेकिन नागरिकों की ओर से स्वतंत्र और स्वतःस्फूर्त।
दुर्गा पूजा, एक बहुआयामी घटना, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की लगभग हर कसौटी पर खरी उतरती है। फिर भी, जिन कॉमरेडों को तीन दशकों तक पंडालों के बाहर स्टॉल लगाने में कोई आपत्ति नहीं थी, उन्हें दुर्गा पूजा को धर्मनिरपेक्षता का वाहक बताने वाली समाजशास्त्रीय बकवास बिलकुल पसंद नहीं आई।
दुर्गा पूजा की धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का सबसे बड़ा दावा इसकी प्रतिनिधित्वात्मकता में निहित है – लगभग। मुसलमान न केवल कारीगरों के रूप में पूजा की असंख्य शिल्प परंपराओं का अभिन्न अंग हैं, बल्कि कलकत्ता के कई इलाकों में, समुदाय के सदस्यों का इस उत्सव में भाग लेना कोई अनोखी या औपचारिक बात नहीं है; यह स्वाभाविक है।
धर्मनिरपेक्षता का मूलमंत्र, समायोजन की यह भावना, अन्य, क्रांतिकारी तरीकों से प्रकट होती है, जिससे रूढ़िवादिता की रेखाओं का पुनर्गठन — पीछे हटना — होता है। महिलाओं द्वारा संचालित पूजा संगठन और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि महिला पुजारियाँ अब अकेली नहीं रह गई हैं: शुभमस्तु के तत्वावधान में महिला पुजारियों की एक टीम पिछले कुछ समय से शहर में दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। एशिया के सबसे बड़े रेड-लाइट इलाकों में से एक, सोनागाछी में, नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई, जिसमें मुकदमेबाजी भी शामिल थी, जीतने के बाद, एक दशक से भी ज़्यादा समय से अपनी दुर्गा पूजा होती आ रही है। शायद एकमात्र राक्षस जिसका देवी ने अभी तक व्यापक रूप से वध नहीं किया है, वह है जाति। हालाँकि, भारत के कुछ पवित्र मंदिरों के विपरीत, पंडालों में प्रवेश किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त रहता है, लेकिन बहुजन और आदिवासी समुदायों का इस विशेष त्योहार से रिश्ता जटिल है, जिसमें न केवल निम्न वर्गीय प्रति-आख्यान और प्रतिरोध शामिल हैं – दुर्गा पूजा के दौरान असुर समुदाय का ‘शोक’ इसका एक उदाहरण है – बल्कि उल्लास भी। यह एक ऐसे सामाजिक-धार्मिक आयोजन से अपेक्षित ही है जिसका जन्म सामंती और ब्राह्मणवादी परिवेश में हुआ था।
दुर्गा पूजा के धर्मनिरपेक्ष महत्व को और भी मज़बूत करता है, भौतिक और कलात्मक क्षेत्रों पर गहरी छाप छोड़ते हुए दिव्यता के दायरे से आगे बढ़ने की इसकी क्षमता। 2019 में, बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से ब्रिटिश काउंसिल द्वारा संकलित एक रिपोर्ट, “मैपिंग द क्रिएटिव इकोनॉमी अराउंड दुर्गा पूजा” में, बंगाल की दुर्गा पूजा से जुड़े केवल रचनात्मक उद्योगों का आर्थिक मूल्य 32,377 करोड़ रुपये आंका गया था; चार साल बाद, ‘पूजा अर्थव्यवस्था’, जैसा कि अब कहा जाता है, का मूल्य अनुमानित 50,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह निर्विवाद है कि यह त्योहार लोक कला का भी उत्सव है। ‘थीम पूजा’ का उद्भव, जो कि कलात्मक संवेदनाओं और सामूहिक आस्था का एक शानदार मिश्रण है, शुद्धतावादियों को परेशान कर सकता है, लेकिन तापती गुहा-ठाकुरता ने अपनी विद्वत्तापूर्ण और सौंदर्यपरक पुस्तक, इन द नेम ऑफ द गॉडेस में बताया है कि “… पूरे महानगर में फैले एक प्रदर्शनी कार्यक्रम के रूप में, यह [दुर्गा पूजा]… व्यापक दर्शक वर्ग के लिए वास्तुशिल्प और पुरातात्विक स्थलों, शिल्प झांकियों, जनजातीय कला गांवों और सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के नए क्रमों का एक विशाल प्रदर्शन प्रस्तुत करता है।”
भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दर्शन के दो केंद्रीय तत्व हैं – सद्भाव और सहवास। दुर्गा पूजा इन दोनों पहलुओं का एक माध्यम है, जो भक्तों और संशयवादियों को एक साथ खड़ा करती है – मंत्रमुग्ध – पवित्र और अपवित्र, मनमोहक कला और स्पष्ट व्यापारिकता का एक साथ अनुभव करते हुए, दृश्य – अपनी भव्यता और वैभव में विराजमान देवी – ध्वनियाँ – जयकार, ढाक, नए कपड़ों की सरसराहट – गंध – धूप, मिठाइयाँ, पंडाल में एक-दूसरे से सटे शरीरों का पसीना – दिव्य, लौकिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, ये सभी रेखाएँ एक संक्षिप्त, मंत्रमुग्ध कर देने वाले क्षण में एक साथ प्रतिच्छेद करती हैं।
और उस अतार्किक आनंद, उस आशा की भावना का क्या, जो गरीबी और विशेषाधिकार की परवाह किए बिना, लिंग, वर्ग और जाति की सीमाओं के पार, बंगाली मानस में उमड़ पड़ती है, जैसे-जैसे शरद ऋतु के दिन षष्टी की ओर बढ़ते हैं? यदि धर्मनिरपेक्षता की धुरी महान समतावादी के सिद्धांत पर घूमती है, तो शायद दस भुजाओं वाली देवी से बड़ा कोई नहीं है।
बेशक, दुर्गा पूजा का राजनीतिक और प्रदर्शनात्मक रूप से धर्मनिरपेक्ष होने का दावा निर्विवाद नहीं है। अपनी पुस्तक में, गुहा-ठाकुरता एक ऐसे देश के संदर्भ में एक दमदार प्रतिवाद प्रस्तुत करती हैं जहाँ धर्म, दिखावे, तमाशे और सामूहिक उपभोग को अलग करने वाली सीमाएँ जटिल और काल्पनिक रूपों में एक साथ मिल जाती हैं। इस प्रकार गुहा-ठाकुरता दुर्गा पूजा को सीमांतता में रखने के पक्ष में तर्क देती हैं। “मेरा मानना है कि इस त्योहार ने… सामाजिक प्रभाव और लेन-देन का एक ऐसा दायरा खोल दिया है जहाँ ‘धार्मिक’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ की मानक, संस्थागत श्रेणियाँ न तो सहजता से एक जगह बैठ सकती हैं और न ही एक-दूसरे के विरोध में खड़ी हो सकती हैं।” जियोर्जियो अगम्बेन के अनुसार, ‘धार्मिक’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ की इन श्रेणियों को ‘पवित्र’ और ‘अपवित्र’ श्रेणियों से प्रतिस्थापित करना और उनके सह-मिश्रण और सह-संरचना के बारे में सोचना उचित होगा, जिसे वे ‘अपवित्रीकरण’ कहते हैं, जिसमें ईश्वर की पवित्र वस्तु लगातार ‘मनुष्यों के स्वतंत्र उपयोग और व्यापार’ के लिए वापस लौटती रहती है। पूजाओं को उस रोज़मर्रा के सीमांत क्षेत्र में रखा जा सकता है…”
हालाँकि, यह देवी के सीमांत क्षेत्र से एक ऐसे क्षेत्र में लौटने का समय है जो स्पष्ट रूप से राजनीतिक और बहुलवादी है। एक ऐसे राष्ट्र में जहाँ एक बुकर पुरस्कार विजेता मुस्लिम लेखक को मैसूर में दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने से रोकने के लिए शरारती प्रयास किए जा रहे हैं, जहाँ नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने से पहले उत्साही लोगों के आधार विवरण की जाँच करने के लिए सलाह जारी की जा रही है ताकि मुसलमानों को बाहर रखा जा सके, जहाँ स्वयंभू सनातनी हिंदू दुर्गा पूजा के दौरान बंगालियों के मांस खाने पर आपत्ति करते हैं, या, एक अन्य खुलासा करने वाली घटना में, समन्वयवाद को दर्शाने के लिए संस्कृत भजन और अज़ान बजाने वाले पंडाल का उपहास करते हैं, देवी और उनके प्रशंसक – श्रद्धालु और नास्तिक – बीच के, अमूर्त स्थानों पर कब्जा करने का जोखिम नहीं उठा सकते।
उसे विभाजन के दानव के हृदय को भेदकर सांसारिक – सामाजिक-राजनीतिक – धरातल को पुनः प्राप्त करना होगा।