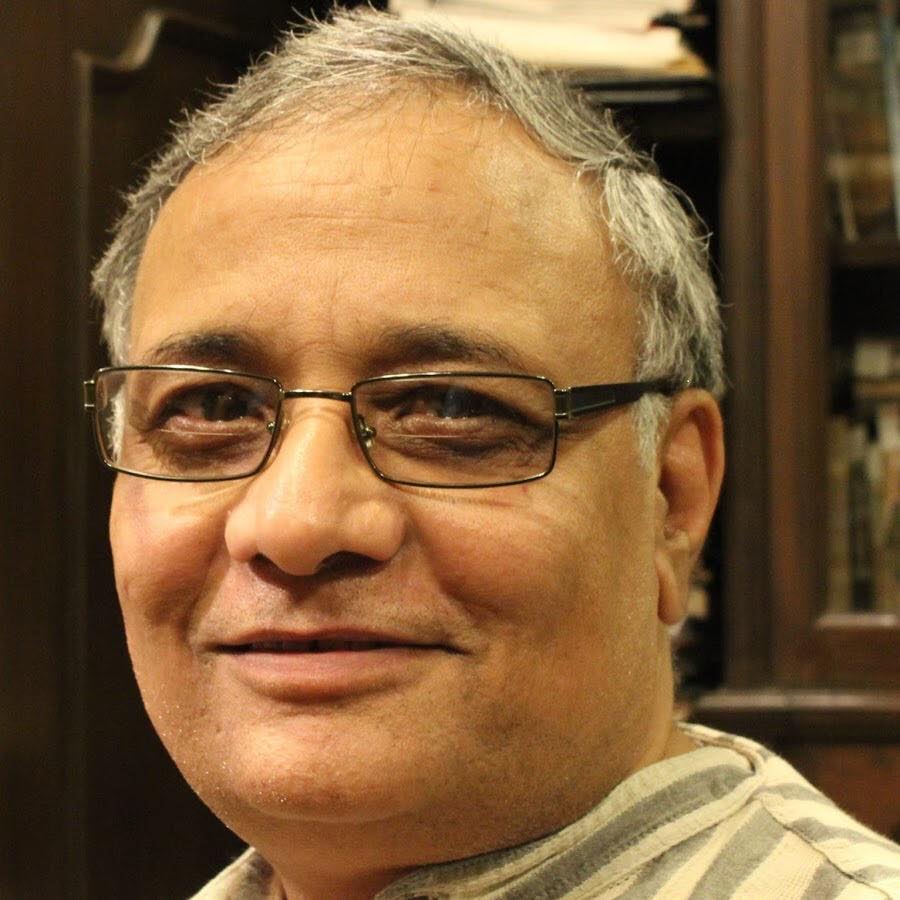अरुण माहेश्वरी ने सीपीएम की वर्तमान स्थिति पर यह लेख लिखा है। वह और उनका पूरे परिवार का सीपीएम से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। उन्होंने ‘ निजी सफाई’ में बताया भी है। उनके लेख से सहमत असहमत हुआ जा सकता है लेकिन चर्चा तो होनी ही चाहिए। यह लेख उनके चतुर्दिक ब्लॉग से साभार लिया गया है। संपादक
प्रमाता के वस्तुकरण की विडंबना में फँसी सीपीआई(एम)
(A Reflection on the Reification of the Subject in the Contemporary Crisis of CPI(M))
अरुण माहेश्वरी
एक निजी सफ़ाई :
सीपीआई(एम) के साथ हमारा संबंध सिर्फ़ संगठनात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक, ऐतिहासिक और निजी साझेदारी का रहा है। करीब पैंतालीस वर्षों तक पार्टी के भीतर रहते हुए हमारा कार्यक्षेत्र मुख्यतः पार्टी के मुखपत्र में लेखन, और आलोचना का ही रहा। इसीलिए, कोई चाहे तो इसे हमारी विडंबना कह सकता है, जब आज हम संगठन से बाहर हैं, तब भी हम अपनी वैचारिक भागीदारी और उत्तरदायित्व को पहले की भांति ही यथावत मानते हैं। पहले भी तमाम खास अवसरों पर पार्टी के मुखपत्र के पृष्ठों पर ही हमने पार्टी की कथित लाइन से अपने को अलगाते हुए लिखने में कोताही नहीं की है।
दरअसल, हर प्रतिनिधिमूलक संगठन की जीवंतता इसी पर निर्भर करती है कि वह अपनी स्वीकृत मान्यताओं के प्रति मतभेदों को किसी ‘बाहरी हस्तक्षेप’ की तरह न देखे, बल्कि संगठन के अपने ही आत्मसंवाद के हिस्से की तरह ग्रहण करने की कोशिश करे।
और यदि ऐसा नहीं होता है, यदि मतभेद को हमेशा किसी ‘बाहरीपन’ की तरह देखा जाने लगता है, तो वह इस बात का संकेत है कि संगठन का उद्देश्य उसके घोषित लक्ष्यों से हट कर कुछ और ही हो गया है। किसी भी संगठन के नैतिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व की माँग है कि वह मतभेद को केवल विरोध नहीं, बल्कि संगठन की चुनौतियों पर विचार की गहराई में प्रवेश करने की एक कोशिश की तरह देखें।
हमारी आलोचना मतभेद के लिए मतभेद नहीं है, लकानियन भाषा में ‘कोरे मतभेद पर टिकी मरीचिका’ नहीं है। बल्कि वह एक ऐसा प्रयास है जो विचार के गहरे तल में उतर कर यह पूछना चाहता है कि क्या आज की पार्टी अपने Real को देख पाने, उससे टकराने की ताक़त रखती है?
हमारे इस नोट के पीछे यही भाव है कि हम मनोविश्लेषण के लकानियन दृष्टिकोण से रणनीति, कार्यनीति और वस्तु की जड़-पूजा (fetish) की संरचनाओं का विश्लेषण करते हुए, यह देखें कि क्या पार्टी अपनी प्रतीकात्मक संरचना की सीमा से बाहर आकर अपनी राजनीति के Real से मुठभेड़ करने के लिए तैयार है?
और इसी बिंदु पर बाहर रह कर भी हम अपने को ‘बाहरी’ नहीं, बल्कि वाम राजनीति में विचार के अंदरूनी हिस्सेदार मानते हैं। यही वजह है कि अनायास ही स्वभावतः हम पार्टी की गतिविधियों के अनेक छोटे-बड़े विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। इस टिप्पणी को भी कुछ उसी प्रकार के हस्तक्षेप के रूप में लिया जाए, यह एक निजी अनुरोध है । — अ.मा.)

कल ( 20 अप्रैल ) को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सीआईटीयू, किसान सभा, खेत मज़दूर यूनियन और बस्ती उन्नयन समिति की तरह के सीपीआई(एम) के जनसंगठनों के आह्वान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ । सभा की दृश्य-भाषा ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति पर क्षण भर सोचने का अवसर दिया। यह अकारण नहीं है कि यह सभा हमारे सामने अपने आकार और अनुशासन, दोनों के कारण ही पार्टी की अतीत की शक्ति और उसके वर्तमान की विडंबना—दोनों का प्रतीक बन कर सामने आई ।
सभा में पुराने चेहरों की अनुपस्थिति और युवाओं की प्रबल उपस्थिति को वैसे तो नेतृत्व-परिवर्तन के संकेत के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यह सवाल अपनी जगह बना रह गया कि वह कथित परिवर्तन वास्तव में कहाँ तक चरितार्थ हो पाया है । ‘टेलिग्राफ़‘ में इस सभा की रिपोर्ट के अंत में कुछ नेता-कार्यकर्ताओं के हवाले से ही यह लिखा गया है कि “As leaders and supporters returned home, satisfied over the Brigade turnout, conversations among them raised the obvious question – will the CPM be able to buck the trend and put up a better show in 2026 elections.”
सभा के बाद लोगों के मन में रह गया यह सवाल ही इस बात का संकेत थी कि यह जनसभा किसी जन-आंदोलन की लहर से आलोड़ित जितनी आम जनता की सभा नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा सीपीआईएम और उसके जनसंगठनों के व्यापक तानेबाने से आज भी बड़ी संख्या में जुड़े कार्यकर्ताओं की सभा थी । वह जनता जो कभी वाम की समग्र विचारधारात्मक परियोजना का जीवंत घटक हुआ करती थी, वाम की विडंबना है कि वही अब उसके लिए जैसे एक दृश्यात्मक अनुपस्थिति में बदल चुकी है । जनता, जो एक समय में पार्टी के साथ एक जीवंत संवाद में थी, अब एक दूरस्थ वस्तु बन गई है, जिस पर पार्टी केवल प्रक्षेपण करती है— उससे संवाद क़ायम नहीं कर पा रही है ।
जहां तक मंच पर पुराने नेतृत्व की अनुपस्थिति का सवाल है, उनकी उपस्थिति अब लकान के नाम-का-पिता ( The Name-of-the-Father ) की तरह हैं, जिनका स्थान खाली होने पर भी वह खालीपन किसी नई विधि अथवा घटना से नहीं भर पाया है, बल्कि महज़ एक औपचारिकता के निर्वाह की वजह से वह एक शून्य में तब्दील हो गया है, जो शून्य इसीलिए पार्टी की बची-खुची जन-राजनीति को भी निगल सकता है, क्योंकि वह किसी घटना से उत्पन्न नए नेतृत्व के आगमन को सूचित नहीं करता है।
इस प्रकार, ब्रिगेड परेड ग्राउंड की सभा एक देखने लायक़ दृश्य अवश्य थी, एक प्रदर्शनात्मक शक्ति । लेकिन यह न तो जन-लामबंदी की आत्म-अभिव्यक्ति थी, न ही किसी राजनीतिक प्रमाता की यथार्थ उपस्थिति का प्रमाण ।
कुल मिला कर यह एक ऐसी संरचना की तरह है जिसकी दोहरी विडंबना यह है कि पारंपरिक नेतृत्व की जगह एक शून्य ने ले ली है और जनता का कार्यकर्ताओं से स्थानापन्न हो गया है । जॉक लकान के शब्दों में यह एक ऐसी स्थिति है जब signifier (संकेतक) और signified ( संकेतित) के बीच का अंतर मिट जाता है । कार्यकर्ता ही अब जनता के संकेतक (signifier) के रूप में काम करने लगते हैं और वांछनीय वस्तु (objet a) यानी जनता की जीवंत उपस्थिति ग़ायब हो जाती है।
लकान के अनुसार, हर प्रमाता का यह धर्म है कि वह हमेशा एक किसी ऐसी वस्तु की तलाश में होता है जो उसके अधूरेपन (अभाव) को भर सके । यह वही वस्तु है जिसकी चाह उसे हमेशा गतिशील रखती है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह वस्तु जनता का प्रेम, उसकी वैधता और संवाद होती है । परन्तु वही अब तक सीपीएम के लिए बंगाल में एक मरीचिका (स्लावोय जिजक की शब्दावली में phantasmatic projection ) बन कर रह गई है।
यही वह प्रक्रिया है जिसे प्रमाता का वस्तुकरण कहते हैं । प्रमाता तब तक प्रमाता रहता है जब तक वह अन्य से भाषिक-संकेतों के आदान-प्रदान की स्थिति में बना रहता है—यानी वह दूसरों की गूँज को अपने में सुनता है। जब संगठन स्वयं किसी प्रशासनिक वस्तु में बदल जाए, वह केवल अपनी निरंतरता और अनुशासन पर बल दे, तब वह एक ऐसे आदिम दृश्य (primal scene) में बदल जाता है—जहाँ सिर्फ़ दोहराव होता है, अर्थ का उत्पादन नहीं।
यही वजह है कि आज ब्रिगेड की विशाल सभा की तरह की परिघटना हमें मात्र किसी राजनीतिक विश्लेषण के बजाय कहीं ज्यादा गहरे जाकर वाम के प्रतीकात्मक विघटन के विश्लेषण के लिए प्रेरित करती है। हम इस किसी सामान्य ‘सभा’ के बजाय इसमें कहीं न कहीं सीपीएम के प्रमातृत्व के लोप की छाया और वस्तु में बदल गए एक जीवंत संगठन के मौन की आवाज़ को ज्यादा सुन रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं है कि एक अर्से से सीपीआई(एम) का संगठनात्मक ढाँचा लकानियन प्रमाता की संरचना से दूर हो चुका है, जो आज उसकी सारी समस्याओं के मूल में है । वह अब एक संवादशील इकाई नहीं, बल्कि एक वस्तु बन चुका है—जिसके पास स्मृति है, अनुशासन है, आकृति है, पर जिसके संवाद का तंतु टूट चुका है। संगठन प्रमाता नहीं, एक वस्तु, एक संरचना बन गया है—जो बात नहीं कर सकता, केवल आदेश दे सकता है। यही उसका जनता से अलगाव है।
फ़्रांसीसी दार्शनिक आल्थूसर (Louis Althusser) के अनुसार, Ideological State Apparatuses (ISA) जैसे राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल आदि विचारधारा के ज़रिए व्यक्तियों को संबोधित करते हैं — उन्हें प्रमाता के रूप में interpellate (संवादशील) बनाते हैं।सीपीआई (एम) की वर्तमान स्थिति में यह संबोधन अब केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहता है जो पहले से दीक्षित, संगठित और अनुशासित हैं — बल्कि आज भी किसी प्रकार से उसके सांगठनिक ताने-बाने से जुड़े हुए हैं ।
आज के समय के प्रमुख दार्शनिक स्लावोय जिजेक (Slavoj Zizek) के शब्दों में विचारधारा केवल कोई वैचारिक संरचना नहीं, बल्कि एक फ़ैंटेसी भी होती है जिसे हम जीते हैं ताकि हम यथार्थ का सामना कर सके, उसे सहन कर सकें। हमारे यहाँ बूंदी के नक़ली क़िले पर फ़तह की कहानी प्रचलित है । वह यह भी बताती है कि असली मैदान पर हार-जीत से कम महत्वपूर्ण नहीं है एक प्रकार का प्रतीकात्मक नियंत्रण । सीपीआई(एम) की यह ब्रिगेड परेड की सभा भी वैसी ही प्रतीकात्मक विजय के भाव को बनाए रखने के आयोजन की तरह थी ।
यह स्थिति ग्राम्शी ( Antonio Gramsci) की “Passive Revolution” की उस प्रक्रिया की ओर भी इशारा करती है जिसमें परिवर्तन ऊपर से लागू किया जाता है, जनता उसमें क्लासिकल ढंग से द्वंद्वात्मक रूप में भागीदार नहीं होती है । सीपीआई (एम) की राजनीति कमोबेश अभी कुछ उसी प्रकार के passive mode के भरोसे में फँसती हुई है ।
पार्टी कांग्रेस के आयोजनों की मुग्ध करने वाली भव्यता बरकरार है, पर उसका घटनामूलक सार-तत्व किसी को नज़र नहीं आता। भले-भले में सब निपट गया कहते हुए सब “एकता” का डंका पीटते हुए अपने घरों में लौट गए । ‘Congress of Unity’ का दावा ही अस्तित्व के एक वास्तिविक संकट की घड़ी में प्रमाता के अंत के जश्न जैसा प्रतीत होता है !
हमारे समय के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट दार्शनिक एलेन बाद्यू ( Alain Badiou) के अनुसार, राजनीति की वास्तविक शुरुआत एक सत्य-घटना (truth-event) से होती है—एक ऐसा क्षण जो चालू व्यवस्था में, अर्थात् यथास्थिति में दरार पैदा करता है और जो अप्रकट था, उसे एक नया नाम देता है। सीपीआई (एम) न तो ऐसी कोई घटना की इबारत गढ़ रही है, न किसी घटना के प्रति अपनी पूर्ण सत्यनिष्ठा का परिचय दे पा रही है। ‘नेतृत्व परिवर्तन’ भी आयु सीमा संबंधी पूर्व के निर्णय पर औपचारिक रूप से अमल के नाते पार्टी में किसी घटना का सूचक नहीं बन पाया । बल्कि कुल मिला कर ‘Congress of Unity’ की तरह की व्याख्याओं से पार्टी में घटना से परहेज को ही श्रेयस्कर माना जा रहा है।
मोदी सरकार के आकलन में फासीवादी और नव-फासीवादी रुझान के बीच की उलझनें भी पार्टी को परिस्थितियों के साथ घिसटने की मजबूरी से बाँधती है । फासीवाद को एक समग्र वैचारिक संकल्पना, जो अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग रूप में प्रकट हो सकती है, के रूप में ग्रहण न कर पाने, उसे एक जड़ वस्तु रूप में ही देखने के आग्रह के कारण उसके विरुद्ध लड़ाई में पार्टी की दशा जर्मन सोशल डेमोक्रेटों की तरह की हो जाती है, अपने लिए अवसर की तलाश में नाजियों के खिलाफ एकजुट लड़ाई के प्रति अनिर्णय की स्थिति में रहने की । वाम के भीतर ऐसे झूठे द्वंद्वों की एक परिणति पर दो दिन पहले ही जेएनयू के प्रसंग में हम अपने इसी ब्लाग पर चर्चा कर आए हैं ।
फलतः आज सीपीआई (एम) उसी दोराहे पर खड़ी है जहाँ संगठन का बाह्य ढाँचा—जनसंगठन, अनुशासन, स्मृति और नैतिकता—सब कुछ जीवित नज़र आने पर भी उस ढाँचे के भीतर के प्रमाता का भाषिक-संवेदनशील केंद्र लुप्त हो चुका है। उसका विचारधारात्मक निकायी रूप एक आत्ममुग्ध चक्र में तब्दील हो गया है, जिसमें नए सोच और संरचना की प्रविष्टि के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आम जनता उसकी पुकार में अपने प्रति संबोधन को नहीं पकड़ पाती है ।
फिर भी, यह सच है कि अभी स सीपीआई(एम ) को राजनीतिक तौर पर मृत कहना किसी रूप में उचित नहीं है । यह सही है कि वह कठिन वैचारिक और सांगठनिक प्रतीकों की जकड़बंदी में फँस गई है, जिससे उसकी पुनर्रचना की शर्तें बहुत मुश्किल हैं । इसीलिए हमारे सामने सवाल है कि क्या –
1. पार्टी जनता से संवाद के लिए कोई नया भाषिक ढाँचा तैयार कर सकती है?
2. क्या वह अपनी पुरातन प्रतीकात्मक संरचनाओं को तोड़ कर नए रूप में रीयल से मुठभेड़ कर सकती है?
3. क्या वह पराजय से उपजी फैंटेसी को तोड़कर ‘घटना’ की साहसिकता अर्थात् अप्रकट सत्य के सूत्रों के साथ जुड़ सकती है? फासीवाद (जो उसके लिए अभी अप्रकट है) को उसकी प्राणघातक परिणतियों के साथ आत्मसात् करते हुए साहस के साथ अपनी पुरानी अंतरबाधाओं को झटक कर नए-नए गठबंधनों और सांगठनिक क्रियाकलापों का रास्ता अपना सकती है ? चुनावों में जीत-हार पर केंद्रित राजनीति के दर्शक के बजाय ज़मीनी स्तर पर अपने पुनर्गठन से घटनाओं के निर्माण की नई भूमिका अपना सकती है ?
हमारी नज़र में आज वाम की सबसे बड़ी मूलगामी ज़िम्मेदारी है— स्वयं की एक नये प्रमाता के रूप में रचना करना। यह प्रमाता जो न केवल ‘अतीत का वारिस’ होगा, बल्कि ‘भविष्य का उद्घोषक’ भी होगा । वह जनता से संवाद करेगा, जनता को पहचान देगा, और जनता की ओर से बोलेगा – प्रतिनिधि बनकर नहीं, भागीदार बनकर। पार्टी के नये महासचिव एम ए बेबी ने पार्टी को जनता के बीच जाने का आह्वान भी किया है, पर ऐसे आह्वान के लिए ज़रूरी है पार्टी का अधिकतम संवाद-संवेदनशील बनना ।
बंगाल में अभी आर.जी.कार के बलात्कार कांड और शिक्षकों की नियुक्तियों के मसले पर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश दिखाई देती है, पर ज़रूरत ऐसे आंदोलनों को भी शुद्ध राजनीतिक स्वरूप दे कर उनके सत्य को छिपाने की कोशिशों से बचने की होनी चाहिए । इससे कोई भी घटना घटना नहीं रह जाती, एक राजनीतिक वस्तु में तब्दील हो कर जन्म के साथ ही मौत के घाट उतार दी जाती है।
जॉक लकान कहते हैं कि प्रमाता जब अपने ‘Real’ से टकराता है, तो वह या तो विघटित होता है, या एक नयी पहचान में ढलता है। हमारे कहने का का तात्पर्य भी यही है कि — विघटन से बचें और रूपांतरण की ओर बढ़ें।
प्रमाता का पुनर्जन्म असंभव नहीं—बशर्ते वह अपने वर्तमान की संवादहीन हो चुकी भाषा से बाहर निकल कर बोलने का साहस करे।