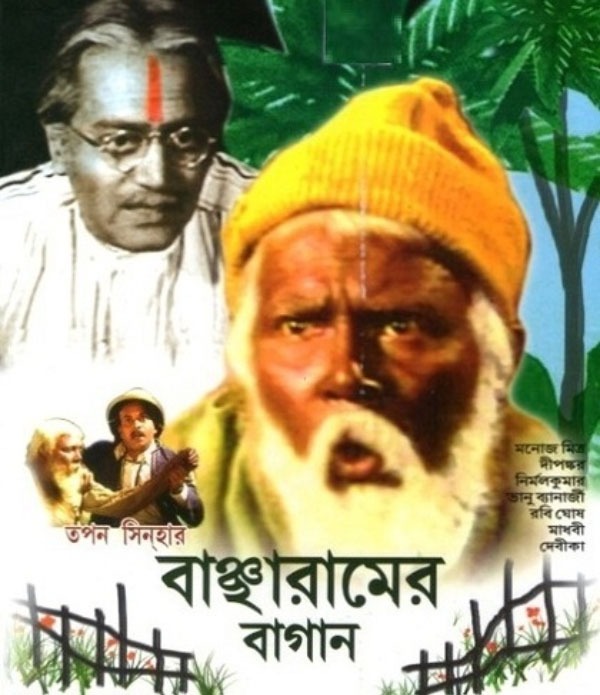मार्क्सवादी आलोचक विमल वर्मा का अभी हाल ही में 18 जून को निधन हो गया। 1931 में यूपी के आजमगढ़ जिले के लसड़ा कलां ग्राम में पैदा हुए विमल वर्मा आजीविका की तलाश में कलकत्ता पहुंचे और वहां अध्यापन कार्य में जुट गए। वहीं पर वह मार्क्सवाद की ओर आकृष्ट हुए, फिर उसे जीवन में आत्मसात कर लिया। साहित्य में आलोचना को लेखन के तौर पर चुना। विमल वर्मा ने कम लिखा लेकिन जितना लिखा गंभीर लिखा, साहित्य जगत ने उस पर नोटिस लिया। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन – प्रकाशन किया। सामयिक, सामयिक परिदृश्य और चंद्रयान प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी की पत्रिका धूमकेतु का संपादन भी किया। वह जनवादी लेखक संघ के संस्थापक सदस्यों में थे। उनका निधन हिंदी साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रतिबिम्ब मीडिया श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका एक लेख प्रकाशित कर रहा है। संपादक
स्मृति शेष
संक्रमण की जटिलता
विमल वर्मा
‘every text on pleasure will be nothing but an introduction to heart will never be written ‘
–Ronald Barth
किसी कृति का सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यांकन अंतिम नहीं होता। टेक्स्ट का अंकन और अर्थोत्पादन, उसका आकारिक रूप सामाजिक संरचनात्मक संबंध प्रकट करता है। पाठ प्रक्रिया में पाठक जिस बिन्दु -पथ को संकेतित करता है उस पाठकीय अवग्रहण में पाठक की अपनी निजी रुझान भी हो सकती है। वह रुझान भी व्याख्या -विश्लेषणपरक हो सकती है। इस तरह के पठन में कृति का एक और विमर्श रचित होता है। परंतु उसे अवग्रहण का तर्क भी अमूर्त नहीं होता। वह इतिहास एवं समाज की गतिशीलता और ऐतिहासिक नवीनता से सम्बद्ध होता है।
पाठकीय अवग्रहण में कृति विशेष के कलात्मक मूल्यों की व्याख्या का आधार भौतिकता के बाहर नहीं होता। कहना न होगा कि पाठ में इतिहास का प्रवेश, उसका तर्क समाज की संश्लिष्टता के स्वरूप को व्यंजित करता है। नरेशन की प्रक्रिया पाठक को, नॉरेटिव से प्रदत्त ऐतिहासिक सांस्कृतिक पाठ्य -विन्यास, भाषा के क्षेत्र में सघन मुठभेड़ करता है। इस संश्लिष्ट पाठ में जहां एक ओर इतिहास की वर्तमानतता का ज्ञान होता है वहीं उसे संभावना के प्रगटन के अंकुर भविष्य के गर्भ में छिपे आभासित होते हैं। इसी भाषायी वस्तुनिष्ठ आधार पर हम जिन वस्तुस्थितियों, दृश्यों, वातावरण, चारित्रिक वैभिन्य का विजन प्राप्त करते हैं उनके नरेशन और संलाप में हमें अनेक प्रकार के टेक्स्ट से उपजे संबंध जो अवचेतन से उभर आते हैं, उनकी रोशनी में विचारधारा के उत्पादन के नियमों की भी जानकारी होती है। उसमें चरित्रों का निजी मनोविज्ञान भी सामाजिक उत्पाद ही होता है। उसके विचारधारात्मक क्षेत्र में विश्व संबंधी विरोधी और अंतर विरोधी विचार भी हो सकते हैं। इस तरह कृति के पाठ में ‘अस्तित्व’ और ‘व्यक्तित्व’ की भूमिका पाठ को तथा भाषा को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। इन संश्लिष्टताओं की ओर इशारा करते हुए अमेरिकी मार्क्सवादी आलोचक फ्रेडरिक जेम्सन ने लिखा है कि महाआख्यान अब भूमिगत होकर हमारे सामूहिक अवचेतन में समा गया है। यूं अवचेतन इच्छाएं हमारी भाषा के अंतरालों के बीच में ही अभिव्यक्ति पाती हैं।
प्रस्तुत टेक्स्ट के विमर्श को यथार्थ के अवग्रहण के लिए इसकी फैंटसी के आक्रामक रूप का अनुभव कितना वास्तविक लगता है यहीं से रमेश उपाध्याय की कहानी ‘डाक्यूड्रामा’ के चित्र पर गौर करेंगे।
“कथा के नेटवर्क में मिताली विश्वविख्यात वैज्ञानिक एस्ट्रोफिजिसिस्ट अरुण राय पर डाक्यूड्रामा बनाना चाहती है। ” उसने (मिताली ) प्रसिद्ध संगीतकार विश्वमोहन की कला को उनके निजी जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया है। विश्वमोहन के प्रेम प्रसंगों और विवाहेतर यौन संबंधों की खुली चर्चा उस फिल्म में की गयी है, इसलिए फिल्म काफी चर्चित और सफल हुई है। फ़िल्म समीक्षकों ने उसे सूचना और मनोरंजन के मिले रूप ‘इन्फोटेनमेंट उत्कृष्ट कला तथा वृत्तचित्र और नाटक के मिले-जुले रूप डाक्यूड्रामा नामक नई सिने विधा का श्रेष्ठ भारतीय नमूना बताया है। इस फिल्म के लिए मिताली को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और वह सेक्स को जीवन का मूल सत्य तथा फिल्म का अनिवार्य तत्व बताने वाली बोल्ड और सेंसिटिव फिल्मकार बन गई है।”
इसी पृष्ठभूमि में वह अरुण राय पर ‘सनस्पाट ‘ नामक डाक्यूड्रामा बनाना चाहती है।। यानी सूर्य में धब्बे होते हैं, उसी तरह अरुण राय का विवाहेतर प्रेम -प्रसंगों-अरुण राय के शब्दों में “वह (मिताली) मनुष्य को आहार, निद्रा, भय और मैथुन में रत पशु के रूप में देखती है। नहीं, इतना भी नहीं देखती वह। आहार के लिए मनुष्य को क्या-क्या करना पड़ता है, इससे उसे कोई मतलब नहीं। मनुष्य कौन सी नींद में सो रहा है और किस नींद के लिए जाग रहा है, इसकी उसे कोई खबर नहीं। मनुष्य किस भय को भगा रहा है, इसका भी उसे कोई बोध नहीं। उसका ध्यान केवल मैथुन पर केन्द्रित है, मानो वही एकमात्र मूलभूत और सबसे बड़ा सत्य हो। … उसे तो शायद यह भी मालूम नहीं कि वह किस बाजार में बैठी है किसके लिए धंधा कर रही है। ”
यू ऐसे सेक्स चित्रण संस्कृत काव्य में भरे पड़े हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है- ” परंतु संस्कृत के नाटकों और काव्यों को केवल भरत और धनंजय के नायिका भेद ही नहीं संचालित कर रहे थे, उनके सामने एक और महत्वपूर्ण शास्त्र था जो प्रत्यक्ष रूप से उनकी कृतियों को संचालन कर रहा था। वह शास्त्र है वात्स्यायन का कामसूत्र। ” मुद्राराक्षस ने ‘सौन्दर्य को खारिज करते हुए ‘ नामक लेख में लिखा है- ” … मान्यता पाने के लिए कवि भवभूति ने जो पहला श्लोक ही सभा में सुनाया था, उसे इतना पसन्द किया गया था कि उनका नाम श्रीकंतभट्ट की जगह भवभूति हो गया था। सभा श्लोक की जिस ‘रमणीयता’ पर मुग्ध हुई थी, वह इसकी दूसरी पंक्ति से समझी जा सकती है। जाहर तौर पर यह देवी पार्वती की वंदना है पर इसकी जिस रमणीयता से सभा प्रसन्न हुई होगी, वह न देवी की उपासना है न आस्था की सघनता । मुग्ध जो करता है वह एक समूचा दृश्य है जिसमें गिरिजा के स्तन दीखते हैं जिन पर शिव से आलिंगन करने के कारण भस्म लगी हुई है। जाहिर है, वस्त्रों से ढके स्तनों पर सफेद भस्म नहीं लगी। ”
आजकल भूमंडलीकरण की संवृत्ति जनता को जन समाज में परिवर्तित कर रही है। यह साम्राज्यवादी शोषण और प्रभुत्व की उत्प्रेरक है। इसने अलोकतांत्रिक मानसिकता का विकास किया है। जन समाज यानी मास कल्चर में हमारी इच्छा और हमारे सरोकार समाजोन्मुख नहीं होते। इच्छाओं का वस्तुकरण होने लगता है। दिशाहीनता, आलोचना विमुखता, चीजों, घटनाओं, संवृत्तियों, प्रवृत्तियों के माध्यम से ह्रासशील, सहजात प्रवृत्तियां ऐश्वर्यमयी जीवन शाली द्वारा यथार्थ से दूसी पैदा करती है। बाजार का प्रभुत्व शिखर पर है। सामाजिक और सांस्कृतिक असन्तुलन की यह हालत है कि केवल पूर्वी यूरोप में पांच लाख औरतों की बिक्री की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। हरवर्ट शिलर ने लिखा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की तकनीक ने बेशुमार पूंजी दोहन की क्षमता के माध्यम से कार्पोरेट मार्केटिंग आडियंस मनीपुलेशन उपभोक्ता और विचारधारात्मक प्रकृति निर्माण द्वारा स्वामित्व, संरचना, वितरण, सामाजिक संरचनाओं और अन्तर्वस्तु के मूल्यांकन का आधार बदल दिया है। इसी माध्यम साम्राज्यवाद की झांकी ‘मिताली’ के माध्यम से व्यक्त की गई है। ऐसी अन्धलोकवादी रुझान के बारे में मुद्राराक्षस ने लिखा है कि ” आजकल विद्या वणिक समुदाय पृथ्वीराज रासो तो नहीं लिखता, वह शक्ति भर जनसमुदाय को तर्क, विवेक और प्रश्नाकुलता से विरत करता है। वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वेच्छाचारी आचरण के प्रति आज्ञाकारिता सिखाता है।… इन कंपनियों ने जैसे अपने उत्पाद की परिकल्पित और गढ़ी हुई कीमतों को चुकाना उपभोक्ता अपनी हैसियत का प्रतीक मानने लगता है, इसी तरह इन कंपनियों ने रचना को महंगा उत्पाद बनाकर उसे एक सिंथेटिक आदमी के सिंथेटिक विषयों में सीमित कर दिया है। ” (वही)
“डाक्यूड्रामा” में मिताली की कार्य-शैली का परिप्रेक्ष्य क्या इन वक्तव्यों से अलग है? कथा की विचारधारा का मास कल्चर की इन्हीं विडम्बनाओं क उद्घाटन से प्रारंभ होती है।
चूंकि मिताली विवाहेत्तर यौन संबंधों और सेक्स को प्रमुखता देती है। इसलिए स्त्री परम्परा को समाज व्यवस्था से जोड़कर देखने की जरूरत है। ऊपर हमने संस्कृत साहित्य के सौन्दर्य मूल्य की बात की है । अतएव यह स्पष्ट करना अत्यंत अनिवार्य है कि ऐसे सौन्दर्य-मूल्य को सार्वभौम बनाना और मानना इतिहास -दृष्टि को नजरंदाज करना है। यह विशिष्ट पितृसत्ता व्यवस्था में पुरुष स्त्री को परिवार सेवी एवं उऩ्हें कामुक आनंद का बन्दी बनाये। यानी स्त्री पुरुष की कामुक संपत्ति है। यानी ‘लिंग’ की धारणा के निर्माण में पुरुष सत्ता की विचारधारा की वरीयता है।
भूमंडलीय संस्कृति के विकास की व्याख्या की जाए तो वहां विभिन्न संस्कृतियों का आत्मसातीकरण होता है। संस्कृति उद्योग में स्थानीय पवित्रता को तहस-नहस करके उसको एक सार्वभौमत्व प्रदान करने के लिए उसे विभिन्न रचनात्मक रूप देती है। इस तरह संस्कृति का स्थानीय बोध लुप्त हो जाता है। स परिवर्तन की प्रक्रिया बहआयामी होती है। वह प्रतिगामी अभियान का शोषण और दोहन प्रक्रिया की हमलावर रणनीति है। क्योंकि इस संस्कृति उद्योग में ” वास्तविक अस्मिता” रूपान्तरित होकर ” सार्वभौमिक अस्मिता ” बन जाती है। ” वह रूपान्तरण मनुष्यों की अनचाही वस्तुओं के संयोग से पैदा हो रहा है। ” इस अनचाहे संयोग को सांस्कृतिक विचार, राजनीति, सिनेमा, गीत आदि में सहज ही देखा जा सकता है । कुछ थोड़ा इससे और कुछ थोड़ा उससे लेकर नया इस दुनिया में प्रवेश कर रहा है। यह वर्ण संकरत्व पापुलर कल्चर में सहज ही देखा जा सकता है। ” (लेखक- सलमान रुश्दी)
मार्क्स ने लिखा है- ” रूप अपनी अन्तर्वस्तु के अनुरूप ऐतिहासिक आधार पर निर्धारित होता है। … समाज की भौतिक अन्तर्वस्तु यानी उत्पादन की पद्धति समाज के रूप पक्ष यानी उसकी अधिरचना का निर्धारण करता है। ” रचनाकार नरेशन में विचारधारा को ही एक नये रूप में आकार में ढाल देता है। ट्राटस्की ने भी ‘लिटरेचर एंड रेव्यूलेशन ‘ नामक ग्रन्थ में लिखा है- ” रूप और अन्तर्वस्तु में संबंध का निर्धारण इसलिए होता है कि अन्तर्वस्तु के दबाव तथा सामूहिक मस्तिष्क की मांग से नये किस्म के रूप का निर्माण होता है। ” इस तरह सामाजिक परिवर्तन को विचारधारा में आये विकास बदलाव की दृष्टि से जा सकता है। इस तरह यह सामाजिक परिवर्तन कला और उपभोक्ता के बीच बनते – बिगड़ते नवीनतम संबंधों को भी पैदा करता है। साथ ही साथ पाठ की सहायता से कृतिकार का मानसिक बोध भी उजागर होता है।
चूंकि प्रत्येक पाठक अपने युग की अपेक्षाओं की सीमा के अनुसार कृति का पठन और मूल्यांकन करता है। पढ़ने के सिलसिले में कृति पाठक के अभ्यन्तर का हिस्सा बन जाती है, इसलिए पाठक उससे दूरी रखकर अपना नया आन्तरिक अस्तित्व पाने लगता है। माध्यम साम्राज्यवाद और संप्रति पूंजीवाद के छद्म को चीरने के लिए लेखक को उत्पादक होना पड़ता है। जिस तरह उत्पादन में नयी-नयी प्रविधियों, नयी-नयी तकनीकों का आविष्कार एवं व्यवहार अनिवार्य है उसी प्रकार बेंजामिन के शब्दों में ” ये तकनीकें कला की उत्पादन शक्तियों का हिस्सा और कलात्मक उत्पादन के विकास के चरण का हिस्सा होती हैं।”
चूंकि ‘डाक्यूड्रामा’ सूचना और मनोरंजन के मिले-जुले रूप ‘इन्फोटेनमेंट ‘ की उत्कृष्ट कला तथा वृत्तचित्र और नाटक के मिले-जुले रूप ‘डाक्यूड्रामा ‘ नामक नयी सिनेविधा का श्रेष्ठ भारतीय नमूना है, इसमें सेक्स जीवन का मूल सत्य तथा फिल्म का अनिवार्य तत्व है। अतएव अरुण राय पर इस डाक्यूड्रामा के फिल्म संग्रथन के पहले एक दूसरी फिल्म की तकनीक का उल्लेख करना चाहूंगा जो इस रचना-विधि को समझने में मददगार होगी। वस्तुतः पाठक एवं दर्शकों की दृष्टि में ‘संवेग ‘ (चित्त-विक्षोभ या भाव) का रूप पारस्परिक स्थितियों पर निर्भर करता है। इसी पर ध्यान रखते हुए गडार्ड ने चलचित्र के माध्यम से संवेग (संवेदना) के प्रभाव के रूपांकन के लिए 1962 ई. में एक फिल्म तैयार की। 1962ई. में बनी इस फिल्म के निर्देशक रूस के विख्यात कलाविद् कुलशेव और पुदोकिन थे। इसमें अभिनेता मसजुखिन थे। मसजुखिन के शान्तचित्त चेहरे का एक क्लोजअप लेकर उसे तीन विभिन्न चित्रों के साथ जोड़ दिया। पहले चित्र में एक प्लेट सूप था। दूसरे चित्र में एक कोफीन थी जिसमें मृतक का शव रखा जाता है। तीसरे चित्र में एक बालिका थी। वहाँ विचित्र ढंग के कपड़े से बना हुआ एक भालू था जिससे वह खेल रही थी। जो दर्शक इसके संबंधों की जानकारी नहीं रखते थे, उन्हें ही ये चित्र दिखाए गए। दर्शकों ने अभिनेता के भावों को देखकर भूरि-भूरि प्रशंसा की। सभी दर्शकों की प्रतिक्रिया एक ही तरह की थी। पहले चित्र को देखकर उन्हें प्रतीत हुआ कि अभिनेता किसी विशेष मूड में भावमग्न है। वह सूप पर ध्यान नहीं देता। दूसरे चित्र कोफीन को देखकर वह शोक में डूबने लगता है। तीसरे चित्र में बालिका को खेलते हुए देखकर एक हल्के आनंद में उसके चेहते पर हँसी -खुशी झलक उठती है। दर्शक उल्लसित तो थे , परन्तु वे यह समझ नहीं पाये कि एक ही चेहरे के अलग-अलग पारस्परिक अवस्था की विभिन्न संवेदना व्यंजित की गई है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संवेदना का पूर्वापर घटनाओं और परिवेश से घनीभूत संबंध होता है। जाहिर है संवेदना की अभिव्यक्ति पर केवल चेहरे, आँखों तथा हाव-भाव को देखकर समझना अधूरा है।
‘ डाक्यूड्रामा’ के संग्रथन में भी कथा को फिल्म संग्रथन की तरह मानवीय- चरित्रों ( अरुण राय, उनकी पत्नी, उनका बेटा व्योमकेश, मिताली) को जैसे अलग-अलग शाट्स में बांटकर फिर उन्हें जोड़ दिया गया है। इस संरचना में पाठकों को आवेग मुक्त करने के लिए तथा परस्पर विरोधी सामान्य क्रियाओं के रूपायन की दृष्टि से हर शाट्स के भीतर एक काउंटर प्वाइंट निर्मित किया गया है। जैसे ‘” अरुण राय … सच्चाई, सादगी और देशभक्ति के मूल्यों को अपनाते रहे।” ” पत्नी बड़े घर की बेटी थी। महत्वाकांक्षी थी… उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई , तो वह अरुण राय को निकम्मा समझने लगी, उनसे नफरत करने लगी… पति पर सन्देह करने लगी… अरुण राय उससे नहीं किसी दूसरी औरत से प्रेम करते हैं.. उसकी उपेक्षा और अवज्ञा करते हैं। अरुण राय अपने दफ्तर या वेधशाला में व्यस्त होते और वह समझती कि दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं… वह दबे पांव आकर उनके कमरे में ताकझांक किया करती कि वे वहां उस दूसरी औरत के साथ तो नहीं हैं।” “यामिनी मुझसे कहती थी कि मुझे छोड़ दो या अपने काम को छोड़ दो। ”
अरुण राय झुंझला उठते हैं, ” क्या तुम (व्योमकेश) सारी दुनिया को यह बताना पसंद करोगे कि तुम्हारा बाप जब अपने काम में व्यस्त होता था. तुम्हारी माँ उसके साथ सोने के लिए सारा घर सिर पर उठा लेती थी और अपने कपड़े फाड़ती हुई तुम्हारे सामने आ जाती थी।”
व्योमकेश- ” क्यों, जो सच है, उसे सामने आना चाहिए।” ” फिल्म के लिए त एक सच बड़ा उपयोगी है। ऐसा एक भी दृश्य मिताली की फिल्म को चमका देगा।”
” यह सुनकर अरुण राय आपा खो बैठते हैं… स्वार्थ के लिए गू भी खाना पड़े तो खा लेना चाहिए। माँ-बाप को बेचना पड़े तो बेच देना चाहिए।”
व्योमकेश- ” आप बेकार चिल्ला रहे हैं, बाबा ! मुझ पर आपकी इस भाषा का कोई असर नहीं होगा। ”
मिताली- ” लेकिन अरुण दा, मेरी समझ में अब भी यह बात नहीं आ रही है कि वे (अरुण राय की पत्नी) ऐसा क्यों समझती थीं। जब कोई दूसरी औरत आपके जीवन में थी ही नहीं, तो वे उसके होने को सत्य क्यों मानती थीं? ”
” जो चीज उसका इलाज करने वाले मनोचिकित्सक भी नहीं समझ सके, उसे मैं कैसे बता सकता हूं।” … ” वैज्ञानिक ज्यादा दुनियादार होगा, तो अपना काम नहीं कर पायेगा। इसलिए वैज्ञानिक का शादीशुदा होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मामला केवल सेक्स का नहीं है, सहानुभूति कै है, समझदारी का है, संवेदनशीलता का है।” ” लेकिन जब वह मुझे झटपट उन्नति करके बड़ा आदमी बन जाने के लिए प्रेरित करने लगी और तथाकथित बड़े लोगों से संबंध अच्छे बनाने के लिए कहने लगी तो इस चीज को अपने स्वभाव, संस्कारों के विरुद्ध पाकर मैं उससे अपना मतभेद प्रकट करने लगा। ” ” अरुण दा! आपके एक दब्बू किस्म की घरेलू पत्नी चाहते थे, जबकि वे दबंग महिला थीं। ” ” अब तो फिल्म बनाने की ऐसी नई तकनीक भी निकल आयी है … किसी का रेप करते हुए भी उसके बाद कनफेस करते हुए भी।” इस नरेशन ने मुझे बोरस्टोन की उक्ति ” अमरीकी माध्यमों में जो छद्म घटनाएं और अर्ध सूचनाएं पेश की जाती हैं, वे न तो सच साबित होती हैं, न झूठ, किन्तु विश्वसनीय होती हैं।” प्रासंगिक लगती हैं।
यदि इस रचनात्मकता के विधायक पहलू पर गौर किया जाय तो रचनाकार ने रचना की विषय वस्तु की विचारधारा की गठन-प्रक्रिया में एलिनिएशन या विछिन्नता की विधि अपनायी है। शब्दों के इशारों में, लेखक की अन्तर्निहित भावना घुस गई है। यह एक तरह का रिएक्टिव टेक्स्ट है। रिएक्टिव टक्स्ट के बारे में रोला बार्थ ने लिखा है कि इसमें ” क्रोध, भय, विभ्रम घटनाओं से बना देशकाल है। इसकी अभिव्यक्ति वाक्य विन्यास के उभरे और खिंचे तन्तुओं में देखी जा सकती है। ” इसमें चित्रित प्रत्येक पात्र समाज के ही अनंत स्पंदनों का प्रत्यक्ष रूप है। अरुण रा, उसकी पत्नी, व्योमकेश एक दूसरे की क्रिया से उद्विग्न हैं यानी संबंधों को असहजता के एहसास से उद्विग्न। यह उद्विग्नता ही उनकी चारित्रिक विशेषताएँ हैं। अरुण की पत्नी और बेटे व्योमकेश का सिनिकल एक्ट अपनी फलश्रुति में समकालीन जीवन की वस्तुपरक दशा क अभिव्यंजित करता है।
यामिनी (अरुण राय की पत्नी) की चेतना उपभोक्तामयी दुनिया के बीच अपनी स्थिति का अपरिभाषेय अबूझ रहस्य सवार हो जाता है। उसका अपना ही पति अपनी व्याख्या से, अपने विवेक से परे होकर एक आतंकदायी मिथक बन जाता है। उसकी पूर्णाहुति तब होती है जब यामिनी आत्महत्या कर लेती है और व्योमकेश अपने पिता से घृणा करने लगता है। लेखक ने जक्स्टापोजीशन द्वारा द्वैध, विडम्बना , विद्रूप की चेतना की भाषा में अनेक प्रतिरोधी ध्वनियों की संयोजकता और चेतना -प्रवाही अर्थों को सक्रिय कर दिया है।
पाठक रचना -सत्ता के आकार में संरचना का ऐसा परिप्रेक्ष्य अवग्रहण करता है जिसमें जीवन की विडम्बना, अन्तर्विरोध मरणशीलता उजागर हो जाती है।
रमेश जी अपनी साहित्यिक युक्तियों (लिटरेरी डिवाइसेज) द्वारा अलग-अलग चरित्रों के अलग-अलग दृष्टिकोणों को स्वतंत्र रूप से उभरने देते हैं। अरुण राय के भीतर भी घबराहट भरी उद्विग्नता किस तरह बहने लगती है यह आत्मसात करके पाठक रचना के पूरे आशय की गहराई पा लेता है।
भाषायी दृष्टि से प्रत्येक शब्द गोचर यथार्थ के एक अंश को अभिव्यक्त करते हैं। पाठक वस्तुस्थिति के विपर्यय की तीव्र अनुभूति होती है। इसलिए कहा गया है कि रचना की अन्तर्वस्तु केवल उसके विषय में ही नहीं उसकी प्रक्रिया और उसके व्यवहार में खोजी जानी चाहिए। ‘ डाक्यूड्रामा’ की प्रत्येक पंक्ति चेतना के अमूर्त परिदृश्य को मूर्त और घटनात्मक परिदृश्य में बदलती हुई वायवीयता को ऐन्द्रिक बना देती है।
मेरी समझ में पाठक निष्क्रिय नहीं होता। यूं आज के पूंजीवादी जगत में पूंजी के नियम ने मनुष्य ने मनुष्य की उदारता को नष्ट कर दिया है। इसलिए रचनाकार डाइलेटिक्स के माध्यम से रचना द्वारा पाठक का शाक ट्रीटमेंट करता है। चूंकि प्रत्येक वस्तु में उसका विरोध निहित रहता है। इन दो द्वन्द्वों के माध्यम से पाठक में आभास और यथार्थ के संज्ञान के माध्यम से यह चेतना जागृत होती है कि चरित्र, क्रिया, घटना के कार्य-कारण को वह समझे और उसमें उन परिस्थितियों को बदलने की जागरूकता पैदा हो। इसे ब्रेख्त दूरी के विचार के मध्य निकट का अहसास कराना कहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि रचना एक अवधारणा होती है। उसके माध्यम से गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का संज्ञान होता है। इसलिए रचना-प्रक्रिया में द्वंद्वों, घटनाओं, क्रियाओं के माध्यम से इन सभी पहचान को अपरिचित बना दिया जाता है। मार्क्स ने मनुष्य, सत्ता और अस्तित्व का विश्लेषण किया है। मनुष्य बाहरी जगत पर क्रिया करके ही अपनी प्रजाति सत्ता प्रमाणित करता है। उत्पादन उसका सक्रिय प्रजाति जीवन है। श्रम का लक्ष्य मनुष्य के प्रजाति जीवन का यथार्थीकरण है। ‘डाक्यूड्रामा ‘ में प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चरित्र को एक दूसरे से विपरीत बनाकर कथा को एकतान न बनाकर खंडित कर दिया है। यदि इन विभक्त अंशों को एकत्र कर दिया जाए तो यथार्थ का एक नया चेहता उपस्थित हो जाता है। कुछ पाठक इसमें अमूर्तन देख सकते हैं । उसमें पाजिटिव नजर नहीं आएगा। परन्तु ध्यान में रखने की बात है कि सच एक ही होता है उसे अभिव्यक्त करने की अलग-अलग विधियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए ‘पूंजी ‘ ग्रन्थ में श्रमशक्ति, श्रम मूल्य, विनिमय मूल्य, अतिरिक्त मूल्य का अलग-अलग गंभीर विश्लेषण करके फिर उसे पूंजीवाद की समग्र प्रक्रिया से युक्त किया गया है।
आज की छटपटाहट समाज व्यवस्था के भीतर सर्वव्यापी संकट की व्यापकता और गहराई के बारे में मेजोरस ने लिखा है- ” Today’s crisis is not that some educational institution but the structural crisis of the hole system of capitalist interiorization. ” उन्होंने श्रमिकों के अतिरिक्त समाज के अन्य लोगों के बारे में भी लिखा है कि, The succeed in this only because the particular individual interiorize the outside pressure.”
विछिन्नतावाद का कैसे विस्फोट हो रहा है इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ” Thus wider sense, is the gretest challange to capitalism in general for it direct affected the very process of interiorization through which allenation and reification could so for prevail over the consciousness of individual.” (Marx theory of alienation, लेखक – मेजारस )
इस कथा संरचना में पाठक अपनी पढ़त में यह अनुभव करता है कि कैसे एक चित्त प्रवृत्ति से दूसरी चित्त प्रवृत्ति में सूक्ष्म तथा अप्रतिम संक्रमण की अभिव्यक्ति की गयी है। चरित्रों के कार्यकलापों में निहित विरोधाभासों में अद्यतन सामाजिक प्रणाली उनके व्यक्तित्व को स्पर्श करती है। इस कलात्मक विधि में यथार्थ से रचनाशीलता के तथा रचनाशीलता से पाठक के संबंध के विश्लेषण द्वारा नए सूक्ष्म अर्थान्तर की प्राप्ति होती है। इस कर्कशता और निर्ममता के पीछे कौन सी तर्क प्रणाली व्यवस्थित की गई है? उतार-चढ़ावों के बीच किन मुख्य उपादानों की झांकी पायी जाती है जो अत्यंत नाजुक क्षणों में उनके आचरण को निर्धारित करती है। उस ऐतिहासिक स्वरूप पर मार्क्स द्वारा दर्शन की समस्या पर गौर करना लाजमी है- ‘सामाजक कार्यकलाप का यह स्थिरण – उस चीज का सुदृढ़ीकरण जिसे हम स्वयं अपने ऊपर की एक वस्तुपरक शक्ति बना डालते हैं, जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, हमारी प्रत्याशाओं को विफल बना देता है, हमारे लखमीनों पर पानी फेर देता है। ‘ … ‘ पूरा इतिहास- मानव के दुष्कर और विरोधाभाषों से भरे परंतु अग्रगामी विकास की चक्करदार कमानी में एक तरह की कुण्डली। ‘
फिलहाल समकालीनता के अध्ययन से तो यह प्रकट हो रहा है कि पूंजीवादी सामाजिक संबंधों तथा पूंजीवादी श्रम विभाजन के अनिवार्य फल के रूप में व्यक्ति के ‘ पूर्ण आत्मध्वंस की ओर’ अभिमुख होने की प्रवृत्ति गतिमान है। शायद इसीलिए कला के तमाम रूप एकाएक रूपान्तरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।
इस रूपान्तरण की शक्ल क्या है, इसका संकेत इस रचना से मिल जाता है।
हमारी कामनाओं के मैनिपुलेशन की फलश्रुतियों ने पाठ में विभेद को जन्म दिया है। रोला बार्थ ने ‘डेथ आफ आर्थर’ लेख में ‘कृतिकार पाठ का उत्स है’ का खंडन करते हुए लिखा है कि पाठक ही पाठ को बहुमुखी बनाता है। रचना में संदर्भपरकता, लाक्षणिक प्रयोग, पदमैत्रियों के संबंध को अन्तर्पाठ कहा जाता है। इसी तरह फूको ने भी कृति के नेटवर्क की व्याख्या करते हुए बताया है कि यह एक फेनोमिना है ‘ जो चीजों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसमें व्यापक पैमाने पर अन्तर्विरोधी दृष्टियां, व्याख्याएं, कैटेगरी, नियम आब्जर्वेशन आदि शामिल हैं।’
‘डाक्यूड्रामा’ में उस परिस्थितीय यथार्थ की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है जो पाठ के निर्माण में उपादान बनाए गए हैं। यह यथार्थ है जो मीडिया द्वारा कामुक व्यवहार को व्यक्तिगत और सामाजिक एजेंडा बनाया जा रहा है। कहना न होगा कि ‘पोनोग्राफी’ संस्कृत पुरुष की उपचेतना बनती जा रही है।
नौजवान (व्योमकेश राय) के सामने अभिभावक से मुक्ति पाकर स्वायत्ता की उपलब्धि उसकी प्रमुख समस्या बना दी गई है। एडवर्ड सईद ने ‘विगनिंग्स’ की भूमिका में लिखा है- ‘ कोई भी शाब्दिक प्रारम्भ एक साथ सृजनात्मक और समीक्षात्मक क्रिया होती है। ठीक वैसे ही जैसे जिस क्षण कोई व्यक्ति भाषा को अनुशासित ढंग से प्रयोग करने की बात सोचता है, ठीक उसी क्षण सृजनात्मक और समीक्षात्मक विचार के बीच रूढ़ अंतर ढह जाता है। पाठ की यात्रा, कई चरणों में पूरा नहीं किया जा सकता अपितु इसकी अवधारणा किसी ऐसी चीज के रूप में की जाती है जो उस विशाल प्रयास की भी पहुंच के बाहर होती है जो जीवन के लगातार चलने वाले महाउद्यम का लक्षण होता है।’ अरुण राय का उद्यम सईद की बातों की पुष्टि करता है।
कथा की अन्तर्वस्तु में ‘वर्चुअल रियलिटी’ की ओर भी संकेत है। वस्तुतःआज के ‘आभासी जगत’ का प्रतिबिम्ब वैज्ञानिक अरुण राय की पत्नी है। इस हाइपर रियल जगत में वह अपनी इच्छाओं को वस्तुओं में अभिव्यक्त पाना चाहती है। आजकल साहित्य में ‘अन्य’ की चर्चा जोरों पर है। अन्य का उद्देश्य भिन्न या ‘डिफरेंस’ के रूप में खोजना होता है। इस अन्य की खोज ने व्यक्तियों की कैटेगरी को मालों की कैटेगरी में खोजना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि ‘रियल’ से ‘हाइपर रियल’ में बदलाव तब होता है जब वास्तव को मिथ्याभास में बदल दिया जाता है। आज की वास्तविकता यह है कि हम ‘सिमुलेशन’ या अनुकरण के युग में प्रवेश करने लगते हैं। वह महिला अपनी इच्छाओं से खेलना चाहती थी जिसकी ट्रैजिक परिणति यह हुई कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। एडवर्ड सईद ने ‘इन्वेंशियों’ की व्याख्या करते हुए आज के पाठकों के पठन के लिए बताया है कि विको ने लिखा है कि उन्हें चीजों को खोजने और उघाड़ने की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। शायद इसी दृष्टि से फूको ने भी लिखा है कि ‘लेखन में राजनीतिक उपपाठ अन्तर्ग्रथित रहता है।’
‘पाठकीय क्रीड़ा वास्तव में शक्ति क्रीड़ा होती है और प्रत्येक पाठ की तह में शक्ति का व्यूहन मौजूद रहता है।’
‘ पाठक या समीक्षक ऊपरी सतह को तोड़कर रचना के भीतर छिपे हुए उपपाठ को प्रकाश में लाता है।’
इसे एडवर्ड सईद ने और स्पष्ट करते हुए लिखा है- ‘ राजनीति सब ओर होती है। इससे बचने के लिए शुद्ध कला (निर्मल वर्मा की तरह) के क्षेत्र में या यूं कहें हित निरपेक्ष वस्तुनिष्ठा अथवा अतीन्द्रिय सत्ता की अधिकल्पना के क्षेत्र में शरण नहीं ली जा सकती।’
कथा के वातावरण का जो ताना-बाना बुना गया है उस नेटवर्क का पाठ मैकलुहन की उक्ति को प्रासंगिक बना देती है।
‘वातावरण वह है, जो एक साथ हमारे ऊपर चारों तरफ से प्रहार करे। यह सिर्फ कन्टेनर नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया हैजो निरन्तर अन्तर्वस्तु को बदलती रहती है।’
अतएव वह क्राइसिस संस्कृति में प्रवेश कर गयी है। इसका जीवन संशय का जीवन हो गया है। प्रत्येक मूल्य, लक्ष्य प्रश्नांकित हो गये हैं। शायद हाइडेगर ने ऐसी ही स्थिति में लिखा था- ‘estoric meiaditions culminate in a kind of Asthetic Ontology.’
आज की भावनात्मक विच्छिन्नता के संकट की बेला में संकट के विभिन्न प्रत्यक्ष और छद्म को पहचानने वाला पाठ क्या प्रगति या विकास की आयरनी को प्रगट नहीं करता ?
इस कथा – संरचना में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि लेखक सब कुछ लिखकर पाठक को स्वयं के लिए सोचने का अवकाश नहीं देता।