हिन्दी दिवस पर विशेष
हिन्दी भाषा के समक्ष चुनौतियाँ
अरुण कुमार कैहरबा
हर रोज दिन-रात हम भाषा के जरिये अपना काम करते हैं। अपने भावों, विचारों व उधेड़बुन को अन्य लोगों के सामने रखते हैं। दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। पढ़ते और लिखते हुए भी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम ही होता है कि जिस भाषा का हम सदा प्रयोग करते हैं, उसके बारे में बात करते हों। हिन्दी दिवस व मातृभाषा दिवस आदि कुछ दिन आते हैं, जब हम भाषा के बारे में बात करते हैं।
भाषा के बारे में कम सोचने और बात करने का एक कारण यह है कि अपनी भाषा हमें बिना कोई विशेष प्रयास मिल जाती है। जैसे पानी, हवा और धूप आदि हमें प्रकृति से मिलती है, वैसे ही भाषा हमें समाज से स्वत: मिल जाती है। उसके लिए अधिक कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन हवा, पानी, धरती व धूप की तरह ही भाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए भाषा जीवन रेखा है। मानव जीवन को जो इतनी गरिमा, सम्मान व ऊंचाईयां मिली हैं, वे भाषा की बदौलत ही हैं। हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सहित अनेक प्रकार के पर्यावरणीय संकटों के प्रति थोड़ा बहुत सजग हैं, लेकिन भाषा के प्रदूषण के बारे में बहुत कम ही सजगता देखने को मिलती है। यही कारण है कि स्थान-स्थान पर गाली-गलौज धड़ल्ले से होता रहता है, जो कि हमारी सोच, समझ, संस्कारों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। भाषा का चीर-हरण मनुष्य को भला कैसे गौरवान्वित कर सकता है।
भाषा के ही माध्यम से हम मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतर करते हैं। मनुष्य ने जो विकास किया है वह भाषा की बदौलत किया है। जितना किसी समाज की भाषा विकास करेगी, उतना ही वह समाज विकास करेगा। मनुष्य के साथ-साथ भाषा का और भाषा के साथ-साथ मनुष्य का विकास हुआ। भाषा की सीमाएं ही मनुष्य और उसके विकास की सीमाओं को निर्धारित करती हैं। अपनी भाषा के विकास के लिए विभिन्न भाषाओं के साहित्य को हम अपनी भाषा में अनुवादित करते हैं। भाषा केवल विचार-अभिव्यक्ति का ही साधन नहीं है, बल्कि सोचने और महसूस करने का भी माध्यम है। भाषा के बिना हम समाज-संस्कृति व साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते।
अन्य प्रकार की विविधताओं के अलावा भारत की भाषायी विविधता दुनिया भर के लिए आश्चर्य का विषय है। भारत में बहुत सी मातृभाषाएं हैं। 121 भाषाओं को 10 हजार से अधिक लोग बोलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाएं हैं। शायद ही दुनिया के किसी देश में इतनी अधिक भाषाएं और बोलियां हों और उनमें ज्ञान का इतना विपुल भंडार हो। लेकिन साथ ही ऐसा भी शायद ही कोई देश होगा, जहां पर इतनी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद शासन व लोगों में अन्य किसी भाषा के प्रति इतनी दीवानगी हो। अंग्रेजों की दासता के परिणामस्वरूप भारत में आई और फैली अंग्रेजी भाषा सीखने-सिखाने का धंधा यहां चरम पर है। यहां पर गांव-गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलते ही जा रहे हैं। बहुत से संस्थानों में हिन्दी या मातृभाषाओं के गलती से भी शब्द बोले जाने की स्थिति में आर्थिक-शारीरिक दंड दिया जाता है। सरकारी स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने को ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रूप में प्रचारित करने का काम हमारे राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि हरियाणा सहित कईं राज्यों के सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी व पहली कक्षा से ही अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। आईलेट्स की तैयारी करने और करवाने का बहुत बड़ा कारोबार भारत में पनप गया है। हिन्दी को प्रचारित करने के लिए हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह और हिन्दी पखवाड़ा मनाए जाते हैं, जिनमें हिन्दी बुलवाने के लिए ईनाम दिए जाते हैं। यह बेहद विडंबनादायी स्थिति है। सवाल यह है कि क्या दिवस, सप्ताह व पखवाड़े मना कर ही किसी भाषा को बचाया या समृद्ध किया जा सकता है?
आम जन की भाषा के प्रयोग के द्वारा ही लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तव में सफल हो सकती है। लेकिन हमारे यहां भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है। सत्ताधीशों ने जन भाषाओं को कभी स्वीकार्यता नहीं दी। संविधान की धारा 343 में देवनागरी में लिखी जाने वाली हिन्दी को राजभाषा बनाया गया। हिन्दी का सहयोग करने के लिए 15 सालों के लिए अंग्रेजी को दायित्व सौंपा गया था। अब अंग्रेजी सहयोगी नहीं सर्वेसर्वा हो गई है। आम जन की भाषा को राजकाज के काम में लेने में हमेशा गुरेज किया जाता रहा। शासन व नौकरशाही में बैठा देश का आभिजात्य वर्ग संविधान की मूलभावना को पूरा करने में असफल रहा। संभवत: यह आम लोगों को सत्ता से दूर रखने का ही एक प्रयास था। क्योंकि हिन्दी व भारतीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता तो इससे अंतत: देश की आम जनता ही सशक्त होती और लोकतंत्र मजबूत होता। आज प्रशासन हो या न्यायपालिका हर क्षेत्र में अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। न्यायालयों की कार्रवाई और निर्णयों का उन लोगों को पता तक नहीं होता, जिनके वर्षों न्यायालयों के चक्कर काटते गुजर जाते हैं। हरियाणा के एक जिला न्यायालय में किसान अपने मामले की खुद पैरवी कर रहा था। वह अपनी बात कहने लगा तो जज ने कहा- मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप वकील कर लीजिए। किसान ने तुरंत जवाब दिया- आपको मेरी भाषा समझ नहीं आती तो आप करो वकील।
किसी भाषा को आगे बढ़ाने में उसके पढ़े-लिखे वर्ग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारत विशेष तौर पर हिन्दी भाषी क्षेत्र के पढ़े-लिखे वर्ग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वह औपनिवेशिक भाषा अंग्रेजी का पिछलग्गू बना रहा या अपने ही हित साधता रहा। जिन हिन्दी विद्वानों को हिन्दी की क्षमता को बढ़ाते हुए लोगों की अभिव्यक्ति सामथ्र्य को समृद्ध करना था, उन्होंने हिन्दी को संस्कृतनिष्ठता के चंगुल में उलझाने की ही कोशिश की।
हिन्दी एक जनभाषा है। हिन्दी को आम जन व जन कवियों ने समृद्ध किया है। कबीर, मीरा, सूरदास, तुलसी, मलिक मोहम्मद जायसी व आधुनिक काल के निराला सहित अनेक कवियों की विरासत हिंदी के पास है। आम जन से निकले इन कवियों को ही पाठकों ने सम्मान दिया है। दरबारों में रह कर काव्य-रचना करने वाले कवियों व लेखकों को वह सम्मान नहीं मिला। न ही हिंदी जगत ने उन्हें अपना माना। हिन्दी स्वाभाविक रूप से उर्दू सहित विभिन्न भाषाओं से आदान-प्रदान करती रही है। हिन्दी की किसी भी भाषा के साथ प्रतियोगिता व प्रतिद्वंद्विता नहीं हो सकती, न ही किसी भाषा को समाप्त करके आगे बढऩे की कामना की है। लेकिन शुद्धतावादियों ने हिन्दी को उसकी मूल जड़ों से काट कर संस्कृत के शब्दों को ठूंस डाला और हिन्दी को कठिनता, जटिलता व क्लिष्टता की ओर धकेल दिया। यही कारण है कि बनावटी भाषा में अनुदित की गई रचनाएं सामान्य भाषा से भी अधिक कठिन हो गई हैं। जबकि जनता की जुबान पर चढ़े जनभाषा के आसान शब्दों को भाषा में स्थापित करने की जरूरत है। हिन्दी भाषा को हमें संस्कृत के शब्दों का संग्रहालय बनाने से बचना चाहिए। भाषा में विकार आने पर विकास होता है। यह भाषा की प्रकृति है। इसलिए भाषाई प्रयोगों का दिल खोल कर स्वागत किया जाना चाहिए।
फिल्मों ने संस्कृतनिष्ठ, बनावटी और दिखावटी हिन्दी पर व्यंग्यात्मक अंदाज में कड़ी प्रतिक्रिया की। लेकिन हिन्दी विद्वान इस सवाल को सुलझाने कीे बजाय उलझाते ही गए। अमीर खुसरो, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र सहित कितने ही साहित्यकारों की लोकप्रियता को खारिज करते हुए कथित विद्वानों ने हिन्दी के जन्म के मनगढ़ंत किस्से चलाए।
आज जब भी हिन्दी की बात होती है तो कुछ लोग संस्कृत को हिन्दी की जननी बताने में गौरव महसूस करते हैं। जबकि एतिहासिक दृष्टि भाषाओं के विकास को भावनात्मक की बजाय यथार्थपरक ढंग से समझने की जरूरत है। संस्कृत के बारे में सर्वमान्य जानकारी है कि यह विद्वानों की भाषा रही है। वैदिक और लौकिक संस्कृत के दौर में भी पालि जनभाषा के रूप में मौजूद थी। आम जन पालि सहित अन्य लोकभाषाओं में आचार-व्यवहार करते थे। पालि में बौद्ध साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। जैन साहित्य लिखने के लिए प्राकृत भाषा को मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश व अवहट्ट से होते हुए हिन्दी के मौजूदा रूप का जन्म हुआ। अमीर खुसरो को आधुनिक खड़ी बोली हिन्दी का पहला कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ।
पूरे देश में कोई एक तरह की हिन्दी नहीं है। अवधी, ब्रज व हिन्दी भाषी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों में लिखा गया साहित्य हिन्दी का ही साहित्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है- ‘अब तक बहुत लोगों का खयाल था कि हिन्दी की जननी संस्कृत है। यह ठीक नहीं। हिन्दी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से है और अपभ्रंश की उत्पत्ति प्राकृत से है।’
स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी साहित्य व पत्रकारिता ने अग्रणी भूमिका निभाई। देश को एक सूत्र में जोडऩे के लिए जब एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत महसूस की जा रही थी। तब हिन्दी भाषी साहित्यकारों से भी अधिक बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र व दक्षिण भारत के कितने ही समाज सुधारकों व स्वतंत्रता सेनानियों ने हिन्दी को आगे रखने की जरूरत रेखांकित की। महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था- ‘राष्ट्रभाषा का स्थान हिन्दी ही ले सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं।’ राजाराम मोहन राय बंगाली थी। उन्होंने हिन्दी के बारे में कहा था-‘हिन्दी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है।’ गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था- ‘हिन्दी द्वारा सारे भारत को एकसूत्र में पिरोया जा सकता है।’ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कहना था- ‘राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार से हिन्दी ही ऐसी भाषा है।’ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था-‘देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा हिन्दी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है।’
भाषा को धर्म की संकीर्णताओं के साथ जोड़ा जाना सबसे बड़ी चुनौती है। हिन्दी को हिन्दुओं और मुसलमानों को उर्दू के साथ जोड़े के प्रयास हुए हैं। किसी शायर ने कहा है- ‘सिर्फ ले देके यही एक कमी है हममें, हम उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं।’ हिन्दी में संस्कृत शब्दों को ठूंसा जाने लगा और उन शब्दों को जबरदस्ती बाहर किया जाने लगा, जिनका मूल फारसी या उर्दू भाषा से था। इससे हिन्दी की स्वाभाविकता व मिठास को ठेस पहुंची। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी का हिन्दुस्तानी स्वरूप ही लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने इसी हिन्दी में अपनी रचनाएं लिखीं और उनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई व आगे भी रहेंगी। इससे साबित होता है कि भाषाओं का धर्मों से कोई संबंध नहीं होता है। एक ही धर्म को मानने वाले विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की एक ही भाषा हो सकती है।
किसी भाषा के निर्माण व विकास में उसकी बोलियों व उपभाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असल में तो ये बोलियां ही किसी भाषा की शक्ति होती हैं, जो उसका रूप निखारती हैं और उसमें प्राण डालती हैं। हिन्दी की मुख्यत: पांच उपभाषाएं और उनसे संबंधित 18 बोलियां हैं। उपभाषाओं और बोलियों की अपनी विशिष्टताएं हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं- खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली व कन्नौजी। पूर्व हिन्दी की अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी की मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी व मालवी, पहाड़ी हिंदी की कुमाऊंनी व गढ़वाली तथा बिहारी की मगही, मैथिली व भोजपुरी आदि बोलियां हैं। इन बोलियों से ही हिंदी भाषा जीवन रस ग्रहण करती है और फलती-फूलती है। बोलियों से ही जीवंत संपर्क ही किसी भाषा को सजीव बनाता है। भाषा का निर्माण गलियों, चौराहों, बाजारों, खेतों-खलिहानों व मेलों-ठेलों में होता है। जीवन संघर्षों में ही नए-नए शब्द व मुहावरे पैदा होते हैं। सरकारी दफ्तरों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के भाषा-विभागों में भाषा नहीं बनती। ना ही समाज का अभिजात्य वर्ग ही भाषा का निर्माण करता है। किसी भाषा के मानकीकरण में इन वर्गों व संस्थानों की भूमिका जरूर होती है।
लोकभाषाओं के महत्व को दर्शाने के लिए गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर और बलराज साहनी का एक किस्सा है। टैगोर के लिए शांतिनिकेतन में बलराज साहनी आए। वे उस समय अंग्रेजी में लिखते थे। टैगोर ने उनसे सवाल किया-आप पंजाबी में क्यों नहीं लिखते। साहनी ने जवाब दिया- मैं अपनी बात को पूरी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। टैगोर ने कहा- मैं तो बांगला में ही लिखता हूँ। और मुझे मेरी कविता के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। कुछ समय के बाद फिर से टैगोर ने फिर से पूछा कि आप पंजाबी में क्यों नहीं लिखते? इस पर बलराज साहनी ने जवाब दिया-पंजाबी भाषा इतना लोड नहीं उठा सकती। पंजाबी में इतनी क्षमता नहीं है। इस पर टैगोर ने कहा- पहली बात तो यह है कि पंजाबी में आपकी माँ बात करती है। दूसरी बात यह है कि जिस भाषा में गुरु नानक ने लिखा है वह भाषा कमजोर कैसे हो सकती है। बलराज साहनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद साहनी पंजाबी में लिखने लगे।
आजादी के बाद जितने भी शिक्षा आयोग व शिक्षा नीतियां बनीं, सभी ने हिन्दी व मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषाओं में देने की बात कर रही है। इसके बावजूद बाजार के हितों की रक्षा करने के लिए हिन्दी व भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है। यदि लोगों को यह लगता है कि हिन्दी व मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो देश पिछड़ जाएगा, तो हमें रूस, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस व इटली सहित मातृभाषाओं को शिक्षा व राजकाज का माध्यम बनाने वाले देशों से सीखना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा भी है-निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय का सूल।। प्रचलित करो जहान में निज भाषा करि जत्न। राज काज दरबार में फैलावहु यह रत्न।।
आज हिन्दी को साहित्य की भाषा माना जाता है। लेकिन जब ज्ञान-विज्ञान की बात आती है और जब शिक्षा के माध्यम की बात आती है तो विज्ञान, वाणिज्य व समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का रूख कर लिया जाता है। कोई भी भाषा पठन-पाठन के बिना विस्तार नहीं प्राप्त कर सकती। जबकि शिक्षा विभाग द्वारा अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नन्हे बच्चों को मातृभाषा के साथ-साथ विदेशी अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ रही है। इससे बच्चों के मन-मस्तिष्क पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। जबकि दुनिया के कितने ही देशों में प्राथमिक शिक्षा केवल मातृभाषा में ही दी जा रही है, जोकि सीखने-सिखाने के नियमों के अनुकूल है। प्राथमिक के बाद हरियाणा के कक्षा छह से आठवीं तक के स्कूलों में हिन्दी भाषा को संस्कृत से जोड़ दिया गया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में हिन्दी भाषा को पढ़ाने के लिए स्कूलों में पहला पद संस्कृत अध्यापक का सृजित किया जाता है। इस तरह से शिक्षा में दोयम दर्जा दिया जाना हिन्दी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कॉलेजों व विश्वविद्यालय में हिन्दी व कला संकाय के विषयों को छोड़ दें तो अंग्रेजी का ही बोलबाला है। जबकि पूरी दुनिया में बार-बार यह साबित हो चुका है कि शिक्षा में जितनी सफलता मातृभाषा माध्यम से प्राप्त होती है, उतनी सफलता विदेशी भाषा माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। मातृभाषा आधारित शिक्षा में विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं।
प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी प्रो. जोगा सिंह मातृभाषा व विदेशी भाषा के बारे में तीन अंधविश्वासों का पुरजोर ढंग से खंडन करते हैं। पहला अंधविश्वास- विदेशी भाषा सीखने का अच्छा तरीका यह है कि इसका शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग हो। जबकि विदेशी भाषा को माध्यम की बजाय एक विषय के रूप में पढऩा अधिक कारगर होता है। दूसरा अंधविश्वास- विदेशी भाषा सीखने के लिए जितना जल्दी शुरू किया जाए, उतना अच्छा है। जबकि सच्चाई यह है कि जल्दी शुरू करने से लहजा तो बेहतर हो सकता है पर लाभ की स्थिति में यह होता है जो प्रथम भाषा पर अच्छी महारत हासिल कर चुका हो। तीसरा अंधविश्वास- मातृभाषा विदेशी भाषा सीखने के मार्ग में रूकावट है। जबकि असल में मातृभाषा में मजबूत नींव से विदेशी भाषा बेहतर सीखी जाती है।
कुछ लोग तो हिन्दी की क्षमता पर भी प्रश्रचिह्न लगाने लगते हैं। जबकि किसी भी भाषा की क्षमता तभी बढ़ती है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हर भाषा पूरी तरह से क्षमतावान है। जरूरत पड़ने पर उसमें नए तकनीकी शब्द व संरचनाएं विकसित की जा सकती हैं। सबको शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया ही जाना चाहिए। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने त्रिभाषा फार्मूला दिया है। इस फामूर्ले से कुछ प्रदेशों में हिन्दी के विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हिन्दी भाषी राज्यों में त्रिभाषा पढ़ाने के लिए देश के दक्षिणी राज्यों की भाषाओं की उपेक्षा की है। जैसे हरियाणा के स्कूलों व कॉलेजों में हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत के शिक्षण को त्रिभाषा मान लिया गया है। जबकि जरूरत इस बात की है कि हिन्दी भाषी राज्य देश के अन्य राज्यों की मातृभाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था करें ताकि देश में एकता व सद्भाव का संचार हो सके। इससे अन्य राज्य भी हिन्दी को अपनाने के प्रति उत्साहित होंगे। हिन्दी देश की बड़ी आबादी की मातृभाषा है। अत: त्रिभाषा फार्मूला को अपनाने व परस्पर सहयोग का हाथ बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हिन्दी वालों की ज्यादा है। हिन्दी को समृद्ध तभी किया जा सकता है जब उसे अन्य भाषाओं के शब्द लेकर उसका दायरा बढ़ाया जाए। अगर दूसरी भाषाओं के शब्दों के प्रति संकीर्ण नजरिया रखेंगे तो दूसरी भाषाओं के लोग भी वैसा ही करेंगे। हिन्दी के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए जरूरी है कि दूसरी भाषा के शब्दों को हिन्दी के साथ जोड़ा जाए और उसे समृद्ध किया जाए।
मोबाइल ऐप, डिजिटल प्लेटफार्म, बॉलीवुड, धारावाहिक सहित मनोरंजन जगत व मीडिया में हिन्दी के लिए अपार संभावनाएं हैं। लेकिन विचारणीय यह है कि क्या इन सभी क्षेत्रों में हिन्दी मौलिक रचनात्मक कार्यों में कितनी इस्तेमाल होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिन्दी का बाजार होने की वजह से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता हो। हालांकि हिन्दी के नए मंच तैयार हो रहे हैं। लेकिन हिन्दी पत्र व पत्रिकाओं का बंद होना दिखाता है कि हिन्दी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। मनोरंजन जगत में थोड़ा सा झांकते हैं तो पता चलता है कि कलाकारों को मिलने वाले संवाद देवनागरी की बजाय रोमन में लिखे हुए मिलते हैं। डिजिटल माध्यमों को विकसित करने का काम करने में हिन्दी जगत की नाममात्र या फिर नगण्य भूमिका है। चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वविद्यालयों में हिन्दी के पाठ्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुसार ढाला जाए। ऐसा ना हो कि मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद हिन्दी के विद्यार्थी अपने बुजुर्गों से पूछ रहे हों कि अब वे क्या करें?
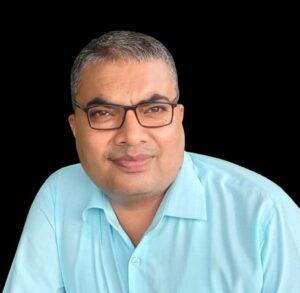
लेखक- अरुण कुमार कैहरबा




