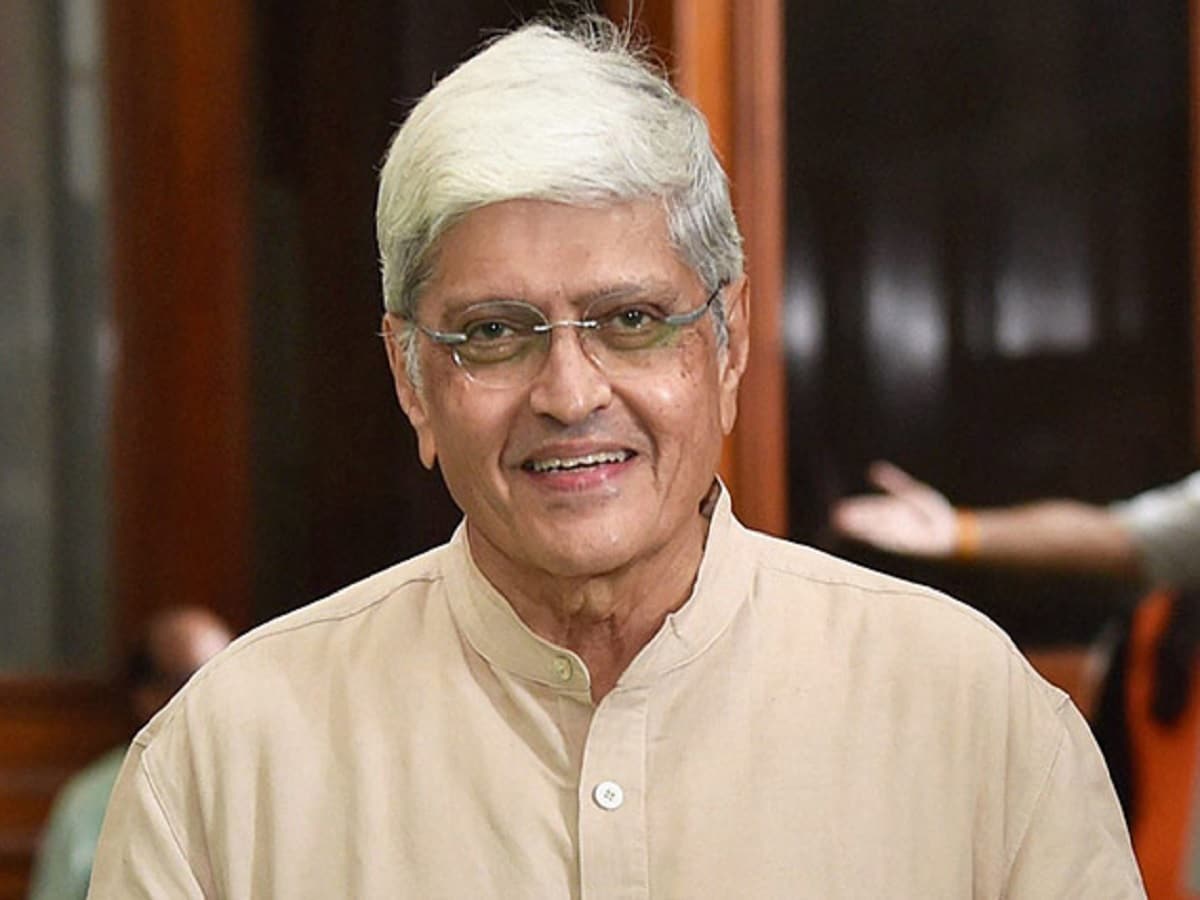एक मूक क्रांति
उपासना मिश्रा
वैश्विक तकनीक और ऊर्जा के उच्च-दांव वाले क्षेत्र में 17 अज्ञात तत्वों का एक समूह एक मूक क्रांति का केंद्रबिंदु बन गया है। दुर्लभ मृदा तत्व स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर उन्नत रक्षा मिसाइलों की मार्गदर्शन प्रणालियों और पवन टर्बाइनों के जनरेटर तक, हर चीज़ को शक्ति प्रदान करते हैं। दशकों से, इन महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति पर चीन का दबदबा रहा है। हालाँकि, भारत एक उभरता हुआ नायक है।
भारत में अनुमानित 6.9 मिलियन मीट्रिक टन प्रमाणित REE भंडार मौजूद हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र मोनाज़ाइट रेत से समृद्ध हैं, जो REE भंडार का लगभग 75% है। व्यवहार्य दुर्लभ मृदा ऑक्साइड ग्रेड की ये रेत, घरेलू प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक तैयार फीडस्टॉक प्रदान करती है। भूमिगत अन्वेषणों ने राजस्थान में कार्बोनेटाइट परिसरों में भारी दुर्लभ मृदाओं के आशाजनक अवशेष भी खोजे हैं। इसके अलावा, भारत के कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश एक अपरंपरागत लेकिन विशाल संसाधन है। प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली इस राख में 160 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक, पुनर्प्राप्ति योग्य REEs होती हैं।
भारत की कमज़ोरी खनन में नहीं, बल्कि इन मज़बूती से जुड़े तत्वों को अलग करने और अंतिम उत्पाद बनाने की जटिल, मूल्यवर्धित प्रक्रिया में रही है। भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन ने इन सीमाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, तमिलनाडु में अपनी पृथक्करण क्षमता का विस्तार कर रही है।
लेकिन असली बदलाव सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने से आया है। उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत, टाटा केमिकल्स-आईआईटी मद्रास जैसे संघों को उन्नत पृथक्करण तकनीकों के लिए पायलट प्लांट स्थापित करने हेतु वित्त पोषित किया जा रहा है।
भारत का अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र भी नवाचार से गुलज़ार है। आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीवों के विकास से लेकर, निम्न-श्रेणी के अयस्कों से चुनिंदा रूप से REE निकालने, और जीवन-अंत चुम्बकों और लैंपों के हाइड्रोमेटेलर्जिकल रिसाइकिलिंग में अग्रणी भूमिका निभाने तक, भारतीय प्रयोगशालाएँ हरित और टिकाऊ निष्कर्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों को अपने कूटनीतिक ताने-बाने में बड़ी चतुराई से पिरोया है। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में एक महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी है और यह ढाँचा पहले से ही ठोस परिणाम दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओडिशा में संयुक्त अन्वेषण और प्रसंस्करण परियोजनाओं का सह-वित्तपोषण कर रहा है; संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसंस्करण को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए भारतीय प्रयोगशालाओं में उन्नत अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है; जापान ने भारत में बड़े पैमाने पर चुंबक निर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए निवेश का वादा किया है।
निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने महत्वपूर्ण नियामक सुधार किए हैं। खनिज रियायतों के लिए अनुमोदन की समय-सीमा कम कर दी गई है और रॉयल्टी छूट व कर लाभ सहित कई वित्तीय प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं।
खनन क्षेत्रों में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए पर्यावरणीय नियमों को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। प्रमुख संस्थानों में महत्वपूर्ण खनिज इंजीनियरिंग के लिए एक विशिष्ट राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
जापान के तोहोकू विश्वविद्यालय जैसे वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत के इंजीनियरों की अगली पीढ़ी को इस विशिष्ट क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रशिक्षण मिले। वैश्विक REE की मांग में सालाना 9% की वृद्धि का अनुमान है, और भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक हल्के दुर्लभ मृदा की 15% और भारी दुर्लभ मृदा की 7% मांग को पूरा करना है।
समृद्ध औद्योगिक विरासत और लंबी तटरेखा वाले कलकत्ता और पूर्वी भारत के पास नए युग के खनिज और प्रौद्योगिकी उद्योग का केंद्र बनने का अवसर है।
अपने भंडार को गतिशील बनाकर तथा एक सम्पूर्ण घरेलू मूल्य श्रृंखला का निर्माण करके, भारत REEs की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में उभर रहा है, तथा प्रौद्योगिकी के युग में एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। द टेलीग्राफ से साभार
उपासना मिश्रा जादवपुर विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सामरिक अध्ययन स्कूल में पीएचडी स्कॉलर हैं।