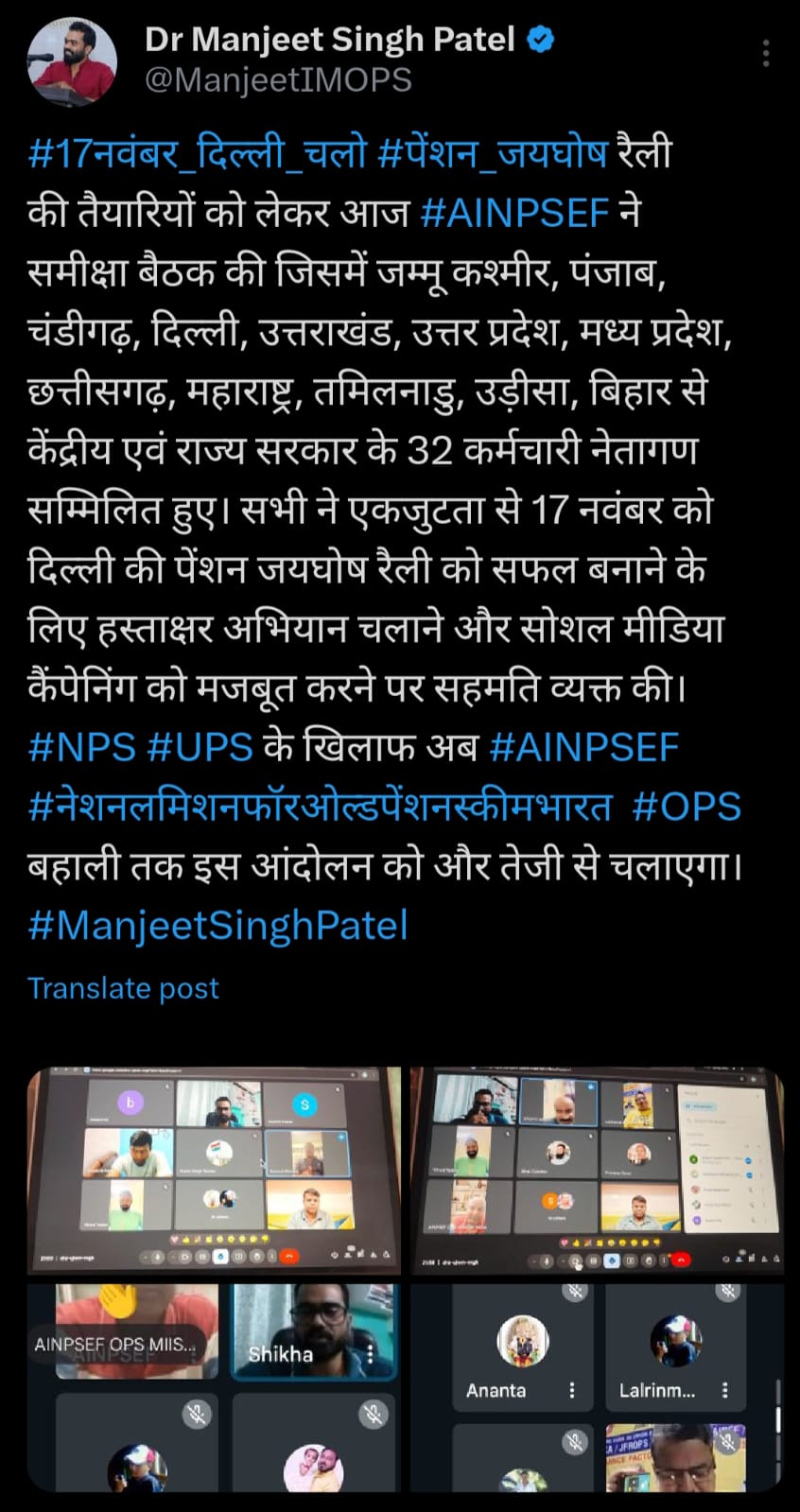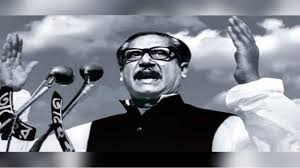अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले आठ राज्य, निर्यात का 0.13%
संगमुआन हैंगसिंग
जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार घाटे, रूसी कच्चे तेल की खरीद और जवाबी मिसाल का हवाला देते हुए अगस्त 2025 में भारत से आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ पर हस्ताक्षर किए, तो नई दिल्ली ने अपनी सामान्य मुद्रा के साथ जवाब दिया – संतुलित भाषा, बंद दरवाजे की कूटनीति और कोई सार्वजनिक प्रतिशोध नहीं।
नृत्य-रचना जानी-पहचानी थी। वाशिंगटन ने प्रहार किया, भारत ने आत्मसात कर लिया। सरकारी आख्यानों ने इसे द्विपक्षीय अशांति के एक और प्रकरण के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन ये नीतियाँ न केवल दो राजधानियों के बीच, बल्कि देश के भीतर भी मौजूद दरारों को काटती हैं। ये केवल व्यापार असंतुलन ही नहीं, बल्कि एक गहरे स्थानिक असंतुलन को भी उजागर करती हैं, जिसे नई दिल्ली लंबे समय से नज़रअंदाज़ करती रही है।
भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन चार राज्यों का कुल वस्तु निर्यात में 70% से अधिक का योगदान है। अकेले गुजरात में यह 33% से अधिक है। यह संकेन्द्रण (एकाग्रता) कोई संयोग नहीं है। इन क्षेत्रों में दशकों से बुनियादी ढाँचे, प्रोत्साहनों और राजनीतिक निरंतरता का समन्वय रहा है। इस बीच, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, हाशिये पर बने हुए हैं, जिनके बीच देश के कुल व्यापार का बमुश्किल 5% ही होता है।
पूर्वोत्तर का हाशिए पर जाना
फिर पूर्वोत्तर है, जिसका भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था में स्थान जानबूझकर हाशिए पर है। 5,400 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले आठ राज्य राष्ट्रीय निर्यात में सिर्फ़ 0.13% की हिस्सेदारी रखते हैं।
उन्हें विदेशी बाज़ारों से जोड़ने वाला कोई चालू व्यापार गलियारा नहीं है। और, नीति निर्माण में भूमिका या मात्रा का समर्थन करने के लिए कोई रसद ढाँचा भी नहीं है। इसके बजाय, जो मौजूद है वह एक सुरक्षा तंत्र है जिसे आतंकवाद-रोधी और निगरानी के लिए तैयार किया गया है। व्यापार कभी भी इस अधिदेश का हिस्सा नहीं रहा।
भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने वाली संस्थाओं में पूर्वोत्तर का संरचनात्मक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक भी सदस्य इस क्षेत्र से नहीं है। भारत की निर्यात रणनीति को दिशा देने वाले व्यापार बोर्ड में मिज़ोरम, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश का कोई ठोस प्रतिनिधित्व नहीं है।
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी योजनाएँ गुजरात से तमिलनाडु तक फैले औद्योगिक क्षेत्रों में धूमधाम से लागू की जा रही हैं। लेकिन पूर्वोत्तर के पहाड़ी और घाटियों को बिना बुनियादी ढाँचे, बिना रसद और बिना संस्थागत लाभ के वैश्विक बाज़ारों में आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया है।
यह महज़ नौकरशाही की अनदेखी नहीं है। यह एक बेतुकी गणना है कि इस क्षेत्र को प्रतीकात्मक रूप से अपनाया जा सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से अनाथ बना दिया जा सकता है। हाल ही में 2024 में, विदेश व्यापार महानिदेशालय की रणनीतिक निर्यात योजना में 87 पृष्ठ ऐसे थे जिनमें पूर्वोत्तर के गलियारों पर एक भी खंड नहीं था। इस चूक का विरोध नहीं किया गया। यह बस मान लिया गया था।
असम में, चाय की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। कीमतें स्थिर हैं, मज़दूरों की कमी बनी हुई है, और बागानों पर बोझ बढ़ रहा है। प्रमुख पश्चिमी बाज़ारों में 25% टैरिफ़ बढ़ोतरी से मुनाफ़े के कम होने का ख़तरा है। डिब्रूगढ़ के एक बागान मालिक, जो 500 से ज़्यादा मज़दूरों की देखरेख करते हैं, ने कहा, “हम ‘टिप्स’ के सहारे काम चला रहे हैं। अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ के खरीदार ऑर्डर कम कर देते हैं, तो हमें तुरंत काम कम करना होगा।”
इस क्षेत्र में भारत के कुल चाय उत्पादन का आधे से ज़्यादा हिस्सा होता है, लेकिन उच्च-मूल्य वाली पैकेजिंग या ब्रांडिंग लगभग न के बराबर होती है। ज़्यादातर चाय अभी भी सीटीसी-ग्रेड की होती है, नीलामी में बेची जाती है और बाज़ार के हर उतार-चढ़ाव के संपर्क में रहती है। खरीदार पुनर्मूल्यांकन के दौर में हैं और ऊपरी असम क्षेत्र और दोआर्स में लागत में कटौती शुरू हो गई है। मज़दूरी कम हो रही है। उत्पादन कम हो रहा है। अगली चीज़ जो जाएगी वह है नौकरियाँ।
नुमालीगढ़ में, रिन्यूरी असम की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में एक तंत्रिका धमनी की तरह बहती है। इसका अधिकांश कच्चा तेल अभी भी ऑयल इंडिया और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आस-पास के क्षेत्रों से आता है, लेकिन यह स्थिति बदल रही है। नौ मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक विस्तार का मतलब है कि इसे पारादीप की ओर, और धीरे-धीरे, रियायती रूसी कार्गो की ओर देखना होगा।
यहीं से ख़तरा पैदा होता है। वाशिंगटन का टैरिफ़, जो आंशिक रूप से भारत के रूस के साथ गठबंधन की प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया गया है, यहाँ एक लंबी छाया डालता है। अगर प्रतिबंधों का अगला दौर कड़ा होता है या शिपिंग लेन कड़ी होती हैं, तो इसका असर मुंबई की बैलेंस शीट पर नहीं दिखेगा। गोलाघाट ही काँपेगा।
म्यांमार, आसियान के साथ एक मौन सीमा
नेपीडॉ में 2021 के तख्तापलट के बाद से, भारत-म्यांमार सीमा पर व्यापार कम हो गया है। कभी क्षेत्रीय एकीकरण की धमनियों के रूप में देखे जाने वाले राजमार्ग अब चौकियों, नाकाबंदी चौकियों और नौकरशाही के कोहरे में खो गए हैं। कभी छिद्रपूर्ण और आदान-प्रदान से जीवंत, यह सीमा अब खामोशी से बोलती है।
म्यांमार के लिए भारत के दो प्रमुख प्रवेश द्वार, मिज़ोरम में ज़ोखावथर और मणिपुर में मोरेह, अब कंकाल जैसी चौकियों में तब्दील हो चुके हैं। कभी एक्ट ईस्ट के सपनों के केंद्र रहे ये मार्ग अब व्यापार केंद्रों से ज़्यादा सुरक्षा अवरोधों की तरह काम करते हैं। बुनियादी ढाँचा अब भी दिखावटी है—सड़कें सिर्फ़ कागज़ों पर हैं, सीमा शुल्क कार्यालय कमज़ोर हैं, और कोल्ड-चेन सुविधाएँ कहीं नज़र नहीं आतीं। 2024 में मुक्त आवागमन व्यवस्था को ख़त्म करना एक बड़ा झटका था, जिसने न सिर्फ़ व्यापार, बल्कि रिश्तेदारी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और पहाड़ों की आपस में जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी तहस-नहस कर दिया।
वाणिज्य की जगह निगरानी ने ले ली। ये अब व्यापार के गलियारे नहीं, बल्कि नियंत्रण ग्रिड हैं, जो बाज़ार की माँग के बजाय आतंकवाद-रोधी तर्क से बने हैं। जहाँ सामान नहीं चलता, वहाँ सैनिक चलते हैं। और जैसे-जैसे बुनियादी ढाँचा कमज़ोर होता जाता है, ये शहर आर्थिक रूप से प्रासंगिकता खोकर रणनीतिक शून्यता में पहुँचते जाते हैं, जिनका मानचित्रण कनेक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के लिए किया जाता है। सीमा केवल बंद करने के विचार के लिए खुली है।
पूर्वोत्तर को कभी भारत के रणनीतिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के लिए एक सेतु के रूप में देखा जाता था। यह सेतु कभी भी ड्राइंग बोर्ड से बाहर नहीं निकला। नीतिगत हलकों में, व्यापार लचीलेपन का अर्थ अब एक उत्पाद श्रेणी से दूसरी श्रेणी में बदलाव है, इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर, कपड़ा से फार्मा तक। भूगोल इस समीकरण का हिस्सा नहीं है।
यह धारणा “निश्चित” है – व्यापार उन्हीं गलियारों से होकर गुजरता है जिनसे औपनिवेशिक बंदरगाहों और स्वतंत्रता के बाद के औद्योगिक समूहों को सेवा मिलती थी। पूर्वोत्तर उस दायरे से बाहर है, लापरवाही से नहीं, बल्कि जानबूझकर।
एशिया की चालें, भारत की जड़ता
जैसे-जैसे चीन बुनियादी ढाँचे में निवेश, मिलिशिया गठबंधनों और बढ़ती खुफिया गतिविधियों के ज़रिए उत्तरी म्यांमार पर अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है, भारत अपनी ही जेबें गँवाता जा रहा है। मोरेह से शुरू होने वाला भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग अब जंगल में गायब हो गया है।
भारत के सीमांत रुख़ को वाणिज्य नहीं, बल्कि निगरानी परिभाषित करती है। जहाँ सामान नहीं आता, वहाँ सीमा बल आते हैं। और जब आवाजाही गश्त तक सीमित हो जाती है, तो सीमावर्ती इलाके स्थिर नहीं रहते; वे अव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं।
ज़रूरत पुनर्निर्माण की नहीं, बल्कि बुनियादी सरकारी कामकाज की है। व्यापार सड़कों पर चलता है, बयानबाज़ी से नहीं। यह गोदामों से होकर गुज़रता है, श्वेत पत्रों से नहीं। पूर्वोत्तर में, ये धमनियाँ गायब हैं। बुनियादी ढाँचा छिटपुट है, और नीतिगत उपस्थिति और भी कम है।
श्री ट्रम्प के टैरिफ को क्षणिक परेशानी मानकर, भारत गहरी संरचनात्मक खामी को नज़रअंदाज़ कर रहा है—इसकी व्यापारिक अर्थव्यवस्था स्थानिक रूप से असंतुलित है। गुजरात में बाढ़ या तमिलनाडु में मज़दूरों की हड़ताल राष्ट्रीय पाइपलाइन को जाम करने के लिए काफ़ी है। यह फैलाव नहीं, बल्कि निर्भरता है। वैश्विक बिसात बदल गई है। आपूर्ति श्रृंखलाएँ गतिमान हैं। चीन पूँजी का पुनःस्थापन कर रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया वैकल्पिक गलियारे बना रहा है। भारत हिंद-प्रशांत समीकरण में अपनी भूमिका का दावा करता है, लेकिन उसका निर्यात ढाँचा अभी भी कुछ तटीय इलाकों पर टिका है। जब पूर्वी सीमांत क्षेत्र वाणिज्य मानचित्र से कटा हुआ रहता है, तो रणनीतिक बातें खोखली लगती हैं।
कोई राज्य क्षेत्रीय ताकत का दावा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका पूर्वी किनारा आर्थिक रूप से कमज़ोर बना रहे। पूर्वोत्तर ने कभी नारों की माँग नहीं की। उसे शासन-कौशल के न्यूनतम व्याकरण की आवश्यकता है: बाज़ारों तक पहुँचने वाली सड़कें, भूगोल को समझने वाली नीतियाँ, और चुनावी गणित से परे देखने वाला शासन।
दशकों से, इस क्षेत्र को विद्रोहों, युद्धविरामों और खोखली नीतियों के बीच इंतज़ार करने के लिए कहा जाता रहा है। लेकिन दुनिया आगे बढ़ रही है। व्यापार में व्यवधान ज़्यादा बार आ रहे हैं। गलियारे बदल रहे हैं। और अब देरी एक योजना की तरह लग रही है।
कोई भी एक लक्ष्य भारत को नहीं तोड़ सकता, लेकिन बार-बार क्षेत्रीय चूक एक समेकित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को नष्ट कर देती है। यह प्रतिशोध का आह्वान नहीं है। यह लचीलेपन को पुनर्परिभाषित करने की माँग है, शक्ति के संकेंद्रण के रूप में नहीं, बल्कि मानचित्र के हर हिस्से से आने वाले झटकों को सहने की क्षमता के रूप में। तब तक, यह अस्पष्ट बिंदु बरकरार रहेगा। द हिंदू से साभार
संगमुआन हैंगसिंग एक शोधकर्ता और कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के पूर्व छात्र हैं