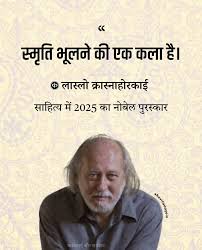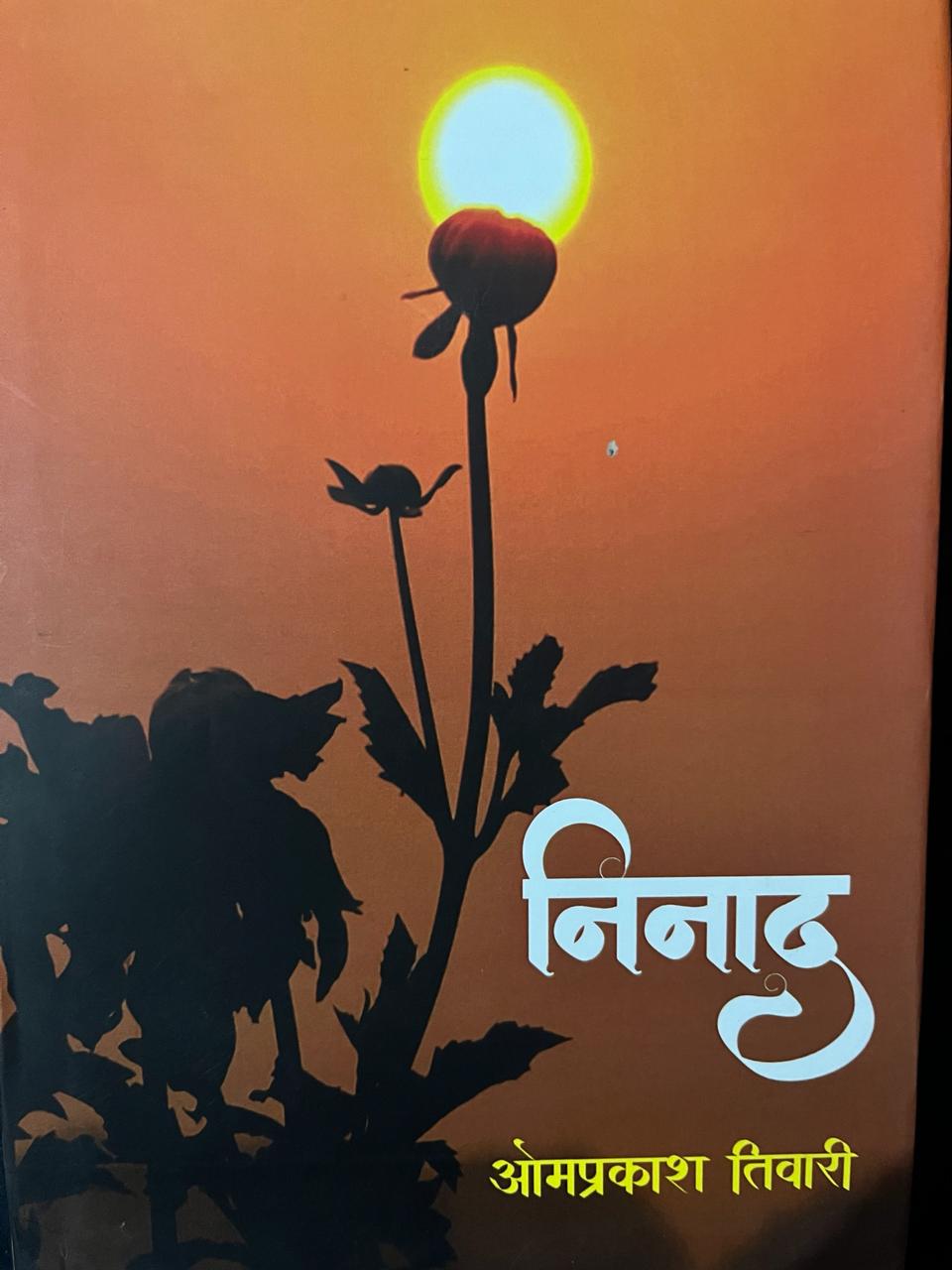लास्लो क्रास्नाहोर्काई ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते समय जो व्याख्यान दिया उसका हिंदी में अनुवाद राकेश कुमार मिश्र ने किया है। उसे प्रकाशित किया है वेब प्रत्रिका समालोचन ने। हम यहां समालोचन से आभार सहित यहां प्रतिबिम्ब मीडिया के पाठकों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं, साथ में समालोचन की व्याख्यान को लेकर टिप्पणी भी दे रहे हैं।-
लास्लो क्रास्नाहोरकाई का 7 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम में दिया गया नोबेल-व्याख्यान आधुनिकता की उस थकान का सघन दस्तावेज़ है, जो अब केवल सामाजिक या राजनीतिक संकट भर नहीं रह गई है, बल्कि मनुष्य की संवेदनात्मक संरचना को भीतर से भी बीमार कर चुकी है. यह व्याख्यान एक गहन विलाप की तरह है, जिसमें उदासी अलंकार नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल अवस्था बन जाती है. पूरी सृष्टि यहाँ चुप्पी में ढहती प्रतीत होती है. जैसे कोई अंतिम प्रार्थना हो. इस आततायी समय में साहित्य किसी समाधान या प्रतिकार के रूप में नहीं, बल्कि अंतिम आश्रय के रूप में उपस्थित होता है. एक ऐसी जगह, जहाँ भाषा अब दुनिया को बदलने का दावा नहीं करती, बल्कि उसके विघटन का साक्ष्य बन कर ही संतोष कर लेती है. यह व्याख्यान क्रास्नाहोरकाई के गद्य की तरह ही विडंबनाओं से भरा और गहरे अलगाव में रचा-बसा है. पर इसी निराशा में एक अदृश्य विद्रोह भी निहित है. ऑटिली मूज़लेट द्वारा मूल हंगेरियन से अंग्रेज़ी में किए अनुवाद का यह हिंदी रूपांतरण कवि राकेश कुमार मिश्र ने मन से किया है. स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से फुटनोट भी दिए हैं. यह ख़ास अंक आपके लिए प्रस्तुत है.
लास्लो क्रास्नाहोर्काई का 7 दिसंबर, 2025 को दिया गया नोबेल व्याख्या
आशा की शुरुआत और अंत के बारे में
प्रिय देवियों और सज्जनों,
2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद, मैंने सोचा था कि मैं आज आपसे आशा के बारे में बात करूँगा. लेकिन सच कहूँ तो, मेरे भीतर अब ज़रा-सी भी आशा बची नहीं है. इसलिए मैंने तय किया है कि आज मैं आपसे फ़रिश्तों के बारे में बात करूँगा.
I.
मैं इधर-उधर टहल रहा हूँ और फ़रिश्तों के बारे में सोच रहा हूँ. हाँ, अभी भी टहल ही रहा हूँ, ऊपर-नीचे, एक तरफ़ से दूसरी तरफ़. अपनी आँखों पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ खड़ा होकर माइक्रोफ़ोन में बोल रहा हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं लगातार कमरे में घूम रहा हूँ, एक कोने से दूसरे कोने तक, फिर वापस. बार-बार. और इसी दौरान मेरा दिमाग़ फ़रिश्तों में उलझा हुआ है.
और मैं सबसे पहले आपको बस यह बता देना चाहता हूँ कि जिन फ़रिश्तों की मैं बात कर रहा हूँ, वे पुराने वाले फ़रिश्तों जैसे बिल्कुल नहीं हैं. इनके पंख नहीं होते. इसलिए अब हमें यह सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि अगर दो बड़े पंख उनकी पीठ से निकले हों, या चोग़े के बाहर फैल रहे हों, तो स्वर्ग का दर्ज़ी उन्हें कपड़े कैसे पहनाता होगा. ऊपर उसके कारखाने में कैसी अद्भुत कलाएँ होंगी!
पुराने फ़रिश्तों के बारे में तो यह सवाल भी था कि जब वे देहहीन-सी मुलायम चादर ओढ़ते थे, तो अपने पंख छुपा लेते थे. या फिर वह चोग़ा उनके पंखों को ढक लेता था. ओह, बेचारे सैंड्रो बोत्तिचेल्ली[i] (1445–1510)! बेचारे लियोनार्दो दा विंची (1452–1519)[ii], बेचारे माइकलएंजेलो बुओनारोत्ती (1475–1564) [iii]! यहाँ तक कि बेचारे ज्योत्तो दी बोंदोन (1267–1337)[iv] और फ़्रा आंजेलिको[v] (1395–1455) भी! सबने फ़रिश्तों को पंखों के साथ चित्रित करने में कितनी मेहनत की. लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बचा है. क्योंकि जिन फ़रिश्तों की मैं बात कर रहा हूँ, वे बिल्कुल नए हैं.
मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ. भले ही आप मुझे इस वक्त माइक्रोफ़ोन के सामने खड़े हुए देखें, जबकि मैं असल में अपने कमरे में चक्कर लगा रहा हूँ. और इसी समय यह घोषणा कर रहा हूँ कि इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाला मैं, जो आशा पर बोलने वाला था, अब आशा पर नहीं बोलेगा; मैं फ़रिश्तों पर बोलूँगा.
अब मैं फिर उसी जगह लौटता हूँ जहाँ यह खयाल पहली बार आया था. मेरे दिमाग़ में धीरे-धीरे कुछ आकार लेने लगा था, जब मैं अपने छोटे-से अध्ययन कक्ष में ध्यान लगाए बैठा था. कमरा बस चार बाई चार मीटर का है. अगर उस हिस्से को हटा दें जहाँ से सीढ़ियाँ भूतल की ओर जाती हैं, तो जगह और भी कम बचती है. और हाँ, इसे किसी कीमती हाथीदाँत की मीनार जैसा न समझें. यह टावर-कमरा नॉर्वे स्प्रूस की सस्ती लकड़ी से बना हुआ है, एकमंज़िला लकड़ी की इमारत के दाहिने कोने में.
मेरी ज़मीन ढलान पर है, इसलिए यह कमरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, जैसे कोई छोटा-सा टावर हो. जब नीचे वाले कमरों को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि किताबें हर ओर फैलती जा रही थीं और अब उन्हें संभाले बिना काम नहीं चलता था. तो इसी ढलान की वजह से नया कमरा बनते-बनते ऊपर की ओर उठ गया और टावर जैसा लगता है, जैसे नीचे की मंज़िल पर किसी ने एक भारी चीज़ रख दी हो. खैर, मैं यहाँ सिर्फ़ फ़रिश्तों की बात करना चाहता हूँ.
और मैं आशा के बारे में बात नहीं करूँगा.
और नहीं, मैं पुराने फ़रिश्तों के बारे में बात नहीं कर रहा. यानि उन प्राचीन फ़रिश्तों के बारे में, जिन्हें आप मध्ययुग और पुनर्जागरण के अनगिनत ‘एननसिएशन चित्रों’ (Annunciation Paintings)[vi] में देखते हैं. वे पंखों वाले फ़रिश्ते होते थे, जो एक ही काम लेकर आते थे. ऊपर से भेजा गया संदेश सुनाना. यह बताना कि जिसे जन्म लेना है, वह जन्म लेगा. वही पुराने स्वर्गीय दूत. जो हमेशा किसी न किसी संदेश के साथ धरती पर उतरते रहते थे.
देवदूत-विद्या (angelology) बताती है कि वे अक्सर संदेश ज़ुबान से सुनाते थे, या फिर जैसा नौवीं-दसवीं शताब्दी की चित्रकला में दिखता है. एक लहराती हुई काग़ज़ की पट्टी से पढ़ते थे, एक ऐसी पट्टी जिस पर लिखा हुआ हर शब्द बेहद अहम माना जाता था. जो भी हो, उनका मुख्य काम यही था. ऊपरवाले के किसी संदेश को उसके चुने हुए लोगों तक पहुँचाना. संदेश कभी उजाले में आता था या कभी कान में धीरे से फुसफुसा दिया जाता था.
फ़रिश्ते ख़ुद एक तरह से वही संदेश बन जाते थे. उस सत्ता की तरफ़ से आया हुआ, जिसे न कोई पुकार सकता है, न प्रार्थना कर सकता है. उसी ने उन्हें भेजा था. हमारी ओर, हम लोगों की ओर, जो मिट्टी में संघर्ष करते रहते हैं, भटकते रहते हैं और अकल्पनीय परिणामों के लिए जैसे अभिशप्त हैं. क्या दिन थे वे!
कुल मिलाकर, हर पुराना फ़रिश्ता किसी और की तरफ़ से किसी और को दिया गया संदेश था. जिसमें कभी आदेश जैसा स्वर होता, कभी रिपोर्ट जैसा. लेकिन यहाँ, आपके सामने खड़े होकर या कहें कि अपने टावर जैसे कमरे में लगातार चक्कर लगाते हुए मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता. वह कमरा जिसे आप जानते हैं. सस्ती नॉर्वे स्प्रूस की लकड़ी से बना, जिसे गरम करना लगभग असंभव है, और जो सिर्फ़ इसलिए ‘टावर’ कहलाता है क्योंकि पूरी ज़मीन ढलान पर है.
तो नहीं, मैं पुराने फ़रिश्तों की बात नहीं करने वाला. उन चित्रों के बावजूद जो अब भी हमारे भीतर बसे हुए हैं, मध्ययुग और शुरुआती आधुनिक काल के महान कलाकारों— ज्योत्तो और उनके बाद आने वालों की वजह से. वे पुराने फ़रिश्ते आज भी अपने लिए वही विशेषण लेकर खड़े हैं: आवेगपूर्ण, उज्ज्वल, और आत्मीय.
यहाँ तक कि आज भी वे हमें भीतर तक छू सकते हैं. हमारी उस आत्मा को, जो अब किसी बात पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाती. सदियों तक उन्हीं फ़रिश्तों की दुर्लभ मौजूदगी ने हमें यह कल्पना करने का मौका दिया कि स्वर्ग नाम की कोई जगह है. और इसी के सहारे हम “दिशा” का अर्थ समझ पाए क्योंकि दिशा होती है तो दूरी होती है; और जहाँ दूरी है, वहाँ समय भी है. और इस तरह सदियों यहाँ तक कि हज़ारों सालों तक वही दुनिया बनी रही, जिसे सृष्टि माना गया, वह दुनिया जहाँ इन फ़रिश्तों से हुई मुलाक़ातों ने हमें “ऊपर” और “नीचे” को एक असली, महसूस करने योग्य अनुभव दिया.
तो अगर मैं आपसे पुराने फ़रिश्तों के बारे में बात करता, तो शायद मैं एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाता रहता. लेकिन नहीं, पुराने फ़रिश्ते अब नहीं रहे. अब सिर्फ़ नए फ़रिश्ते हैं. और जहाँ तक मेरी बात है. मैं यहाँ, आपकी ध्यानमग्न नज़रों के बीच, खड़ा हूँ और उन नए फ़रिश्तों पर विचार कर रहा हूँ. बिना इधर-उधर चहलकदमी किए, क्योंकि जैसा कि मैं शायद पहले भी कह चुका हूँ:
हमारे फ़रिश्ते अब ये नए वाले हैं.
और अपने पंख खो देने के बाद, अब उनके पास वे नरम, लिपटे हुए आवरण भी नहीं बचे हैं. वे हमारे बीच बिल्कुल साधारण कपड़ों में आते-जाते हैं. हमें यह भी नहीं पता कि उनकी संख्या कितनी है, लेकिन किसी धुँधले-से संकेत से लगता है कि जितने पहले थे, आज भी शायद उतने ही हैं. और जैसे पुराने ज़माने में पुराने फ़रिश्ते अचानक कहीं भी प्रकट हो जाया करते थे, वैसे ही ये नए वाले भी किसी अनजानी घड़ी में, किसी अनजानी जगह पर, हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं बस यूँ ही, बिना बताए. और सच कहूँ तो अगर वे चाहें कि हम उन्हें पहचान लें, अगर वे अपने भीतर छिपी हुई बात को छिपाएँ नहीं तो उन्हें पहचानना मुश्किल भी नहीं है. क्योंकि जिस तरह वे हमारे बीच चलते हैं, उनकी चाल, उनकी लय, उनका पूरा अस्तित्व ही किसी अलग ही सुर में चलता हुआ लगता है. हमसे थोड़ा-सा हटकर, किसी दूसरी धुन में.
हम, जो इस धरती की धूल में भटकते, उलझते, गिरते-पड़ते चलते रहते हैं. हम तो यह भी नहीं कह सकते कि ये नए देवदूत कहीं ‘ऊपर’ से आ रहे हैं. क्योंकि अब तो ऐसा भी नहीं लगता कि कोई “ऊपर” बचा है. मानो वह भी पुराने देवदूतों के साथ किसी अनंत, अज्ञात जगह में खो गया हो. एक ऐसे कहीं में, जहाँ आजकल एलन मस्क जैसे लोगों की उथल-पुथल भरी योजनाएँ ही समय और अंतरिक्ष की दिशा तय कर रही हैं.
और इसी से यह अजीब सा दृश्य बनता है कि आप अपने सामने एक बूढ़े आदमी को सुन रहे हैं. जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार ले रहा है, और जो आपकी ही भाषा जैसी किसी अजीब-सी भाषा में आपसे बोल रहा है. और आप जानते हैं कि यह बूढ़ा आदमी- जो मैं हूँ, असल में अभी भी उसी टावर जैसे कमरे में टहल रहा है, नॉर्वे स्प्रूस की तख़्तों और बेकार इन्सुलेशन (गर्मी या ठंड से सुरक्षा करने वाली सामग्री) के बीच, उसी ठंड में काँपते हुए. और मैं अपनी चाल तेज़ कर देता हूँ, मानो यह जताना चाहता हूँ कि इन नए देवदूतों के बारे में सोचने के लिए विचारों को भी किसी दूसरी गति की ज़रूरत है. कदमों की किसी दूसरी ताल की.
और जैसे ही मैं तेज़ चलता हूँ, मुझे अचानक एहसास होता है कि इन नए देवदूतों के पास न सिर्फ़ पंख नहीं हैं बल्कि उनके पास कोई संदेश भी नहीं है. एक भी नहीं. वे हमारे बीच सिर्फ़ अपने साधारण कपड़ों में मौजूद हैं. और अगर वे चाहें, तो पहचान में भी न आएँ; और अगर पहचान में आना चाहें, तो अचानक एक व्यक्ति को चुन लेते हैं. उसके पास आते हैं और उसी पल हमारी आँखों से जैसे मोतियाबिंद हट जाता है, दिल की जमी हुई परतें टूटकर झर जाती हैं.
यानी कि एक तरह की मुठभेड़ होती है. हम ठगे-से रह जाते हैं. अरे, यह तो देवदूत है. वह हमारे सामने खड़ा है. लेकिन… वह हमें कुछ भी नहीं देता. कोई शब्द नहीं, कोई चमकती हुई पट्टी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं. कुछ भी नहीं. वह बस खड़ा रहता है, हमें देखता है. हमारी आँखों में एक नज़र की तलाश करता हुआ. और उस तलाश में एक विनती छिपी होती है कि हम उसकी आँखों में झाँकें, ताकि…
ताकि शायद
हम ही उसे कोई संदेश दे सकें.
लेकिन दु:ख की बात यह है कि हमारे पास देने को कोई संदेश होता ही नहीं. क्योंकि जो कुछ कभी कहा जा सकता था, वह बहुत पहले कहा जा चुका था. तब सवाल भी थे और जवाब भी. अब तो न सवाल बचा है न जवाब.
तो फिर यह कैसी मुलाक़ात है? यह कैसा दृश्य है. देवदूत और मनुष्य आमने-सामने, दोनों चुप, दोनों उलझे हुए? वह हमें देखता है, हम उसे देखते हैं. यदि उसे इस मौन का कोई अर्थ समझ आता होगा, हमें तो नहीं आता. मौन और बधिरता में भला संवाद कैसे जन्म ले? कैसे समझ बने? दिव्य उपस्थिति का अनुभव तो दूर की बात है.
तभी. और यह हर अकेले, थके हुए, दुख में डूबे, संवेदनशील व्यक्ति के भीतर होता है. कुछ एकदम से कौंधता है. अभी मेरे साथ हो रहा है. हाँ, अगर मैं ख़ुद को भी आपके बीच गिनूँ तो यह बात मेरे भीतर भी उठती है. मैं, जो आपको माइक्रोफ़ोन में बोलता नज़र आ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ऊपर उस टावर-रूम में चल रहा हूँ, सस्ती लकड़ी और शर्मनाक इन्सुलेशन के बीच चक्कर काटता हुआ.
तभी यह अहसास होता है कि ये नए देवदूत अपने अनंत मौन में शायद अब देवदूत भी नहीं रह गए. ये तो त्याग हैं. उस प्राचीन, पवित्र अर्थ में त्याग .
मैं तुरंत अपना स्टेथोस्कोप निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं उसे हमेशा साथ रखता हूँ और बहुत धीरे से उसका ठंडा डायाफ्राम आपके सीने पर रखता हूँ, एक-एक कर. और तुरंत मैं सुन लेता हूँ- भाग्य की आवाज़. आपके-हम सब के भाग्य की धड़कन.
और उसी पल मैं एक ऐसी सीमा पार कर लेता हूँ, जहाँ एक नया भाग्य धड़क रहा होता है. एक ऐसा क्षण, जो अगले क्षण को बदल देता है. वह अगला क्षण, जो आने वाला था, आता ही नहीं. उसकी जगह एक और क्षण आता है. टकराव का, ढह जाने का. क्योंकि मेरा स्टेथोस्कोप इन नए देवदूतों की भयावह कहानी सुन लेता है. यह कि वे त्याग हैं. त्याग. सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी वजह से; हममें से हर एक की वजह से.
पंखों के बिना देवदूत, संदेश के बिना देवदूत. और हमारे कारण घायल. यह जानते हुए भी कि दुनिया युद्ध में है. हर तरफ़ युद्ध. प्रकृति में युद्ध, समाज में युद्ध.
और यह युद्ध सिर्फ़ हथियारों, यातना और विनाश से नहीं लड़ा जा रहा. वह तो इसकी चरम सीमा है. युद्ध तो दूसरी तरफ़ भी होता है. सिर्फ़ एक बुरा शब्द काफ़ी है. एक ताना, एक चोट, एक अपमान… बस एक ही काफ़ी है इन नए देवदूतों को भीतर तक घायल कर देने के लिए. क्योंकि वे इस दुनिया में यह सब सहने के लिए पैदा नहीं हुए थे.
वे असहाय हैं. क्रूरता के सामने, उपहास के सामने, उस हिंसा के सामने जो उनकी कोमलता और पवित्रता को रौंद देती है.
एक ही चोट काफ़ी है. यहाँ तक कि एक बुरा शब्द भी कि वे हमेशा के लिए टूट जाएँ. और मैं दस हज़ार शब्द बोलकर भी उसे ठीक नहीं कर सकता. क्योंकि ऐसी चोट की कोई मरम्मत संभव नहीं.
II.
अरे, देवदूतों की बात काफी हुई!
अब आइए मनुष्यों की गरिमा के बारे में बात करें.
मनुष्य. अजीब, चमत्कारिक जीव. आख़िर तुम हो कौन?
तुमने पहिया बनाया, आग खोजी, यह समझा कि अकेले जीना मुमकिन नहीं, सहयोग ही बचने का तरीका है. तुमने नेक्रोफैगी (मृत जीवों का मांस खाना ) तक अपना ली ताकि दुनिया पर काबू पा सको. तुमने दिमाग़ की ऐसी क्षमता हासिल की कि उसी के भरोसे तुमने इस धरती पर, सीमित ही सही एक शक्ति पा ली. तुमने इस दुनिया को नाम दिए, उसे समझा, और ऐसी-ऐसी “सच्चाइयों” पर भरोसा किया जो बाद में झूठ निकलीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने में मदद की. तुम्हारा विकास झटकों, छलांगों और छोटे-छोटे विस्फोटों की तरह आगे बढ़ा और तुम पूरे ग्रह पर फैलते चले गए.
तुम झुंडों में रहने लगे, समाज बने, सभ्यताएँ खड़ी हुईं. तुम विलुप्त भी हो सकते थे, लेकिन तुमने बचने का तरीका खोज लिया. फिर तुम दो पैरों पर सीधे खड़े हुए, होमो हैबिलिस (Homo Habilis)[vii] बने. पत्थर के औज़ार बनाए. फिर होमो इरेक्टस (Homo Erectus)[viii] हुए. आग की खोज की. और सिर्फ़ एक छोटे-से फर्क की वजह से कि तुम्हारा लैरिंक्स (स्वरयंत्र) और सॉफ़्ट पैलेट (कोमल तालू) चिंपैंज़ी की तरह आपस में नहीं छूते. तुम भाषा बोल पाए, ठीक उसी समय जब दिमाग़ का भाषिक हिस्सा विकसित हो रहा था.
तुम ईश्वर के साथ बैठने वाले जीव बने. अगर बाइबिल की ओल्ड टेस्टामेंट की दबा दी गई पंक्तियों पर भरोसा करें. तुमने ईश्वर की बनाई चीज़ों को नाम दिया.
फिर तुमने लिखना सीखा. तब तक तुम सोचने-समझने और चीज़ों को जोड़कर देखने लगे थे. पहले घटनाओं को, फिर धर्म से बाहर आकर दुनिया को. तुमने अपने अनुभव से समय की रचना की. तुमने वाहन बनाए, नावें बनाईं, धरती के “अज्ञात” को जीत लिया, जो मुमकिन था लूट लिया. तुमने समझा कि ताकत और शक्ति को कैसे इकट्ठा किया जाता है.
तुमने उन ग्रहों तक को चिह्नित किया जिन्हें जानना कभी असंभव माना जाता था. सूरज अब तुम्हारे लिए देवता नहीं रहा, न तारे तुम्हारी किस्मत लिखते थे. तुमने. या यूँ कहें. तुम्हारी सभ्यता ने यौनिकता को बदला, स्त्री-पुरुष की भूमिकाएँ बदलीं; और देर से सही, प्रेम की खोज की.
तुमने भावनाओं को समझा, सहानुभूति को जन्म दिया, ज्ञान के ढेरों रूप तैयार किए.
और फिर तुमने उड़ना सीख लिया. पक्षियों को पीछे छोड़कर. चाँद पर पहुँचे. ऐसे हथियार बनाए जो धरती को कई बार मिटा सकते हैं.
और फिर तुमने विज्ञान की रचना की. इतना लचीला, इतना तेज़ कि हर नया कल, आज की कल्पनाओं को तोड़ देता है.
तुमने कला बनाई. गुफाओं की चित्रकारी से लेकर लीओनार्डो दा विंची (1452–1519)[ix] की लास्ट सपर (The Last Supper)[x] तक; गहरे, जादुई संगीत से लेकर जोहान सेबेस्टियन बाख (1685–1750)[xi] तक.
और आखिरकार, समय के साथ, तुमने अचानक किसी भी चीज़ पर विश्वास करना बंद कर दिया. और उन उपकरणों की मदद से जिन्हें तुमने खुद बनाया जिन्होंने कल्पना की दुनिया को कमज़ोर कर दिया. अब तुम्हारे पास सिर्फ़ अल्पकालिक स्मृति बची है.
और इस तरह तुमने ज्ञान, सौंदर्य और नैतिक भलाई जैसी ऊँची, साझा धरोहरों को भी छोड़ दिया. अब तुम समतल ज़मीन की ओर बढ़ रहे हो जहाँ तुम्हारे पाँव धँसते चले जाएँगे.
हिलो मत. क्या तुम मंगल पर जा रहे हो?
नहीं, रुक जाओ. यह कीचड़ तुम्हें खींच लेगा, पूरा निगल लेगा. लेकिन हाँ, यह सच है. तुम्हारी विकास-यात्रा अद्भुत थी, सांस रोक देने जितनी ख़ूबसूरत.
बस अफ़सोस यह है कि इसे फिर से दोहराया नहीं जा सकता.
III.
चलो, अब मानव गरिमा की बातें भी बहुत हो गईं.
अब ज़रा विद्रोह पर बात करते हैं.
मैंने इस बारे में अपनी किताब The World Goes On (2017) में कुछ लिखने की कोशिश की थी, लेकिन उससे मैं खुद संतुष्ट नहीं था. इसलिए आज फिर से कोशिश करता हूँ.
उन्नीस सौ नब्बे के दशक की शुरुआत की बात है. एक उमस भरी, भारी-सी दोपहर थी. मैं बर्लिन में था, यू-बान मेट्रो (U-Bahn)[xii] के एक स्टेशन पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था. वहाँ, जैसे हर स्टेशन पर होता है, ट्रेन जिस तरफ़ जाती है उस दिशा में थोड़ा आगे एक बड़ा-सा दर्पण लगा था, जिसमें लाइटें लगी रहती थीं. उसके दो कार्य थे:
1. चालक पूरी ट्रेन को एक नज़र में देख सके.
2. और उसे ठीक-ठीक पता चल सके कि ट्रेन को किस सेंटीमीटर पर रोकना है.
प्लेटफ़ॉर्म पर एक मोटी, चमकीली पीली रेखा भी बनी थी. उसका मतलब था: इस रेखा को किसी भी हालत में पार मत करो. भले प्लेटफ़ॉर्म आगे तक फैला हो. इस रेखा और सुरंग के बीच का हिस्सा पूरी तरह “निषिद्ध क्षेत्र” था. वहाँ किसी यात्री का जाना पूरी तरह मना था.
मैं क्रॉय़त्सबर्ग (Kreuzberg)[xiii] दिशा से आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र पड़ी. कोई आदमी उस पीली रेखा के अंदर, बिल्कुल निषिद्ध जगह में खड़ा था.
वह एक क्लोशार (बेघर भिखारी) था. बेघर, टूटा हुआ, दर्द से झुका हुआ. उसका चेहरा जैसे हमारी ओर मदद की उम्मीद में मुड़ा हुआ था. वह ट्रैक के ऊपर बने पथ पर खड़ा होकर बहुत मुश्किल से पेशाब करने की कोशिश कर रहा था. हर बूंद उसके लिए यातना जैसी थी.
जब तक मैं समझ पाता, आसपास के लोग भी इसकी ओर देखने लगे. उस दोपहर की चुप्पी को तोड़ता हुआ एक बेचैन-सा दृश्य.
अचानक, हम सबके भीतर जैसे एक ही राय बन गई कि यह बहुत गलत है. इसे तुरंत रोका जाना चाहिए. क्लोशार को हटना ही होगा, और उस पीली रेखा की “सत्ता” फिर से लागू होनी चाहिए. अगर वह अपना काम जल्दी से पूरा कर लेता, भीड़ में वापस मिल जाता, और ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़कर गायब हो जाता तो शायद कोई बात नहीं होती. लेकिन वह रुक ही नहीं पा रहा था. इसी बीच सामने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर एक पुलिसकर्मी आ गया. उसने लगभग आँख से आँख मिलाते हुए उसे डाँटकर आदेश दिया कि वह तुरंत बंद करे.
यू-बान मेट्रो प्लेटफ़ॉर्मों के बीच लगभग दस मीटर चौड़ी और एक मीटर गहरी खाई होती है. यही सुरक्षा व्यवस्था है. इसका मतलब यह था कि पुलिसकर्मी सीधे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कूदकर आ ही नहीं सकता था. उसे पूरा चक्कर लगाना पड़ता. सीढ़ियाँ ऊपर, फिर कॉरिडोर, फिर हमारी तरफ़ वाली सीढ़ियाँ. यानी वही रास्ता जो किसी भी यात्री के लिए है. और उससे हटकर जाना समझ से बाहर था, मना भी, और खतरनाक भी.
पुलिसकर्मी ने कई बार उस बेघर भिखारी को आवाज़ दी. लेकिन कोई असर नहीं. उसने उसकी तरफ़ देखा भी नहीं. उसका चेहरा अब भी हमारी तरफ़ ही था. दर्द में जकड़ा हुआ.
और यह बात कि उसने पुलिसकर्मी को अनदेखा किया. किसी “कानून” के हिसाब से सबसे बड़ा अपमान थी. पुलिसकर्मी को इससे और गुस्सा आ गया.
क्लोशार (बेघर भिखारी) समझ गया था कि पुलिसकर्मी उससे कहीं तेज़ है, और देर-सबेर वह पहुँचेगा ही. और जैसे ही उसने देखा कि पुलिसकर्मी ऊपर चढ़ने के लिए दौड़ा. वह भी किसी तरह कराहते हुए भागने लगा, हमारी सीढ़ियों की तरफ़.
यह एक भयानक-सी दौड़ थी.
हम सब चुप हो गए.
साफ़ था कि यह दौड़ बेकार है.
क्लोशार (बेघर भिखारी) काँप रहा था. मानो उसके पैर उसका साथ छोड़ रहे हों. उधर पुलिसकर्मी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था.
ये दस मीटर दोनों के बीच एक अजीब-सी दूरी बन गए थे. कानून और दुष्टता के बीच, व्यवस्था और अराजकता के बीच.
मैं उन्हें देख रहा था. मिटरों और सेंटीमीटरों की इस अमानवीय दौड़ को.
और अचानक ऐसा लगा. मानो समय रुक गया हो.
वह क्षण जब दोनों ने एक-दूसरे को देखा:
पुलिसकर्मी देख रहा था कि “दोषी” क्लोशार नियम तोड़ रहा है.
और क्लोशार देख रहा था कि “कानून” उसके पीछे पड़ चुका है.
पुलिसकर्मी के हाथ में डंडा था. वह दौड़ने को तैयार था. पर एक पल रुका, जैसे सोच रहा हो कि क्या वह उस दस मीटर को छलाँग लगाकर पार कर ले? क्लोशार वहीं काँप रहा था. असहाय.
और आज भी, उस दृश्य की स्मृति मेरे भीतर उसी बिंदु पर अटकी हुई है. जहाँ भलाई और दुष्टता आमने-सामने खड़े थे.
मैंने देखा:
उधर— तेज़ी से आता पुलिसकर्मी.
इधर— एक टूटा हुआ, थका हुआ क्लोशार, जो एक-एक सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा था.
और मुझे समझ आ गया:
इन दस मीटरों की वजह से ‘भलाई’ कभी ‘बुराई’ को पकड़ नहीं पाएगी.
चाहे पुलिसकर्मी अंत में उसे पकड़ भी ले. मेरे भीतर तो वे दस मीटर हमेशा के लिए मौजूद हैं.
क्योंकि मैं सिर्फ़ यह देख पाता हूँ:
‘भलाई’ उस कांपती हुई, कमजोर ‘बुराई’ तक कभी पहुँच नहीं पाती, क्योंकि दोनों के बीच अब किसी तरह की उम्मीद बची ही नहीं है.
मेरी ट्रेन आ गई. मैं रूलेबेन (Ruhleben) (बर्लिन में स्थित एक इलाका) की ओर चला गया. लेकिन वह दृश्य मेरे दिमाग़ से नहीं निकला.
और अचानक. बिजली की तरह. एक सवाल उठा:
यह क्लोशार और इसके जैसे बाकी परित्यक्त लोग. कब विद्रोह करेंगे? और वह विद्रोह कैसा होगा?
खूनी?
निर्मम?
भयावह?
फिर मैंने खुद से कहा. नहीं, जिस विद्रोह की मैं सोच रहा हूँ. वह अलग होगा.
क्योंकि वह विद्रोह संपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध होगा.
देवियों और सज्जनों,
हर विद्रोह एक दूसरे से जुड़ा होता है. वह हमेशा किसी संपूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में ही अर्थ पाता है. और अब, जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ. और मेरे कदम फिर उसी टावर-रूम में धीमे पड़ रहे हैं. तब फिर वही यू-बान मेट्रो की यात्रा याद आ जाती है.
स्टेशन दर स्टेशन, रोशनियाँ गुजरती जाती हैं. और मैं कहीं नहीं उतरता.
तब से मैं उसी मेट्रो में हूँ. क्योंकि कोई ऐसा स्टेशन है ही नहीं जहाँ उतर सकूँ.
मैं बस दृश्य को गुजरते हुए देखता हूँ. और महसूस करता हूँ कि विद्रोह, मानव गरिमा, देवदूतों. और शायद हाँ, आशा. सब पर जो कहना था, मैं कह चुका हूँ.
साभार : www.nobelprize.org