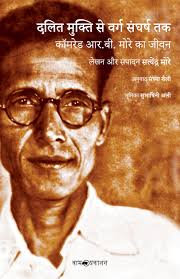वाम वैचारिकी में जातिगत चेतना और वर्गीय चेतना का अंतर्द्वंद्
प्रणव प्रियदर्शी
भारत में कम्यूनिस्ट आंदोलन की बात की जाए तो जाति का प्रश्न एक ऐसी पहेली के रूप में सामने आता है, जिससे न तो बचते बनता है और न ही उलझते. वर्गीय चेतना और जातीय चेतना को किस हद तक एक-दूसरे का विरोधी माना जाए और किस हद तक एक-दूसरे का पूरक, इसका कोई तर्कपूर्ण उत्तर आज तक नहीं ढूंढा जा सका है. हालांकि इसका सही उत्तर तलाशने की जरूरत हमेशा महसूस की जाती रही है. ऐसी कोशिशें भी होती रही हैं. लेकिन ऐसी तमाम कोशिशों की परिणति या तो जाति और दलित के सवाल को नजरअंदाज करने के आरोपों में हुई है या वर्गीय दृष्टिकोण को धूमिल करने, वर्गीय चेतना को कुंद करने की शिकायत में. इन दोनों ही स्थितियों का दोष मढ़ने के लिए दो सॉफ्ट टारगेट भी हमेशा उपलब्ध रहे हैं. एक तो दलित राजनीति का कथित अवसरवादी स्वरूप और दूसरा वामपंथी दलों का सवर्ण नेतृत्व.
ऐसे में हाल ही प्रकाशित पुस्तक ‘दलित मुक्ति से वर्ग संघर्ष तक’ की उपयोगिता और प्रासंगिकता को निस्संदेह स्वतःसिद्ध करार दिया जा सकता है. हालांकि यह बात खास तौर पर हिंदीभाषी पाठकों के संदर्भ में कही जा रही है. वजह यह है कि मूल पुस्तक मराठी में है जो करीब दो दशक पहले छप चुकी है. इसका अंग्रेजी अनुवाद भी लेफ्टवर्ड बुक्स कुछ साल पहले प्रकाशित कर चुका है. हिंदीभाषी पाठक जरूर अब तक इस पुस्तक से वंचित थे. इसी जरूरत को पूरा करने का काम वाम प्रकाशन ने पिछले दिनों संध्या शैली द्वारा किया गया इसका हिंदी अनुवाद सामने लाकर किया.
पुस्तक की खास बात यह है कि यह एक साथ आत्मकथा और जीवनी दोनों है. रामचंद्र बाबाजी मोरे (1903 से 1972) दलित समाज को जगाने, संगठित करने और उसे आवाज देने वाले शुरुआती व्यक्तित्वों में रहे हैं. वे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के करीबी सहयोगी ही नहीं, उनके नेतृत्व में हुए दो प्रमुख आंदोलनों- पहला, दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने वाला और दूसरा मनुस्मृति के दहन का – के मुख्य आयोजक रहे. 1927 में चवदार तालाब आंदोलन के लिए बाबा साहेब को महाड़ लाने का श्रेय भी रामचंद्र मोरे को ही दिया जाता है. दिलचस्प है कि दलित आंदोलन में बढ़-चढ़कर शिरकत ही नहीं, उसका नेतृत्व करने वाले आरबी मोरे 1930 में कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए. उन्होंने बाकायदा बाबा साहेब से मिलकर उन्हें यह जानकारी दी कि कम्यूनिस्ट सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दलितों समेत सभी पीड़ितों, शोषितों और वंचितों की मुक्ति का मार्ग उन्हीं सिद्धांतों से होकर गुजरता है. बाबा साहेब ने न केवल उन्हें इसकी इजाजत दी, बल्कि उसके बाद भी उनसे निकट सहयोग और संपर्क बनाए रखा.
रामचंद्र बाबाजी मोरे की शख्सियत की खूबी यह है कि इसमें हम दलित और कम्यूनिस्ट दोनों धाराओं का अद्भुत और दुर्लभ मेल देख सकते हैं. यही बात इस पुस्तक को भी खास बनाती है. कम्यूनिस्ट सिद्धांतों की आंच में तपे आर बी मोरे ने त्याग, बलिदान और संघर्षों से भरा जीवन तो जिया ही, व्यक्तिवाद से जुड़ी बुराइयों को लेकर भी आजीवन सतर्क रहे. इसलिए आत्मकथा लिखने जैसे अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया. इसके उलट यही कोशिश करते रहे कि खुद को परदे के पीछे रखते हुए ही समाज, पार्टी और विचारधारा के हित में काम करते रहें. जीवन के आखिरी वर्षों में ही, उनके करीबी सहयोगी उन्हें यह बात समझा सके कि दलित समाज को जगाने, उसमें स्वाभिमान की भावना भरने वाले शुरुआती प्रयासों और कम्यूनिस्ट कार्यकर्ताओं के त्यागपूर्ण, संघर्षमय जीवन का एक प्रामाणिक दस्तावेज उनकी आत्मकथा के जरिए सामने आ सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत काम का होगा. इसके बाद उन्होंने आत्मकथा लिखनी शुरू की, लेकिन 1927 यानी 24 साल की उम्र तक ही पहुंचे थे कि 1972 में उनकी मृत्यु हो गई. ऐसे में आत्मकथा अधूरी रह गई. बाद में आरबी मोरे के पुत्र सत्येंद्र मोरे ने पुस्तक के अगले हिस्से को जीवनी के रूप में पूरा किया. बताना जरूरी है कि सत्येंद्र मोरे भी आजीवन मार्क्सवादी विचारों के प्रति समर्पित रहे. वह 1978 में मुंबई के धारावी क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे.
आरबी मोरे उन गिने-चुने व्यक्तियों में रहे जो दलित राजनीति से शुरुआत करके कम्यूनिस्ट सिद्धांतों की ओर आए और आजीवन इन सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे. खास बात यह कि दलित समाज से, उसके सुख-दुख और संघर्षों से भी उनका नाता कभी कमजोर नहीं हुआ. वे इस बात को भी महसूस करते और कहते रहे कि कम्यूनिस्ट आंदोलन को जिस शिद्दत से दलितों के सवाल उठाने चाहिए, वह नहीं उठा रहा है. इस लिहाज से यह किताब खासी महत्वपूर्ण हो जाती है. आर बी मोरे के जीवन और संघर्षों में हम उस सोच की झलक देख सकते हैं जो कम्यूनिस्ट आंदोलन के जरिए दलितों की मुक्ति के सपने देखता था. इस सोच ने दोनों धाराओं को जोड़ने के लिए किस तरह के प्रयास किए और इन प्रयासों का कैसा असर शुरुआती दिनों में दिखा, यह भी हमें इस किताब से पता चलता है.
छुआछूत के खिलाफ संघर्ष के शुरुआती दौर में समाज के अग्रणी नेताओं के रुख का ब्योरा इस पुस्तक में बड़ी बारीकी से पेश किया गया है. मसलन जब 23-24 मार्च 1918 को मुंबई में पहला छुआछूत निवारण सम्मेलन बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, तो रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी से लेकर करवीर पीठ के शंकराचार्य तक ने उसे शुभकामना संदेश भेजे. विपिनचंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, विट्ठलभाई पटेल आदि इस सम्मेलन के प्रमुख वक्ता थे. लेकिन, इन सबका नजरिया सहानुभूति का था, अछूतों के स्वाभिमान और उनके मानवीय हक के आधार पर छुआछूत खत्म करने का नहीं. इसका पता इस बात से भी चलता है कि सम्मेलन में लोकमान्य तिलक ने जबरदस्त भाषण देते हुए कहा, ‘मैं अछूतों के विरोध में नहीं हूँ और छुआछूत को नष्ट होना चाहिए’, लेकिन जब ‘हम छुआछूत को नहीं मानेंगे और जातिपांति के बंधन को तोड़ेंगे’, इस आशय के शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो तिलक पीछे हट गए. सम्मेलन के 380 प्रतिनिधियों ने जिस शपथपत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उस पर लोकमान्य तिलक ने हस्ताक्षर नहीं किए. तिलक के ‘केसरी’ में इस सम्मेलन की कोई रिपोर्ट भी नहीं छपी. तत्कालीन नेताओं के इस सहानुभूतिपूर्ण नजरिए को देखते हुए ही बाबा साहेब आंबेडकर ने इस सम्मेलन से दूरी बनाए रखी. वे इसमें शामिल नहीं हुए थे.
इस सम्मेलन के बरक्स 1929 में आरबी मोरे और शामराव परुलेकर की पहल पर बाबा साहेब की अध्यक्षता में चिपलून में हुए रत्नागिरी जिला बहिष्कृत परिषद के दूसरे सम्मेलन को देखें तो फर्क स्पष्ट नजर आता है. इस सम्मेलन में महारों के साथ कुणबी, मराठा किसान और खेत-मजदूर उपस्थित थे. इस ऐतिहासिक सम्मेलन ने खोती (कोंकण क्षेत्र में प्रचलित राजस्व वसूली की व्यवस्था जो जमींदारी प्रथा का ही एक रूप थी) और बंधुआ मजदूरी को खत्म करने और जोतने वाले को जमीन देने की मांग की. इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में शामिल अछूत और गैरअछूत किसानों ने एक साथ बैठकर खाना खाया. ऐसे समय जब मुंबई जैसे बड़े औद्योगिक शहर में, जहाँ वर्गीय जागरूकता का स्तर बढ़ा हुआ था, हिंदू कामगार छुआछूत माना करते थे, कोंकण के एक पिछड़े हुए गांव में इस तरह अछूतों और गैर अछूतों का साथ बैठकर खाना निश्चित रूप से ऐतिहासिक घटना थी. इसका महत्व इस मायने में था कि इसमें छुआछूत निर्मूलन के लिए आवश्यक वर्गीय एकता का आधार छिपा था.
मोरे के इस ठोस नजरिए की झलक आगे के उनके कार्यों में भी दिखती है. 1932 में जब वे बाकायदा कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल हो चुके थे, तब मजदूर नेताओं पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) के प्रभाव को खत्म करने के लिए बीटी रणदिवे और एसवी देशपांडे के नेतृत्व में रेड ट्रेड युनियन कांग्रेस की स्थापना की गई. इसके बैनर तले कपड़ा मिल मजदूरों की यूनियन का गठन हुआ जिसकी कार्यकारिणी में मोरे को शामिल किया गया. तब उस कपड़ा मिल यूनियन के दफ्तर में परंपरानुसार पानी के दो मटके रखे जाते थे. एक मटका सवर्ण कामगारों के लिए और दूसरा दलित कामगारों के लिए. आलम यह था कि दलितों वाले मटके से कम्यूनिस्ट नेता पानी पी लेते थे, लेकिन सवर्ण मजदूर नहीं पीते थे. यहाँ तक कि यूनियन के अध्यक्ष भिसे को भी दलितों वाले मटके से पानी पीना पड़ता था क्योंकि वे दलित थे. मोरे को यह बात नहीं पची. उन्होंने पार्टी की बैठक में यह मुद्दा उठाया. पहले पार्टी नेताओं के सामने इस बात की उलझन थी कि पता नहीं आम मजदूर इसे किस रूप में लेगा. लेकिन आरबी मोरे के मन में कोई असमंजस नहीं था. उन्होंने कहा, “इस ऑफिस में एक ही मटका रखिए. जो छुआछूत मानेंगे वे बाहर होटल में जाकर पानी पिएंगे. इससे लोगों के बीच यह साफ संदेश जाएगा कि जातिगत भेदभाव को लेकर हम कम्यूनिस्ट कितने कठोर हैं. हम निडर होकर यह करते नहीं हैं, इसलिए दलितों का स्वतंत्र आंदोलन खड़ा होता है.”
मोरे के इस स्पष्ट रुख ने बाकी नेताओं को भी सहमत किया और उस दफ्तर में दलितों के लिए अलग मटका रखने की परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो गई. यही नहीं, उन दिनों मुंबई में बीडीडी चॉल, सीमेंट चॉल, बीआईटी चॉल आदि में अछूतों के लिए अलग नल हुआ करते थे. कॉमरेड मोरे ने अछूतों के अलग नल बंद करवाने और सभी मजदूरों को एक ही सार्वजनिक नल से पानी लेने का अधिकार दिलवाने के लिए भी कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से आंदोलन खड़ा करने की पहल की थी. देखा जाए तो यह बाबा साहेब आंबेडकर के आंदोलन के सिपाही मोरे की ओर से कम्यूनिस्ट आंदोलन को एक तोहफा था.
इस तोहफे को अगर कम्यूनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व पूरे मन से और सही अर्थों में अपनाता तो देश में शायद इसका अलग इतिहास लिखा जा सकता था. लेकिन वर्ग और जाति से जुड़े मसलों पर इस तरह का ठोस और संतुलित नजरिया कम्यूनिस्ट नेतृत्व आगे नहीं दिखा सका. यह बात आने वाले वर्षों में जाति के सवाल पर खुद मोरे द्वारा पार्टी के अंदर चलाए गए संघर्ष से भी स्पष्ट होती है. लेकिन उस बारे में बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वर्ग और जाति के इस अंतर्विरोध का शिकार सिर्फ कम्यूनिस्ट पार्टी नहीं, दलित नेतृत्व भी रहा है. खुद बाबा साहेब आंबेडकर ने भी भले ही आर बी मोरे को कम्यूनिस्ट राह पर चलने की इजाजत दे दी हो और उसके बाद भी उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान में कमी न आने दी हो, लेकिन दलित नेतृत्व और कम्यूनिस्ट धारा को साथ लाने की मोरे की कोशिशों को झटका आंबेडकर के रुख से भी लगा.
इसका अच्छा उदाहरण 1952 में हुआ देश का पहला आम चुनाव था. इन चुनावों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर एक-एक उम्मीदवार इन समुदायों का चुनकर भेजना था. लेकिन इन्हीं सीटों पर सामान्य जाति के एक-एक प्रत्याशी को चुना जाना था. हाँ, अनारक्षित सीटों पर एक ही प्रत्याशी निर्वाचित होना था. इन चुनावों में मुंबई से लोकसभा की आरक्षित सीट पर बाबा साहेब आंबेडकर को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अपना उम्मीदवार बनाया था. उनके खिलाफ कांग्रेस की ओर से नारायणराव काजरोलकर खड़े थे. सामान्य सीट पर कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से एस ए डांगे, समाजवादियों की ओर से अशोक मेहता औऱ कांग्रेस की ओर से विट्ठल बालकृष्ण गांधी प्रत्याशी बनाए गए थे.
कम्यूनिस्ट पार्टी ने सामान्य क्षेत्र से अपने प्रत्याशी डांगे और आरक्षित क्षेत्र से आंबेडकर को समर्थन देने का निर्णय किया. कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से कॉ. मोरे ने यह बात बाबा साहेब को बताई. उन्होंने मोरे की बात सुनने के बाद कहा, ‘पहले मैं पार्टी का घोषणापत्र जारी करूंगा, फिर देखते हैं.’ 6 अक्टूबर 1951 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का घोषणापत्र जारी हुआ. लेकिन इसके बाद बाबा साहेब ने समाजवादियों के साथ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी. अपनी नीति बताते हुए उन्होंने कहा, ‘हम लोगों ने तय किया है कि कम्यूनिस्टों और जातिवादी संगठनों से कोई सहयोग नहीं करेंगे. कांग्रेस यदि समर्थन मांगती तो उसकी गलतियां दिखाकर उन्हें सुधारने की मांग मैंने की होती.‘
बाबा साहेब के इस रुख की कम्यूनिस्टों के बीच तीखी प्रतिक्रिया हुई. बहुमत से यह फैसला किया गया कि सामान्य क्षेत्र से डांगे को वोट दिया जाए, लेकिन सुरक्षित स्थान से किसी को भी वोट नहीं देना है. हालांकि मोरे समेत कई लोग इस मत के थे कि बाबा साहेब दलितों के स्वतंत्र आंदोलन की पहचान हैं. इसलिए उनका रुख जो भी हो, पार्टी को उनका समर्थन करना चाहिए. लेकिन इन लोगों की राय का ज्यादा पभाव नहीं पड़ा और पार्टी के बहुमत का फैसला ही अमल में आया. नतीजा यह रहा कि बाबा साहेब 14,561 वोटों से चुनाव हार गए. हालांकि चुनाव परिणाम के बाद हुए मंथन में पार्टी ने अपनी गलती मानी और इस आशय का एक प्रस्ताव भी पास किया.
सार्वजनिक तौर पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से कम्यूनिस्टों से जवाब मांगने के लिए मुंबई के वरली में एक विशाल आमसभा की गई. इसमें कॉमरेड मोरे ने पार्टी का पक्ष रखते हुए बाबा साहेब की हार पर दुख व्यक्त किया और कहा कि दोनों ही पार्टियों को एक-दूसरे को समझकर काम करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कम्यूनिस्टों के साथ एकजुटता किए बगैर दलितों की अंतिम मुक्ति असंभव है.
पुस्तक के मुताबिक आमसभा में मोरे का भाषण सुनने के लिए बाबा साहेब भी आए थे, लेकिन ‘उन्होंने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी.’ बाद में मोरे से मिलकर उन्होंने उनके भाषण के लिए बधाई दी थी. (पृष्ठ 170)
बाबा साहेब और आर बी मोरे जैसे बड़े और समर्पित नेताओं के स्तर पर भले दलित और कम्यूनिस्ट का यह द्वंद्व वैचारिक बहसों तक सीमित रहा हो, लेकिन आम कार्यकर्ताओं के बीच इसका रूप कहीं ज्यादा आक्रामक और तीखा था. आलम यह था कि खुद को बाबा साहेब का कट्टर अनुयायी कहने वाले कई कम्यूनिस्ट विरोधियों ने दलित कम्यूनिस्टों पर हमले करने शुरू कर दिए थे. मुंबई में ये हमले डिलाइल रोड, माटुंगा लेबर कैंप और नायगांव के बीडीडी चॉल में हुए. इसकी आंच नाशिक में भी पहुंची. शुरू में ये हमले महार समाज के भीतर के कम्यूनिस्टों पर हुए, बाद में मातंग, मेहतर आदि समाज के कम्यूनिस्टों को भी निशाना बनाया गया. हिंसा की इन घटनाओं में कई लोगों के सिर भी फूटे, खून बहा. कई जगहों पर महार समाज के कम्यूनिस्टों को बहिष्कृत किया गया. पीड़ित लोग मोरे से मिले. मामले की गंभीरता को देखते हुए मोरे ने खुद बाबा साहेब से मिलकर शिकायत की. बाबा साहेब ने न केवल इन घटनाओं पर दुख व्यक्त किया बल्कि अपनी पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाकर उन्हें फटकारा. उसके बाद ये घटनाएं रुकीं और बहिष्कार भी काफी हद तक कमजोर पड़ गया.
मोरे और बाबा साहेब की मौजूदगी की बदौलत यह विरोध उस समय मंद भले पड़ गया, लेकिन दलितों के बीच कम्यूनिस्टों की वर्ग दृष्टि का और कम्यूनिस्टों के बीच दलितों की जातिगत चेतना का विरोध बरकरार रहा जो सैद्धांतिक बहसों में ही नहीं व्यावहारिक फैसलों में भी लगातार दिखता रहा है. कम्यूनिस्ट पार्टी के अंदर खुद मोरे भी इस बारे में सार्वजनिक तौर पर भले कुछ न कह रहे हों, लेकिन पार्टी के रुख से उनका विरोध लगातार बना रहा. पार्टी के अंदर वे अपना यह विरोध उपयुक्त मौकों पर व्यक्त भी करते रहे.
मिसाल के तौर पर 1948 की दूसरी कलकत्ता कांग्रेस में पार्टी ने छुआछूत पर जो प्रस्ताव पारित किया, उसमें कहा गया था कि ‘अछूत जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि समाज के दूसरे शोषितों-पीड़ितों के साथ एकजुटता में ही उसका कल्याण निहित है और जनवादी क्रांति की सफलता के साथ उसकी सामाजिक दुरवस्था और गुलामी खत्म हो जाएगी.‘ इतना ही नहीं, बाबा साहेब का नाम लिए बगैर इस प्रस्ताव में कहा गया था कि ‘खुद अछूतों के भीतर के अवसरवादी और भेदभाव पैदा करने वाले नेताओं के असली चेहरे को जनता के सामने लाना होगा, अछूत समाज पर उनका असर खत्म करना होगा…’.
कॉ. मोरे ने 1953 में पार्टी को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताते हुए कहा था कि पार्टी ने जाति के सवाल को नजरअंदाज किया और डॉ. आंबेडकर को लेकर भी पार्टी की उपरोक्त विश्लेषण सही नहीं है. मोरे के मुताबिक पार्टी जाति के सवाल को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने के बजाय यांत्रिक तरीके से देख रही थी और यह मानकर चल रही थी कि केवल आर्थिक सुधार होने पर यह समस्या खत्म हो जाएगी.
मोरे ने यह लंबा पत्र 21 दिसंबर 1953 को पार्टी के तत्कालीन नेता ई एम एस नंबूदिरीपाद को भेजा था और उनसे मांग की थी कि 27 दिसंबर 1954 से 2 जनवरी 1955 तक मदुरै में होने वाली तीसरी पार्टी कांग्रेस में निर्वाचित नई केंद्रीय कमिटी पार्टी को छुआछूत की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेष समिति के गठन का आदेश दे. पोलित ब्यूरो ने कॉमरेड मोरे का यह पत्र सभी प्रदेश इकाइयों को भेजा ताकि वे इस पर चर्चा करके अपना मत भेजें.
पार्टी ने उनके मत का संज्ञान लिया था, लेकिन उसके प्रतिसाद को पर्याप्त न मानकर मोरे ने 16 दिसंबर 1957 को वही पत्र थोड़े-बहुत फेरबदल के साथ तत्कालीन पार्टी महासचिव कॉ, अजय घोष को, उनके मुंबई आने पर खुद सौंपा. निस्संदेह पार्टी ने उनके इस मत को न केवल देखा-परखा बल्कि उसे यथासंभव महत्व देने की भी कोशिश की, लेकिन पार्टी के नजरिए में उससे कोई बुनियादी फर्क आया हो, यह नहीं दिखा.
बहरहाल, यह न तो सिर्फ मोरे की बात है और न ही कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की. पूरे कम्यूनिस्ट आंदोलन में इस मसले पर असहमति, भ्रम, अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति दिखती है. यह नब्बे के दशक के दौरान और उसके बाद भी अलग-अलग मौकों पर अलग-अळग धड़ों, ग्रुपों, समूहों और पार्टियों में भी बहसों-फूटों के रूप में सामने आती रही है.
आज भी यह सैद्धांतिक गुत्थी अनसुलझी है कि कम्यूनिस्ट दृष्टिकोण में जाति के प्रश्न को कितना महत्व दिया जाना चाहिए. हालांकि सिर्फ वर्गीय दृष्टि पर ध्यान केंद्रित रखकर चलने वाली शास्त्रीय धारा रही हो या जाति के सवाल पर जोर देकर आगे बढ़ने वाली व्यावहारिक धाराएं – कामयाबी किसी के हाथ नहीं लगी है. इसलिए कम से कम कम्यूनिस्ट आंदोलन की नाकामी का ठीकरा इस एक सवाल पर नहीं फोड़ा जा सकता.
फिर भी इस विचारधारा के लिए यह चुनौती तो है ही कि जातिगत चेतना और वर्गीय चेतना के टकराव को कैसे दूर किया जाए. वक्त ही बताएगा कि 21वीं सदी में अपने अस्तित्व की सार्थकता साबित करने की चुनौती से जूझती यह विचारधारा इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब ढूंढ भी पाती है या नहीं.

लेखक – प्रणव प्रियदर्शी